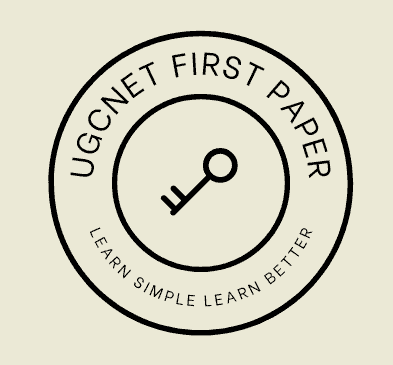(Source : IGNOU)
तर्कसंग्रह (अन्नम्भट्ट)
आचार्य अन्नम्भट्टकृत् तर्कसंग्रह’ यद्यपि वैशेषिक दर्शन का प्रकरण ग्रन्थ है तथापि इसमें न्यायदर्शनसम्मत चतुर्विध प्रमाणव्यवस्था का विवेचन किया गया है। इन्द्रिय तथा अर्थ (विषय) के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है। अनुमान प्रमाण लिगपरामर्श से जन्य होता है। सज्ञासझिसम्बन्ध का ज्ञान कराने वाला प्रमाण उपमान कहलाता है। आप्तवाक्य से जन्य प्रमाण को शब्द प्रमाण कहते हैं।
प्रत्यक्ष प्रमाण
‘सर्वव्यवहारोहेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानम्। सा द्विविधा स्मृतिरनुभवश्च ।
व्याख्या: न्याय-वैशेषिक दर्शन में बुद्धि को गुण माना गया है। तर्कसग्रहकार आचार्य अन्नम्भट्ट बुद्धि का लक्षण करते हैं ‘सर्वव्यवहारहेतुर्बुद्धिः ज्ञानम्’ अर्थात् समस्त व्यवहार के असाधारण कारणरूप गुण को ज्ञान अर्थात् बुद्धि कहते हैं। अभिप्राय यह है कि ज्ञानरूप बुद्धि से सभी प्राणियों का प्रवृत्ति, निवृत्ति, आहार-विहार आदि सभी प्रकार का व्यवहार होता है। बुद्धि के अभाव में प्राणी किसी भी प्रकार का व्यवहार करने में समर्थ नहीं हो सकता है क्योंकि कोई भी व्यवहार तभी सफल एवं सम्भव होता है जब की व्यवहार करने वाले को व्यवहार किए जाने वाले विषय (वस्तु / पदार्थ) का बोध हो। जब तक वस्तु का ज्ञान प्राणी को नहीं होता है तब तक उसके सम्बन्ध में कोई भी व्यवहार नहीं हो सकता है। न्याय-वैशेषिक गतानुसार गनुष्य का व्यवहार – ‘हान, उपादान एवं उपेक्षा’ रूप से तीन प्रकार का हुआ करता है। हान का अर्थ है कि किसी वस्तु का परित्याग, उपादान का अर्थ है किसी वस्तु का ग्रहण तथा उपेक्षा का अर्थ है ग्रहण-त्याग से भिन्न उदासीनता का भाव होना। यह त्रिविध व्यवहार तभी सम्भव होता है जब प्राणी वस्तु के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वस्तु के स्वरूप का ज्ञान बुद्धि से ही सम्पन्न किया जाता है इसीलिए बुद्धि को समस्त व्यवहारों का असाधारण कारण कहा जाता है। प्रस्तुत लक्षण में यदि ‘व्यवहारहेतु’ इतना ही लक्षण करते तो दण्ड आदि में भी बुद्धि का लक्षण चला जाता क्योंकि यह दण्ड है इस व्यवहार के प्रति दण्ड भी हेतु है। इसलिए सर्व पद को लक्षण में रखा गया है, जिससे आ रहे दोष का निवारण किया जा सके। बुद्धि के इस लक्षण में निर्विकल्पक ज्ञान का समावेश नहीं होता है क्योंकि निर्विकल्पक ज्ञान से किसी भी प्रकार का साक्षात् व्यवहार नहीं होता है। इसीलिए ‘तर्कसंग्रहदीपिका’ में इस लक्षण का परिष्कार करते हुए कहा गया है ‘जानामीत्यनुव्यवसायगम्यज्ञानत्वम् । अर्थात् बुद्धि वह ज्ञान है जो अनुव्यवसाय (मैं जानता हूँ इस प्रकार के ज्ञान का) ज्ञान का विषय बनता है। न्याय-वैशेषिक दर्शन की ज्ञानप्रक्रिया के अनुसार जब कोई ज्ञानकर्त्ता किसी भी पदार्थ (यथा-घट) का किसी भी प्रमाण की सहायता से ज्ञान करता है तो उसे ‘अय घटः’ इस प्रकार का ज्ञान होता है; यह निश्चयात्मक ज्ञान ‘व्यवसाय’ कहलाता है। इस व्यवसायात्मक ज्ञान के पश्चात् आत्मा में ‘अहं घटं जानामि’ इत्याकारक ज्ञान होता है, जिसे अनुव्यवसाय’ कहा जाता है। बुद्धि (ज्ञान) इसी अनुव्यवसायात्मक ज्ञान का विषय बनता है।
बुद्धि के भेदो का निरूपण करते (1) स्मृति तथा, (2) अनुभव । हुए आचार्य कहते हैं कि बुद्धि दो प्रकार की होती है-
विशेष : न्याय-वैशेषिक दर्शन में बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, बोध, प्रतीति, प्रत्यय इन सभी को पर्याय माना जाता है जैसा कि न्यायसूत्रकार का वचन है
स्मृति प्रमाण
बुद्धिरूपलब्धिर्ज्ञानमित्यर्थान्तरम्’ । बुद्धि इस दर्शन में स्वीकृत चतुर्विंशति गुणों में एक विशेष गुण है जो आत्मा’ में समवाय सम्बन्ध से रहता है। स्मृति की परिभाषा इस प्रकार दी गई है सस्कारमात्रजन्य ज्ञान स्मृतिः ।
व्याख्या: तर्कसंग्रहकार आचार्य अन्नम्भट्ट बुद्धि का लक्षण करते हैं सर्वव्यवहारहेतुर्बुद्धि ज्ञानम्’ अर्थात् समस्त व्यवहार के असाधारण कारणरूप गुण को ज्ञान अर्थात् बुद्धि कहते हैं। बुद्धि दो प्रकार की होती है (1) स्मृति तथा (2) अनुभव।
इनमें से प्रथम भेद ‘स्मृति’ का निरूपण करते हुए आचार्य कहते हैं संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः’ अर्थात् संस्कार मात्र से जन्य उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। यदि संस्कारमात्रजन्यं स्मृतिः ऐसा लक्षण करें तो संस्कारध्वंस में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि सस्कार का ध्वस भी सस्कार से जन्य होता है। इसलिए लक्षण में ज्ञानपद का समावेश किया गया है, क्योंकि संस्कारध्वंस ज्ञान नहीं है। यदि ‘जन्य ज्ञान स्मृतिः इतना ही लक्षण किया जाय तो घटादि के प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि सभी प्रकार के ज्ञान में स्मृति का लक्षण चला जायेगा, जो अतिव्याप्ति होगी। इस अतिव्याप्ति के निवारणार्थ लक्षण में ‘संस्कारमात्र’ पद योजित किया गया है। स्मृति के इस लक्षण में ‘मात्र’ पद के रखने से ‘प्रत्यभिज्ञा’ में इसकी अतिव्याप्ति नहीं होती है। प्रत्यभिज्ञा एक ऐसा ज्ञान है जो संरकार एवं अनुभव दोनों से मिलकर उत्पन्न होता है इसलिए लक्षण में मात्र पद का निवेश कर देने से स्मृति की प्रत्यभिज्ञा में होने वाली अतिव्याप्ति रूक जाती है।
जब कोई प्रमाता किसी प्रमाण की स्मृति के उत्पन्न होने की प्रक्रिया इस प्रकार है सहायता से किसी वस्तु का अनुभव प्राप्त करता है तो उस अनुभव का एक संस्कार (भावना) उसकी आत्मा में सूक्ष्म रूप से स्थित हो जाता है। कालान्तर में सादृश्य, चिन्ता, अदृष्ट आदि कारणों के उपस्थित होने पर यह सस्कार उद्बुध हो जाता है जिसे स्मृति कहा जाता है।
उसे विशेष : स्मृति जिस संस्कार से उत्पन्न होती है, न्याय वैशेषिक दर्शन में ‘भावना’ कहा जाता है। भावना, अनुभव से उत्पन्न होती है तथा स्मृति को उत्पन्न करती है। अनुभव एव स्मृति के मध्य में रहने के कारण भावना को स्मृति की प्रक्रिया में ‘व्यापार’ माना जाता है। व्यापार का लक्षण है तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनक’ अर्थात् जो हेतु से उत्पन्न होकर कार्य का जनक हो, वह व्यापार कहलाता है।
तद्मिन्न ज्ञानमनुभव । स द्विविधः यथार्थोऽयथार्थश्च। तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभव यथार्थ । यथा रजते ‘इदं रजतम्’ इति ज्ञानम्। सैव प्रमेत्युच्यते । तदभाववति तत्प्रकारकोऽनुभवोऽयथार्थः । यथा शुक्तौ इद रजतम्’ इति ज्ञानम्। सैवाऽप्रमेत्युच्यते ।
व्याख्या: तर्कसग्रहकार आचार्य अन्नम्भट्ट बुद्धि का लक्षण वर्णित करते हैं सर्वव्यवहारहेतुर्बुद्धिः ज्ञानम्’ अर्थात् समस्त व्यवहार के असाधारण कारणरूप गुण को ज्ञान अर्थात् बुद्धि कहते हैं। बुद्धि दो प्रकार की होती है (1) स्मृति तथा (2) अनुभव ।
अनुभव की शाब्दिक व्युत्पत्ति है ‘अनु (पश्चात्) भवति इति अनुभवः। प्रमाणव्यापार के पश्चात् जो ज्ञान होता है उसे अनुभव कहते हैं। ‘अनुभव’ का निरूपण करते हुए आचार्य कहते हैं ‘तद्मिन्नं ज्ञानमनुभव’ अर्थात् तद् (स्मृति) से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। स्मृति से अतिरिक्त सभी प्रकार के ज्ञान अनुभव कहलाते हैं। अनुभव के इस लक्षण में यदि ‘ज्ञानमनुभवः’ इतना ही लक्षण करें तो स्मृति में भी अनुभव का लक्षण चला जायेगा और स्मृति में अतिव्याप्ति होने लगेगी। इस अतिव्याप्ति दोष से बचने के लिए लक्षण में ‘तभिन्नम्’ पद को जोड़ा गया है।
- 11 – भाद्रपद मासकी ‘अजा’ और ‘पद्मा’ एकादशीका माहात्य
- 14 – पुरुषोत्तम मासकी ‘कमला’ और ‘कामदा’
- 13 – कार्तिक मासकी ‘रमा’ और ‘प्रबोधिनी’एकादशीका माहात्म्य
- 12 – आश्विन मासकी ‘इन्दिरा’ और ‘पापाङ्कुशा’ एकादशीका माहात्य
- 10 – श्रावण मासकी ‘कामिका’ और ‘पुत्रदा’ एकादशीका माहात्म्य
- About Culture-संस्कृति के विषय में
- About Institution-संस्था के विषय में
- ACT.-अधिनियम
- Awareness About Geography-भूगोल के विषय में जागरूकता
- Awareness About Indian History-भारतीय इतिहास के विषय में जागरुकता
- Awareness About Maths-गणित के बारे में जागरूकता
- Awareness about Medicines
- Awareness About Politics-राजनीति के बारे में जागरूकता
- Awareness-जागरूकता
- Basic Information
- Bharat Ratna-भारत रत्न
- Biography
- Chanakya Quotes
- CLASS 9 NCERT
- CMs OF MP-मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
- CSIR UGC NET
- e-Test-ई-टेस्ट
- Education
- Education-शिक्षा
- Ekadashi Mahatmya
- FULL TEST SERIES
- GK
- Granthawali-ग्रन्थावली
- Hindi Biography – जीवन परिचय
- Hindi Literature
- Hindi Literature-हिंदी साहित्य
- HINDI NATAK-हिंदी नाटक
- Hindi Upanyas-हिंदी उपान्यास
- ICT-Information And Communication TEchnology
- Jokes-चुटकुले
- Kabir ji Ki Ramaini-कबीर जी की रमैणी
- KAHANIYAN
- Katha-Satsang-कथा-सत्संग
- Kavyashastra-काव्यशास्त्र
- Meaning In Hindi-मीनिंग इन हिंदी
- Meaning-अर्थ
- MOCK TEST
- Motivational Quotes in Hindi-प्रेरक उद्धरण हिंदी में
- MPESB(VYAPAM)-Solved Papers
- MPPSC
- MPPSC AP HINDI
- MPPSC GENERAL STUDIES
- MPPSC GS PAPER
- MPPSC-AP-HINDI-EXAM-2022
- MPPSC-Exams
- MPPSC-मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
- Nibandha
- Padma Awardees-पद्म पुरस्कार विजेता
- PDFHUB
- PILLAR CONTENT
- QUOTES
- RSSU CHHINDWARA-राजा शंकर शाह वि.वि. छिंदवाड़ा
- RSSU QUESTION PAPERS
- SANSKRIT
- SANSKRIT VYAKARAN
- SANSKRIT-HINDI
- Sarkari Job Advertisement-सरकारी नौकरी विज्ञापन
- Sarkari Yojna-सरकारी योजना
- Sarkari-सरकारी
- Sarthak News-सार्थक न्यूज़
- SCHOOL
- SOLVED FIRST PAPER CSIR NET
- Theoretical Awareness-सैद्धांतिक जागरूकता
- UGC
- UGC NET
- UGC NET COMPUTER SCIENCE
- UGC NET HINDI MOCK TEST
- UGC NET NEWS
- UGC_NET_HINDI
- UGCNET HINDI
- UGCNET HINDI PRE. YEAR QUE. PAPERS
- UGCNET HINDI Solved Previous Year Questions
- UGCNET-FIRST-PAPER
- UGCNET-FIRSTPAPER-PRE.YEAR.Q&A
- UPSC-संघ लोक सेवा आयोग
- Various Exams
- VEDIC MATHS
- Yoga
- इकाई – 02 शोध अभिवृत्ति (Research Aptitude)
- इकाई – 03 बोध (Comprehension)
- इकाई – 04 संप्रेषण (Communication)
- इकाई – 07 आंकड़ों की व्याख्या (Data Interpretation)
- इकाई – 10 उच्च शिक्षा प्रणाली (Higher Education System)
- इकाई -01 शिक्षण अभिवृत्ति (Teaching Aptitude
- इकाई -06 युक्तियुक्त तर्क (Logical Reasoning)
- इकाई -09 लोग विकास और पर्यावरण (People, Development and Environment)
- इकाई 08 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT-Information and Communication Technology)
- इकाई-05 गणितीय तर्क और अभिवृत्ति (Mathematical Reasoning And Aptitude)
- कबीर ग्रंथावली (संपादक- हजारी प्रसाद द्विवेदी)
- कविताएँ-Poetries
- कहानियाँ – इकाई -07
- कहानियाँ-KAHANIYAN
- कहानियाँ-Stories
- खिलाड़ी-Players
- प्राचीन ग्रन्थ-Ancient Books
- मुंशी प्रेमचंद
- व्यक्तियों के विषय में-About Persons
- सार्थक न्यूज़
- साहित्यकार
- हिंदी व्याकरण-Hindi Grammar