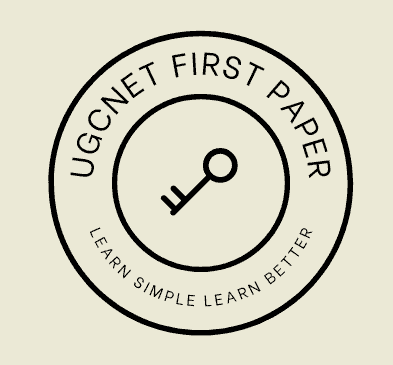khoi hui dishayen – kamleshwar
सड़क के मोड़ पर लगी रेलिंग के सहारे चंदर खड़ा था। सामने, दाएँ-बाएँ आदमियों का सैलाब था। शाम हो ही थी और कनॉट प्लेस की बत्तियाँ जगमगाने लगी थीं। थकान से उसके पैर जवाब दे रहे थे। कहीं दूर आया गया भी तो नहीं, फिर भी थकान सारे शरीर में भरी हुई थी। दिल और दिमाग़ इतना थका हुआ था कि लगता था, वही थकान धीरे-धीरे उतरकर तन में फैलती जा रही है।
पूरा दिन बरबाद हो गया। यही खड़ा सोच रहा था। घर लौटने को भी मन नहीं कर रहा था। आती-जाती एक-सी औरतों को देखकर मन और ऊबने लगता था।
भूख पता नहीं, लगी है या नहीं। वह दिमाग़ पर ज़ोर डालता है-सवेरे आठ बजे घर से निकला था। एक प्याली कॉफ़ी के अलावा तो कुछ पेट में गया नहीं। और तब उसे अहसास हुआ कि थोड़ी-थोड़ी भूख लग रही है। दिमाग़ और पेट का साथ ऐसा हो गया है कि भूख भी सोचने से लगती है।
निगाह दूर आसमान पर अटक जाती है, जहाँ चीलें उड़ रही हैं और मोज़े की शक्ल में कटा हुआ आसमान दिखाई दे रहा है। उस गंदले आसमान के नीचे जामा मस्जिद का गुंबद और मीनार दिखाई पड़ रही है, उनकी नोकें बड़ी अजीब-सी लग रही हैं।
पीछेवाली दुकान से बाहर चोलियों का विज्ञापन है। रीगल बस-स्टॉप के नीम के पेड़ों से धीरे-धीरे पत्तियाँ झड़ रही हैं। बसें जूं-जूं करती आती हैं- एक क्षण ठिठकती हैं—एक ओर से सवारियों को उगलती हैं और दूसरी ओर से निगलकर आगे बढ़ जाती हैं। चौराहे पर बत्तियाँ लगी हैं। बत्तियों की आँखें लाल-पीली हो रही हैं। आस-पास से सैकड़ों लोग गुज़रते हैं पर कोई उसे नहीं पहचानता। हर आदमी या औरत लापरवाही से दूसरों को नकारता या झूठे दर्प में डूबा हुआ गुज़र जाता है।
और तब उसे अपना वह शहर याद आता है, जहाँ से तीन साल पहले वह चला आया था-गंगा के सुनसान किनारे पर भी अगर कोई अनजान मिल जाता तो नज़रों में पहचान की एक झलक तैर जाती थी।
और यह राजधानी! जहाँ सब अपना है, अपने देश का है पर कुछ भी अपना नहीं है, अपने देश का नहीं है।
तमाम सड़कें हैं जिन पर वह जा सकता है, लेकिन वे सड़कें कहीं नहीं पहुँचातीं। उन सड़कों के किनारे घर हैं, बस्तियाँ हैं, पर किसी भी घर में वह नहीं जा सकता। उन घरों के बाहर फाटक हैं, जिन पर कुत्तों से सावधान रहने की चेतावनी है, फूल तोड़ने की मनाही है और घंटी बजाकर इंतज़ार करने की मजबूरी है।
“घर पर निर्मला इंतज़ार कर रही होगी। वहाँ पहुँचकर भी पहले मेहमान की तरह कुर्सी पर बैठना होगा, क्योंकि बिस्तर पर कमरे का पूरा सामान सजा होगा और वह हीटर पर खाना पका रही होगी। उन्मुक्त होकर वह हवा के झोंके की तरह कमरे में घुस भी नहीं सकता और न उसे बाँहों में लेकर प्यार कर सकता है, क्योंकि गुप्ताजी अभी मिल से लौटे नहीं होंगे और मिसेज गुप्ता बेकारी में बैठी गप लड़ा रही होंगी या किसी स्वेटर की बुनाई सीख रही होंगी। अगर वह चला भी गया तो कमरे में बहुत अदब से घुसेगा, फिर मिसेज़ गुप्ता से इधर-उधर की दो-चार बातें करेगा। तब बीवी खाना खाने की बात कहेगी। और खाने की बात सुनकर मिसेज़ गुप्ता घर जाने के लिए उठेंगी…
और फिर उसके बाद बड़ी खिड़की का परदा खिसकाना पड़ेगा। किसी बहाने खुराना की तरफ़वाली खिड़की को बंद करना पड़ेगा घूमकर मेज के पास पहुँचना होगा और तब पानी का एक गिलास माँगने के बहाने वह पत्नी को बुलाएगा, और तब उसे बाँहों में लेकर प्यार से यह कह सकने का मौक़ा आएगा-“बहुत थक गया हूँ।”
लेकिन ऐसा होगा नहीं। इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के पहले ही उसका मन झुंझला उठेगा और यह कहने पर मजबूर हो जाएगा, “अरे भई, खाने में कितनी देर है”, सारा प्यार और समूची पहचान न जाने कहाँ छिप चुकी होगी, अजीब-सा बेगानापन होगा। बेकरीवालों के यहाँ भर्रायी आवाज़ में रेडियो गा रहा होगा और गुलाटी के थके क़दमों की खोखली आवाज़ जीने पर सुनाई पड़ेगी।
गली में कोई स्कूटर आकर रुकेगा और उसमें से कोई बिन-पहचाना आदमी किसी और के घर में चला जाएगा। मोटरों की मरम्मत करनेवाले गैरेज का मालिक सरदार चाबियाँ लेकर घर जाने के इंतज़ार में आधी रात तक बैठा रहेगा क्योंकि उसे पंद्रह साल पुराने मैकेनिक पर भी शायद विश्वास नहीं है।
और सामने रहनेवाले बिशन कपूर के आने की आहट-भर मिलेगी। पिछले दो साल से उसने सिर्फ़ उनके नाम की प्लेट देखी है-बिशन कपूर, जर्नलिस्ट और उसकी शक्ल के बारे में वह सिर्फ़ यह जानता है कि सामनेवाली खिड़की से जब बिजली की रोशनी छनने लगती है और सिगरेट का धुआँ सलाखों से लिपट-लिपटकर बाहर अँधेरे में डूब जाता है तो बिशन कपूर नाम का एक आदमी भीतर होता है और सुबह जब उसकी खिड़की के नीचे अंडे का छिलका, डबल रोटी का रैपर और जली हुई सिगरेटें, तीलियाँ और राख बिखरी हुई होती हैं तो विशन कपूर नाम का आदमी जा चुका होता है।
सोचते-सोचते उसे लगा कि मोज़े की बदबू और भी तेज होती जा रही है और अब रेलिंग के पास खड़ा रहना मुश्किल है। जेब से डायरी निकालकर उसने अगले दिन की मुलाक़ातों के बारे में जान लेना चाहा।
…अंग्रेज़ी दैनिक में पहले फ़ोन करना है, फिर समय तय करके मिलना है। रेडियो में एक चक्कर लगाना है। पिछला चेक रिजर्व बैंक से कैश कराना है और घर एक मनीआर्डर भेजना है। कल का पूरा वक्त भी इसी में निकल जाएगा, क्योंकि अखबार का संपादक परिचित नहीं है जो फ़ौरन बुला ले और खुलकर बात कर ले और कोई बात तय हो जाए। रेडियो में भी कोई बात दस मिनट में तय नहीं हो सकती और रिजर्व बैंक के काउंटर पर इलाहाबाद वाला अमरनाथ नहीं है, जो फ़ौरन चेक लेकर रुपया ला दे। डाकखाने पर व्यापारियों के चपरासियों की भीड़ होगी जो दस-दस मनीआर्डर के फार्म लिए लाइन में खड़े होंगे और एक काग़ज़ पर पूरी रकम और मनीआर्डर कमीशन का मीज़ान लगाने में मशगूल होंगे। उनमें से कोई भी उसे नहीं पहचानता होगा।
एक क्षण की जान-पहचान का सिलसिला सिर्फ़ पेन होगा, जो कोई-न-कोई दो हरुफ़ लिखने के लिए माँगेगा और लिख चुकने के बाद अपना ख़त पढ़ते हुए वह बाएँ हाथ से उसे क़लम लौटाकर शायद धीरे से थैंक्यू कहेगा और टिकटवाले काउंटर की ओर बढ़ जाएगा।
और तब उसे झुंझलाहट-सी हुई। डायरी हाथ में थी और उसकी निगाहें फिर दूर की ऊँची इमारतों पर अटक गई थीं, जिन पर बिजली के मुकुट जगमगा रहे थे। और उन नामों में से वह किसी को नहीं जानता था। इलाहाबाद में सबसे बड़े कपड़ेवाले के बारे में इतना तो मालूम था कि पहले वह बहुत ग़रीब था और कंधे पर कपड़ा रखकर फेरी लगाता था और अब उसका लड़का विदेश पढ़ने गया हुआ है और वह खुद बहुत धार्मिक आदमी है, जो अब माथे पर छापा-तिलक लगाकर मनमाना मुनाफ़ा वसूल करता है और कार्पोरेशन का चुनाव लड़ने की तैयारियाँ कर रहा है। यहाँ कुछ भी पता नहीं चलता, किसी के बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ता।
कनॉट-प्लेस में खुले हुए लॉन हैं। तनहा पेड़ हैं और उन दूर-दूर खड़े तनहा पेड़ों के नीचे नगर निगम की बेंचें हैं, जिन पर थके हुए लोग बैठे हैं और लॉन में एकाध बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चों की शक्लें और शरारतें तो बहुत पहचानी-सी लगती हैं, पर गोलगप्पे खाती हुई उनकी मम्मी अजनबी है, क्योंकि उसकी आँखों में मासूमियत और गरिमा से भरा प्यार नहीं है। उसके शरीर में मातृत्व का सौन्दर्य और दर्प भी नहीं है, उसमें सिर्फ़ एक खुमार है और एक बहुत बेमानी और पिटी हुई ललकार है, जिसे न तो नकारा जा सकता है और न स्वीकार किया जा सकता है-वह ललकार सब कानों में गूंजती है और सब बहरों की तरह गुज़र जाते हैं।
लॉन पर कुछ क्षण बैठने को मन हुआ पर उसे लगा कि वहाँ भी कोई ठिकाना नहीं, अभी कल ही तो चोर की तरह दबे पाँव घास में बहता हुआ पानी आया था और उसके कपड़े भीग गए थे।
तनहा खड़े पेड़ों और उनके नीचे सिमटते अँधेरे में अजीब-सा खालीपन है। तनहाई ही सही, पर उसमें अपनापन तो हो। वह तनहाई भी किसी की नहीं है क्योंकि हर दस मिनट बाद पुलिस का आदमी उधर से घूमता हुआ निकल जाता है। झाड़ियों की सूखी टहनियों में आइस्क्रीम के खाली काग़ज़ और चने की ख़ाली पुड़ियाँ उलझी हुई हैं या कोई बेघरबार आदमी शराब की खाली बोतल फेंककर चला गया है।
डायरी पर फिर उसकी नज़र जम जाती है, और शोर-शराबे से भरे उस सैलाव में वह बहुत अकेला-सा महसूस करता है और लगता है कि इन तीन सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो उसका अपना हो, जिसकी कचोट अभी तक हो, खुशी या दर्द अब भी मौजूद हो। रेगिस्तान की तरह फैली हुई तनहाई है, अनजान सागर-तटों की ख़ामोशी और सूनापन है और पछाड़ खाती हुई लहरों का शोर-भर है, जिससे वह ख़ामोशी और भी गहरी होती है।
मोज़े की शक्ल मे कटा हुआ आसमान है और जामा मस्जिद के गुंबद के ऊपर चक्कर काटती हुई चीलें हैं। औरतों का पीछा करते हुए फूल बेचनेवाले और यतीम बच्चों के हाथ में शाम की ख़बरों के अख़बार हैं।
…और तभी चंदर को लगा कि एक अरसा हो गया, एक जमाना गुज़र गया, वह खुद अपने से नहीं मिल पाया। अपने से बातें करने का वक्त ही नहीं मिला। यह भी नहीं पूछा कि आखिर तेरा हाल-चाल क्या है और तुझे क्या चाहिए? हल्की-सी मुस्कराहट उसके होंठों पर आई और उसने हर शुक्रवार के आगे नोट किया- “खुद से मिलना है। शाम सात बजे से नौ बजे तक।” और आज भी तो शुक्रवार ही है। यह मुलाक़ात आज ही होनी चाहिए। घड़ी पर नज़र जाती है, सात बजा है। पर मन का चोर हावी हो जाता है। क्यों न टी-हाउस में एक प्याला चाय पी ली जाए? न जाने क्यों मन अपने से मिलने में घबराता है। रह-रहकर कतराता है।
तभी उस पार से आता हुआ आनंद दिखाई देता है। वह उसे भी नहीं चाहता। बड़ा बुरा मर्ज़ है आनंद को वह इस छूत से बचा रहना चाहता है। आनंद दुनिया में दोस्त खोजता है, ऐसे दोस्त जो ज़िन्दगी में गहरे न उतरें पर उसके साथ कुछ देर रह सकें और बात कर सकें। उसकी बातों में अजीब-सा बनावटीपन है, वह बनावटीपन जो आदमी किताबों से सीखता है। और उसे लगता है कि वही बनावटीपन खुद उसमें भी कहीं-न-कहीं है जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दर्जों में बैठ-बैठकर वह किताबों से जिन्दगियों के भरे हुए ब्यौरे पढ़ रहा था।
और अब आज उसे लगता है कि वह सारा वक्त बड़ी बेरहमी से बरबाद किया गया है। उसने उन खंडहरों में समय बरबाद किया है जिनकी कथाएँ अधपढ़े गाइडों की ज़बान पर रहती हैं, जो हर बार उन मरी हुई कहानियों को हर दर्शक के सामने दोहराते जाते हैं- “यह दीवाने-खास है, जरा नक्काशी देखिए, यहाँ हीरे जवाहरातों से जड़ा सिंहासन था, यह जनाना हमाम है और यह वह जगह है जहाँ से बादशाह अपनी रिआया को दर्शन देते थे, यह महल सर्दियों का है, यह बरसात का और यह हवादार महल गर्मियों का और इधर आइए संभल के, यह वह जगह है जहाँ फाँसी दी जाती थी।”
चंदर को लगा, ज़िन्दगी के पचीस साल वह उन गाइडों के साथ खंडहरों में बिताकर आया है, जिनकी जीवंत कथाओं को वह कभी नहीं जान पाया, सिर्फ दीवाने-खास उसे दिखाया गया, नक्काशी दिखाई गई और जनाने हमाम में घुमाकर गाइड ने उसे फाँसीवाले अँधेरे और बदबूदार कमरे में छोड़ दिया, जहाँ चमगादड़ लटके हुए बिलबिला रहे हैं और एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक रस्सी लटक रही है जिसका फंदा गरदन में कस जाता है और आदमी झूल जाता है और उसके बाद अंधे कुएँ में फेंकी गई सिर्फ़ वे लाशें रह जाती हैं। उसमें और उनमें कोई अंतर नहीं है।
और आनंद भी उनसे अलग नहीं है। चंदर कतरा जाना चाहता था, क्योंकि आनंद आते ही किताबी तरीक़े से कहेगा, “यार तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, ब्रिलक्रीम लगाते हो? लड़कियाँ तो तबाह हो जाती होंगी।”
और तभी चंदर को सामने पाकर आनंद रुक जाता है, “हलो, यहाँ कैसे? क्यों लड़कियों पर जुल्म ढा रहे हो?” सुनकर उसे हँसी आ जाती है।
“किधर से आ रहे हो ?” डायरी जेब में रखते हुए वह पूछता है।
“आज तो यूँ ही फँस गए, आओ एक प्याला कॉफ़ी हो जाए।” आनंद कहता है, फिर एक क्षण रुककर वह दूसरी बात सुझाता है, “या और कुछ ” चंदर इसका मतलब समझकर न कर देता है। वह ज़ोर देता है, “चलो फिर
आज तो हो ही जाए, क्या रखा है इस ज़िन्दगी में?” कहते हुए वह झूठी हँसी हँसता और धीरे से हाथ दबाकर पूछता है, “प्लीज, इफ़ यू डोण्ट माइंड, कुछ पैसे हैं?” उसके कहने में कोई हिचक नहीं है और न उसे शरम ही आती है। बड़ी सीधी-सी बात है, पैसे कम हैं।
“अच्छा पार्टनर, मैं अभी इंतजाम करके आया,” वह विश्वास को गहराता हुआ कहता है, “यहीं रुकना, चले मत जाना,” और वह जाता है तो फिर नहीं आता। चंदर यह पहले से जानता है। कुछ देर बाद वह टी-हाउस में घुस जाता है और मेजों के पास चक्कर काटता हुआ कोने वाले काउंटर से सिगरेट का पैकेट लेकर एक मेज पर जम जाता है। “”हलो!” कोई एक अधजाना चेहरा कहता है, “बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ और वह भी वहीं बैठ जाता है। दोनों के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है।
टी-हाउस में बेपनाह शोर है। खोखली हँसी के ठहाके हैं और दीवार पर एक घड़ी है, जो हमेशा वक़्त से आगे चलती है। तीन रास्ते बाहर से आने और जाने के लिए हैं और चौथा रास्ता बाथरूम जाता है। बाथरूम के पॉट्स में फ़िनाइल की गोलियाँ पड़ी हैं और गैलरी में एक शीशा लगा हुआ है। हर वह आदमी जो बाथरूम जाता है, उस शीशे में अपना मुँह देखकर लौटता है।
गेलार्ड में डिनर डांस की तैयारी हो रही है। कुर्सियों की तीन कतारें बाहर निकालकर रख दी गई हैं। उधर बोल्गा पर विदेशियों की भीड़ बढ़ रही होगी।
और तभी एक जोड़ा भीतर आता है। महिला सजी-धजी है और जूड़े फूल भी हैं। आदमी के चेहरे पर अजीब-सा गरूर है और वे दोनों फैमिलीवाली सीट पर आमने-सामने बैठ जाते हैं। बैठने से पहले उनमें कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ़ इतना-भर कि जब महिला बैठने के लिए मुड़ी थी तो साथवाले आदमी ने उसकी कमर पर हाथ रखकर सहारा-भर दिया था। इतना सा साथ था दोनों में।
उनके पास भी बात करने के लिए शायद कुछ नहीं है। महिला अपना जूड़ा ठीक करते हुए औरों को देख रही है और साथवाला आदमी पानी के गिलास को देख रहा है। किसी के देखने में कोई मतलब नहीं है। आँखें हैं इसलिए देखना पड़ता है। अगर न होतीं तो सवाल ही नहीं था। एक जगह देखते-देखते आँखों में पानी आ जाता है इसलिए ज़रूरी है कि इधर-उधर देखा जाए।
बेयरा उनकी मेज़ पर सामान रख जाता है और दोनों खाने में मशगूल हो जाते हैं। कोई बात नहीं करता। आदमी खाना खा के दाँत कुरेदने लगता है और वह महिला रूमाल निकालकर अंदाज़ से लिपस्टिक ठीक करती है।
अंत में बेयरा आकर पैसे लौटाता है तो आदमी कुछ टिप छोड़ता है, जिसे महिला ग़ौर से देखती है और दोनों लापरवाही से उठ खड़े होते हैं। फिर उन दोनों में हल्का-सा संबंध उसे नज़र आता है, वह आदमी ठिठककर साथवाली महिला को आगे निकलने का इशारा करता है और उसके पीछे-पीछे चला जाता है।
चंदर का मन और भारी हो जाता है। अकेलेपन का नागपाश और भी कस जाता है। अपने साथ बैठे हुए अनजान दोस्त की तरफ़ वह गहरी नज़रों से देखता है और सोचता है, अजनबी ही सही, पर इसने पहचाना तो इतनी पहचान भी बड़ा सहारा देती है चंदर को अपनी ओर देखते हुए देख वह साथवाला दोस्त कुछ कहने को होता है, पर जैसे उसे कुछ याद नहीं आता, फिर अपने को सँभाल कर उसने चंदर से पूछा, “आप आप तो शायद कॉमर्स मिनिस्ट्री में हैं। मुझे याद पड़ता है कि कहते हुए वह रुक जाता है।
चंदर का पूरा शरीर झनझना उठता है और एक घूँट में बची हुई कॉफ़ी पीकर वह बड़े संयत स्वर में जवाब देता है, “नहीं, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में कभी नहीं था “
वह आदमी आगे अटकलें भिड़ाने की कोशिश नहीं करता, सीधे-सीधे उस अनजान संबंध को मजबूत बनाते हुए कहता है, “ऑल राइट पार्टनर, फिर कभी मुलाक़ात होगी।” और सिगरेट सुलगाता हुआ उठ जाता है।
चंदर बाहर निकलकर बस-स्टॉप की ओर बढ़ता है। मद्रास होटल के पीछे बस-स्टॉप पर चार-पाँच लोग खड़े हैं और पुलिसवाला स्टॉप की छतरी के नीचे बैठा सिगरेट पी रहा है।
चंदर वहीं आकर खड़ा हो जाता है। सब जानना चाहते हैं कि बस कब तक आएगी, पर कोई किसी से कुछ भी नहीं पूछता। पेड़ के अँधेरे में वह चुपचाप खड़ा है। नीचे पीले पत्ते पड़े हैं, जो उसके पैरों से दबकर चुरमुराने लगते हैं और पीले पत्तों की आवाज़ उसे वर्षों पीछे खींच ले जाती है। इस आवाज़ में एक बहुत गहरा अपनापन है, उसे बड़ी राहत-सी मिलती है।
“ऐसे ही पीले पत्ते पड़े हुए थे। उस राह पर बहुत साल पहले इंद्रा के साथ एक दिन वह चला जा रहा था, कुछ भी नहीं था उसके सामने वह खंडहरों में अपनी जिन्दगी ख़राब कर रहा था और तब इंद्रा ने ही उससे कहा, “चंदर, तुम क्या नहीं कर सकते!” वही पहचानी हुई आवाज़ फिर उसके कानों से टकराती है, “तुम क्या नहीं कर सकते!” और यह कहते-कहते इंद्रा की आँखों में अदम्य विश्वास झलक आया था।
और इंद्रा की उन प्यार-भरी आँखों में झाँकते हुए उसने कहा था, “मेरे पास है ही क्या? समझ में नहीं आता कि ज़िन्दगी कहाँ ले जाएगी इंद्रा! इसीलिए मैं यह नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िन्दगी मेरी ख़ातिर बिगाड़ लो। पता नहीं मैं किस किनारे लगें, भूखा मरूँ या पागल हो जाऊँ “
इंद्रा की आँखों में प्यार के बादल और गहरे हो गए थे और उसने कहा था, “ऐसी बातें क्यों करते हो चंदर, मैं तुम्हारे साथ हर हालत में सुखी रहूँगी!”
चंदर ने उसे बहुत ग़ौर से देखा था। इंद्रा की आँखों में नमी आ गई थी। उसकी कँटीली बरौनियों से विश्वास भरी मासूमियत छलक रही थी। माथे पर आई हुई लट छूने को उसका मन हो आया था, पर वह झिझककर रह गया था। इंद्रा के कानों में पड़े हुए कुंडल पानी में तैरती मछलियों की तरह झलक जाते थे और तब उसने कहा था, “आओ, उधर पेड़ के नीचे बैठेंगे।”
वे दोनों साथ-साथ चल दिए थे। सिरस के पेड़ के नीचे एक सीमेण्ट की बेंच बनी थी। राह पर पीली पत्तियाँ बिखरी हुई थीं। उनके कुचलने से ऐसी ही आवाज़ आई थी, जो अभी-अभी उसने सुनी थी वही पहचान भरी आवाज़। दोनों बेंच पर बैठ गए थे और चंदर धीरे से उसकी कलाई पर अंगुली से लकीरें खींचने लगा था। दोनों खामोश बैठे थे, बहुत-सी बातें थीं, जो वे कह नहीं पा रहे थे। कुछ क्षणों बाद इंद्रा ने आँखें चुराते हुए उसे देखा था और शरमा गई थी, फिर उसी बात पर आ गई थी, जैसे उसी एक बात में सारी बातें छिपी हों, “तुम ऐसा क्यों सोचते हो, चंदर? मुझ पर भरोसा नहीं?”
” तब चंदर ने कहा था, “भरोसा तो बहुत है इंद्रा, पर मैं खानाबदोशों की तरह जिन्दगी-भर भटकता रहूँगा उन परेशानियों में तुम्हें खींचने की बात सोचता हूँ तो बरदाश्त नहीं कर पाता। तुम बहुत अच्छी और सुविधाओं से भरी ज़िन्दगी जी सकती हो। मैंने तो सिर पर क़फ़न बाँधा है मेरा क्या ठिकाना!”
“तुम चाहे जो कुछ बनो चंदर, अच्छे या बुरे, मेरे लिए एक से रहोगे। कितना इंतजार करती हूँ तुम्हारा, पर तुम्हें कभी वक्त ही नहीं मिलता!” फिर कुछ देर मौन रहकर उसने पूछा था, “इधर कुछ लिखा ?”
“हाँ!” धीरे से चंदर ने कहा था। “दिखाओ।” इंद्रा ने माँगा था।
और तब चंदर ने पसीजे हुए हाथों से डायरी बढ़ा दी थी। इंद्रा ने तुरंत उस डायरी को अपनी किताबों में रख लिया था और बोली थी, “अब यह कल मिलेगी, इस बहाने तो अब आओगे.”
“नहीं-नहीं मैं डायरी अपने साथ ले जाऊँगा, मुझे वापस दो।” चंदर ने कहा था, तो इंद्रा शैतानी से मुस्कराती रही थी और उसकी आँखों में प्यार की गहराइयाँ और बढ़ गई थीं।
हारकर चंदर वापस चला आया था और दूसरे दिन अपनी डायरी लेने पहुँचा था तो इंद्रा ने कहा था, “इसमें कुछ मैंने भी लिखा है, पढ़कर फाड़ देना जरूर से।”
“मैं नहीं फाड़ूँगा”
“तो कुट्टी हो जाएगी, ” इंद्रा ने बच्चों की तरह बड़ी मासूमियत से कहा था और उस वक्त उसके मुँह से वह बेहद बचपने की बात भी बड़ी अच्छी लगी थी। और एक दिन….
एक दिन इंद्रा घर आई थी। इधर-उधर से घूम-घामकर वह चंदर के कमरे में पहुँच गई थी और तब चंदर ने पहली बार उसे बिलकुल अपने पास महसूस किया था और उसके माथे पर रंग से बिंदी बना दी थी और कई क्षणों तक मुग्ध-सा देखता रह गया था, और अनजाने ही उसने होंठ इंद्रा के माथे पर रख दिए थे। इंद्रा की पलकें झप गई थीं और रोम-रोम से गंध फूट उठी थी। उसकी अंगुलियाँ चंदर की बाँहों पर थरथराने लगी थीं और माथे पर आया पसीना उसके होंठों ने सोख लिया था। रेशमी रोएँ पसीने से चिपक गए थे और उन उन्माद के क्षणों में दोनों ने ही प्रतिज्ञा की थी वह प्रतिज्ञा जिसमें शब्द नहीं थे, जो होंठों तक भी नहीं आई थी! तब से उसे ये शब्द हमेशा याद रहते हैं, “तुम क्या नहीं कर सकते!”
और तभी एक दूसरे नंबर की बस आती है और ठिठककर चली जाती है। चंदर को अहसास होता है कि वह बस-स्टॉप पर खड़ा है, वह गहरी पहचान कहीं कोई तो है और वह बहुत दूर भी तो नहीं।
इंद्रा भी तो यहीं है दिल्ली में..
दो महीने पहले ही तो वह मिला था। तब भी इंद्रा की आँखों में वह चार बरस पहले की पहचान थी और उसने पति से किसी बात पर कहा था, “अरे चंदर की आदतें मैं खूब जानती हूँ।” और इंद्रा के पति ने खुले दिल से कहा था, “तो फिर भई, इनकी खातिर-वातिर करो..”
और इंद्रा ने मुस्कराते हुए चार बरस पहले की तरह चिढ़ाने के अंदाज़ में बयान किया था, “चंदर को दूध से चिढ़ है और कॉफ़ी इन्हें धुआँ पीने की तरह लगती है, चाय में अगर दूसरा चम्मच चीनी डाल दी गई तो इनका गला खराब हो जाएगा, ” कहकर वह खिलखिलाकर हँस दी थी और इस बात से उसने पिछली बातों की याद ताज़ा कर दी थी सचमुच चंदर दो चम्मच चीनी नहीं पी सकता।
बस आने का नाम नहीं ले रही थी।
खड़े-खड़े चंदर को लगा कि इस अनजानी और बिन जान-पहचान से भरी नगरी में एक इंद्रा है जो उसे इतने सालों के बाद भी पहचानती है, अब तक जानती है। उसका मन अपने-आप इंद्रा से मिलने के लिए छटपटाने लगा, ताकि यह अजनबीपन किसी तरह टूट सके….
तभी एक फटफटवाला आवाज़ लगाता हुआ आ जाता है, “गुरदारा रोड” क्रोलबाग गुरदारा रोड!” चंदर एक क़दम आगे बढ़ता है और वह सरदार उसे देखते ही जैसे एकदम पहचान जाता है, “आइए बाबूजी क्रोलबाग गुरदारा रोड।” उसकी आँखों में पहचान की झलक देखकर चंदर का मन हल्का हो जाता है। आख़िर एक ने तो पहचाना। चंदर सरदार पहचानता है, बहुत बार वह इसी सरदार के फटफट में बैठकर कनॉट प्लेस आया है।
आँखों में पहचान देखते ही चंदर पलटकर फटफट पर बैठ जाता है। तीन सवारियाँ और आ जाती हैं और दस मिनट बाद ही गुरुद्वारा रोड के चौराहे पर फटफट रुकता है। चंदर एक चवन्नी निकालकर सरदार की हथेली पर रख देता है और पहचान-भरी नज़रों से उसे देखता हुआ चलने लगता है।
तभी पीछे से आवाज़ आती है, “ऐ बाबूजी, कितना पैसा दिया है?” चंदर मुड़कर देखता है तो सरदार उसकी तरफ़ आता हुआ कहता है, “दो आने और दीजिए, साहब!”
“हमेशा चार आने लगते हैं सरदारजी!” चंदर पहचान जताता हुआ कहता है, पर सरदार की आँखों में पहचान की परछाई तक नहीं है। वह फिर कहता है, “सरदारजी, आपके फटफट पर ही बीसों बार चार आने देकर आया हूँ।”
“किसे होरने लए होणगे चार आने असी ते है आने तो घट नहीं लेंदे बादशाहो!” सरदार इस बार पंजाबी में बोला था और उसकी हथेली फैली हुई थी। बात दो आने की नहीं थी। चंदर ने बाकी पैसे उसकी हथेली पर रख दिए और इंद्रा के घर की तरफ़ मुड़ गया।
और इंद्रा उसे मिली तो वैसे ही वह अपने पति का इंतजार कर रही थी। बड़ी अच्छी तरह उसने चंदर को बैठाया और बोली, “इधर कैसे भूल पड़े आज फिर आँखों में वही पहचान की परछाईं तैर गई थी। कुछ क्षणों बाद इंद्रा ने कहा था, “अब तो नौ बज रहे हैं, ये आठ ही बजे फ़ैक्ट्री बंद करके लौट आते हैं, पता नहीं आज क्यों देर हो गई, अच्छा चाय तो पियोगे?”
“चाय के लिए इनकार तो नहीं की जा सकती।” चंदर ने बड़े उत्साह से कहा था और कुरसी पर आराम से टाँगें फैलाकर बैठ गया था। उसकी सारी थकान उतर गई थी और मन का अकेलापन डूब गया था।
नौकरानी आकर चाय रख गई। इंद्रा ने प्याले सीधे करके चाय बनाई, तो वह उसकी बाँहों, चेहरे और हाथों को देखता रहा सब कुछ वही था, वैसा ही या चिर-परिचित। तभी इंद्रा ने पूछा, “चीनी कितनी दूँ?”
और एक झटके से सब कुछ बिखर गया, उसका गला सूखने-सा लगा और शरीर फिर थकान से भारी हो गया। माथे पर पसीना आ गया। फिर भी उसने पहचान का रिश्ता जोड़ने की एक नाकाम कोशिश की और बोला, “दो चम्मच।” और उसे लगा कि अभी इंद्रा को सब कुछ याद आ जाएगा और वह कहेगी कि दो चम्मच चीनी से अब गला खराब नहीं होता ?
पर इंद्रा ने प्याले में दो चम्मच चीनी डाल दी और उसकी ओर बढ़ा दिया। ज़हर के घूँटों की तरह वह चाय पीता रहा। इंद्रा इधर-उधर की बातें करती रही, पर उनमें उसे मेहमानबाज़ी की बू लग रही थी और चंदर का मन कर रहा था कि इंद्रा के पास से किसी भी तरह भाग जाए और किसी दीवार पर अपना सिर पटक दे। जैसे-तैसे उसने चाय पी और पसीना पोंछता हुआ बाहर निकल आया। इंद्रा ने क्या-क्या बातें कीं, उसे बिलकुल याद नहीं ।
सड़क पर निकलकर वह एक गहरी साँस लेता है और कुछ क्षणों के लिए खड़ा रह जाता है। उसका गला बुरी तरह सूख रहा है और मुँह का स्वाद बेहद बिगड़ा हुआ है।
चौराहे पर कुछ टैक्सी-ड्राइवर नशे में गालियाँ बक रहे हैं और एक कुत्ता दूर सड़क पर भागा चला जा रहा है। मछलियाँ तलने की गंध यहाँ तक आ रही है और पानवाले की दुकान पर कुछ जवान कोकाकोला की बोतलें मुँह में लगाए खड़े हैं। स्कूटरों में कुछ लोग भागे जा रहे हैं, और शहर से दूर जानेवाले लोग बस स्टॉप पर में खड़े अब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कारें, टैक्सियाँ, बसें और स्कूटर आ-जा रहे हैं। चौराहे पर लगी बत्तियों की आँखें अब भी लाल-पीली हो रही हैं।
चंदर थका-सा अपने घर की ओर लौट रहा है। अंगुलियों पर जूता काट रहा है और मोज़े की बदबू और तेज हो गई है।
आख़िर वह थका-हारा घर पहुँचता है और मेहमान की तरह कुरसी पर बैठ जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। निर्मला उसे देखकर मुस्कराती है और धीरे से बाँहों पर हाथ रखकर पूछती है, “बहुत थक गए?”
“हाँ!” चंदर कहता है और उसे प्यार से देखता है। उसका मन भीतर से उमड़ आता है। वह किराए का मकान भी उस क्षण उसे राहत देता है और लगता है कि वह उसी का है।
निर्मला खाना लगाते हुए कहती है, “हाथ-मुँह धो लो…”
“अभी खाने का मन नहीं है।” चंदर कहता है तो वह बहुत प्यार से देखते हुए पूछती है, “क्यों? क्या बात है? सुबह भी तो खा के नहीं गए थे, दोपहर में कुछ खाया था?”
“हाँ।” वह कहता है और निर्मला को देखता रह जाता है। निर्मला कुछ अचकचाती है और कुछ देर बाद थकी-सी उसके पास बैठ जाती है।
चंदर कुछ देर खोई-खोई नज़रों से कमरे की हर चीज़ देखता रहता है और बीच-बीच में बड़ी गहरी नज़रों से निर्मला को ताकता है। निर्मला कोई किताब खोलकर पढ़ने लगती है और चंदर उसे देखे जा रहा है।
पीछे से पड़ती हुई रोशनी में निर्मला के बाल रेशम की तरह चमक रहे हैं, उसकी बरौनियाँ मुलायम काँटों की तरह लग रही हैं और कनपटी के पास रेशमी बालों से सिरे अपने-आप घूम गए हैं। पलक के नीचे पड़ती हुई परछाईं बहुत पहचानी-सी लग रही है। उसने कड़ा आधी कलाई तक सरका लिया है।
चंदर की निगाहें उसके अंग-प्रत्यंग में पुरानी पहचान खोज रही हैं, उसके नाखून, अँगुलियाँ और कानों की गुदारी लवें..
उठकर वह परदे खींच देता है और आराम से लेट जाता है। उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। अजनबी और तनहा नहीं है। सामनेवाला गुलदस्ता उसका अपना है, पड़े हुए कपड़े उसके अपने हैं, उनकी गंध वह पहचानता है।
इन सभी चीज़ों में एक गहरी पहचान है। घोर अँधेरी रात में भी वह उन्हें टटोलकर पहचान सकता है। किसी भी दरवाजे से बिना टकराए निकल सकता है।
” तभी जीने पर गुलाटी के थके क़दमों की खोखली आहट सुनाई पड़ती है और उसे घबराहट-सी होती है। वह धीरे से निर्मला को अपने पास बुला लेता है। उसे लिटाकर छाती पर हाथ रख लेता है।
कई क्षणों तक वह उसकी साँस से उठती-बैठती छाती को महसूस करता है और चाहता है कि निर्मला के शरीर का अंग-अंग और मन की हर धड़कन उसे पहचान की साक्षी दें गहरी आत्मीयता और निर्बंध एकता का अहसास दें…
अँधेरे ही में वह उसके नाखूनों को टटोलता है, उसकी पलकों को छूता है, उसकी गरदन में मुँह छिपाकर खो जाना चाहता है, धुले हुए वालों की चिर-परिचित गंध उसके रंध्र-रंध्र में रिसने लगती है और उसके हाथ पहचान के लिए पोर-पोर पर थरथराते हुए सरकते हैं। निर्मला की साँस भारी हो आती है।
वह उसकी मांसल बाँहों को महसूस करता है और गोल-गुदारे कंधों पर हाथ से थपथपाता रहता है। निर्मला के शरीर का अंग-अंग अनूठे अनुराग से खिंचता-सा आता है। उसका रोम-रोम उसे पहचान रहा था, जोड़-जोड़ कसाव से पूरित था, तन के भीतर गरम रक्त के ज्वार उठ रहे थे और हर साँस पास खींचती जा रही थी। अंग-प्रत्यंग में पोर-पोर में गहरी पहचान थी…
तभी बिशन कपूर की खिड़की में उजाला होता है और धुआँ सलाखों से लिपट-लिपटकर गली के अँधेरे में डूबने लगता है।
और उसका तनहा मन तनहाइयों को छोड़कर उस परिचित गंध, परिचित साँसों और पहचाने स्पर्शो में डूबता जाता है। उसे और कुछ भी नहीं चाहिए परिचय की एक माँग है और उस अँधेरे में वह साँस से, गंध से, तन के टुकड़े-टुकड़े से पहचान चाहता है, पुरानी प्रतीति चाहता है।
चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है।
और उस ख़ामोशी में वह आश्वस्त होता है-वह दोनों बाँहों में उसे भर लेता है। ज्वार और उठता है। तन की गरमाहट और बढ़ती है और रंध्र-रंध्र में एकता का सागर लहराने लगता है।
धीरे-धीरे निर्मला की तेज़ साँसें धीमी पड़ती हैं और चुंबकीय कशिश ढीली पड़ जाती है। खिंचाव टूटने लगता है और अंगों के ज्वार उतरने लगते हैं।
चंदर कसकर उसकी बाँहों को जकड़े रहता है उतरता हुआ ज्वार उसे फिर अकेला छोड़े जा रहा है अनजान तटों पर छोड़ी हुई सीपी की तरह। निर्मला अपनी दबी हुई बाँह निकाल लेती है और गहरी साँस लेकर ढीली-सी लेट जाती है।
धीरे-धीरे सब कुछ सो जाता है और रात बहुत नीचे उतर आती है। कहीं कोई आवाज़ नहीं, आहट नहीं।
धीरे से निर्मला करवट बदलती है और दूसरी ओर मुँह करके गहरी नींद में डूब जाती है।
करवट बदलकर लेटी हुई निर्मला को वह अलसाया-सा देखता रहता है…
और चंदर फिर अपने को बेहद अकेला महसूस करता है वह निर्मला के कंधे पर हाथ रखता है, चाहता है कि उसकी करवट बदल दे, पर उसकी अंगुलियाँ बेजान होकर रह जाती हैं। कुछ क्षण वह अँधेरे में ही निर्मला को उधर मुँह किए लेटा। देखता है और हताश-सा खुद भी लेट जाता है। पता नहीं कब उसकी पलकें झपक जाती हैं…
और फिर बहुत देर बाद थाने का घड़ियाल दो के घंटे बजाता है और उसकी नींद उचट जाती है। नींद के खुमार में ही वह चौंक-सा पड़ता है। कमरे की खामोशी और सूनेपन से उसे डर-सा लगता है। अँधेरे में ही वह निर्मला को टटोलता है, तकिए पर बिखरे उसके बालों पर उसका हाथ पड़ता है और उन बालों की चिकनाई को महसूस करता है सिर झुकाकर वह उन्हें सूँघता है….
फिर निर्मला पर हाथ रखता है उसके गोल कंधों को छूता है वह स्पर्श भी पहचाना हुआ है धीरे-धीरे वह उसके पूरे शरीर को पहचानने के लिए टटोलता है और उसकी साँसों की हल्की आवाज को सुनने और पहचानने की कोशिश करता है।
निर्मला अब भी करवट लिए पड़ी थी। वह धीरे से नींद में कुनमुनाती है। चंदर का दिल धक् से रह जाता है। कहीं निर्मला जाग न जाए, अनजाने ही इस स्पर्श से अजनबियों की तरह चौंक न जाए।
निर्मला सोते सोते एक बार रुक-रुककर साँस लेती है, जैसे उसे डर-सा लग रहा हो या कोई भयंकर सपना देख रही हो चंदर सुन्न-सा रह जाता है क्या वह उसके स्पर्श को नहीं पहचानती?
और फिर निर्मला को झकझोरकर वह उठाता है। “निर्मला निर्मला “वह बदहवासी में कहता है।
निर्मला चौंककर उठती है और आँखें मलते हुए प्रकृतिस्थ होने की कोशिश करती है।
और बिजली जलाकर वह निर्मला को दोनों कंधों से पकड़कर अपना मुँह उसके सामने करके डरी हुई आवाज़ में पूछता है, “मुझे पहचानती हो? मुझे पहचानती हो निर्मला ?”
निर्मला आँखें फाड़े देखती रह जाती है, धीरे से आश्चर्य-भरे स्वर में कहती है, “क्या हुआ?”
और वह निर्मला को ताकता रह जाता है। उसकी आँखें उसके चेहरे पर कुछ खोजती रह जाती हैं।
शेखर जोशी : कोसी का घटवार
अभी खप्पर में एक-चौथाई से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उलटा-पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाडक़र एक ढेर बना दिया। बाहर आते-आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांककर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी हैं, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस्स-खस्स की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेशद्वार बहुत कम ऊंचा था, खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बांहों पर आटे की एक हलकी सफेद पर्त बैठ गई थी।
खंभे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, ”जा, स्साला! सुबह से अब तक दस पंसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहां का कहां चला गया है। कैसी अनहोनी बात!”
बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है। आकाश में कहीं बादलों का नाम-निशान ही नहीं। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान-रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी-नाले सब सूखे पडे हैं। खेतों की सिंचाईं तो दरकिनार, बीज की क्यारियां सूखी जा रही हैं। छोटे नाले-गूलों के किनारे के घट महीनों से बंद हैं। कोसी के किनारे हैं गुसाईं का यह घट। पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्दू घोडे क़ी चाल को मात देती हैं।
चक्की के निचले खंड में छिच्छर-छिच्छर की आवाज के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज! अच्छे खाते-पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती और अब तो भले नदी पार कोई बोले, तो बात यहां सुनाई दे जाय।
छप्प ..छप्प ..छप्प ..पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोडक़र गुसांईं पानी की गूल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सूराख-निकास हो, तो बंद कर दे। एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद-बूंद की कीमत है इन दिनों। प्रायः आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौडाई को घेरकर पानी का बहाव घट की गूल की ओर मोड दिया गया था। किनारे की मिट्टी-घास लेकर उसने बांध में एक-दो स्थान पर निकास बंद किया और फिर गूल के किनारे-किनारे चलकर घट पर आ गया।
अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहारकर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोडा-बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर आया।
दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गुसांईं ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज दे दी, ”हैं हो! यहां लंबर देर में आएगा। दो दिन का पिसान अभी जमा है। ऊपर उमेदसिंह के घट में देख लो।”
उस व्यक्ति ने मुडने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकारकर वह बोला,”जरूरी है, जी! पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे?”
गुसांईं होंठों-ही-होठों में मुस्कराया, स्साला कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज इतनी हो कि मैं सुन न सकूं! कुछ कम ऊंची आवाज में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, ”यहां जरूरी का भी बाप रखा है, जी! तुम ऊपर चले जाओ!”
वह आदमी लौट गया।
मिहल की छांव में बैठकर गुसांईं ने लकडी क़े जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड-ग़ुड क़रता धुआं उडाता रहा
खस्सर-खस्सर चक्की का पाट चल रहा था।
किट-किट-किट-किट खप्पर से दाने गिरानेवाली चिडिया पाट पर टकरा रही थी।
छिच्छर-छिच्छर की आवाज क़े साथ मथानी पानी को काट रही थी। और कहीं कोई आवाज नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती-पाथरों के बीच में टखने-टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप! कहीं चिरैया भी नहीं बोलती। किसी प्राणी का प्रिय-अप्रिय स्वर नहीं।
सूखी नदी के किनारे बैठा गुसांईं सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया? लौट तो वह जाता ही, घट के अंदर टच्च पडे पिसान के थैलों को देखकर। दो-चार क्षण की बातचीत का आसरा ही होता।
कभी-कभी गुसांईं को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी-भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही। जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते-बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का, जिसका घर-द्वार नहीं, बीबी-बच्चे नहीं, खाने-पीने का ठिकाना नहीं ..
घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड क़ो गुसांईं ने खोला। गूल में चलते हुए थोडा भाग भीग गया था। पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते-करते गुसांईं ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बांएं कोने पर हलकी-सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुसांईं सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है ..नहीं, याद करने को मन नहीं करता। पुरानी,बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवालदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती।
ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवालदार धरमसिंह आया था, लॉन्ड्री की धुली, नोकदार, क्रीजवाली पैंट! वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसांईं फौज में गया था। पर फौज से लौटा, तो पैंट के साथ-साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया।
पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबध्द हैं। उस बार की छुट्टियों की बात ..
कौन महीना? हां, बैसाख ही था। सर पर क्रास खुखरी के क्रेस्ट वाली, काली, किश्तीनुमा टोपी को तिरछा रखकर, फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल-लीव पर घर आया, तो चीड वन की आग की तरह खबर इधर-उधर फैल गई थी। बच्चे-बूढे, सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था, ठसाठस्स। बिस्तर की नई, एकदम साफ, जगमग, लाल-नीली धारियोंवाली दरी आंगन में बिछानी पडी थी लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे-बूढे, सभी आए थे। सिर्फ चना-गुड या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था, कल के शर्मीले गुसांईं को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था। पर गुसांईं की आंखें उस भीड में जिसे खोज रही थीं, वह वहां नहीं थी।
नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लछमा आई थी। पर गुसांई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गुसांईं की जान को बवाल हो गए थे। बुढ्ढे नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे, आजकल गुसांईं को देखकर सोबनियां का लडक़ा भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन-रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट-बीडी या गपशप के लोभ में।
एक दिन बडी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लछमा को पात-पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से कांकड क़े शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर, काफल के पेड क़े नीचे गुसांईं के घुटने पर सर रखकर, लेटी-लेटी लछमा काफल खा रही थी। पके, गदराए, गहरे लाल-लाल काफल। खेल-खेल में काफलों की छीना-झपटी करते गुसांईं ने लछमा की मुठ्ठी भींच दी थी। टप-टप काफलों का गाढा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लछमा ने कहा था, ”इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बांह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी।”वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी।
पुरानी बात – क्या कहा था गुसांईं ने, याद नहीं पडता ..तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा, मेरी सुवा! या कुछ ऐसा ही।
पर लछमा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी – पहाडी पार के रमुवां ने, जो तुरी-निसाण लेकर उसे ब्याहने आया था?
”जिसके आगे-पीछे भाई-बहिन नहीं, माई-बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखनेवाले को छोकरी कैसे दे दें हम?” लछमा के बाप ने कहा था।
उसका मन जानने के लिए गुसांईं ने टेढे-तिरछे बात चलवाई थी।
उसी साल मंगसिर की एक ठंडी, उदास शाम को गुसांईं की यूनिट के सिपाही किसनसिंह ने क्वार्टर-मास्टर स्टोर के सामने खडे-ख़डे उससे कहा था, ”हमारे गांव के रामसिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढानी पडीं। ऌस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है, यार! शक्ल-सूरत भी खूब है,एकदम पटाखा! बडी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नजदीक की ही है। लछमा-लछमा कुछ ऐसा ही नाम है।”
गुसांई को याद नहीं पडता, कौन-सा बहाना बनाकर वह किसनसिंह के पास से चला आया था, रम-डे थे उस दिन। हमेशा आधा पैग लेनेवाला गुसांईं उस दिन पेशी करवाई थी – मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में। सोचते-सोचते गुसांईं बुदबुदाया, ”स्साल एडजुटेन्ट!”
गुसांईं सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से बिदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लछमा से मिला था।
”गंगनाथज्यू की कसम, जैसा तुम कहोगे, मैं वैसा ही करूंगी!” आंखों में आंसूं भरकर लछमा ने कहा था।
वर्षों से वह सोचता आया है, कभी लछमा से भेंट होगी, तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी-देवताओं की झूठी कसमें खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ? जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ, वह कभी फल-फूल नहीं पाया। पर लछमा से कब भेंट होगी, यह वह नहीं जानता। लडक़पन से संगी-साथी नौकरी-चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लछमा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता।
जितने दिन नौकरी रही, वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वालंटियरी ट्रांसफर लेनेवालों की लिस्ट में नायक गुसांईसिंह का नाम ऊपर आता रहा – लगातार पंद्रह साल तक।
पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा, पंद्रह साल बाद, रिजर्व में आने पर। काले बालों को लेकर गया था, खिचडी बाल लेकर लौटा। लछमा का हठ उसे अकेला बना गया।
आज इस अकेलेपन में कोई होता, जिसे गुसांईं अपनी जिंदगी की किताब पढक़र सुनाता! शब्द-शब्द, अक्षर-अक्षर कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने ..
पर नदी किनारे यह तपती रेत, पनचक्की की खटर-पटर और मिहल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुडग़ुडाता गुसांईं। और चारों ओर अन्य कोई नहीं। एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान –
एकाएक गुसांईं का ध्यान टूटा।
सामने पहाडी क़े बीच की पगडंड़ी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी ओर चली आ रही थी। गुसांईं ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने, काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला-चिल्लाकर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोडक़र नदी के मार्ग में आ पहुंची थी।
चक्की की बदलती आवाज को पहचानकर गुसांईं घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्नवाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिडियों को उलटा कर दिया। किट-किट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी-जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिच्छर-छिच्छर की आवाज भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपरवाले पाट की घिसटती हुई घरघराहट का हल्का-धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसांईं ने सुना अपनी पीठ के पीछे, घट के द्वार पर, इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठस्वर, ”कब बारी आएगी, जी? रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है।”
सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गुसांईं को उसका स्वर परिचित-सा लगा। चौंककर उसने पीछे मुडक़र देखा। कपडे में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुसांईं उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुडा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर-उधर रखने लगा। काठ की चिडियां किट-किट बोल रही थीं और उसी गति के साथ गुसांईं को अपने हृदय की धडक़न का आभास हो रहा था।
घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्य का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसांईं के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृध्द-सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना।
उसने दुबारा वे ही शब्द दुहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुसांईं का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उलटे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती।
दूसरी बार के प्रश्न को गुसांईं न टाल पाया, उत्तर देना ही पडा, ”यहां पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही।” उसने दबे-दबे स्वर में कह दिया।
स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय-विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पडी।
गुसांईं झुककर घट से बाहर निकला। मुडते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश-सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाडक़र एक-दो कदम आगे बढा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी, जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसांईं के अंतर में तीव्र उथल-पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया, लडख़डाती आवाज में उसने पुकारा, ”लछमा!”
घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गुसांईं ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, ”लछमा!”
लछमा ने पीछे मुडक़र देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे, यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था। परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्कीवाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दुबारा उसे बुला रहा है या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, ”मुझे पुकार रहे हैं, जी?
गुसांईं ने संयत स्वर में कहा, ”हां, ले आ, हो जाएगा।”
लछमा क्षण-भर रूकी और फिर घट की ओर लौट आई।
अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसांईं व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ मिहल की छांह में चला गया।
लछमा पिसान का थैला घट के अंदर रख आई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड क़ी छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर-उधर देखा। मिहल के पेड क़ी छाया में घट की ओर पीठ किए गुसांईं बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाडिम के एक पेड क़ी छांह को छोडक़र अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी।
गुसांईं की उदारता के कारण ॠणी-सी होकर ही जैसे उसने निकट आते-आते कहा, ”तुम्हारे बाल-बच्चे जीते रहें, घटवारजी! बडा उपकार का काम कर दिया तुमने! ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में लंबर मिलता।”
अजाज संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसांईं ने मन-ही-मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल-पुथल कुछ कम हो गई। लछमा उसकी ओर देखें, इससे पूर्व ही उसने कहा, ”जीते रहे तेरे बाल-बच्चे लछमा! मायके कब आई?”
गुसांईं ने अंतर में घुमडती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया, जैसे वह भी अन्य दस आदमियों की तरह लछमा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो।
दाडिम की छाया में पात-पतेल झाडक़र बैठते लछमा ने शंकित दृष्टि से गुसांईं की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल-प्लावित होकर बहने लगती, तो भी लछमा को इतना आश्चर्य न होता, जितना अपने स्थान से केवल चार कदम की दूरी पर गुसांईं को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाडक़र वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है, वह उसका पूर्व-परिचित गुसांईं ही है।
”तुम?” जाने लछमा क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए।
”हां, पिछले साल पल्टन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया।” गुसांईं ने ही पूछा, ”बाल-बच्चे ठीक हैं?”
आंखें जमीन पर टिकाए, गरदन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाडिम के फूल को हाथों में लेकर लछमा उसकी पंखुडियों को एक-एक कर निरूद्देश्य तोडने लगी और गुसांईं पतली सींक लेकर आग को कुरेदता रहा।
बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसांईं ने पूछा, ”तू अभी और कितने दिन मायके ठहरनेवाली है?”
अब लछमा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप्-टप्-टप्, वह सर नीचा किए आंसूं गिराने लगी। सिसकियों के साथ-साथ उसके उठते-गिरते कंधों को गुसांईं देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे।
इतनी देर बाद सहसा गुसांईं का ध्यान लछमा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरेऊ (सुहाग-चिह्न) नहीं था। हतप्रभ-सा गुसांईं उसे देखता रहा। अपनी व्यावहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी।
आज अचानक लछमा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया, जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल-मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसांईं की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लछमा आंसूं पोंछती हुई अपना दुखडा रोने लगी, ”जिसका भगवान नहीं होता, उसका कोई नहीं होता। जेठ-जेठानी से किसी तरह पिंड छुडाकर यहां मां की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोडक़र चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड रहा है। नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता।”
”यहां काका-काकी के साथ रह रही हो?” गुसांईं ने पूछा।
”मुश्किल पडने पर कोई किसी का नहीं होता, जी! बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, सोचते हैं, कहीं मैं हक न जमा लूं। मैंने साफ-साफ कह दिया, मुझे किसी का कुछ लेना-देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो-ढोकर अपनी गुजर कर लूंगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी।”
गुसांईं ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की। केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता-भर रहा। दाडिम के वृक्ष से पीठ टिकार लछमा घुटने मोडक़र बैठी थी। गुसांईं सोचने लगा, पंद्रह-सोलह साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते, समय का यह अंतराल लछमा के चेहरे पर भी एक छाप छोड ग़या था, पर उसे लगा, उस छाप के नीचे वह आज भी पंद्रह वर्ष पहले की लछमा को देख रहा है।
”कितनी तेज धूप है, इस साल!” लछमा का स्वर उसके कानों में पडा। प्रसंग बदलने के लिए ही जैसे लछमा ने यह बात जान-बूझकर कही हो।
और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया, जहां लछमा बैठी थी। दाडिम की फैली-फैली अधढंकीं डालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड रही थी। सूरज की एक पतली किरन न जाने कब से लछमा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डूबा रही थी। गुसांईं एकटक उसे देखता रहा।
”दोपहर तो बीत चुकी होगी,” लछमा ने प्रश्न किया तो गुसांईं का ध्यान टूटा, ”हां, अब तो दो बजनेवाले होंगे,” उसने कहा, ”उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जा छांव में।” कहता हुआ गुसांईं एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया।
”नहीं, यहीं ठीक है,” कहकर लछमा ने गुसांईं की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था।
घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी-जल्दी लछमा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया।
धीरे-धीरे चलकर गुसांईं गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भर-भरकर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और अलमुनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया।
आस-पास पडी हुई सूखी लकडियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक कालिख पुती बटलोई में पानी रखकर जाते-जाते लछमा की ओर मुंह कर कह गया, ”चाय का टैम भी हो रहा है। पानी उबल जाय, तो पत्ती डाल देना, पुडिया में पडी है।”
लछमा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जानेवाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही।
सडक़ किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते-लौटते गुसांईं को काफी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा, एक छः-सात वर्ष का बच्चा लछमा की देह से सटकर बैठा हुआ है।
बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लछमा ने कहा, ”इस छोकरे को घडी-भर के लिए भी चैन नहीं मिलता। जाने कैसे पूछता-खोजता मेरी जान खाने को यहां भी पहुंच गया है।”
गुसांई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार-बार उसकी दृष्टि बचाकर मां से किसी चीज के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लछमा ने उसे झिडक़ दिया, ”चुप रह! अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी-सी देर में क्यों मरा जा रहा है?”
चाय के पानी में दूध डालकर गुसांईं फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गूल के किनारे बैठा-बैठा उसे गूंथने लगा। मिहल के पेड क़ी ओर आते समय उसने साथ में दो-एक बर्तन और ले लिए।
लछमा ने बटलोई में दूध-चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक एनेमल का मग और एक अलमुनियमके मैसटिन में गुसांईं ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा।
हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लछमा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुसांईं ना न कह सका। वह खडा-खडा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल-गोल डिबिया-सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगीं। वर्षों बाद गुसांईं ने ऐसी रोटियां देखी थीं, जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडौल रोटियों से एकदम भिन्न थीं। आटे की लोई बनाते समय लछमा के छोटे-छोटे हाथ बडी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कडे ज़ब कभी आपस में टकरा जाते,तो खन्-खन् का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकरानेवाली काठ की चिडियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसांईं ने आज पहली बार अनुभव किया।
किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बडी देर तक खाली बर्तन-डिब्बों को उठाता-रखता रहा।
वह लौटकर आया, तो लछमा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी।
गुसांईं ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसांईं को देखे जा रहा था। लछमा ने आग्रह के स्वर में कहा, ”चाय के साथ खानी हों, तो खा लो। फिर ठंडी हो जाएंगी।”
”मैं तो अपने टैम से ही खाऊंगा। यह तो बच्चे के लिए ..” स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो।
”न-न, जी! वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है। मैं रोटियां बनाकर रख आई थी,” अत्यंत संकोच के साथ लछमा ने आपत्ति प्रकट कर दी।
”अैंऽऽ, यों ही कहती है। कहां रखी थीं रोटियां घर में?” बच्चे ने रूआंसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बतें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड ग़या था।
”चुप!” आंखें तरेरकर लछमा ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी, इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा।
”बच्चा है, भूख लग आई होगी, डांटने से क्या फायदा?” गुसांईं ने बच्चे का पक्ष लेकर दो रोटियां उसकी ओर बढा दीं। परंतु मां की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर, कभी मां की ओर देख लेता था।
गुसांईं के बार-बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा, तो लछमा ने उसे झिडक़ दिया, ”मर! अब ले क्यों नहीं लेता? जहां जाएगा, वहीं अपने लच्छन दिखाएगा!”
इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दें, गुसांईं ने रोटियों के ऊपर एक टुकडा गुड क़ा रखकर बच्चे के हाथों में दिया। भरी-भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा, और गुसांईं कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा।
इस छोटे-से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव-सा आ गया था, जिसे गुसांईं और लछमा दोनों ही अनुभव कर रहे थे।
स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते-खाते गुसांईं ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कराकर कहा, ”लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है।”
लछमा ने करूण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसांईं हो-होकर खोखली हंसी हंस रहा था।
”कुछ साग-सब्जी होती, तो बेचारा एक-आधी रोटी और खा लेता।” गुसांईं ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की।
”ऐसी ही खाने-पीनेवाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पडता? दो दिन से घर में तेल-नमक नहीं है। आज थोडे पैसे मिले हैं,आज ले जाऊंगी कुछ सौदा।”
हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसांईं ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, ”लछमा!”
लछमा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसांईं ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढाते हुए कहा, ”ले, काम चलाने के लिए यह रख ले,मेरे पास अभी और है। परसों दफ्तर से मनीआर्डर आया था।”
”नहीं-नहीं, जी! काम तो चल ही रहा है। मैं इस मतलब से थोडे क़ह रही थी। यह तो बात चली थी, तो मैंने कहा,” कहकर लछमा ने सहायता लेने से इन्कार कर दिया
गुसांईं को लछमा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में वह बोला, ”दुःख-तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया, तो बेकार है! स्साला! कितना कमाया, कितना फूंका हमने इस जिंदगी में। है कोई हिसाब! पर क्या फायदा! किसी के काम नहीं आया। इसमें अहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है स्साला! किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी!”
परन्तु गुसांईं के इस तर्क के बावजूद भी लछमा अडी रही, बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, ”गंगनाथ दाहिने रहें, तो भले-बुरे दिन निभ ही जाते हैं, जी! पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो, कम हो जाय। अपने-पराये प्रेम से हंस-बोल दें, तो वह बहुत है दिन काटने के लिए।”
गुसांईं ने गौर से लछमा के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहां कोई चिह्न शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था।
रूपया लेने के लिए लछमा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ। पर गहरे असंतोष के कारण बुझा-बुझा-सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लछमा उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी-जल्दी अपने नीजी आटे के टीन से दो-ढाई सेर के करीब आटा निकालकर लछमा के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाडता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हांक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोडना चाहता था।
बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लछमा के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठककर खडा हो गया, मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही हो। अटक-अटककर वह बोला, ”लछमा ..।”
लछमा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसांईं को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है,इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुसांईं ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, ”कभी चार पैसे जुड ज़ाएं, तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल-चूक की माफी मांग लेना। पूत-परिवारवालों को देवी-देवता के कोप से बचा रहना चाहिए।” लछमा की बात सुनने के लिए वह नहीं रूका।
पानी तोडनेवाले खेतिहार से झगडा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामनेवाले पहाड क़ी पगडंडी पर सर पर आटा लिए लछमा अपने बच्चे के साथ धीरे-धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाडी क़े मोड तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा।
घट के अंदर काठ की चिडियां अब भी किट-किट आवाज कर रही थीं, चक्की का पाट खिस्सर-खिस्सर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी, और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान, निस्तब्ध!