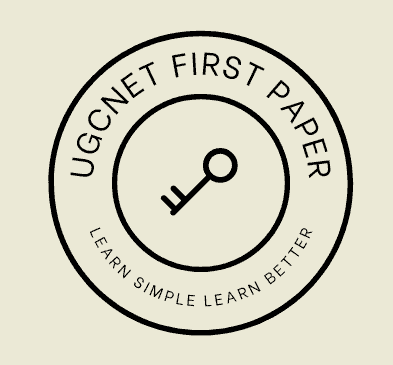‘अशोक के फूल’ केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है; और इस अध्याय का अनंगलेख पढ़नेवाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारीप्रसाद द्विवेदी। पहली बार उन्हें ही यह अनुभव हुआ कि ‘एक-एक फूल, एक-एक पशु, एक-एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति-परंपरा है। आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है?’ अब तो खैर हिंदी में फूलों पर ‘ललित’ लेख लिखनेवाले कई लेखक निकल आए हैं, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं कि ‘अशोक के फूल’ आज भी अपनी जगह है। कालिदास के प्रेमी पंडितों को पहली बार इस रहस्योद्घाटन से अवश्य ही धक्का लगा होगा कि जिस कवि को वे अब तक अपनी आर्य संस्कृति का महान गायक समझते आ रहे थे वह गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्येतर जातियों के विश्वासों और सौंदर्य-कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी है। वैसे तो भारत को ‘महामानव सागर’ कहनेवाले रवींद्रनाथ ठाकुर एक अरसे से यह बतलाते आ रहे थे कि जिसे हम हिंदू रीतिनीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण है, किंतु यही संदेश ‘अशोक के फूल’ के माध्यम से आया तो उसकी चोट कुछ और ही थी। क्या इसलिए कि यह मनोजन्मा कन्दर्प के धनुष से छूटा है? फूल की मार कितनी गहरी हो सकती है इसका एहसास कराने के लिए ‘अशोक के फूल’ के ये दो वाक्य काफी हैं: ‘देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। सबकुछ में मिलावट है, सबकुछ अविशुद्ध है।’ और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही ‘अशोक के फूल’ लिखा गया है, प्रकृति-वर्णन करने के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदीजी के शुद्ध पुष्प-प्रेम का प्रमाण नहीं, बल्कि संस्कृति-दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है।
अब तो भारत की ‘सामाजिक संस्कृति’ की दिन-रात माला जपनेवाले बहुतेरे हो गए हैं। दिनकरजी ने तो ‘संस्कृति के चार अध्याय’ नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला; किंतु जैसा कि अज्ञेय ने लिखा है: ‘काव्य की पड़ताल में तो दिनकर ‘शुद्ध’ काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह ‘मिश्र संस्कृति’ पर ही खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उसकी संग्राहकता को नहीं। संस्कृति का चिंतन करनेवाले किसी भी विद्वान के सामने यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि संस्कृतियाँ प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया मिश्रण की नहीं है। संस्कार नाम ही इस बात को स्पष्ट कर देता है। यह मानना कठिन है कि संस्कृति की यह परिभाषा दिनकर की जानी हुई नहीं थी; उनका जीवन भी कहीं उस मिश्रता को स्वीकार करता नहीं जान पड़ता था, जिसकी वकालत उन्होंने की। तब क्या यह संदेह संगत नहीं कि उनकी अवधारणा एक वकालत ही थी, दृष्टि का उन्मेष नहींᣛ? और अगर वकालत ही थी तो उनका मुवक्किल क्या समकालीन राजनीति का एक पक्ष ही नहीं था, जिसके सांस्कृतिक कर्णधार स्वयं भी मिश्रता का सिद्धांत नहीं मानते थे, लेकिन अपनी स्थिति दृढ़तर बनाने के लिए उसे अपना रहे थे?’ (स्मृतिलेखा, पृ.118)
इस ‘मिश्र संस्कृति’ की राजनीति से द्विवेदीजी कितने अलग थे, इसका प्रमाण यह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब से राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित नीति के रूप में ‘सामाजिक संस्कृति’ का बोलबाला हुआ, द्विवेदीजी ने इस विषय पर लिखना लगभग बंद कर दिया। स्पष्ट है कि वे ‘मिश्र संस्कृति’ के वकील न थे और न एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास से तथ्य बटोरने ही गए थे। उन्होंने तो उस अनुभूति को वाणी दी जो अपने अतीत के साहित्य को पढ़ते और कलाकृतियों को देखते समय अंतर्तम में उठी थी; और इस बात से तो संभवत: अज्ञेय भी इनकार न करेंगे कि द्विवेदीजी के लिए वह एक अमूर्त बौद्धिक ‘अवधारणा’ नहीं थी, बल्कि ‘दृष्टि का उन्मेष’ था। इसीलिए जब द्विवेदीजी कहते हैं कि ‘सबकुछ अविशुद्ध है’, तो तुरंत बाद यह भी जोड़ते हैं कि ‘शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा।’ वह गंगा की अबाधित-अनाहत धारा के समान सबकुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है!’
इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि अज्ञेय जहाँ संस्कृति की केवल ‘संग्राहकता’ की हिमायत करते हैं, वहाँ द्विवेदीजी ‘त्याग’ का जिक्र करना नहीं भूलते। ‘अशोक के फूल’ में ही, में ही, उसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक द्रष्टा की तरह ‘मानवजाति की दुर्दम-निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ’ देखते हुए वे कहते हैं: ‘मनुष्य की जीवनी-शक्त्िा बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती-बहाती यह जीवनधारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है।’
इसलिए द्विवेदीजी के सामने योजनाबद्ध रूप से एक ‘मिश्र संस्कृति’ तैयार करने की समस्या नहीं है, समस्या यह है कि ‘आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है’ उसे किस प्रकार ध्वस्त किया जायᣛ?
इस दृष्टि से यदि दिनकर का ‘मिश्र संस्कृति’ की एक राजनीति है जो अज्ञेय की संस्कार-धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुषंग से बच नहीं जाती। जब वे कहते हैं कि संस्कृतियाँ प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती है तो उसमें एक ‘मूल संस्कृति’ का अस्तित्व पहले ही से स्वीकार कर लिया गया है जो किसी प्रभाव से पहले ‘विशुद्ध’ है। आकस्मिक नहीं है कि अज्ञेय द्वारा स्थापित वत्सल निधि की ‘हीरानंद शास्त्री स्मारक व्याख्यानमाला’ के प्रथम आयोजन में प्रकाशित ‘भारतीय परंपरा के मूल स्वर’ में डॉ.गोविंदचंद्र पांडे भी लगभग ऐसे ही शब्दों में ‘सामासिक संस्कृति’ का विरोध करते हैं। डॉ.पांडे यह स्वीकार करते हैं कि ‘विज्ञान, प्रविधि और भौतिक उपादानों के स्तर पर नाना समाजों में आदान-प्रदान अनायास और चिरपरिचित है; (और) इन साधनों का उपयोग समाज को प्रभावित करता है।’ किंतु इसके साथ ही वे यह भी मानते हैं कि ‘अतर्क्य भावों, अनुभूतियों और आध्यात्मिक उपलब्धियों के स्तर पर संस्कृतियों का वास्तविक मिलन अत्यंत कठिन होता है।’ (पृ.18-19) कुल मिलाकर ‘इस विमर्श का निष्कर्ष यह है कि भारतीय संस्कृति की तथाकथित सामासिकता वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में ही लागू होती है और इस क्षेत्र में वह भारत की कोई विशेषता नहीं है।’ (पृ.20)
सवाल यह है कि ‘सभ्यता’ और ‘संस्कृति’ की जिन दो यूरोपीय अवधारणाओं को डॉ.पांडे ने भारत की संस्कृति के विवेचन के लिए अपनाया है, उनका संबंध ‘सभ्यता’ से है या संस्कृति से? आदान-प्रदान यदि सभ्यता के ही क्षेत्र में भी आदान-प्रदान होता है। फिर भी जिस तरह ‘राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित सामासिक संस्कृति’ का विरोध डॉ.पांडे ने किया है उसे किसी अन्य पक्ष की राजनीति की वकालत न मानना अज्ञेय के लिए भी कठिन होगा। तर्क वही है जिसका इस्तेमाल उन्होंने दिनकर के संदर्भ में किया है। यदि दिनकर की ‘सामाजिक संस्कृति’ का संबंध राजनीति के एक पक्ष से है तो स्वयं अज्ञेय और गोविंदचंद्र पांडे की ‘शुद्ध संस्कृति’ का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है। शुद्ध होने से ही वह राजनीति से मुक्त नहीं हो जाती।
द्विवेदीजी की दृष्टि में संस्कृति का यह आग्रह भी एक प्रकार का ‘मोह’ है जो बाधा उपस्थित करता है। संस्कृति में निहित जिस ‘संस्कार’ की ओर अज्ञेय ने संकेत किया है, उसकी अर्थवत्ता से द्विवेदीजी अपरिचित हैं, यह तो स्वयं अज्ञेय भी न स्वीकार करेंगे; फिर भी उन्हें यह देखकर आश्चर्य न होना चाहिए कि उन्होंने अक्सर इस ‘संस्कार’ को भी बाधा माना है। लखनऊ विश्वविद्यालय के ‘साहित्य का मर्म’ (1948) शीर्षक व्याख्यानों में उनका जोर इसी बात पर है कि विवेक के परिष्करण के लिए किए गए संस्कार भी काल पाकर किसी नए सृजन के ग्रहण के लिए बाधा बन जाते हैं। कहते हैं: ‘संस्कार’ शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा है। संस्कार शब्द अच्छे अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, परंतु मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धापरायण होता है और प्राचीनकाल से संबंद्ध होने के कारण कुछ ऐसी धारणाओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगता है जो जब शुरू हुई होंगी तो निश्चय ही उपयोगी रही होगी परंतु बाद में उनकी उपयोगिता घिस गई और वे रुढ़ि मात्र रह गईं। ऐसे संस्कार सब समय वृहत्तर मानव पट भूमिका पर खरे नहीं उतरते।’ इन कालगत संस्कारों की चर्चा करने के बाद वे उन देशगत और जातिगत संस्कारों की ओर भी संकेत करते हैं जो ‘अन्य देश और अन्य जाति के विश्वासों पर आधारित साहित्य को समझने में बाधक होते हैं।’ प्रसंग यद्यपि साहित्य का है फिर भी संस्कार की यह भूमिका संस्कृति के क्षेत्र में भी स्वीकार की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कार के उल्लेख मात्र से संस्कृति के क्षेत्र में दृष्टिगत होनेवाली संकीर्णता का परिहार नहीं हो जाता। ‘संस्कार’ की प्रक्रिया अंतत: संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धीकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणति वर्जनशीलता में होती है – यह वही ‘वर्जनशीलता’ है जिस पर भारतीय संस्कृति के बहुत से हिमायतियों को अभिमान है। ‘हमारे यहाँ’ वाला ब्रम्हास्त्र इस वर्जनशील अहंकार की उपज है, जिसका मुकाबला द्विवेदीजी को अक्सर करना पड़ता था।
बहुत क्लेश होने पर ही ‘हिंदी साहित्य की भूमिका’ के उपसंहार में उन्होंने लिखा : ‘आए दिन श्रद्धापरायण आलोचक यूरोपियन मतवादों को धकिया देने के लिए भारतीय आचार्य-विशेष का मत उद्धृत करते हैं और आत्मगौरव के उल्लास से घोषित कर देते हैं कि ‘हमारे यहाँ’ यह बात इस रूप में मानी या कही गई है। मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार्य उपस्थापित कर सकता है, मानो भारतवर्ष के हजारों वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य एक ही कोई आचार्य हुआ है, और दूसरे या तो हैं ही नहीं, या हैं भी तो एक ही बात मान बैठे हैं। यह रास्ता गलत है। किसी भी मत के विषय में भारतीय मनीषा ने गड्डलिका-प्रवाह की नीति का अनुसरण नहीं किया है। प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं।’ (पृ. 129)
पंडितों की समझ का यह इकहरापन द्विवेदीजी की दृष्टि में एक बड़ी बाधा है। इस संकीर्ण इकहरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुन: सृजन किया। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आर्येतर जातियों के अवदान की उल्लसित चर्चा का कारण यही है। यदि इस प्रयास में कहीं आर्य-श्रेष्ठता के अहंकार को ठेस लगती है तो द्विवेदीजी इस बात से चिंतित नहीं दिखते। वस्तुत: यह दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास है जिसका प्रयोजन मुख्यत: पंडितों की इकहरी परंपरा की संकीर्णता का निदर्शन है।
प्रसंगवश द्विवेदीजी के इस प्रयास की एक परंपरा हिंदी में पहले से दिखाई पड़ती है। एक दशक पहले जयशंकर प्रसाद को भी ऐसे ही भारत-व्याकुल लोगों से पाला पड़ा था, जिनके जवाब में कवि को ‘काव्य और कला’ तथा ‘रहस्यवाद’ आदि निबंध लिखने पड़े थे। नए काव्य-प्रयोगों की ‘प्रतिक्रिया के रूप में’ उन्हें भी ‘भारतीयता की दुहाई’ सुनाई पड़ी थी। ‘काव्य और कला’ निबंध का आरंभ ही इस प्रकार होता है कि ‘भारतीय वाड़्मय की’ ‘सुरुचि-संबंधी विचित्रताओं को बिना देखे ही अत्यंत शीघ्रता में आजकल अमुक वस्तु अभारतीय है अथवा भारतीय संस्कृति की सुरुचि के विरुद्ध है, कह देने की परिपाटी चल पड़ी है।’ प्रसाद ने भी यह लक्षित किया था कि ‘ये सब भावनाएँ साधारणत: हमारे विचारों की संकीर्णता से और प्रधानत: अपनी स्वरूप-विस्मृति से उत्पन्न हैं।’ यह संकीर्णता और स्वरूप-विस्मृति अपनी परंपरा के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन से ही दूर हो सकती है। किंतु प्रसाद ने अनुभव किया कि ‘इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन होने की संभावना जैसी पाश्चात्य साहित्य में है, वैसी भारतीय साहित्य में नहीं। उनके पास अरस्तू से लेकर वर्तमान काल तक ही सौंदर्यानुभूति-सबंधिनी विचारधारा का क्रमविकास और प्रतीकों के साथ-साथ उनका इतिहास तो है ही, सबसे अच्छा साधन उनकी अविछिन्न सांस्कृतिक एकता भी है। हमारी भाषा के साहित्य में वैसा सामंजस्य नहीं है। बीच-बीच में इतने अभाव या अंधकार-काल हैं कि उनमें कितनी ही विरुद्ध संस्कृतियाँ भारतीय रंग स्थल पर अवतीर्ण और लोप होती दिखाई देती हैं; जिन्होंने हमारी सौंदर्यानुभूति के प्रतीकों को अनेक प्रकर से विकृत करने का ही उद्योग किया है।’
अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार-काल के बावजूद प्रसाद ने ‘रहस्यवाद’ शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुननिर्मित करने का प्रयास किया। इस परंपरा का आरंभ भी ऋग्वेद से ही होता है, किंतु यह आर्यजन की वह परंपरा है जिसके प्रतिनिधि इंद्र हैं और जिसमें ‘काम’ की पूर्ण स्वीकृति है। वह वरुण के अधिनायकत्व में विकसित होनेवाली असुर परंपरा से सर्वथा भिन्न है जो विधि-विधान और विवेक को विशेष महत्व देती थी। प्रसाद ने इन दोनों परस्पर-विरोधी परंपराओं के विकास की मनोरंजक रूपरेखा प्रस्तुत की है और कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी दृष्टि में जीवन में ‘काम’ को पूर्णत: स्वीकार करके चलनेवाली आनंदवादी परंपरा ही मुख्य है अथच काम्य भी।
किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण यह कहना कठिन है कि द्विवेदीजी प्रसाद द्वारा निरूपित आनंदवादी परंपरा से किस हद तक परिचित थे, किंतु तत्त्वत: यह वही परंपरा है जिसका श्रेय वे गंधर्व, नाग, द्रविड़ आदि आर्येतर जातियों को देते हैं। ‘विचार और वितर्क’ (1945) में संकलित अपने एक आरंभिक निबंध ‘हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध’ में लिखा है कि ‘सबसे अधिक आर्येतर-संश्रव साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ है।अजंता के चित्रित, साँची, भरहुत आदि में उत्कीर्ण चित्र और मूर्तियाँ आर्येतर सभ्यता की समृद्धि के परिचायक हैं। महाभारत और कालिदास के काव्यों की तुलना करने में जान पड़ेगा कि दोनों दो चीजे़ं हैं। एक में तेज है, दृप्तता है और अभिव्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में लालित्य है, माधुर्य है और व्यंजना की छटा है। महाभारत में आर्य उपादान अधिक है, कालिदास के काव्यों में आर्येतर। जिन लोगों ने भारतीय शिल्पशास्त्र का अनुशीलन किया है, वे जानते हैं कि भारतीय शिल्प में कितने आर्येतर उपादान हैं और काव्यों तथा नाटकों में उनका कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ा है। पता चला है कि साँची, भरहुत आदि के चित्रकार यक्षों और नागों की पूजा करनेवाली एक सौंदर्य-प्रिय जाति थी, जो संभवत: उत्तर भारत से लेकर असम तक फैली हुई थी। बहुत सी ऐसी बातें कालिदास आदि कवियों ने इन सौंदर्य-प्रेमी जातियों से ग्रहण कीं, जिनका पता आर्यों को न था। कामदेव और अप्सराएँ उनकी देव-देवियाँ हैं, सुंदरियों के पदाघात से अशोक का पुष्पित होना उनके घर की चीज है, अलकापुरी उनका स्वर्ग है – इस प्रकार की अन्य अनेक बातें उनसे और उन्हीं की तरह अन्यान्य आर्येतर जातियों से महाकवि ने ली हैं।’ इसी क्रम में आगे भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के बारे में भी, उसके आर्यों की विद्या न माननेवाले मत का जिक्र करते हुए कहते हैं: ‘शुरू में एक कथा में बताया गया है कि ब्रम्हा ने नाट्यवेद नामक पाँचवे वेद की सृष्टि की थी। अगर आर्यों के वेदों से इसका कुछ भी संबंध होता तो पंडितों का अनुमान है, इस कथा की जरूरत न हुई होती। वास्तव में भारतीय नाटक पहले केवल अभिनय के रूप में ही दिखाए जाते थे। उनमें भाषा का प्रयोग करना आर्य संशोधन का परिवर्धन है।’ (प्रथम संस्करण, पृ.186-87) आर्येतर अवदान की इस सूची में यदि ‘भक्ती द्राविड़ ऊपजी’ और आभीरों के आराध्यवदेव बालकृष्ण तथा देवी राधा को जोड़ लें तो हमारी परंपरा में सुंदर माना जानेवाला ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आर्येतर न हो! एक भक्तिकाव्य को छोड़कर प्रसाद और हजारीप्रसाद द्विवेदी में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि क्या-क्या सुंदर है? अंतर केवल यह है कि प्रसाद जिसे आर्यों के एक समुदाय की परंपरा कहते हैं, हजारीप्रसाद द्विवेदी उसे ही विभिन्न आर्येतर जातियों का अवदान मानते हैं। फिर भी एक बात में उभयत्र समानता है कि हमारी परंपरा में जो भी सुंदर है वह आर्य नाम से प्रचारित मिथक से भिन्न है। इस मिथकीय आर्यसे इतनी चिढ़ इसलिए है कि इसके ध्वजाधारियों को ‘सुंदर’ से परहेज है। जैसा कि प्रसाद ने ‘रहस्यवाद’ शीर्षक निबंध में स्पष्ट लिखा है: ‘आनंद पथ को उनके कल्पित भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढाँचा ढीला पड़ जाता है। इसलिए वे इस बात को स्वीकार करने में डरते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है, ज्ञान से वा अज्ञान से मनुष्य उसी की खोज में लगा है। आदर्शवाद ने विवेक के नाम पर आनंद और उसके पथ के लिए जो जनरव फैलाया है, वही उसे अपनी वस्तु कहकर स्वीकार करने में बाधक है।’ इसलिए नैतिकतावादियों को प्रत्युत्तर देने के लिए प्रसाद ने यदि ‘सुंदर’ की परंपरा को अपनी ही परंपरा के अंदर आर्येतर तत्त्वों के अभिन्न मिश्रण के रूप में विवेचित किया। एक की परंपरा और दूसरे की प्रति-परंपरा दो दिशाओं से चलकर एक ही बिंदु पर मिलती है – थोथे नैतिकतावाद के विरुद्ध ‘सुंदर’ की प्रतिष्ठा! ‘सुंदर’ को ही लेकर यह सारा विवाद इसलिए है कि जैसा कि प्रसाद ने कहा है : ‘संस्कृति सौंदर्यबोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है।’
यह आकस्मिक नहीं है कि भारतीय संस्कृति के नाम पर नैतिकता की ध्वजा फहरानेवाले प्रकृति के सौंदर्य को तो किसी प्रकार सह लेते हैं, पर नारी-सौंदर्य के सामने आँखे चुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए शुक्लजी के लोकमंगल में प्रकृति के सौंदर्य के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे स्वयं विद्यापति के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे स्वयं विद्यापति और सूर जैसे भक्त कवियों का नारी-सौंदर्य भी ग्राह्य नहीं है। आनंद और माधुर्य को लोकमंगल की सिद्धावस्था का गौरवपूर्ण पद देकर उन्होंने साधनावस्था का मार्ग अपनी ओर से सर्वथा निष्कटंक कर लिया, क्योंकि साधना के मार्ग में माधुर्य से बाधा पहुँचने की आशंका है।
संभवत: ऐसे ही पूर्वग्रह का प्रत्याख्यान करने के लिए द्विवेदीजी ने अपनी साहित्य-साधना के आरंभिक सोपान पर ही ‘हिंदी साहित्य की भूमिका’ के साथ ही ‘प्राचीन भारत का कला-विलास’ (1940) नामक पुस्तक लिखी जो आगे चलकर परिवर्धित रूप में ‘प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद’ नाम से छपी। प्राचीन भारत में प्रचलित कलाओं के लगभग सौ संदर्भों का तथ्यात्मक विवरण उपस्थित करने से पहले ‘कलात्मक विनोद’ में द्विवेदीजी ने आरंभ में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझा कि ‘विलासिता और कलात्मक विलासिता एक ही वस्तु नहीं है। थोथी विलासिता में केवल भूख रहती है – नंगी बुभुक्षा पर कलात्मक विलासितासंयम चाहती है, शालीनता चाहती है, विवेक चाहती है। सो,कलात्मक विलास किसी जाति के भाग्य में सदा-सर्वदा नहीं जुटता। उसके लिए ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, त्याग और भोग का सामर्थ्य चाहिए और सबसे बढ़कर ऐसा पौरुष चाहिए जो सौंदर्य और सुकुमारता की रक्षा कर सके। परंतु इनता ही काफी नहीं है। उस जाति में जीवन के प्रति ऐसी एक दृष्टि सुप्रतिष्ठित होनी चाहिए जिससे वह पशुसुलभ इंद्रिय-वृत्ति को और बाह्य पदार्थों को ही समस्त सुखों का कारण न समझने में प्रवीण हो चुकी हो, उस जाति की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा बड़ी और उदार होनी चाहिए और उसमें एक ऐसा कौलीन्य गर्व होना चाहिए जो आत्म-मर्यादा को समस्त दुनिया की सुख-सुविधाओं से श्रेष्ठ समझता हो, और जीवन के किसी भी क्षेत्र में असुंदर को बर्दाश्त न कर सकता हो। जो जाति सुंदर की रक्षा और सम्मान करता नहीं जानती वह विलासी भले ही हो ले, पर कलात्मक विलास उसके भाग्य में नहीं बदा होता।’
संक्षेप में यह उस सौंदर्यबोध की ‘संस्कृति’ है, जिसका अत्यंत संवेदनशील औश्र सूक्ष्मविवरण ‘कलात्मक विनोद’ के बाद के पृष्ठों में मिलता है, या फिर ‘बाणभट्ट की आत्मकथा’, ‘चारु चंद्रलेख’, ‘पुनर्नवा’ और ‘अनामदास का पोथा’ जैसी सर्जनात्मक कृतियों के उन प्रसंगों में जहाँ नारी-सौंदर्य अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट होता है तथा नृत्य-कला के प्रदर्शन के अवसर अक्सर उपस्थित होते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदीजी के इस सौंदर्यबोध में सर्वथा शास्त्रीय प्रत्यभिज्ञान ही नहीं, बल्कि उसमें एक सजग ऐंद्रिय संवेदन की प्रत्यग्रता भी है। रूप, शोभा, सुषमा, सौभाग्य, चारुता, लालित्य, लावण्य आदि का ऐसा सूक्ष्म परिज्ञान और संवेदन हिंदी में दुर्लभ ही है।
इस सौंदर्यबोध को सामंती संस्कृति का पर्याय समझ लिए जाने का भ्रम न हो इसलिए ‘मेघदूत-एक पुरानी कहानी’, (1957) से पूर्व मेघ के ‘पुष्पलावी मुखानम्’ वाले 26वें छंद पर द्विवेदीजी की व्याख्या का एक अंश प्रस्तुत है : ‘जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती, और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है। सात्विक सौंदर्य वहाँ है, जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। पसीना बड़ा पावक तत्व है मित्र, जहाँ इसकी धारा रुद्ध हो जाती है वहाँ कलुष और विकार जमकर खड़े हो जाते हैं। विदिशा के प्रच्छन्न विलासियों में यह पावनकारी तत्व नहीं है। उनके चेहरों पर सात्विक तेज और उल्लसित करनेवाली दीप्ति नहीं रह गई है। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि विश्राम करके आगे बढ़ना; क्योंकि प्रात:काल निचली पहाड़ी के इर्दगिर्द तुमको मनुष्य की सात्विक शोभा दिखाई देगी। वहाँ सवेरे सूर्योदय के साथ ही साथ तुम श्रम-जल-स्नात नारियों की दिव्य शोभा देख सकोगे। नागरिक लोगों के आनंद और विलास के लिए कृषकों ने फूलों के अनेक बगीचे लगा रखे हैं। प्रात:काल कृषक-वधुएँ फूल चुनने के लिए इन पुष्पोद्यानों में आ जाती हैं, उस प्रदेश में इन्हें ‘पुष्पलावी’ कहते हैं। ‘पुष्पलावी’ अर्थात् फूल चुननेवाली। ये पुष्पलावियाँ घर का कामकाज समाप्त करके उद्यानों में आ जाती हैं और मध्यान्ह तक फूल चुनती रहती हैं। सूर्य के ताप से इनका मुखमंडल ग्लान हो उठता है, गंडस्थल से पसीने की धारा बह चलती है और इस स्वेदधारा के निरंतर संस्पर्श से उनके कानों के आभरण रूप में विराजमान नीलकमल मलिन हो उठते हैं। दिन-भर की तपस्या के बाद वे इतना कमा लेती हैं कि किसी प्रकार उनकी जीवन-यात्रा चल सके। परंतु तुमको यहीं सात्विक सौंदर्य के दर्शन होंगे। उनके दीप्त मुखमंडल पर शालीनता का तेज देखोगे; उनकी भ्रू-भंग-विलास से अपरिचित आँखों में सच्ची लज्जा के भार का दर्शन कर पाओगे और उनके उत्फुल्ल अधरों पर स्थिर भाव से विराजमान पवित्र स्मित-रेखा को देखकर तुम समझ सकोगे कि ‘शुचि-स्मिता’ किसे कहते हैं। इस पवित्र सौंदर्य को देखकर तुम निचली पहाड़ी की उद्दाम और उन्मत्त विलास-लीला को भूल जाओगे। वहाँत तुम संचय का विकार देखोगे और यहाँ आत्मदान का सहज रूप।’ (प्रथम संस्करण, पृ. 45-46)
पुष्पलावियों का यह श्रम-जल-स्नात सौंदर्य कालिदास का नहीं, द्विवेदीजी के ‘कालिदास’ का सौंदर्य है – क्लासिकी परंपरा से फूटती हुई आधुनिकता! संस्कृति को भी संस्कार देनेवाली यह एक और परंपरा है जो अनजाने ही निराला की ‘श्याम तन भर बँधा यौवन’ वाली ‘वह तोड़ती पत्थर’ से जुड़ जाती है।
इसलिए जो लोग द्विवेदीजी के सौंदर्य-संस्कार को रवींद्रनाथ के शांतिनिकेतन की देन बतलाते हैं वे सिर्फ आधी बात कहते हैं। शांतिनिकेतन में चारों ओर संगीत और कला का जो वातावरण था उसने निश्चय ही द्विवेदीजी के सुप्त सौंदर्यबोध को जागृत किया था। स्वयं द्विवेदीजी ने भी शांतिनिकेतन के संस्मरणों में आश्रम के उस वातावरण की चर्चा की है जिसमें संगीत जीवन का अविच्छेद्य अंग बन गया था और छोटे-से-छोटे बच्चों में भी सौंदर्य-निर्माण की सहज प्रेरणा काम कर रही थी। फिर भी उनके अपने सौंदर्यप्रेम का एक बहुत बड़ा स्त्रोत अपना लोक-संस्कार था। यही वजह है कि जीवन के संदर्भ में जब भी सौंदर्य-सृष्टि की बात उठती थी तो वे उसे सामान्य जन-जीवन में उतारने की कल्पना करते थे। इस दृष्टि से ‘विचार-प्रवाह’ (1959) में संकलित ‘जनता का अंत: स्पंदन शीर्षक लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
निबंध इस चिंता से आरंभ होता है : ‘कुछ ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि इस वंचित जनता के भीतर रसग्राहिका संवेदना उत्पन्न हो, वे भी ‘सुंदर’ का सम्मान करना सीखें, ‘सुंदर’ ढंग से जीवन बिताना सीखें, ‘सुंदर’ को पहचानना सीखें।’ एक सत्ख्यातिवादी की तरह द्विवेदीजी कहते हैं कि जनता के अंत:करण में अगर सौंदर्य के प्रति सम्मान का भाव नहीं है, तो जनता कभी भी सौंदर्य-प्रेमी नहीं बनाई जा सकती। किंतु उनका विश्वास है कि जनता के भीतर वह वस्तु स्तब्ध पड़ी हुई है। उपयुक्त उद्दीपक के अभाव में वह स्पंदित नहीं हो रही है। इस उद्दीपक वस्तु को समाज में प्रतिष्ठित करना वांछनीय है। जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति से वे बेखबर नहीं हैं। वे अनुभव करते हैं कि जिस जनता को पेट-भर अन्न नहीं मिलता, वह सौंदर्य का सम्मान नहीं कर सकती। नींव के बिना इमारत नहीं उठ सकती। ‘भूखे भजन न होहिं गोपाला।’ किंतु इसके साथ ही यह भी सच है कि ‘जो जाति ‘सुंदर’ का सम्मान नहीं कर सकती वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज है। वह छोटी-छोटी बातों के लिए झगड़ती है, मरती है और लुप्त हो जाती है।’
स्पष्टत: यह दृष्टि उस विचारधारा से नितांत भिन्न है जो जनता को तात्कालिक आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष में उतारने की विश्वासी है क्योंकि वहाँ यह समझ निहित है कि जनता के बोध का स्तर इतना ही नीचा है। जो जनता के ‘अंत:स्पंदन’ से अपरिचित हैं वे सारी शक्ति फौरी लड़ाइयों में ही क्षय करते हैं। कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है तो इसलिए कि वह सिर्फ जीना नहीं चाहती, बल्कि ‘सुंदर’ ढंग से जीना चाहती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज के अनेक राजनीतिक संगठन और आंदोलन सिर्फ इसलिए असफल हो रहे हैं कि उनके सामने जीवन का यह बड़ा उद्देश्य नहीं है और वे ‘सुंदर’ को एक अतिरिक्त या फालतू चीज समझते हैं।
द्विवेदीजी भी ‘सौंदर्य’ को ‘अतिरिक्त’ मानते हैं किंतु उनके ‘अतिरिक्त’ का अर्थ वह है जो आनंदवर्धनकृत ‘लावण्य’ की परिभाषा में है। वह किसी वस्तु के प्रसिद्ध अवयवों में से कोई भी नहीं है, उनसे अतिरिक्त है और फिर भी उन अवयवों को छोड़कर नहीं रह सकता। सो, सौंदर्य रूप नहीं है, लेकिन रूप को छोड़कर रह भी नहीं सकता। इस शास्त्रीय परिभाषा से द्विवेदीजी जीवन के लिए जो निष्कर्ष निकालते हैं, वह द्रष्टव्य है। कहते हैं : ‘जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी न करने को भलापन समझते हैं। यह गलत धारणा है। सुंदर जीवन क्रियाशील होता है; क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का ‘सौंदर्य’ टिक नही सकता।’ द्विवेदीजी के अनुसार इस भाव से चालित जन-समाज अंतत: ‘राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों पर कब्जा करने के प्रयास’ से कम पर संतुष्ट नहीं हो सकता क्योंकि ‘ समाज व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना एकदम असंभव हो गया है।’
किंतु उन संकीर्णतावादी क्रांतिकारियों से द्विवेदीजी सहमत नहीं हैं जो मनुष्य के भविष्य को सुखी बनाने के नाम पर आज उसके सौंदर्य-प्रेम को किसी न किसी बहाने कुचल देना चाहते हैं। अंतिम दिनों में लिखित ‘परंपरा और आधुनिकता’ शीर्षक लेख में वे कहते हैं : ‘जो मनुष्य को उसकी सहज वासनाओं और अद्भुत कल्पनाओं के राज्य से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है वह ठूँठ तर्कपरायण कठमुल्ला हो सकता है, आधुनिक बिल्कुल नहीं। वह मनुष्य को समूचे परिवेश से विच्छिन्न करके हाड़-मांस का यंत्र बनाना चाहता है। यह न तो संभव है, न वांछनीय।’ (ग्रंथावली 9/363)
इसलिए द्विवेदीजी मनुष्य की ‘समस्त रचयित्री आनंदिनी वृत्ति’ का विकास आवश्यक समझते हैं, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्मविधान और साहित्य के माध्यम से उसी वृत्ति को अभिव्यक्ति मिलती है।
यह आकस्मिक नहीं है कि अंतिम दिनों में वे ‘सौंदर्यशास्त्र’ पर ‘लालित्य-मीमांसा’ नाम से एक पूरी पुस्तक लिख रहे थे। अपने प्रिय कवि कालिदास पर ‘कालिदास की लालित्य-योजना’ नामक पुस्तक पूरी करके वे स्वयं लालित्यशास्त्र पर ही व्यवस्थित और सांगोपांग विचार करना चाहते थे। उनके जीवन की सुदीर्घ सौंदर्य-चिंता और सौंदर्य-साधना की यह स्वाभाविक परिणति थी। दुर्भाग्य से उस पुस्तक के केवल पाँच ही निबंध पूरे हो पाए, पर उनसे भी उनकी व्यापक और मौलिक सौंदर्य -चिंता का कुछ आभास मिल ही जाता है। उन्हें इस तथ्य का एहसास है कि ‘भारतवर्ष में इस प्रकार के किसी अलग शास्त्र की कल्पना नहीं की गई है; परंतु काव्य, शिल्प, चित्र, मूर्ति, संगीत, नाटक आदि की आलोचना के प्रसंग में और विविध आगमों में ‘चरम सुंदर तत्त्व’ की महिमा बताने के बहाने इसकी चर्चा अवश्य होती रही है।’ इसलिए अपनी इस छिन्न किंतु समृद्ध परंपरा के आधार पर ही उन्होंने लालित्य-चिंतन के भवन-निर्माण का प्रयास किया है।
इस प्रयास का पहला सूत्र है कि वे सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर ‘लालित्य’ कहना चाहते हैं, क्योंकि ‘प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उसके समानांतर चलनेवाला मानवरचित सौंदर्य’ (ग्रंथावली 7/34) उनकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है। लालित्य वह इसलिए है कि मानव द्वारा लालित है। सौंदर्य की इस मानववादी धारणा का स्त्रोत द्विवेदीजी ने अपनी परंपरा से ही ढूँढ निकाला। वह स्त्रोत है भरत मुनि का नाट्शास्त्र। नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है उसके अनुसार देवता नाटक न कर सके और नाटक कर सकने में मनुष्य को ही समर्थ समझा गया, क्योंकि उसमें देवताओं से एक विशिष्ट शक्ति है-अनुकरण की। यही नहीं, भरत मुनि ने अपने समय में प्रचलित रूपकों में से पूर्णांग सिर्फ नाटक और प्रकरण को ही माना जहाँ नायक मनुष्य होता है। नायकपर विचार करते हुए प्रसंगवश नाट्शास्त्र के अनुसार मनुष्य ही धीरोदात्त हो सकते हैं, जबकि ‘देवा धीरोद्धता एवं’ क्योंकि देवों में फलागम के लिए उतावली होती है और धीरोदात्त की भाँति धीरभाव से प्रत्याशा में वे नहीं उलझते। इस प्रकार द्विवेदीजी ‘कला-सृजन में मनुष्य की महिमा का सबल विवेक’ भरत मुनि से प्राप्त करते हैं। सौंदर्य को मनुष्य-लालित मानने का दूसरा स्त्रोत है तांडव और लास्य का अंतर। पुराणगाथा के अनुसार शिव का तांडव रस-भाव-विवर्जित ‘नृत्त’ हैं जबकि पार्वती का लास्य रस-भाव-समन्वित नृत्य है। द्विवेदीजी इससे यह संकेत ग्रहण करते हैं कि ‘तांडव जहाँ मानव पूर्व तत्त्वों का स्वत:स्फूर्त विकास है, वहाँ लास्य मानवीय प्रयासों का ललित रूप। (वही, 7/31) अंत में आगमों में वर्णित विश्वव्यापिनी सर्जनात्मक शक्त्िा ‘ललिता’ के प्रभामंडल से मंडित करते हुए वे मनुष्य-निर्मित सौंदर्य तत्त्व को ‘लालित्य’ की संज्ञा देते है। किंतु कुल मिलाकर समष्टिगत और व्यष्टिगत दोनों ही स्तरों पर द्विवेदीजी की सौंदर्यदृष्टिमूलत: मानव-केंद्रित ही है। इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि सौंदर्य का स्त्रष्टा मनुष्य है, बल्कि यह भी कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य मनुष्य है।
द्विवेदीजी की लालित्य-मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है कि यह ‘बंधन के विरुद्ध विद्रोह’ है और ‘बंधनद्रोही व्याकुलता को रूप देने का प्रयास’ है। (7/38) नृत्य के संदर्भ में इसी बात को ‘जड़ के गुरुत्वाकर्षण पर चैतन्य की विजयेच्छा’ कहा गया है। (7/28) आकस्मिक नहीं है कि द्विवेदीजी ने अपने सभी उपन्यासों में किसी-न-किसी बहाने नृत्य का आयोजन किया है। नृत्य भले ही बंधनों के विरुद्ध विद्रोह को व्यक्त करनेवाली सबसे जीवंत कला हो, किंतु अन्य कलाएँ भी नृत्य के इस धर्म का अनुसरण करती हैं, यह भी द्विवेदीजी ने यथास्थान स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार द्विवेदीजी की दृष्टि में कला और सौंदर्य ने यथास्थान स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार द्विवेदीजी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास-मात्र नहीं बल्कि बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है जो, शास्त्र समर्थित न होते हुए भी, उनकी क्रांतिकारी सौंदर्य-दृष्टि का परिचायक है।
द्विवेदीजी की लालित्य-मीमांसा का तीसरा सूत्र यह है कि सौंदर्य एक सर्जना है – मनुष्य की सिसृक्षा का परिणाम। उल्लेखनीय है कि ‘लालित्य-मीमांसा’ के प्राप्त अंशों में सबसे अधिक विचार सिसृक्षा पर ही है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि वे मनुष्य की सृजनशीलता पर सबसे अधिकबल देना चाहते थे। विवेचन की शब्दावली अवश्य पुरानी है और प्राय: शैव तथा शाक्त दर्शनों की इच्छाशक्त्िा और क्रियाशक्ति का सहारा लिया गया है, किंतु अंतत: इस आध्यात्मिक शब्दावली के बीच से मनुष्य की वह सर्जनात्मक शक्ति ही प्रकाशित होती है जो सौंदर्य, कला और संस्कृति के मूल में है। इसी सृजनशीलता के संदर्भ में उन्होंने उन ‘रूढ़ियों’ की भूमिका पर भी विचार किया है जो कलाकार के लिए सब समय बाधक ही नहीं होतीं, बल्कि कभी-कभी साधक या सहायक भी हो जाती है।
अंत में द्विवेदीजी एक ऐसे ‘समग्र भाव’ के रूप सौंदर्यकी स्थापना करते हैं जो धर्माचरण, नैतिकता आदि (जीवन की) सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों को छापकर, सबको अभिभूत करके, सबको अंतर्ग्रथित करके ‘सामग्र् भाव ‘ का प्रकाश करता है। उन्हीं के शब्दों में : ‘भाषा में, मिथक में, धर्म में, काव्य में, मूर्ति में, चित्र में बहुधा अभिव्यक्ति मानवीय इच्छाशक्ति का अनुपम विलास ही वह सौंदर्य है जिसकी मीमांसा का संकल्प लेकर हम चले हैं।’ (7/34)
मीमांसा दुर्भाग्यवश अपूर्ण ही रह गई; पर संकल्प सार्थक है। ‘जनता का अंत: स्पंदन’ ही नहीं बल्कि अन्य रचनाओं के प्रकाश में ‘लालित्य-मीमांसा’ के सूत्रों को देखें तो संकेत स्पष्ट है : जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुत: एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह इस सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है – मानव-मुक्ति का प्रयास है। (1982)
- 11 – भाद्रपद मासकी ‘अजा’ और ‘पद्मा’ एकादशीका माहात्य
- 14 – पुरुषोत्तम मासकी ‘कमला’ और ‘कामदा’
- 13 – कार्तिक मासकी ‘रमा’ और ‘प्रबोधिनी’एकादशीका माहात्म्य
- 12 – आश्विन मासकी ‘इन्दिरा’ और ‘पापाङ्कुशा’ एकादशीका माहात्य
- 10 – श्रावण मासकी ‘कामिका’ और ‘पुत्रदा’ एकादशीका माहात्म्य
- About Culture-संस्कृति के विषय में
- About Institution-संस्था के विषय में
- ACT.-अधिनियम
- Awareness About Geography-भूगोल के विषय में जागरूकता
- Awareness About Indian History-भारतीय इतिहास के विषय में जागरुकता
- Awareness About Maths-गणित के बारे में जागरूकता
- Awareness about Medicines
- Awareness About Politics-राजनीति के बारे में जागरूकता
- Awareness-जागरूकता
- Basic Information
- Bharat Ratna-भारत रत्न
- Biography
- Chanakya Quotes
- CLASS 9 NCERT
- CMs OF MP-मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
- CSIR UGC NET
- e-Test-ई-टेस्ट
- Education
- Education-शिक्षा
- Ekadashi Mahatmya
- FULL TEST SERIES
- GK
- Granthawali-ग्रन्थावली
- Hindi Biography – जीवन परिचय
- Hindi Literature
- Hindi Literature-हिंदी साहित्य
- HINDI NATAK-हिंदी नाटक
- Hindi Upanyas-हिंदी उपान्यास
- ICT-Information And Communication TEchnology
- Jokes-चुटकुले
- Kabir ji Ki Ramaini-कबीर जी की रमैणी
- KAHANIYAN
- Katha-Satsang-कथा-सत्संग
- Kavyashastra-काव्यशास्त्र
- Meaning In Hindi-मीनिंग इन हिंदी
- Meaning-अर्थ
- MOCK TEST
- Motivational Quotes in Hindi-प्रेरक उद्धरण हिंदी में
- MPESB(VYAPAM)-Solved Papers
- MPPSC
- MPPSC AP HINDI
- MPPSC GENERAL STUDIES
- MPPSC GS PAPER
- MPPSC-AP-HINDI-EXAM-2022
- MPPSC-Exams
- MPPSC-मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
- Nibandha
- Padma Awardees-पद्म पुरस्कार विजेता
- PDFHUB
- PILLAR CONTENT
- QUOTES
- RSSU CHHINDWARA-राजा शंकर शाह वि.वि. छिंदवाड़ा
- RSSU QUESTION PAPERS
- SANSKRIT
- SANSKRIT VYAKARAN
- SANSKRIT-HINDI
- Sarkari Job Advertisement-सरकारी नौकरी विज्ञापन
- Sarkari Yojna-सरकारी योजना
- Sarkari-सरकारी
- Sarthak News-सार्थक न्यूज़
- SCHOOL
- SOLVED FIRST PAPER CSIR NET
- Theoretical Awareness-सैद्धांतिक जागरूकता
- UGC
- UGC NET
- UGC NET COMPUTER SCIENCE
- UGC NET HINDI MOCK TEST
- UGC NET NEWS
- UGC_NET_HINDI
- UGCNET HINDI
- UGCNET HINDI PRE. YEAR QUE. PAPERS
- UGCNET HINDI Solved Previous Year Questions
- UGCNET-FIRST-PAPER
- UGCNET-FIRSTPAPER-PRE.YEAR.Q&A
- UPSC-संघ लोक सेवा आयोग
- Various Exams
- VEDIC MATHS
- Yoga
- इकाई – 02 शोध अभिवृत्ति (Research Aptitude)
- इकाई – 03 बोध (Comprehension)
- इकाई – 04 संप्रेषण (Communication)
- इकाई – 07 आंकड़ों की व्याख्या (Data Interpretation)
- इकाई – 10 उच्च शिक्षा प्रणाली (Higher Education System)
- इकाई -01 शिक्षण अभिवृत्ति (Teaching Aptitude
- इकाई -06 युक्तियुक्त तर्क (Logical Reasoning)
- इकाई -09 लोग विकास और पर्यावरण (People, Development and Environment)
- इकाई 08 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT-Information and Communication Technology)
- इकाई-05 गणितीय तर्क और अभिवृत्ति (Mathematical Reasoning And Aptitude)
- कबीर ग्रंथावली (संपादक- हजारी प्रसाद द्विवेदी)
- कविताएँ-Poetries
- कहानियाँ – इकाई -07
- कहानियाँ-KAHANIYAN
- कहानियाँ-Stories
- खिलाड़ी-Players
- प्राचीन ग्रन्थ-Ancient Books
- मुंशी प्रेमचंद
- व्यक्तियों के विषय में-About Persons
- सार्थक न्यूज़
- साहित्यकार
- हिंदी व्याकरण-Hindi Grammar