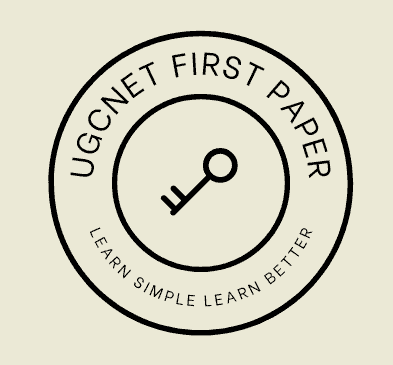अनुपलब्धि प्रमाण (Non-Apprehension) :
अनुपलब्धि प्रमाण का अर्थ एवं स्वरूप
अनुपलब्धि का शाब्दिक अर्थ है जो उपलब्ध न हो अर्थात् जिसकी उपलब्धि (ज्ञान) का अभाव हो उसे ही अनुपलब्धि कहते हैं। प्रमाण के रूप में अनुपलब्धि का प्रमुख कार्य अभाव को ग्रहण करना है। प्रमुख मीमांसक आचार्य ‘पार्थसारथी मिश्र ने ‘शास्त्रदीपिका’ में उल्लिखित किया है कि “भट्टमीमांसा में सर्वप्रथम अनुपलब्धि नामक स्वतंत्र प्रमाण को स्वीकार किया गया जिससे अनुपलब्धि प्रमा का ज्ञान होता है। कालान्तर में अद्वैत वेदान्त में भी इसे स्वतंत्र प्रमाण माना गया। ज्ञातव्य है कि मीमांसा और अद्वैत वेदान्त में अनुपलब्धि के अतिरिक्त प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति को भी ज्ञान का स्वतन्त्र साधन स्वीकार किया गया है।
भाट्ट मीमांसकों और अद्वैत वेदांतियों का यह कथन है कि किसी स्थान विशेष पर कोई वस्तु विद्यमान न हो तो उस स्थान पर उस वस्तु का अभाव माना जायेगा और उस अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि नामक एक पृथक प्रमाण से होगा। जैसे किसी स्थान पर घट नहीं है तो इस घटाभाव का ग्रहण अनुपलब्धि प्रमाण से ही होता है। अतः अनुपलब्धि एक स्वतन्त्र प्रमाण है। इसके स्वरूप को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है- यदि किसी घट को मैंने देखा है, परन्तु इसी स्थान पर उपलब्धि के सभी साधनों के होते हुए भी इस समय घट नहीं दिखायी देता है, अर्थात् घट की उपलब्धि यथ समय, यथा स्थान पर नहीं होती है, तो हमें अन्ततः यह स्वीकार करना होगा कि इस स्थान पर घटभान है और इसका ज्ञान हमें अनुपलब्धि से हो रहा है।
नैयायिक और मीमांसक दोनों ने अभाव को ‘पदार्थ’ तो माना है किन्तु अनुपलब्धि को प्रमाण रूप में केवल मीमांसक ही मानते हैं अर्थात् मीमांसकों के अनुसार ‘अभाव’ पदार्थ और प्रमाण दोनों है। आचार्य कुमारिल ने ‘श्लोकवार्तिक’ में कहा हैं कि-
“प्रमाणपंचकं यत्र वस्तुरूपे न ज्ञायते। वस्तुसत्ताबोधार्थं तत्राभाव प्रमाणता ।।”
अर्थात् अभाव के सन्दर्भ में अन्य पाँ प्रमाण चरितार्थ नहीं हो सकते। अतः उसके ज्ञान के लिए अनुपलब्धि को प्रमाण मानना आवश्यक है। धर्मराजाध्वरीन्द्र के अनुसार ज्ञान रूपी करण से उत्पन्न न होने वाले अभावानुभव के असाधारण कारण को अनुपलब्धि प्रमाण कहा जाता है। अनुमान आदि से जन्य अतीन्द्रिय अभाव (यथा- अहं पुण्याभाववान् सुखाभावत्वात् जो इस व्याप्ति ज्ञान पर निर्भर है कि ‘यत्र-यत्र सुखाभावः तत्र-तत्र पुण्याभावः) में अतिव्याप्ति के निवारण के लिए लक्षण में- “ज्ञानकरणाजन्यत्व’ इस विशेषण का प्रयोग किया गया है। अनुमान व्याप्ति ज्ञान जन्य होता है, जबकि अनुपलब्धि में ऐसा नहीं होता।
अनुपलब्धि प्रमाण की उपादेयता :
न्याय एवं वैशेषिक आदि ने अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण नहीं स्वीकार किया है, किन्तु न्यायशास्त्र में अभाव का व्यापक विश्लेषण किया गया है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रमाण रूप में अनुपलब्धि को न स्वीकारने के बावजूद अभाव के महत्त्व को माना गया है। दार्शनिकों का मानना है कि यदि सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से विचार किया जाय तो भाव के साथ अभाव की समस्या सदैव बनी रहती है। वास्तव में यदि अभाव की सत्ता न होती तो लोगों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ इतना अवश्य है कि इसके ज्ञान को लेकर भारतीय आचार्यों में मतभेद है। भाट्ट मीमासांकें और वेदांतियों ने अभाव के ज्ञान के लिए ही अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में प्रतिपादित किया। किन्तु लोक व्यवहार में नैयायिकों का मत अधिक प्रसिद्ध है। क्योंकि प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान और शब्द से भी अभाव का ज्ञान हो सकता, जबकि अधिकांशतः अभाव के ज्ञान हेतु प्रत्यक्ष का सहारा लिया जाता है।
नैयायिकों की दृष्टि में ‘विशेषण-विशेष्य-भाव’ को एक सम्बन्ध के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जिससे कि अनुपलब्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण में अन्तर्भाव किया जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अनुपलब्धि के प्रमाणत्व को लेकर विवाद होने के बावजूद, ‘अभाव’ को लेकर भारतीय दर्शन में जो विश्लेषण तथा खण्डन-मण्डन प्रस्तुत किया गया वह इसकी उपादेयता को सिद्ध करता है। अतः प्रमाणित होता है कि भारतीय दर्शन में अनुपलब्धि प्रमाण महत्त्व स्वतः सिद्ध है।
अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण भारतीय दर्शन में वेदमूलक दर्शनों में मीमांसा और वेदान्त में स्वीकार्य है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी घटनाएँ या विचार की वस्तुएँ आती है, जिनका हमें केन्द्रीय प्रत्यक्ष नहीं होता, फिर भी उनका अस्तित्व होता है। यदि उनके अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया जाय, तो जीवजगत की बहुत सारी व्याख्याएँ नही हो पायेंगी। अर्थापत्ति जहां दृष्टकार्य या घटनाओं को देखकर उसके पीछे की अदृष्ट (बिना देखी हुई) कारण का बौद्धिक निर्धारण है, वही अनुपलब्धि प्रमाण द्वारा हम किसी भी वस्तु या घटना के किसी देश और काल में अनुपस्थिति को सिद्ध करते हैं। इस प्रकार से अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण भारतीय ज्ञानमीमांसा के क्षेत्र को व्यापकता प्रदान करता है। इन प्रमाणों के ही आधार पर हम आत्मा, ईश्वर या दैवीय सत्ताओं के 0 पर विश्वास कर पाते हैं। ये प्रमाण हमारे जीवन में आस्तीकता का प्रवेश कराते हैं।
शब्द प्रमाण (VERBAL TESTIMONY) :
शब्द प्रमाण (आप्तवाक्यं से तु शब्दः पर्यन्त)
आप्तवाक्यं शब्दः। आप्तस्तु यथार्थवक्ता। वाक्यं पदसमूहः। यथा ‘गामानय’ इति। शक्तं पदम् । अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्य इतीश्वरेच्छासंकेतः शक्तिः ।
व्याख्या : आचार्य अन्नम्भट्ट न्याय-वैशेषिक दर्शन की समावेशी परम्परा के आचार्य हैं। उनका ग्रन्थ ‘तर्कसंग्रह’ एक प्रकरण ग्रन्थ है जिसमें वैशेषिक दर्शन की पदार्थ मीमांसा के साथ न्याय दर्शन में स्वीकृत प्रमाण व्यवस्था का विवेचन किया गया है। प्रमाणों के निरूपण क्रम में आचार्य प्रत्यक्ष, अनुमान एवं उपमान का निरूपण करने के उपरान्त ‘शब्द’ प्रमाण का विवेचन करते हैं। शब्द प्रमाण का लक्षण है ‘आप्तवाक्यं शब्दः अर्थात् आप्त पुरुष के वाक्य को शब्द प्रमाण कहा जाता है। आप्त का अर्थ है – यथार्थ बोलने वाला। कोई व्यक्ति जिस रूप में किसी पदार्थ का अनुभव करता है, जब वह किसी अन्य व्यक्ति को उस वस्तु के बारे में उसी प्रकार का यथार्थ कथन करता है तो उसे ही आप्त कहा जाता है।
‘वाक्य’ का लक्षण करते हुए आचार्य कहते हैं ‘वाक्यं पदसमूहः। पदों का समूह वाक्य कहलाता है। संस्कृत भाषा में वर्णों का समूह मिलकर पद या शब्द का निर्माण करते हैं तथा कई शब्द या पद मिलकर एक वाक्य बनाते हैं। वाक्य का उदाहरण है ‘गाम् आनय’; इस वाक्य में दो पद हैं अनुसार ‘सुप्तिङन्तं पदम् अर्थात् सुबन्त तथा आनय’ में ‘गाम्’ पद सुबन्त है तथा ‘आनय’ समूह होने से यह वाक्य हो जाता है। ‘गाम्’ तथा ‘आनय’। महर्षि पाणिनि के तिड़न्त की पद संज्ञा होती है। ‘गाम् पद तिड़न्त है, इसलिए इन दोनों का पद के स्वरूप का विवेचन करते हुए आचार्य कहते हैं ‘शक्तं पदम्’ अर्थात् जो अर्थबोधक शक्ति से युक्त होता है, उसे पद कहते हैं। शक्ति का लक्षण है ‘अस्मात् पदात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा शक्तिः’ अर्थात् ‘इस पद से यह अर्थ जानना चाहिए’ यह जो ईश्वरकृत् संकेत है, वह शक्ति है। इसी शक्ति से युक्त को पद कहा जाता है। उदाहरणतः घ्+अ+ट्+अ वर्णों के मिलने से ‘घट’ पद निष्पन्न होता है और उक्त प्रकार के संकेतग्रह से घट पद का बोध हो जाता है।
वाक्य के लक्षण (पदसमूहः वाक्यम्) में प्रयुक्त ‘समूह’ का तात्पर्य अनेक वर्णों का समुदाय नहीं समझना चाहिए क्योंकि अनेक स्थलों पर पद ‘एकवर्णात्मक’ भी होता है; आकाश का वाचक ‘ख’ पद, सुख का वाचक ‘क’ पद इत्यादि। ‘समूह’ से ‘एक ज्ञान का विषय होना’ अर्थात् एक ज्ञान में भासित होने वाले वर्णों यथा आशय है का नाम ही पद है।
विशेष: यथार्थ भाषण करने वाला वक्ता ही आप्त है तथा जिस शब्द द्वारा यह यथार्थज्ञान हो वही शब्द प्रमाण है। प्राचीन नैयायिक ईश्वरेच्छा को शक्ति मानते हैं जबकि नव्यनैयायिक इच्छामात्र को शक्ति कहते हैं।
आकांक्षायोग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थज्ञानहेतुः ।
पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्ताऽन्वयाननुभावकत्वमाकांक्षा।
अर्थाबाधो योग्यता।
पदानामविलम्बेनोच्चरणं सन्निधिः।
आकांक्षादिरहितं वाक्यमप्रमाणम्।
यथा गौरश्वः पुरुषो हस्तीति न प्रमाणम् आकांक्षाविरहात्।
अग्निना सिञ्चेत इति न प्रमाणम्, योग्यताविरहात्।
प्रहरे प्रहरेऽसहोच्चारितानि ‘गामानय’ इत्यादिपदानि न प्रमाणम्, सान्निध्याभावात् ।
व्याख्या : तर्कसंग्रहकार आचार्य अन्नम्भट्ट शब्द प्रमाण के लक्षण एवं स्वरूप का निरूपण करने के उपरान्त शाब्दबोध की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। सर्वप्रथम वे वाक्य से होने वाले वाक्यार्थज्ञान के कारणों का विवेचन करते हुए कहते हैं कि ‘आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि किसी वाक्य के अर्थज्ञान में कारण होते है। यदि किसी व्यक्ति को किसी वाक्य का अर्थबोध करना है तो उसे आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि ये तीनों वाक्य का अर्थज्ञान कराने में सहकारी कारण बनते हैं। इनके बिना किसी भी वाक्य का अर्थबोध नहीं किया जा सकता है।
आकांक्षा का लक्षण है ‘पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्ताऽन्वयाननुभावकत्वमाकांक्षा’ । एक पद का दूसरे पद के अभाव में परस्पर अन्वय बोध न हो पाना ‘आकांक्षा’ है। आशय यह कि किसी एक पद के अर्थ को समझने के लिए दूसरे पद की आवश्यकता होती है, यही आवश्यकता ही पदों की परस्पर आकांक्षा कहलाती है। यथा ‘गाम् आनय’ इस वाक्य में यदि केवल गाम् पद या केवल आनय पद का ही उच्चारण किया जाय तो श्रोता को कोई अर्थबोध नहीं हो सकता है। इस वाक्य का अर्थबोध कराने के लिए गाम् पद को आनय पद की तथा आनय पद को गाम् पद की आकांक्षा है। यह आकांक्षा श्रोता की जिज्ञासा रूप होती है तथा यह हृदय में रहती है। एक पद को सुनने के उपरान्त वाक्य के अगले पद को सुनने की इच्छा श्रोता के मन में उत्पन्न होती है। इसी का नाम आकांक्षा है। इसी आकांक्षा का अभाव होने के कारण ‘गौरश्वः पुरुषो हस्ती इति’ इस वाक्य को प्रामाणिक नहीं माना जाता है। योग्यता का लक्षण है ‘अर्थाबाधो योग्यता’ अर्थात् पदों के अर्थों में बाधा का न होना योग्यता कहलाता है। तात्पर्य यह है कि पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध में बाधा का अभाव ही योग्यता है। किसी वाक्य के वाक्यार्थज्ञान हेतु उस वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थों को परस्पर बाधित नहीं होना चाहिए। यदि पदों के अर्थ एक दूसरे को बाधित करते हैं अर्थात् उनका कोई सम्बन्ध नहीं बन पता है तो ऐसे पदसमुदाय को वाक्य नहीं कहा जाता है और न उससे वाक्यार्थबोध होता है। यथा ‘अग्निना सिञ्चति’ यह वाक्य प्रमाण नहीं है क्योंकि पदों में योग्यता का अभाव है। अग्नि में दाहकता होती है जिसके कारण उसमें सेचन शक्ति का अभाव होता है। सेचन क्रिया की सामर्थ्य जल में होता है, अग्नि में नहीं। अतः अग्नि और सेचन क्रिया के सम्बन्ध में बाधा विद्यमान है इसलिए इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता है।
सन्निधि का लक्षण है ‘पदानामविलम्बेनोच्चारणं सन्निधिः। पदों का अविलम्ब से उच्चारण करना सन्निधि कहलाता है। सन्निधि का अभाव होने पर भी पदसमूह को वाक्य नहीं कहा जाता है। यथा ‘गाम् आनय’ इस वाक्य में यदि गाम् पद का उच्चारण प्रथम प्रहर में किया जाय तथा आनय पद का उच्चारण द्वितीय प्रहर में किया जाय तो इस समूह से अर्थबोध पूर्णतः नहीं हो सकता है। अर्थबोध के लिए यहआवश्यक है कि वाक्य में प्रयुक्त समस्त पदों का उच्चारण बिना किसी विलम्ब के किया जाय।
विशेष : आचार्य का अभिमत है कि आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि से रहित वाक्य प्रमाण नहीं होता है अपितु उसे अप्रमाण माना जाता है।
वाक्यं द्विविधम्- वैदिकं लौकिकं च। वैदिकमीश्वरोक्तत्वात्सर्वमेव प्रमाणम्। लौकिकं त्वाप्तोक्तं प्रमाणम्। अन्यदप्रमाणम्। वाक्यार्थज्ञानं शाब्दज्ञानम्। तत्करणं तु शब्दः ।
व्याख्या : तर्कसंग्रहकार आचार्य अन्नभट्ट शब्द प्रमाण का निरूपण करते हुए कहते हैं कि आप्तपुरुष के द्वारा बोला गया वाक्य शब्द प्रमाण कहलाता है। वाक्य का लक्षण करते हुए उनका कथन है ‘पदसमूहः वाक्यम्’ अर्थात् पदों का समूह ही वाक्य है। प्रस्तुत अनुच्छेद में आचार्य वाक्य के भेदों की चर्चा करते हुए शाब्दज्ञान के करण का विवेचन करते हैं।
वाक्य के दो भेद होते हैं वैदिक वाक्य तथा लौकिक वाक्य। इन द्विविध वाक्यों में समस्त वैदिक वाक्य प्रमाण होते हैं क्योंकि उनका कथन ईश्वर ने किया है। न्याय-वैशेषिक परम्परा में ईश्वर को परम आप्त माना जाता है तथा इनकी यह भी मान्यता है कि ईश्वर ने ही वेद की रचना की है। चूँकि समस्त वैदिक वाक्य ईश्वरोक्त है इसलिए उसके अप्रमाण होने की सम्भावना भी नहीं है क्योंकि ईश्वर अयथार्थवक्ता नहीं हो सकता है। लौकिक वाक्यों की प्रमाणता का विवेचन करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो लौकिक वाक्य किसी आप्त व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है केवल वही प्रमाण की कोटि में आता है। अयथार्थ भाषण करने वाले व्यक्ति के द्वारा कहा गया समस्त वाक्य अप्रमाण होता है।
शब्दप्रमाण प्रकरण का उपसंहार करते हुए आचार्य कहते हैं कि आप्त पुरुष के द्वारा बोले गए वाक्य के अर्थज्ञान को ही शाब्दज्ञान कहा जाता है। इस शाब्दज्ञान का असाधारण कारण (कारण) शब्द होता है अतः शाब्दी प्रमा का करण शब्द कहलाता है।
विशेष : न्याय-वैशेषिक मतानुसार वेद पौरुषेय हैं क्योंकि सर्वज्ञ ईश्वर ने उसकी रचना की है। ईश्वररचित होने के कारण ही समस्त वैदिक वाक्य प्रमाण होते हैं।