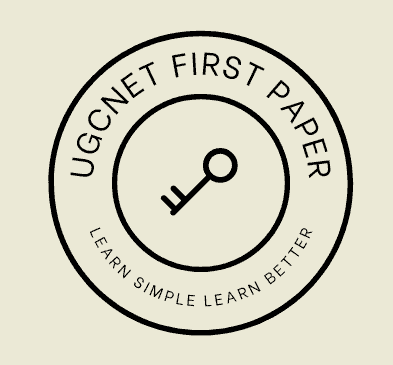02. उपमान प्रमाण (COMPARISION) :
उपमान प्रमाण (उपमितिकरणम् से उत्पद्यते पर्यन्त)
उपमितिकरणमुपमानम्। संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञानमुपमितिः । तत्करणं सादृश्यज्ञानम् । अतिदेशवाक्यार्थस्मरणमवान्तरव्यापारः ।
तथा हि- कश्चिद् गवयशब्दार्थमजानन् कुतश्चिदारण्यकपुरुषात् ‘गोसदृशो गवयः’ इति श्रुत्वा, वनं गतो वाक्यार्थं स्मरन् गोसदृशं पिण्डं पश्यति।
तदनन्तरम् ‘असौ गवयशब्दवाच्यः’ इत्युपमितिरुत्पद्यते ।
व्याख्या : तर्कसंग्रहकार आचार्य अन्नम्भट्ट प्रत्यक्ष एवं अनुमान प्रमाण का निरूपण करने के उपरान्त तृतीय प्रमाण ‘उपमान’ का विवेचन प्रारम्भ करते हैं। उपमान का लक्षण करते हुए उनका कथन है ‘उपमितिकरणम् उपमानम्’ अर्थात् उपमिति का करण उपमान कहलाता है। यहाँ करण का अर्थ असाधारण कारण है। उपमिति ज्ञान की उत्पत्ति में उपमान ही वह असाधारण कारण होता है जिसका प्रयोग करने पर उपमिति की उत्पति तुरन्त हो जाती है। ‘उपमिति’ का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं ‘संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञानमुपमितिः’ अर्थात् संज्ञा और संज्ञी के सम्बन्ध ज्ञान को उपमिति कहते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ के नाम को ‘संज्ञा’ कहते हैं तथा वह पदार्थ ‘संज्ञी’ कहलाता है। यथा ‘कम्बुग्रीवादिमान पात्रविशेष’ संज्ञी है तथा ‘घट’ उसकी संज्ञा है। उपमिति का ज्ञान हमें तभी हो पता है जब हम संज्ञा, संज्ञी तथा उनके मध्य के निश्चित सम्बन्ध को जानते हैं।
सादृश्यज्ञान को उपमिति का करण कहा जाता है क्योंकि उपमिति उपमान का ही सिद्ध रूप है तथा उपमान करने में तुलना या तुल्य पदार्थ का होना अत्यन्त आवश्यक होता है। चूँकि सादृश्यज्ञान इसी आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसलिए वह उपमिति का करण कहलाता है।
उपमिति की प्रक्रिया में अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण अवान्तर व्यापार होता है। ‘अतिदिश्यते प्रतिपाद्यते अनेन साधर्मयादिः इति अतिदेशः इस व्युत्पत्ति के अनुसार साधर्मय (समानता) आदि को बतलाने वाला वाक्य अतिदेश वाक्य कहलाता है। है। अतिदेश वाक्य का उदाहरण है ‘गोसदृशो गवयः’ अर्थात् गाय के समान ही गवय (नीलगाय) होता है। यहाँ ‘गोसदृशो गवयः’ इस वाक्य के द्वारा गवय की गोसदृशता का कथन किया गया है, अतः यह अतिदेश वाक्य है। इसी वाक्य के अर्थ का स्मरण करके गवय को न पहचानने वाला व्यक्ति गोसादृश्य को देखकर गवय की पहचान कर लेता है, इसीलिए अतिदेश वाक्यार्थस्मरण को उपमिति ज्ञान का अवान्तर व्यापार कहा जाता है।
उपमान की प्रक्रिया का निरूपण करते हुए आचार्य कहते हैं किसी नगर में रहने वाला कोई व्यक्ति गवय को नहीं पहचानता है। कोई वनवासी उसे यह बताता है कि ‘यथा गौस्तथा गवयः’ अर्थात् जैसी गाय होती है वैसी ही नीलगाय (गवय) भी होती है। यही अतिदेश वाक्य है जिसे सुनकर वह नगर निवासी जब जंगल में प्रवेश करता है और वहाँ गाय जैसे किसी पशु को देखता है। उसे देखकर उस व्यक्ति को वनवासी द्वारा बताये गए उस अतिदेश वाक्य के अर्थ का स्मरण हो उठता है कि जैसी गाय होती है वैसी ही गवय भी होती है। इसके पश्चात् उसे यह ज्ञान हो जाता है कि यह पशु गवय है। यही उपमिति ज्ञान है। इसी उपमिति का करण उपमान प्रमाण कहलाता है।
अर्थापत्ति (Postulation) :
अर्थापत्ति का अर्थ एवं स्वरूप
सर्वप्रथम यह जानना अनिवार्य है कि अर्थापत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? अर्थापत्ति शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से होती हैं। प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थस्य आपत्तिः यस्मात् अर्थात् अर्थ की आपत्ति जिससे हो, वह अर्थापत्ति है। इसके अनुसार अर्थापत्ति प्रमाण है। द्वितीय व्युत्पत्ति के अनुसार- अर्थस्यआपत्तिः अर्थापत्तिः अर्थात् अर्थ की आपत्ति अर्थापत्ति है। इस व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थापत्ति को प्रमा माना जाय या प्रमाण माना जाय परन्तु इससे एक विशेष प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है अर्थात् अर्थापत्ति से विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। विशिष्ट ज्ञान ही विशिष्ट प्रमा है। विशिष्ट ज्ञान को उदाहरण से समझा जा सकता है। “पीनोऽयं देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते” अर्थात् देवदत्त मोटा है परन्तु दिन में भोजन नहीं करता। अतः वह रात में भोजन करता है। यदि देवदत्त दिन में निराहार रहता है, तो वह रात में आहार (भोजन) अवश्य ग्रहण करता है अन्यथा वह मोटा नहीं हो सकता। इस प्रकार मोटे देवदत्त की व्याख्या रात में भोजन के कारण ही सम्भव है।
अर्थापत्ति के दो भाग किये गये हैं- 1. उपपाद्य और 2. उपपादक। उपरोक्त उदाहरण में देवदत्त का मोटा होना उपपाद्य है तथा देवदत्त का रात में भोजना करना उपपादक है। अतः यह कहा जा सकता है कि अर्थापत्ति उपपादक से उपपाद्य का ज्ञान है। इस उदाहरण के अन्तर्गत हमें देवदत्त के मोटा होने की व्याख्या करनी है। इस व्याख्या के अन्तर्गत ‘देवदत्त के मोटा होने में हमें यह मानना पड़ेगा कि देवदत्त रात में भोजन करता है। अतः कहा जा सकता है कि अर्थापत्ति में उपपाद्य और उपपादक दोनों अर्थों की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य (देवदत्त) दिन में उपवास रखता है और रात में भी भोजन न करें तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता है।
ज्ञात अर्थ की व्याख्या के लिए अज्ञात अर्थ की कल्पना करना अर्थात् जिसकी सहायता के बिना उस ज्ञात अर्थ की उपपत्ति नहीं हो पाती उसे अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे किसी देवदत्त नामक व्यक्ति का जीवन प्रमाणान्तर (ज्योतिषादि) से निश्चित है किन्तु घर में जब उसकी उपलब्धि या उपस्थिति नहीं होती है, तब उसके बाहर होने की कल्पना की जाती है। इसी कल्पना को अर्थापत्ति कहते हैं। यहाँ उपपाद्य जीवन करण है और उपपादक बहिर्भाव फल है। जिसके बिना जो अनुपपन्न हो उसे उपपाद्य कहते हैं जैसे- जीवन तथा जिसके अभाव में जिसकी अनुपपत्ति हो उसे उपपादक कहते हैं जैसे- बहिर्भाव। जीवन और बहिर्भाव में प्रमाण-सिद्ध जो परस्पर विरोध है। वह अर्थापत्ति में करण होता है। किसी प्रमाण से ज्ञात हो कि देवदत्त घर में है या देवदत्त घर से बाहर है और किसी अन्य प्रमाण से यह भी ज्ञात हो कि देवदत्त घर में नहीं है, ऐसी स्थिति में दोनों ही वाक्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। इस विशेष या प्रतिधातु का समाधान बहिर्भाव की कल्पना से किया जाता है। अतः दो प्रामाणिक अर्थों के बीच अर्थान्तर की कल्पना द्वारा समाहित होने वाला पारस्परिक विरोध अर्थापत्ति का कारण कहलाता है। उस विरोध (प्रतिघात) के समाधान हेतु जो अर्थान्तर कल्पना होती है उसे अर्थापत्ति कहते हैं।
प्रमाण के रूप में अर्थापत्ति
सांख्य दर्शन में अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं प्रमाण की है, अपितु अर्थापत्ति को अनुमान प्रमाण के अन्तर्गत रखते हैं। इसी तरह न्याय दर्शन भी अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानना अपितु नैयायिक भी अर्थापत्ति को अनुमान में अन्तर्निहित मानते हैं। मीमांसा एवं वेदांत के अतिरिक्त अन्य दार्शनिक समुदाय ने इसे स्वतंत्र प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं प्रदान किया है।
अर्थापत्ति के भेद
मीमांसा दर्शन में अर्थापत्ति के दो भेद भेद प्राप्त होते हैं- दृष्टार्थापत्ति एवं श्रुतार्थापत्ति । कुमारिल के अनुसार भाष्य में प्रयुक्त श्रुत और दृष्ट शब्द अर्थापत्ति के दो भेदों के वाचक हैं। किन्तु प्रभाकर का यह कथन है कि श्रुत और दृष्ट एक ही प्रमाण के दो नामान्तर हैं। अतः श्रुतार्थापत्ति एक पृथक भेद नहीं है। धर्मराजाध्वरीन्द्र ने श्रुतार्थापत्ति (शाब्दबोध में अनुपपत्ति) को अर्थापत्ति का एक पृथक भेद तो माना ही है। इसके साथ ही अभिधाननुपत्ति और अभिहितानुपपत्ति के रूप में उसके दो उपभेदों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार यदि देखा जाय तो अर्थापत्ति के कुल चार भेद हुए, जिसमें ये दोनों, उपभेद भी शामिल हैं।
अनुपलब्धि प्रमाण (Non-Apprehension) :
अनुपलब्धि प्रमाण का अर्थ एवं स्वरूप
अनुपलब्धि का शाब्दिक अर्थ है जो उपलब्ध न हो अर्थात् जिसकी उपलब्धि (ज्ञान) का अभाव हो उसे ही अनुपलब्धि कहते हैं। प्रमाण के रूप में अनुपलब्धि का प्रमुख कार्य अभाव को ग्रहण करना है। प्रमुख मीमांसक आचार्य ‘पार्थसारथी मिश्र ने ‘शास्त्रदीपिका’ में उल्लिखित किया है कि “भट्टमीमांसा में सर्वप्रथम अनुपलब्धि नामक स्वतंत्र प्रमाण को स्वीकार किया गया जिससे अनुपलब्धि प्रमा का ज्ञान होता है। कालान्तर में अद्वैत वेदान्त में भी इसे स्वतंत्र प्रमाण माना गया। ज्ञातव्य है कि मीमांसा और अद्वैत वेदान्त में अनुपलब्धि के अतिरिक्त प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति को भी ज्ञान का स्वतन्त्र साधन स्वीकार किया गया है।
भाट्ट मीमांसकों और अद्वैत वेदांतियों का यह कथन है कि किसी स्थान विशेष पर कोई वस्तु विद्यमान न हो तो उस स्थान पर उस वस्तु का अभाव माना जायेगा और उस अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि नामक एक पृथक प्रमाण से होगा। जैसे किसी स्थान पर घट नहीं है तो इस घटाभाव का ग्रहण अनुपलब्धि प्रमाण से ही होता है। अतः अनुपलब्धि एक स्वतन्त्र प्रमाण है। इसके स्वरूप को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है- यदि किसी घट को मैंने देखा है, परन्तु इसी स्थान पर उपलब्धि के सभी साधनों के होते हुए भी इस समय घट नहीं दिखायी देता है, अर्थात् घट की उपलब्धि यथ समय, यथा स्थान पर नहीं होती है, तो हमें अन्ततः यह स्वीकार करना होगा कि इस स्थान पर घटभान है और इसका ज्ञान हमें अनुपलब्धि से हो रहा है।
नैयायिक और मीमांसक दोनों ने अभाव को ‘पदार्थ’ तो माना है किन्तु अनुपलब्धि को प्रमाण रूप में केवल मीमांसक ही मानते हैं अर्थात् मीमांसकों के अनुसार ‘अभाव’ पदार्थ और प्रमाण दोनों है। आचार्य कुमारिल ने ‘श्लोकवार्तिक’ में कहा हैं कि-
“प्रमाणपंचकं यत्र वस्तुरूपे न ज्ञायते। वस्तुसत्ताबोधार्थं तत्राभाव प्रमाणता ।।”
अर्थात् अभाव के सन्दर्भ में अन्य पाँ प्रमाण चरितार्थ नहीं हो सकते। अतः उसके ज्ञान के लिए अनुपलब्धि को प्रमाण मानना आवश्यक है। धर्मराजाध्वरीन्द्र के अनुसार ज्ञान रूपी करण से उत्पन्न न होने वाले अभावानुभव के असाधारण कारण को अनुपलब्धि प्रमाण कहा जाता है। अनुमान आदि से जन्य अतीन्द्रिय अभाव (यथा- अहं पुण्याभाववान् सुखाभावत्वात् जो इस व्याप्ति ज्ञान पर निर्भर है कि ‘यत्र-यत्र सुखाभावः तत्र-तत्र पुण्याभावः) में अतिव्याप्ति के निवारण के लिए लक्षण में- “ज्ञानकरणाजन्यत्व’ इस विशेषण का प्रयोग किया गया है। अनुमान व्याप्ति ज्ञान जन्य होता है, जबकि अनुपलब्धि में ऐसा नहीं होता।