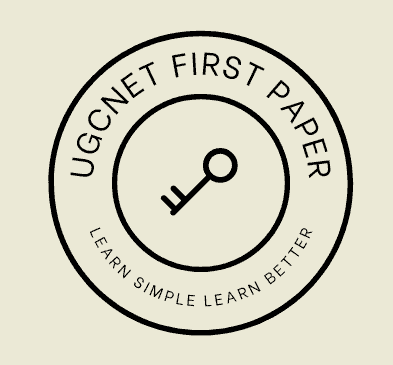हेत्वाभास : हेत्वाभास के 5 प्रकार
सव्यभिचारविरुद्धसत्प्रतिपक्षासिद्धबाधिताः पञ्च हेत्वाभासाः ।
व्याख्या : अनुमान प्रमाण का स्वरूप निरुपित करने के उपरान्त आचार्य अन्नम्भट्ट अनुमान के ही अंगभूत ‘हेत्वाभास’ का विवेचन प्रारम्भ करते हैं। न्याय-वैशेषिक दर्शन में हेत्वाभास यद्यपि असद् हेतु हैं तथापि ये हेतु या सद्हेतु के ही अंग हैं, अतः हेतुज्ञान की पूर्णता तथा अनुचित हेतु के प्रयोग से बचने एवं वाद की प्रकिया में विपक्षी द्वारा ऐसा हेतु का प्रयोग करने पर उसके सिद्धान्त का खण्डन करके उसे परास्त करने के हेत्वाभास के स्वरूप एवं उसके प्रकारों का ज्ञान आवश्यक है। ‘हेतुवद् आभासन्ते ते हेत्वाभासः’ अर्थात् वह हेतु जो सद् हेतु की तरह प्रतीत तो होता है किन्तु वस्तुतः वह सद् हेतु होता नहीं है, उसे ही हेत्वाभास कहते हैं।
हेत्वाभास के 5 प्रकार : –
आचार्य ने हेत्वाभास के 5 प्रकार बतलाये हैं (1) सव्यभिचार, (2) विरुद्ध, (3) सत्प्रतिपक्ष, (4) असिद्ध, (5) बाधित
01. सव्यभिचार हेत्वाभास
सव्यभिचारोऽनैकान्तिकः। स त्रिविधः साधारणासाधारणनुपसंहारिभेदात्। तत्रसाध्याभाववद्वृत्तिः साधारणोऽनैकान्तिकः। यथा पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वात् इति प्रमेयत्वस्य वह्यभाववति हृदे विद्यमानत्वात्। सर्वसपक्षविपक्षव्यावृतोऽसाधारणः। यथा ‘शब्दो नित्यः, शब्दत्वात्’ इति । शब्दत्वं सर्वेभ्यो नित्येभ्योऽनित्येभ्यश्च व्यावृत्तं शब्दमात्रवृत्ति । अन्वयव्यतिरेकदृष्टान्तरहितोऽनुपसंहारी। यथा ‘सर्वमनित्यं, प्रमेयत्वात्’ इति। अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वाद् दृष्टान्तो नास्ति ।
व्याख्या : इनमें से प्रथम सव्यभिचार का निरूपण करते हुए आचार्य कहते हैं। ‘सव्यभिचारोऽनैकान्तिकः’ अर्थात् सव्यभिचार हेत्वाभास को अनैकान्तिक हेत्वाभास भी कहते हैं। इसके तीन भेद हैं –
(1) साधारण,
(2) असाधारण,
(3) अनुपसंहारी।
साधारण सव्यभिचार हेत्वाभासः ‘साध्याभाववद्वृत्तिः साधारणोऽनैकान्तिकः’ अर्थात् जो असद् हेतु साध्य के अभाव वाले पदार्थों में रहा करता है उसे साधारण अनैकान्तिक हेत्वाभास कहते हैं। यथा- ‘पर्वतो अग्निमान, प्रमेयत्वात’ । अर्थात् पर्वत अग्नि वाला है, प्रमेय होने से। इस अनुमान वाक्य में ‘प्रमेयत्व’ हेतु असद् हेतु या दुष्ट हेतु है पर्वत को अग्निवाला होने में यदि प्रमेयत्व को हेतु माना जायेगा तो संसार के समस्त पदार्थ अग्निमान हो जायेंगे क्योंकि उन सभी पदार्थों में प्रमेयत्व विद्यमान है। ऐसा मानने पर अतिव्याप्ति दोष होने लगेगा, अतः यहाँ साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास है।
असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभासः ‘सर्वसपक्षविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रवृत्तिरसाधारणः’ अर्थात् जब कोई हेतु समस्त सपक्ष, विपक्ष में न रहकर केवल पक्ष मात्र में रहता है तो वहाँ असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास होता है। अनुमान वाक्य को सही होने के लिए यह आवश्यक है कि हेतु को पक्ष तथा सपक्ष में रहना चाहिए तथा विपक्ष में नहीं रहना चाहिए। किन्तु जब कोई हेतु सपक्ष में भी नहीं रहता है तो वही असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास की स्थिति है। यथा ‘शब्दो नित्यः, शब्दत्वात् अर्थात् शब्द नित्य है क्योंकि उसमें शब्दत्व है। इस अनुमान वाक्य में शब्द ‘पक्ष’ है, नित्यत्व ‘साध्य’ है तथा शब्दत्व ‘हेतु’ है। यह शब्दत्व हेतु नित्य आकाशादि सपक्षों तथा अनित्य घटादि विपक्षों दोनों में ही नहीं रहता, जबकि इसे पक्ष शब्द के साथ सपक्ष आकाशादि में भी विद्यमान होना चाहिए। ऐसा न होने पर अव्याप्ति दोष प्रसक्त होता है, अतः यहाँ असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास है।
अनुपसंहारी सव्यभिचार हेत्वाभास अन्वयव्यतिरेकदृष्टान्तरहितोऽनुपसंहारी अर्थात् अन्वय (तत् सत्त्वे तत् सत्त्वं अन्वयः) तथा व्यतिरेक (तद् अभावे तद् अभावः व्यतिरेक) दृ ष्टान्त से रहित हेतु को अनुपसंहारी सव्यभिचार हेत्वाभास कहते हैं। अनुपसंहारी हेत्वाभास वह है जिसका न कोई सपक्ष दृष्टान्त हो और न ही कोई विपक्ष दृष्टान्त विद्यमान हो। यथा सर्व अनित्यम्, प्रमेयत्वात्’ अर्थात् सब कुछ अनित्य है क्योंकि सब प्रमेय है। इस वाक्य में सर्व पक्ष है, अनित्यत्व साध्य है तथा प्रमेयत्व हेतु है। प्रकृ त उदाहरण में सम्पूर्ण पदार्थ के पक्ष बन जाने से न तो कोई अन्वय दृष्टान्त मिलता है और न ही कोई व्यतिरेक दृष्टान्त। इसलिए यहाँ अनुपसंहारी सव्यभिचार हेत्वाभास है।
साध्याभावव्याप्तो हेतुर्विरुद्धः। यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति। कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावेनानित्यत्वेन व्याप्तम्।
02. विरुद्ध हेत्वाभास : ‘
साध्याभावव्याप्तो हेतुर्विरुद्धः अर्थात् जो हेतु साध्य के अभाव में व्याप्त रहता है, वह विरुद्ध हेत्वाभास है। आशय यह है कि किसी अनुमान वाक्य में जब कोई ऐसा हेतु साध्य को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है जो साध्य को सिद्ध न करके साध्य के अभाव को सिद्ध करने लगता है तो यह विरुद्ध स्वभाव वाला होने के कारण विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। यथा शब्दो नित्यः, कृतकत्वात् अर्थात् शब्द नित्य है, कृतक होने के कारण। कृतक होने का अर्थ है जन्य होना या उत्पन्न होना। यह सार्वत्रिक नियम है कि संसार में जो भी वस्तु कृतक (जन्य या उत्पन्न) होती है वह अनित्य अवश्य होती है। प्रकृत उदाहरण में शब्द पक्ष है, नित्यत्व साध्य है तथा कृतकत्व हेतु है। यहाँ व्याप्ति का स्वरूप यह होगा ‘यत्र यत्र कृ तकत्वम् तत्र तत्र नित्यत्वम् किन्तु वास्तविक व्याप्ति यह है कि ‘यत्र यत्र कृतकत्वम् तत्र तत्र अनित्यत्वम्’ अर्थात् जो कृतक होता है वह अनित्य होता है। अनित्यत्व का अर्थ है नित्यत्व का अभाव (साध्याभाव)। अतः प्रकृत हेतु नित्यत्व का साधक न होकर उसके विरुद्ध नित्यत्वाभाव को सिद्ध कर रहा है। यही विरुद्ध हेत्वाभास है।
यस्य साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं विद्यते स सत्प्रतिपक्षः। यथा ‘शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्, शब्दत्ववत्’ इति । ‘शब्दोऽनित्यः कार्यत्वात्, घटवत् इति।
03. सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास :
सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास ‘यस्य साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं विद्यते स सत्प्रतिपक्षः’ अर्थात् जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला कोई दूसरा हेतु विद्यमान हो, वह सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहलाता है। सत्प्रतिपक्ष का शाब्दिक अर्थ है ‘सत् अर्थात् विद्यमान है प्रतिपक्ष जिसका’। आशय यह है कि जहाँ पर दो हेतु परस्पर एक दूसरे के विपरीत अर्थ (साध्य) को सिद्ध करते हैं वहाँ वे दोनों हेतु, सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास माने जाते हैं।
यथा ‘शब्दः नित्यः, श्रावणत्वात्, शब्दत्ववत्’ शब्द नित्य है, श्रावणत्व के कारण, शब्दत्व के समान। यहाँ श्रावणत्व हेतु का प्रयोग करके शब्द को अनित्य सिद्ध किया जा रहा है। इसका विरोधी दूसरा अनुमान प्रस्तुत करता है ‘शब्दः अनित्यः, कार्यत्वात्, घटवत् शब्द अनित्य है, कार्य होने से, घट के समान। यहाँ कार्यत्व हेतु के द्वारा शब्द में अनित्यत्व को सिद्ध किया जा रहा है। यहाँ दोनों ही अनुमान वाक्यों में ‘शब्द’ ही एकमात्र पक्ष है जिसे श्रावणत्व हेतु के द्वारा नित्य तथा कार्यत्व हेतु द्वारा अनित्य सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः साध्यविपरीतसाधक तुल्यबल वाला दूसरा हेतु विद्यमान होने से ये दोनों हेतु अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हैं यही सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास है।
04. असिद्ध हेत्वाभास :
असिद्धस्त्रिविध: आश्रयासिद्धः, स्वरूपासिद्धः, व्याप्यत्वासिद्धश्चेति । आश्रयसिद्धो यथा ‘गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्, सरोजारविन्दवत्’ । अत्र गगनारविन्दमाश्रयः। स च नास्त्येव । स्वरूपासिद्धो यथा शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वात्, रूपवत्। अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्तियशब्दस्य श्रावणत्वात्। सोपाधिको हेतुव्याप्यत्वासिद्धः । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापक उपाधिः। साध्यसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं साध्यव्यापकत्वम् । साध्यवन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साधनाव्यापकत्वम्। ‘पर्वतो धूमवान् वह्निमत्त्वात्’ इत्यत्र आर्द्रन्धनसंयोग उपाधिः। तथा हि यत्र धूमस्तत्र आर्देन्धनसंयोग इति साध्यव्यापकता। यत्र वह्निस्तत्र आर्द्रन्धनसंयोगो नास्तिय अयोगोलके आर्द्रन्धनसंयोगाभावादिति साधनव्यापकता। एवं साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वाद् आर्द्रन्धनसंयोग उपाधिः । सोपाधिकत्वाद्वह्निमत्त्वं व्याप्यत्वासिद्धम् ।
असिद्ध हेत्वाभास तर्कसंग्रहकार आचार्य अन्नम्भट्ट ने असिद्ध हेत्वाभास का कोई लक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। असिद्धि का अर्थ है सिद्धि का न होना अर्थात् साध्य व्याप्य हेतु का पक्ष में न रहना। असिद्ध हेत्वाभास के तीन भेद हैं आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध तथा व्याप्यत्वासिद्ध ।
असिद्ध हेत्वाभास के तीन भेद हैं –
- आश्रयासिद्ध,
- स्वरूपासिद्ध तथा
- व्याप्यत्वासिद्ध ।
आश्रयासिद्ध हेत्वाभास का लक्षण है
‘यस्य हेतोः आश्रयः न अवगम्यते स आश्रयासिद्धः’ अर्थात् जिस हेतु का आश्रय (पक्ष) निश्चित न हो, उसे आश्रयासिद्ध कहते हैं। उदाहरण गगनारविन्दं सुरभिः, अरविन्दत्वात्, सरोजारविन्दवत्’ – आकाशकुसुम सुगन्धित होता है, कमल होने के कारण, सरोवर में उत्पन्न कमल के समान। इस अनुमानवाक्य में गगनारविन्द पक्ष (आश्रय) है, सुरभित्व साध्य, अरविन्दत्व हेतु तथा सरोजारविन्द दृष्टान्त है। यहाँ पर गगनारविन्द आश्रय है जिसकी वस्तुतः कोई सत्ता ही नहीं होती है। इस कारण आश्रय (पक्ष) के न होने से ‘अरविन्दत्वात्’ यह हेतु आश्रयासिद्ध हेत्वाभास है।
स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास स्वरूपासिद्ध का अर्थ है जो स्वरूपतः असिद्ध हो अर्थात् जहाँ हेतु स्वयं ही असिद्ध होता है, वह स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। यथा शब्दो गुणः, चाक्षुषत्वात्, रूपवत्’ शब्द गुण है, चाक्षुष होने के कारण, रूप के समान। इस अनुमानवाक्य में शब्द के गुण होने में चाक्षुषत्व को हेतु बतलाया जा रहा है जबकि पक्षभूत शब्द चक्षु का विषय न होकर कर्ण का विषय होता है। अतः यहाँ हेतु के अपने स्वरूप से ही असिद्ध होने के कारण स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है।
व्याप्यात्वासिद्ध हेत्वाभास आचार्य अन्नम्भट्ट व्याप्यात्वासिद्ध हेत्वाभास का लक्षण करते हैं- ‘सोपाधिको हेतुयाप्यत्वासिद्धः’ अर्थात् जो हेतु उपाधि से युक्त होता है उसे व्याप्यात्वासिद्ध कहा जाता है। इस लक्षण में आये हुए उपाधि पद का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं ‘साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमुपाधित्वम्’ अर्थात् जो साध्य का व्यापक हो एवं साधन (हेतु) का व्यापक न हो, उसे उपाधि कहते हैं। उपाधि शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है ‘उपसमीपवर्तिनि आदधाति संक्रामयति स्वीयं धर्म इति उपाधिः’ जो अपने धर्म को समीपस्थ पदार्थ में संक्रान्त कर दे उसे उपाधि कहते हैं। जिस प्रकार जब हम किसी दर्पण के सम्मुख लाल गुलाब का पुष्प रखते हैं तो पुष्प की लालिमा दर्पण में संक्रान्त हो जाती है जिसके कारण दर्पण भी लाल प्रतीत होने लगता है, यहाँ ‘लाल गुलाब का पुष्प अपने लालिमा रूप धर्म को दर्पण में संक्रान्त कर रहा है अतः वह उपाधि है।
उपाधि के लक्षण में आये हुए ‘साध्यव्यापकत्व’ एवं ‘साधनाव्यापकत्व’ पदों का अर्थ स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं ‘साध्यसमानाधिकरणऽत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् साध्यव्यापकत्वम्’ अर्थात् साध्य के अधिकरण (आश्रय) में रहने वाले अत्यन्ताभाव का जो प्रतियोगी नहीं हैं उसे साध्यव्यापक कहते हैं। ‘साध्यवन्निष्ठऽत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् साधनाव्यापकत्वम्’ अर्थात् साधन के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यन्ताभाव है, उसका प्रतियोगि होना ही साधनाव्यापकत्व है। यथा ‘पर्वतो अग्निमान, धूमवत्त्वात्’ इस अनुमानवाक्य में आर्द्रन्धनसंयोग उपाधि है। यहाँ आर्द्रन्धनसंयोग रूप धर्म उक्त अनुमान वाक्य में साध्य धूम का व्यापक है क्योंकि ‘जहाँ-जहाँ धूम होता है वहाँ-वहाँ आर्द्रन्धनसंयोग अवश्य होता है। किन्तु ‘जहाँ-जहाँ अग्नि हो वहाँ-वहाँ आर्द्रन्धनसंयोग का होना अनिवार्य नहीं है, जैसे लोहे के गोले में अग्नि तो होती है किन्तु आर्द्रन्धनसंयोग नहीं होता है। इसलिए आर्द्रन्धनसंयोग रूप धर्म उपरोक्त अनुमान वाक्य में प्रयुक्त साधन (अग्नि) का अव्यापक है। इस प्रकार आर्द्रन्धनसंयोग रूप धर्म में ‘साध्यव्यापकत्व’ एवं ‘साधनाव्यापकत्व’ दोनों अंशों के घटित हो जाने से उसमें उपाधि का लक्षण समन्वित हो जाता है। अतः सोपाधिक होने से अग्निमत्त्व व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास है।
यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण निश्चितः स बाधितः।
यथा वह्निरनुष्णो द्रव्यत्वात्’ इति।
अत्रानुष्णत्वं साध्यं, तदभाव उष्णत्वं स्पार्शनप्रत्यक्षेण गृह्यत इति बाधितत्वम् ।
05. बाधित हेत्वाभास :
पंच हेत्वाभासों में बाधित नामक हेत्वाभास का लक्षण करते हुए आचार्य कहते हैं यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण निश्चितः स बाधितः जिस हेतु के साध्य का अभाव किसी अन्य प्रमाण द्वारा निश्चित होता है वह बाधित हेत्वाभास कहलाता है। आशय यह है कि जब कोई अनुमानकर्त्ता किसी साध्य को सिद्ध करने के लिए हेतु का प्रयोग करता है किन्तु उस हेतु का साध्य किसी अन्य बलवत्तर प्रमाण से बाधित कर दिया जाता है, ऐसी दशा में हेतु अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो पाता है य यही बाधित हेत्वाभास है। उदाहरण ‘अग्निरनुष्णः, द्रव्यत्वात्, जलवत् अर्थात् अग्नि शीतल होती है, द्रव्य होने से, जल के समान। प्रकृत अनुमान वाक्य में अनुष्णत्व साध्य है, अग्नि पक्ष है, द्रव्यत्व हेतु है तथा जलदृष्टान्त है। यदि हम द्रव्यत्व हेतु से अग्नि में अनुष्णत्व को सिद्ध करना चाहते हैं तो वह सम्भव नहीं है क्योंकि अग्नि का उष्णत्व स्पार्शन प्रत्यक्ष से निश्चित है। यहाँ स्पार्शन प्रत्यक्ष रूप प्रबल प्रमाण द्रव्यत्व हेतु के साध्यभूत अनुष्णत्व को बाधित कर देता है, यही बाधित हेत्वाभास है।
विशेष : आचार्य अन्नम्भट्ट के अनुसार हेत्वाभास का अर्थ दुष्ट हेतु है। आचार्य शंकरमिश्र ने दुष्ट हेतु का लक्षण किया है ‘यस्य हेतोर्यावन्ति रूपाणि गमकतौपयिकानि तदन्यतररूपहीनः’ अर्थात् सद् हेतु होने के लक्षणों में से किसी एक से भी हीन होने पर दुष्ट हेतु होता है।