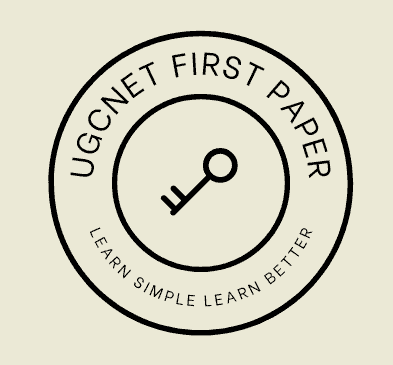कारण
कारणं त्रिविधम्-रामवाय्यमवायिनिमित्तभेदात् । यत्समवेत कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्। यथा तन्तव पटस्य, पटश्च स्वगतरूपादे। कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन्नर्थे समवेत सत् कारणम् असमवायिकारणम्। यथा तन्तु संयोग पटस्य, तन्तुरूपं पटगतरूपस्य च। तदुभयभिन्न कारणं निगितकारणम्, यथा-तुरीवेमादिक पटस्य । तदेत्त्रिविधकारणमध्ये यदसाधारण कारणम् तदेव करणम्।
व्याख्या: आचार्य अन्नम्मभट्ट कारण का लक्षण करते है कारणम्’। जो कार्य का नियत पूर्ववर्ती हो उसे कारण कहते हैं। समवायिकारण, असमवायिकारण और निमित्तकारण। कार्यनियतपूर्ववृत्ति कारण के तीन भेद हैं
इन त्रिविध कारणों में रामवायिकारण का लक्षण है ‘यत्समवेत कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्’। जिसमें समवायसम्बन्ध से रहकर कार्य उत्पन्न होता है, उसे समवायिकारण कहते है। जिस कारण में जो कार्य समवायसम्बन्ध से रहता है, वह कारण समवायिकारण कहलाता है। जैसे तन्तु से पट का निर्माण होता है और जब तक पट रहे तब तक तन्तु रहता ही है अथवा जब तक तन्तु रहे तब तक पट रहता है। इस तरह पट रूप कार्य अपने कारण तन्तुओं में नित्यसम्बन्ध से रहता है। इसलिए तन्तु यहाँ पर पट का समवायिकारण है।
दूसरा उदाहरण में स्वगत रूप के प्रति स्वयं पट समवायिकारण होता है। पट के उत्पन्न होने के बाद उसी पट में रूप समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होने के कारण स्वगतरूप के प्रति पट समवायिकारण बना। तन्तु से पट की उत्पत्ति होने पश्चात् एकक्षण विलम्ब से ही उसमें उत्पन्न होता है, क्योंकि पटरूप के प्रति पटरूप के
समवायिकारण होने से कार्य से पूर्व में कारण का होना आवश्यक है और कारण के बाद ही उससे कार्य की उत्पत्ति मानी जाती है।
असमवायिकारण का लक्षण है ‘कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन्नर्थे समवेत सत् कारणम् असमवायिकारणम्। कार्य अथवा कारण के साथ एक पदार्थ में समवायसम्बन्ध से रहने वाला जो कारण हैं, वह असमवायिकारण है। असमवायिकारण का दो प्रकार से लक्षण किया गया है- प्रथम कार्येण सहैकस्मिन्नर्थे समवेत सत् यत्कारण अर्थात् कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय सम्बन्ध से विद्यमान रहता हुआ जो कारण है, वह असमवायिकारण है। यथा तन्तुसंयोग, पटात्मक कार्य के साथ एक पदार्थ तन्तु में समवाय सम्बन्ध से रहता हुआ कारण है और इसमें तन्तुओं का संयोग जो कारण है, वही असमवायिकारण हुआ। कार्य पट के साथ एकत्र तन्तुओं में समवाय सम्बन्ध से विद्यमान रहता हुआ तन्तुसयोग रूप कारण पट के प्रति असमवायिकारण होता है। असमवायिकारण का दूसरा प्रकार है कारणेन सह एकस्मिन्नर्थे समवेतं सत् यत्कारणम्’ अर्थात् कारण के साथ एक ही पदार्थ में समवाय सम्बन्ध से रहता हुआ जो कारण है, वह भी असमवायिकारण है। यथा तन्तुरूप, पटरूप का असमवायिकारण है अर्थात् पट के रूप का कारण है तन्तुओ का रूप। वह पट अपने कारण तन्तुओं मे समवाय सम्बन्ध से रहता है। इस प्रकार तन्तु में स्थित रूप ही पटगत रूप के प्रति कारण है। वह तन्तुओं का रूप पट के रूप के प्रति असमवायिकारण है। अपने कार्य के समवायिकारण के साथ एकत्र समवाय सम्बन्ध से विद्यमान रहता हुआ कारण ही समवायिकारण है। प्रथम लक्षण के अनुसार अवयवों का सयोग और द्वितीय लक्षण के अनुसार अवयवी के गुण रूप आदि के प्रति अवयव के गुण रूप आदि असमवायिकारण होते हैं।
‘निमित्तकारण’ का स्वरूप बताते हुए आचार्य कहते हैं कि समवायिकारण और असमवायिकारण इन दोनो कारणो से जो भिन्न कारण है, उसे निमित्तकारण कहते है। जैसे कपडे बनाने में सहायक यन्त्र तुरी, वेमा आदि ये निमित्तकारण है।
समवायि, अरामवायि एवं निमित्त तीनों कारणों में जो असाधारण कारण है, उसे ही करण कहा जाता है। विशेष कार्य के त्रिविध कारणों में समवायिकारण केवल द्रव्य होता है। गुण या कर्म किसी कार्य के असमवायिकारण होते हैं। निमित्तकारण द्रव्य, गुण, कर्म के साथ कोई भी पदार्थ हो सकता है।
तन्त्र प्रत्यक्षज्ञानकरणम् प्रत्यक्षम्। इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्य ज्ञान प्रत्यक्षम्। तद्दिवविधम् निर्विकल्पक सविकल्पक चेति। तन्त्र निष्प्रकारक ज्ञान निर्विकल्पकम्, यथेद किचित्। सप्रकारक ज्ञानं सविकल्पकम्, यथा जित्थोऽयं श्यामोऽयमिति ।
व्याख्या: प्रत्यक्ष का निरूपण करते हुए आचार्य अन्नम्भट्ट कहते हैं कि प्रत्यक्षज्ञान का जो असाधारण कारण है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। चक्षु, रसन, श्रोत, घ्राण, त्वक् और मन इन छः इन्द्रियों के द्वारा वस्तुओ का प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष यह प्रमाण भी है और ज्ञान भी। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं।
तर्कसंग्रहकार आचार्य अन्नम्भट्ट के अनुसार इन्द्रिय और अर्थ (विषय) का रान्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु है। ज्ञानेन्द्रियों की संख्या 5 है चक्षु, श्रोत, त्वक्, रसना एवं घ्राण। प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय नियत विषय का ही ग्रहण करती है जैसे चक्षु रूप का, श्रोत शब्द का, त्वक् स्पर्श का, रसना रस का तथा घ्राण गन्ध का। जब कोई इन्द्रिय अपने
नियत विषय के साथ संयुक्त होती है तो उस सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहते हैं। इन्द्रिय और अर्थ (पदार्थ) के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रदत्त लक्षण में सन्निकर्ष पद का अर्थ-सयोग आदि सम्बन्ध विशेष है एव अर्थ पद का अर्थ विषय है। इन्द्रियों का उनके विषयों के साथ सन्निकर्ष होना प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करता है। यथा-इन्द्रिय
अर्थ (विषय)
प्रत्यक्ष – घ्राण
गन्ध -घ्राणज
रसना -रस रासन
चक्षु -रूप चाक्षुष
त्वक स्पर्श स्पार्शन (त्वाक्)
श्रोत्र श्रोतज शब्द
मन मानस सुखदुःख आदि
- 11 – भाद्रपद मासकी ‘अजा’ और ‘पद्मा’ एकादशीका माहात्य
- 14 – पुरुषोत्तम मासकी ‘कमला’ और ‘कामदा’
- 13 – कार्तिक मासकी ‘रमा’ और ‘प्रबोधिनी’एकादशीका माहात्म्य
- 12 – आश्विन मासकी ‘इन्दिरा’ और ‘पापाङ्कुशा’ एकादशीका माहात्य
- 10 – श्रावण मासकी ‘कामिका’ और ‘पुत्रदा’ एकादशीका माहात्म्य
- About Culture-संस्कृति के विषय में
- About Institution-संस्था के विषय में
- ACT.-अधिनियम
- Awareness About Geography-भूगोल के विषय में जागरूकता
- Awareness About Indian History-भारतीय इतिहास के विषय में जागरुकता
- Awareness About Maths-गणित के बारे में जागरूकता
- Awareness about Medicines
- Awareness About Politics-राजनीति के बारे में जागरूकता
- Awareness-जागरूकता
- Basic Information
- Bharat Ratna-भारत रत्न
- Biography
- Chanakya Quotes
- CLASS 9 NCERT
- CMs OF MP-मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
- CSIR UGC NET
- e-Test-ई-टेस्ट
- Education
- Education-शिक्षा
- Ekadashi Mahatmya
- FULL TEST SERIES
- GK
- Granthawali-ग्रन्थावली
- Hindi Biography – जीवन परिचय
- Hindi Literature
- Hindi Literature-हिंदी साहित्य
- HINDI NATAK-हिंदी नाटक
- Hindi Upanyas-हिंदी उपान्यास
- ICT-Information And Communication TEchnology
- Jokes-चुटकुले
- Kabir ji Ki Ramaini-कबीर जी की रमैणी
- KAHANIYAN
- Katha-Satsang-कथा-सत्संग
- Kavyashastra-काव्यशास्त्र
- Meaning In Hindi-मीनिंग इन हिंदी
- Meaning-अर्थ
- MOCK TEST
- Motivational Quotes in Hindi-प्रेरक उद्धरण हिंदी में
- MPESB(VYAPAM)-Solved Papers
- MPPSC
- MPPSC AP HINDI
- MPPSC GENERAL STUDIES
- MPPSC GS PAPER
- MPPSC-AP-HINDI-EXAM-2022
- MPPSC-Exams
- MPPSC-मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
- Nibandha
- Padma Awardees-पद्म पुरस्कार विजेता
- PDFHUB
- PILLAR CONTENT
- QUOTES
- RSSU CHHINDWARA-राजा शंकर शाह वि.वि. छिंदवाड़ा
- RSSU QUESTION PAPERS
- SANSKRIT
- SANSKRIT VYAKARAN
- SANSKRIT-HINDI
- Sarkari Job Advertisement-सरकारी नौकरी विज्ञापन
- Sarkari Yojna-सरकारी योजना
- Sarkari-सरकारी
- Sarthak News-सार्थक न्यूज़
- SCHOOL
- SOLVED FIRST PAPER CSIR NET
- Theoretical Awareness-सैद्धांतिक जागरूकता
- UGC
- UGC NET
- UGC NET COMPUTER SCIENCE
- UGC NET HINDI MOCK TEST
- UGC NET NEWS
- UGC_NET_HINDI
- UGCNET HINDI
- UGCNET HINDI PRE. YEAR QUE. PAPERS
- UGCNET HINDI Solved Previous Year Questions
- UGCNET-FIRST-PAPER
- UGCNET-FIRSTPAPER-PRE.YEAR.Q&A
- UPSC-संघ लोक सेवा आयोग
- Various Exams
- VEDIC MATHS
- Yoga
- इकाई – 02 शोध अभिवृत्ति (Research Aptitude)
- इकाई – 03 बोध (Comprehension)
- इकाई – 04 संप्रेषण (Communication)
- इकाई – 07 आंकड़ों की व्याख्या (Data Interpretation)
- इकाई – 10 उच्च शिक्षा प्रणाली (Higher Education System)
- इकाई -01 शिक्षण अभिवृत्ति (Teaching Aptitude
- इकाई -06 युक्तियुक्त तर्क (Logical Reasoning)
- इकाई -09 लोग विकास और पर्यावरण (People, Development and Environment)
- इकाई 08 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT-Information and Communication Technology)
- इकाई-05 गणितीय तर्क और अभिवृत्ति (Mathematical Reasoning And Aptitude)
- कबीर ग्रंथावली (संपादक- हजारी प्रसाद द्विवेदी)
- कविताएँ-Poetries
- कहानियाँ – इकाई -07
- कहानियाँ-KAHANIYAN
- कहानियाँ-Stories
- खिलाड़ी-Players
- प्राचीन ग्रन्थ-Ancient Books
- मुंशी प्रेमचंद
- व्यक्तियों के विषय में-About Persons
- सार्थक न्यूज़
- साहित्यकार
- हिंदी व्याकरण-Hindi Grammar