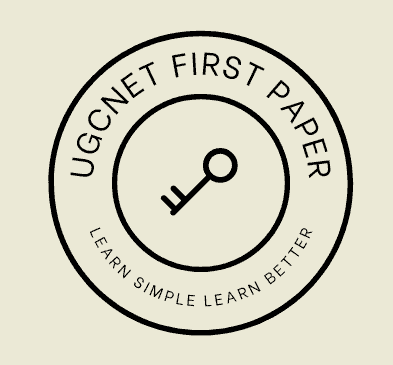प्रेमचंद का परिचय और उनके उपन्यास
(Credit – IGNOU)
प्रस्तावना
प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में साहित्य सर्जन किया है। वे मुख्यतः कथाकार हैं। उन्होंने सेवासदन, रंगभूमि, गोदान आदि महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। पंचपरमेश्वर, दो बैलों की कथा, सवासेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, कफन आदि उनकी चर्चित कहानियाँ हैं। उन्होंने हिंदी में तीन नाटकों की भी रचना की। ‘हंस’ और ‘जागरण’ पत्रिकाओं का संपादन किया। हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद का आगमन युगांतकारी महत्त्व रखता है। उनके लेखन से हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा मिली। उन्होंने हिंदी उपन्यास को सामाजिक यथार्थ से जोड़कर सोद्देश्यता प्रदान की। उनके उपन्यासों में जहाँ शोषित, उत्पीड़ित जनता के दुःख दर्द को स्थान दिया गया, वहीं राष्ट्रीय भावना को भी प्रस्तुत किया गया है। तत्कालीन समाज की यथार्थ स्थिति को उन्होंने हू-ब-हू प्रस्तुत किया है। प्रथमतः उनके उपन्यास आदर्शवादी रहे, उनमें कथा के द्वारा पात्रों के चरित्र को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। धीरे-धीरे आदर्श की जगह यथार्थता का स्थान बढ़ता गया। बाद के उपन्यासों में उन्होंने यथार्थ और आदर्श का समुचित मेल रखा है। जीवन के प्रत्येक पक्ष का उद्घाटन उनके उपन्यासों से मिलता है लेकिन दलितों, महिलाओं और किसानों के प्रति उन्होंने विशेष सहानुभूति जताई है। साहित्यकार के कर्त्तव्य के बारे में वे स्वयं कहते हैं “जो दलित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, चाहे वह व्यक्ति हो या समूह उसकी हिमायत और वकालत करना उसका फर्ज है।” (प्रेमचंद, कुछ विचार)।
प्रेमचंद का जीवन परिचय
प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई, 1880 को बनारस के पास लमही नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी अजायबलाल और माता का नाम आनंदी देवी था। इनके पिता डाकखाने में मुंशी थे। शायद इसी कारण प्रेमचंद को भी मुंशी प्रेमचंद लिखने की परंपरा रही है। इनका बचपन का नाम धनपतराय श्रीवास्तव था। स्कूल में उनका यही नाम लिखवाया गया था। साहित्य लेखन के लिए उन्होंने नवाबराय नाम तय किया। इसी नाम से उन्होंने उर्दू में कहानियाँ लिखना प्रारम्भ किया। आठ वर्ष की अवस्था में इनकी माता का देहान्त हो गया। बाद में इनके पिता ने दूसरा विवाह किया। इस विमाता से प्रेमचंद की अनबन रहती थी, जिसका उल्लेख उन्होंने किया है। इसके बाद प्रेमचंद का भी विवाह हो गया। पत्नी से भी प्रेमचंद की पटरी नहीं बैठी। कहते हैं कि विमाता और उनकी पत्नी के भी संबंध अच्छे नहीं थे। इस गृह कलह तथा अन्य कारणों से प्रेमचंद ने पत्नी को त्याग दिया। पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं था, अतः उनकी पत्नी का फिर से विवाह नहीं हुआ। उनकी पत्नी बहुत दिनों तक अपने भाइयों के पास ही रही। प्रेमचंद ने पुनः विवाह कर लिया। इस बार उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया, जो जीवन भर उनके साथ रहीं। इस विवाह का कारण आर्य समाज के प्रभाव को माना जाता है। फिर जल्दी ही प्रेमचंद के पिता का देहांत हो गया, तब परिवार की सारी आर्थिक-सामाजिक जिम्मेदारी प्रेमचंद पर आ गई। प्रेमचंद के दो पुत्र और एक पुत्री हुई। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को पर्याप्त शिक्षा दी, लेकिन पुत्री को ज्यादा नहीं पढ़ाया तथा उसका जल्दी ही विवाह भी कर दिया।
आरंभिक शिक्षा
प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा मदरसे में हुई तथा उन्होंने प्रारंभिक लेखन भी उर्दू में ही किया। उनकी प्रारम्भिक उपलब्ध रचना, ‘आलिवर क्रामवेल की जीवनी’ (सन् 1903) माना जाता है। यह निबंध दयानारायण निगम के प्रसिद्ध पत्र ‘जमाना’ में प्रकाशित हुआ।
उनका पहला उपन्यास
उनका पहला उपन्यास ‘हम खुर्मा और हम सबाब’ (1906) माना जाता है। उनकी पहली कहानी ‘दुनिया का सबसे अनमोल रतन’ (1907) मानी जाती है। उनका पहला कहानी संग्रह ‘सोज़े-वतन’ सन् 1909 में छपा। इस संग्रह में देशप्रेम की भावुक ललकार मिलती है। कहा जाता है कि सरकार ने यह जानकारी प्राप्त कर ली थी कि धनपतराय श्रीवास्तव और नवाब राय एक ही व्यक्ति है। तब तत्कालीन जिलाधीश ने प्रेमचंद को बुलाकर डाँटा-फटकारा तथा भविष्य में ऐसी कहानियाँ न लिखने की हिदायत देकर इस संग्रह को जब्त कर लिया।
सरकारी नौकरी करते हुए अपने नाम से देशभक्ति का साहित्य लिखना प्रेमचंद के लिए अब संभव नहीं था, इसलिए पहले भी उन्होंने धनपतराय श्रीवास्तव के नाम से लेखन नहीं किया। लेखन के रूप में नवाबराय नाम चुना, परन्तु सरकार को पता चल गया। तब फिर नए नाम की खोज हुई। उन्होंने अपने मित्र दयानारायण निगम से चर्चा की और प्रेमचंद नाम से लेखन करने का निर्णय किया। प्रेमचंद के नाम से ‘बड़े घर की बेटी’ (1910) कहानी पहली बार छपी। इसके बाद सभी लोग प्रेमचंद को प्रेमचंद के नाम से ही जानने लगे।
प्रेमचंद की शिक्षा
क्वींस कॉलेज, बनारस से प्रेमचंद ने दसवीं की परीक्षा पास की। 1899 में प्रेमचंद ने सहायक अध्यापक की नौकरी करनी प्रारम्भ की। उनका वेतन 18 रुपया मासिक तय हुआ। मिशन स्कूल चुनार से उनके शिक्षक जीवन का प्रारम्भ हुआ। कई शहरों में उनका तबादला हुआ। बहराइच, प्रतापगढ़ आदि स्थानों पर वे रहे। बाद में महोबा, गोरखपुर, कानपुर में भी रहे। जुलाई, 1902 में वे शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए इलाहाबाद गये। यहाँ उन्हें ‘जूनियर सर्टिफिकेट टीचर’ की उपाधि मिली। इस उपाधि में लिखा है, ‘गणित पढ़ाने की योग्यता नहीं रखते। चाल-चलन संतोषजनक है और समय के पाबन्द है। धनपत राय ने अपना काम खूब मेहनत से और अच्छी तरह किया। 1904 में प्रेमचंद ने उर्दू और हिंदी में स्पेशल वर्नाकुलर की परीक्षा पास की।
प्रेमचंद को पढ़ने का शौक बचपन से ही था। उन्होंने स्वयं लिखा है, ‘इस वक्त मेरी उम्र कोई तेरह साल की रही होगी। हिन्दी बिल्कुल न जानता था। उर्दू के उपन्यास पढ़ने का उन्माद था। मौलाना शरर, पं. रतननाथ सरशार, मिर्जा रुसवा, मौलवी मोहम्मद अली हरदोई निवासी उस वक्त के सर्वप्रिय उपन्यासकार थे। इनकी रचनाएँ जहाँ मिल जाती थीं, स्कूल की याद भूल जाती थी और पुस्तक समाप्त करके ही दम लेता था। उस जमाने में रेनाल्ड के उपन्यासों की धूम थी। उर्दू में अनेक अनुवाद धड़ाधड निकल रहे थे और हाथों हाथ बिकते थे। मैं भी उनका आशिक था। स्व. हजरत रियाज ने, जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं और जिनका हाल में देहान्त हुआ है, रेनाल्ड की एक रचना का अनुवाद ‘हरमसरा’ के नाम से किया था। उसी जमाने में लखनऊ के साप्ताहिक ‘अवध पंच’ के सम्पादक स्व. मौलाना सज्जाद हुसैन ने, जो हास्य रस के अमर कलाकार थे, रेनाल्ड के दूसरे उपन्यास का अनुवाद ‘धोखा या तिलस्मी कानून’ के नाम से किया था। ये सभी पुस्तकें मैंने उस जमाने में पढ़ीं। और पं. रतननाथ सरशार से तो मुझे तृप्ति ही न होती थी। उनकी सारी रचनाएँ मैंने पढ़ डालीं। उन दिनों मेरे पिता गोरखपुर में रहते थे और मैं भी वहीं के मिशन स्कूल में आठवीं में पढ़ता था, जो तीसरा दरजा कहलाता था। रेती पर एक बुकसेलर बुद्धिलाल नाम का रहता था। मैं उसकी दूकान पर सारे दिन तो बैठ न सकता था, इसलिए मैं उसकी दूकान से अंग्रेजी पुस्तकों की कुंजियाँ और नोट्स लेकर अपने स्कूल के लड़कों के हाथ बेचा करता था और इसकी एवज में उपन्यास दूकान से घर लाकर पढ़ता था। दो-तीन वर्षों में सैकड़ों ही उपन्यास पढ़ डाले होंगे। जब उपन्यास का स्टॉक समाप्त हो गया, तो मैंने नवल किशोर प्रेस से निकले हुए पुराणों के उर्दू अनुवाद भी पढ़े और ‘तिलस्म-ए-होशरुबा’ के कई भाग भी पढ़े। इस वृहद तिलस्मी ग्रंथ के सत्रह भाग उस वक्त निकल चुके थे और एक-एक भाग बड़े सुपर रायल आकार के दो-दो हजार पृष्ठों से कम न होगा। और इन सत्रह भागों के उपरांत उसी पुस्तक के अलग-अलग प्रसंगों पर पचासों भाग छाप चुके थे। इनमें से भी मैंने कई पढ़े। जिसने इस बड़े ग्रंथ की रचना की, उसकी कल्पना शक्ति कितनी प्रबल होगी, इसका केवल अनुमान किया जा सकता है। कहते हैं, ये कथाएँ मौलाना फैजी ने अकबर के विनोदार्थ फारसी में लिखी थी। इसमें कितना सत्य है, कह नहीं सकता, लेकिन इतनी वृहद् कथा शायद ही संसार की किसी भाषा में हो। पूरी इंसाइक्लोपीडिया समझ लीजिए। एक आदमी तो अपने साठ वर्ष के जीवन में उनकी पूरी नकल भी करना चाहे, तो नहीं कर सकता। रचना तो दूसरी बात है।’ कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमचंद ने स्कूली शिक्षा के बाद स्वाध्याय के द्वारा अपने ज्ञान का विस्तार किया। उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और उर्दू का ज्ञान था। लेखन का प्रारम्भ उन्होंने उर्दू में किया। बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारम्भ किया। हिंदी में लिखने के बावजूद वे उर्दू में भी लिखते रहे। इस तरह वे भारतीय भाषाओं के उन गिने-चुने लेखकों में से एक थे, जो हिंदी और उर्दू दोनों पर समान भाव से अधिकार रखते थे और जिन्हें दोनों भाषाओं के लेखक अपनी परंपरा में शामिल करते हैं।
प्रेमचंद ने बी.ए. तक की शिक्षा ग्रहण की। महोबा रहते हुए उनकी पदोन्नति हो गई और वे स्कूल इंस्पेक्टर बना दिए गए। यह समय भारतीय इतिहास में महात्मा गाँधी के स्थापित होने के पहले का था। धीरे-धीरे गाँधी जी देश के सर्वमान्य नेता बने। गाँधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया था। उस समय प्रेमचंद गोरखपुर में नौकरी कर रहे थे।
गांधीजी के प्रभाव में प्रेमचंद
8 फरवरी, 1921 को गाँधी जी इलाहाबाद पहुँचे और एक जन सभा को संबोधित किया। स्वयं प्रेमचंद इस सभा में उपस्थित थे। कहते हैं कि गाँधी जी को सुनने के लिए दो लाख से अधिक लोग पहुँचे थे। महात्मा गाँधी ने जनता से सरकार के असहयोग की अपील की। इसका प्रेमचंद के मन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। घर-परिवार में पत्नी से सलाह करके उन्होंने 15 फरवरी, 1921 को सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया।
नौकरी छोड़ने के बाद प्रेमचंद महावीर प्रसाद पोद्दार के साथ चले गए और चर्खे का प्रचार करने लगे। फिर उन्होंने मारवाड़ी स्कूल, कानपुर, काशी विद्यापीठ आदि कई निजी संस्थानों में अध्यापकी की, परन्तु वे कहीं भी एक जगह स्थिर होकर नहीं रहे। इस बीच उन्होंने पत्रकारिता का कार्य भी किया। कुछ दिनों तक उन्होंने ‘मर्यादा’ का संपादन भी किया।
सरस्वती प्रेस की स्थापना
स्थायी आमदनी के लिए प्रेमचंद प्रयासरत थे। इसी क्रम में उन्होंने जुलाई 1923 में बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना की। इस प्रेस में प्रेमचंद ने 4500/-, महताब राय ने 2000 / बलदेव लाल ने 2000/- और रघुपति सहाय ने 2000/ रुपये, लगाए। कुछ दिनों बाद प्रेमचंद ने 9500/रु. में अकेले ही इस प्रेस को खरीद लिया और शेष हिस्सेदारों को उनके रुपए दे दिए। इसी प्रेस से बाद में प्रेमचंद ने ‘हंस’ और ‘जागरण’ को प्रकाशित किया।
सरस्वती में प्रथम प्रकाशन
प्रेमचंद ने उस समय की प्रतिनिधि पत्रिका ‘सरस्वती’ में एक कहानी प्रकाशनार्थ भेजी- ‘पंचों में ईश्वर’। सरस्वती के यशस्वी सम्पादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शीर्षक को सुधार दिया और जून 1916 की ‘सरस्वती’ में ‘पंच परमेश्वर’ शीर्षक से यह कहानी प्रकाशित हुई। अब प्रेमचंद धीरे-धीरे हिंदी साहित्य में आने लगे। वे अपनी रचना पहले उर्दू में लिखते थे तथा बाद में स्वयं ही उसे हिंदी में लिखते थे। हिंदी में जब ‘सेवासदन’ प्रकाशित हुआ तो हिंदी संसार में धूम मच गई। ‘बाजार-ए-हुस्न’ को इतनी तारीफ उर्दू में नहीं मिली थी। इसी क्रम में प्रेमचंद ने ‘रंगभूमि’ उपन्यास की रचना पहले हिंदी में की और तब उसे उर्दू में प्रकाशित करवाया। बाद की सभी रचनाएँ इसी तरह हिंदी और उर्दू में आगे-पीछे छपती रहीं और वे हिंदी-उर्दू दोनों भाषाओं के मान्य लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हुए।
सरस्वती प्रेस की स्थापना के बाद भी प्रेमचंद की आर्थिक परेशानियाँ दूर नहीं हुईं। इसलिए वे दुलारेलाल भार्गव की गंगा पुस्तक माला, लखनऊ में साहित्यिक सलाहकार बनकर गए। यहाँ उनका वेतन 100 रु. मासिक तय हुआ। सितम्बर 1924 से सितम्बर 1925 तक प्रेमचंद लखनऊ में रहे और उसके बाद वापिस लमही आ गए। इसके डेढ़ साल बाद प्रेमचंद पुनः लखनऊ गए। इस बार उन्हें प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका ‘माधुरी’ का संपादक बनाया गया। प्रेमचंद के साथ कृष्ण बिहारी मिश्र भी थे। यहाँ पर वे लगभग छः वर्ष तक रहे। ‘सरस्वती प्रेस’ बनारस से चल ही रहा था। इस दौरान उनके जीवन में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ घटीं। 1924 में ही अलवर नरेश ने प्रेमचंद को अपनी रियासत में बुलाया। उनका वेतन 400 रुपया प्रस्तावित किया तथा इसके साथ बंगला, मोटर और नौकर-चाकर सबकी व्यवस्था की हामी भरी थी। प्रेमचंद ने नम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसी तरह उन्हें अंग्रेज सरकार ‘रायसाहब’ का खिताब देना चाहती थी। इसे भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। शिवरानी देवी ने ‘प्रेमचंद घर में पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के लेखक थे, अतः उनके मन में इन दोनों भाषाओं की एकेडमी बनाने की इच्छा रहती थी। मार्च 1927 में हिन्दुस्तानी एकेडमी का उद्घाटन हुआ। प्रेमचंद इसकी काउंसिल के सदस्य थे। इस एकेडमी ने प्रेमचंद को ‘रंगभूमि’ उपन्यास पर 500 रु का पुरस्कार प्रदान किया था। धीरे-धीरे प्रेमचंद हिंदी संसार के प्रतिष्ठित लेखक हो गए और उन्हें ‘उपन्यास सम्राट’ कहा जाने लगा।
इसी दौरान प्रेमचंद पर दो गम्भीर आरोप लगे। अवध उपाध्याय ने क्रमिक लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि उनका उपन्यास ‘रंगभूमि’ वेनिटी फेयर की नकल है तथा ‘प्रेमाश्रम’ रिजरेक्शन की नकल है। इसी के साथ ही साथ रामकृष्ण शुक्ल शिलीमुख, ठाकुर श्रीनाथ सिंह और ज्योतिप्रसाद निर्मल ने प्रेमचंद पर आरोप लगाए कि वे ब्राह्मण विरोधी और घृणा के प्रचारक हैं। उस काल की हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में इन बातों की खूब चर्चा हुई। जनवरी 1928 की ‘माधुरी’ में ‘पंडित मोटेराम शास्त्री’ शीर्षक कहानी प्रकाशित हुई। इस कहानी पर किन्हीं शास्त्री जी ने प्रेमचंद पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। यह मुकदमा खारिज हो गया। 1931 में प्रेमचंद ने माधुरी का सम्पादन छोड़ दिया तथा मई 1932 में लखनऊ की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद वे लेखन में प्रवृत्त रहे। 8 अक्टूबर 1936 को उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम उपन्यास ‘मंगलसूत्र’ था।
उपन्यासकार प्रेमचंद
हिंदी-उर्दू में प्रेमचंद की ख्याति एक उपन्यासकार के रूप में है। उन्हें हिंदी समाज ने ‘उपन्यास सम्राट’ की उपाधि दी है। किसी अन्य लेखक को यह उपाधि नहीं मिली है। उन्होंने प्रारम्भ में उर्दू में उपन्यास रचना की, बाद में उन्होंने हिंदी-उर्दू दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया। उनका पहला उर्दू उपन्यास ‘हम खुर्मा और हम सवाब’ है, जो 1906 में प्रकाशित हुआ। यह सामाजिक उपन्यास है। इसका नायक समाज सुधार के कार्य करता है। हिंदी में यह उपन्यास ‘प्रेमा’ के नाम से प्रकाशित हुआ। बाद में उन्होंने इस उपन्यास को ‘प्रतिज्ञा’ शीर्षक से पुनः प्रकाशित किया। इसकी कथा और उद्देश्य को उन्होंने बदल दिया। इसके साथ उन्होंने ‘रूठी रानी’ शीर्षक से एक ऐतिहासिक उपन्यास और ‘वरदान’ नामक उपन्यास की भी रचना की।
सेवासदन
हिंदी में प्रेमचंद की ख्याति ‘सेवासदन’ के प्रकाशन से हुई। यह उनके उर्दू उपन्यास ‘बाजार-ए-हुस्न’ का हिंदी रूपान्तरण है, जो स्वयं प्रेमचंद ने किया। इसका प्रकाशन 1919 में हुआ। इस उपन्यास में समाज की स्थिति और नारी के वेश्या बनने की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है तथा इस वेश्या समस्या के निराकरण के लिए ‘सेवासदन’ की स्थापना की जाती है। ‘सुमन’ इस उपन्यास की केन्द्रीय पात्र है। प्रेमचंद उपन्यासों में सिर्फ कथा नहीं कहते, कथा के बीच में किसी न किसी सामाजिक-राजनीतिक समस्या का चित्रण करते हैं। इसलिए कुछ आलोचक उन्हें समस्या प्रधान उपन्यासकार कहते हैं। उनके उपन्यासों के केन्द्र में चरित्र नहीं होते, वरन् कुछ ठोस समस्याएँ होती हैं। उनके पात्र उन समस्याओं को जीते हैं और उन पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। लेखक के रूप में प्रेमचंद भी उन समस्याओं पर अपना मत रखते हैं और उन समस्याओं को दूर करने के उपाय बताते हैं। यह उनके उपन्यासों का एक पक्ष है और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अलावा भी उनके उपन्यासों में सामाजिक जीवन, पात्र, घटनाएँ, उद्देश्य सब होते हैं, जो उस रचना को महत्वपूर्ण कलाकृति बनाते हैं।
‘सेवासदन’ की मुख्य समस्या भले ही वेश्या समस्या हो, परन्तु इसमें प्रेमचंद ने भारतीय परिवारों में स्त्री की स्थिति, स्त्री-पुरुष संबंधों की असमानता, दहेज जैसी परंपराएँ, मध्यवर्गीय जीवन के सामाजिक-राजनीतिक क्रियाकलाप आदि सभी का चित्रण किया है। इस उपन्यास की समीक्षा उस समय के महत्वपूर्ण आलोचक पद्म सिंह शर्मा और रामदास गौड़ ने की। हिंदी समाज ने उत्साहपूर्वक इस उपन्यास का स्वागत किया तथा उनके अगले उपन्यास की प्रतीक्षा करने लगा। अवध उपाध्याय प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास ‘सेवासदन’ को ही मानते हैं।
प्रेमाश्रम
‘सेवासदन’ के बाद किसान जीवन से संबंधित उपन्यास ‘प्रेमाश्रम’ (1922) में प्रकाशित हुआ। इसकी रचना असहयोग आंदोलन से पहले हो गई थी। असहयोग आंदोलन के पश्चात् प्रेमचंद के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया था। इसके बाद प्रेमचंद यह लिखते रहे कि अंग्रेजी राज किसानों का सबसे बड़ा शत्रु है। ‘प्रेमाश्रम’ में वे यह मानते हैं कि जमींदार वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। इस उपन्यास के मूल में जमींदारी समस्या है। इसमें ज्ञानशंकर और प्रेमशंकर दो पात्र हैं। ज्ञानशंकर जमींदार हैं तथा प्रेमशंकर जमींदारी से दूर हटकर किसानों के लिए प्रेमाश्रम की स्थापना करता है। इस उपन्यास का नायक कोई एक पात्र नहीं है, वरन् लखनपुर गाँव के सारे किसान इस उपन्यास के नायक हैं। उपन्यास के अंत में माया शंकर जमींदारी से इस्तीफा दे देता है और अब सभी किसान खुशहाल हैं। इसी में प्रेमचंद ने नए और पुराने जमींदारों की तुलना भी की है। नया जमींदार, जमींदारी को लाभ की दृष्टि से देखता है, जबकि पुराने जमींदार इसे प्रतिष्ठा और परंपरा की दृष्टि से देखते थे।
रंगभूमि
इसके बाद उनके उपन्यास ‘रंगभूमि’ का प्रकाशन हुआ। यह असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद लिखा गया तथा 1925 में प्रकाशित हुआ। इसे आलोचकों ने महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा दी। प्रेमचंद के जीवनी लेखक अमृतराय ने लिखा है कि यह पहला उपन्यास है जो पहले हिंदी में लिखा गया और बाद में इसका उर्दू रूपान्तरण प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास का केन्द्रीय पात्र नेत्रहीन (दिव्यांग) भिखारी सूरदास है। सूरदास की जमीन को उद्योगपति जॉन सेवक लेना चाहता है। सूरदास उससे सहमत नहीं होता। जमीन के बाद वह पाण्डेपुर की आवासीय जमीन और उसका झोंपड़ा भी लेना चाहता है। फिर संघर्ष होता है। आंदोलन होता है। इस आंदोलन में दो दल बन जाते हैं। राजा महेन्द्र प्रताप, अखबार वाले, सरकार सब जॉन सेवक का पक्ष लेते हैं। विनय और सोफिया, सूरदास का समर्थन करते हैं। अंत में सूरदास मारा जाता है। जॉन सेवक का कारखाना खुल जाता है। नगरीकरण की यह प्रक्रिया पूरी होती है। इन सबका प्रेमचंद ने विस्तार से चित्रण किया है। इसमें पहली बार एक अंग्रेज कलेक्टर मि-क्लार्क पात्र के रूप में आते हैं और वे साम्राज्यवादी नीति को स्पष्ट करते हैं कि सभी अंग्रेज भारत को अनन्त काल तक अपने अधीन रखना चाहते हैं जमींदार और राजा तभी तक अंग्रेज़ों के मित्र हैं, जब तक वे उनके साम्राज्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। उस समय के चर्चित आलोचक अवध उपाध्याय ने ‘सरस्वती’ पत्रिका में धारावाहिक रूप से यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि ‘रंगभूमि’ ‘वेनिटी फेयर’ का अनुवाद है।
निर्मला
‘रंगभूमि’ के पश्चात् प्रेमचंद ने ‘निर्मला’ उपन्यास की रचना की। यह उपन्यास ‘चाँद’ पत्रिका में नवम्बर, 1925 से नवम्बर 1926 तक प्रकाशित हुआ। इसमें दहेज प्रथा के कारण उत्पन्न बेमेल विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। यह नायिका प्रधान उपन्यास है और निर्मला इस उपन्यास की नायिका है। प्रेमचंद अपने उपन्यासों में स्त्री-पुरुष भेद की चर्चा अवश्य करते हैं तथा इस आधार पर स्त्री की पीड़ा का वर्णन करते हैं। यह ऐसा पहला उपन्यास है, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन का वर्णन नहीं किया गया है। आमतौर से प्रेमचंद किसान जीवन और स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण अवश्य करते हैं। इसमें बेमेल विवाह के कारण युवा नारी की “धीमी धीमी हत्या” होती है। इस कारण इस उपन्यास का अंत कारुणिक होता है। किसी तरह का आश्रम या आदर्शवादी आकांक्षा इस उपन्यास में नहीं है, जो उनके अब तक के उपन्यासों में रही है। ‘सेवासदन’ की सुमन अपने ढंग से प्रतिकार करती है और अंत में वेश्याओं के ‘सेवासदन’ में पहुँच जाती है। निर्मला कोई प्रतिकार नहीं करती। वह अपने यथार्थ को अपनी नियति मानकर अपना जीवन बिता लेती है।
कायाकल्प
इसके बाद उनका अपेक्षाकृत कमजोर उपन्यास ‘कायाकल्प’ प्रकाशित होता है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने सामाजिक-राजनीतिक जीवन के साथ अलौकिक-धार्मिक कल्पनाओं को भी चित्रित कर रखा है। इस तरह उपन्यास के दो केन्द्र हैं। एक केन्द्र में जगदीशपुर की रानी देवप्रिया का भोग विलास है। दूसरी के केन्द्र में चक्रधर है, जो इन दोनों कथाओं को जोड़ता है। पहले भाग में धर्म और विज्ञान तथा योग और भोग को मिलाकर चिर यौवन प्राप्त करने की आकांक्षा है। राजनीतिक कथा में साम्प्रदायिक दंगे तथा जन-जागरण की कथा है। ‘रंगभूमि’ में सूरदास की पराजय के बावजूद लेखक के मन में आशावाद बचा रहता है। ‘कायाकल्प’ में ऐसी कोई आशा नहीं है।
गबन
‘गबन’ उपन्यास के लेखन का प्रारम्भ सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले हो जाता है। तब प्रेमचंद स्त्रियों की आभूषण प्रियता की कहानी कहना प्रारम्भ करते हैं। कुछ दिनों तक यह कहानी चलती है। इस बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ हो जाता है। इस उपन्यास का नायक रमानाथ अविचारशील मध्यवर्गीय पात्र है। इसमें अंग्रेज सरकार द्वारा स्वाधीनता सेनानियों की प्रताड़ना का वर्णन भी किया गया है। प्रेमचंद के उपन्यासों में पुलिस अब तक अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप में आती है जो किसानों पर अत्याचार करने में जमींदारों का सहयोग करती है। परन्तु इस उपन्यास में पुलिस अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सामने आती है। पुलिस की प्रताड़ना के खिलाफ जन आक्रोश उमड़ता है। प्रेमचंद ने इस आक्रोश का सहानुभूति पूर्वक चित्रण करते हैं। उपन्यास की नायिका जालपा है, जिसका उपन्यास में चारित्रिक परिवर्तन और विकास होता है। आरम्भ में वह आभूषण प्रिय मध्यवर्गीय नारी है। बाद में वह ओजस्वी और क्रांतिकारी रूप सामने आती है और वह अपने प्रेरक व्यक्तित्व से अपने पति रमानाथ में साहस का संचार करती है। इसमें कुछ अन्य प्रभावशाली पात्र और कथाएँ भी हैं। इन पात्रों में देवीदीन खटिक, रतन, आदि मुख्य हैं। इसमें प्रेमचंद ने उस कानून को बदलने की वकालत भी की है जिसमें पति की मृत्यु के बाद सम्पत्ति पत्नी को नहीं मिल पाती थी। इस विषय पर प्रेमचंद ने लेख और कहानियाँ भी लिखी हैं।
कर्मभूमि
‘गबन’ के पश्चात् प्रेमचंद का महत्वाकांक्षी उपन्यास ‘कर्मभूमि’ प्रकाशित हुआ। आलोचकों का विचार है कि इस उपन्यास में प्रेमचंद ने ‘प्रेमाश्रम’ और ‘रंगभूमि की कथा भूमि को मिलाने का प्रयास किया है। अर्थात् इस उपन्यास में किसान जीवन और नगर में चलने वाले आंदोलन शामिल किए गए हैं। इस उपन्यास में पहली बार अंग्रेजी सिपाही आते हैं। वे मुन्नी का बलात्कार कर देते हैं। कुछ दिनों बाद मुन्नी उन अंग्रेज सिपाहियों का वध कर देती है। इस पर पुलिस मुन्नी को गिरफ्तार कर लेती है। मुन्नी के समर्थन में आंदोलन हो जाता है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने लगान बंदी आंदोलन का चित्रण किया है। इसी के साथ अछूतों (कर्मभूमि के संदर्भ में) के मन्दिर प्रवेश की समस्या आती है। यहाँ सवर्णों से टकराव होता है। इस आंदोलन का प्रमुख पात्र अमरकांत है इसके अलावा सुखदा, मुन्नी, डॉ. शान्ति कुमार, सकीना आदि हैं। उपन्यास में गाँव और शहर के आंदोलन मिल जाते हैं। यह उनमें भाग लेने वाले पात्रों के कारण सम्भव हो पाता है। सरकारी आंदोलन और आंदोलनकारियों के कारण आंदोलन असफल हो जाता है। सरकार और आंदोलनकारियों में एकता स्थापित हो जाती है जो प्रेमचंद के अनुसार क्षणिक है। ऐसा आंदोलन पुनः होगा। इस आंदोलन से और कोई फायदा हुआ हो यान हुआ, जनजागृति जरूर हुई है जो इस आंदोलन के बिना संभव नहीं थी। कलात्मक दृष्टि से यह प्रेमचंद का कमज़ोर उपन्यास है।
गोदान
प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास ‘गोदान’ है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र होरी और धनिया हैं, जो भारतीय किसान के प्रतिनिधि चरित्र हैं। होरी ढीला-ढाला और दब्बू पात्र है, लेकिन धनिया तेज-तर्रार है। होरी का बेटा गोबर शहर चला जाता है जहाँ वह मेहता और मालती के सम्पर्क में आता है। इस उपन्यास में राय साहब अमरपाल सिंह, झिंगुरी सिंह, पंडित दाता दीन, पटेश्वरी, बैंकर खन्ना आदि खल पात्र हैं। इसमें प्रेमचंद ने किसी आश्रम की स्थापना नहीं की, वरन् पूरी निर्भीकता से किसानों के शोषण की कथा कही है। होरी एक सीमान्त किसान है। वह धनी किसान नहीं है। गोदान में गाँव और शहर दोनों की कथाएँ साथ-साथ चलती हैं। कभी मिल जाती हैं और कभी अलग हो जाती हैं। उपन्यास की मूल कथा के साथ अनेक उपकथाएँ भी चलती रहती हैं, जो उपन्यास के अर्थ भूमि का विस्तार करती है।
प्रेमचंद अन्ततः किसानों के लेखक माने जाते हैं, हालाँकि उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों में सम्पूर्ण समाज का चित्रण करने का प्रयास किया है। प्रेमचंद साहित्य का समग्र विश्लेषण करते हुए कहा जा सकता है कि प्रेमचंद साहित्य की विषयवस्तु तो भारतीय किसान का जीवन है, लेकिन उनके साहित्य का पाठक शिक्षित मध्यवर्ग है। प्रेमचंद मध्यवर्ग को किसानों का पक्षधर बनाना चाहते हैं। उन्हें अपने गाँव की कहानी देहात से अनभिज्ञ पढ़े-लिखे पाठक को सुनानी है। इसलिए उनको एक तरफ तो यह ध्यान रखना पड़ता है कि पाठक के मानस पटल पर किसान जीवन का नक्शा उत्तर आए- जो न इतना अपरिचित हो कि शिक्षित वर्ग उससे तादात्म्य ही न कर पाए और न इतना परिचित हो कि शहरी जीवन से अलग उसकी पहचान ही न बन पाए। इस कहानी को प्रेमचंद इस तरह से सुनाते हैं, जिससे पढ़ने वाला किसानों का पक्षधर हो जाये। इसके साथ ही प्रेमचंद को अशिक्षित किसानों के भावों को भाषा में बाँधना है। अपढ़ जनता की बोली को पठनीय बनाना और उसके मूल भाव को बचाना बहुत ही कठिन काम है। प्रेमचंद इसमें पूरी तरह से सफल हुए हैं। उन्होंने किसानों की समस्याओं का वर्णन इस दृष्टि से किया है जिससे स्वाधीनता आंदोलन में मदद मिल सके। प्रेमचंद का अन्तिम अपूर्ण उपन्यास ‘मंगलसूत्र’ है, जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ।
प्रेमचंद का लेखन और उनके विचार निरंतर विकासमान थे। उनमें उन्होंने लगातार परिवर्तन किए। यदि वे और जवित रहते तो हम उनके विचारों को पूर्ण रूप से समझ पाते। इसलिए कई मुद्दों पर प्रेमचंद के विचार हमें अपर्याप्त लगते हैं। कहीं-कहीं अन्तर्विरोध भी दिखाई देता है। कहीं-कहीं हम आधुनिक दृष्टि से उनमें असंगति भी पाते हैं। तब भी निस्संदेह प्रेमचंद हिंदी उपन्यास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण हस्ती हैं।
प्रेमचंद का रचना वैशिष्ट्य
प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में युगान्तकारी परिवर्तन किया। उन्होंने अपने युग के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन के सूक्ष्म अध्ययन और अनुभव से प्रेरित होकर मानव चेतना, युगीन संघर्ष तथा मानवीय मन के भावों और विचारों को सरल, प्रवाहमय, सशक्त भाषा में प्रस्तुत किया।
प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्र
प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में मानव चरित्र का चित्रांकन करना ही श्रेष्ठ साधन माना है। अर्थात् वे उपन्यास के पात्रों द्वारा मानव मन की वास्तविकताओं को उद्घाटित करना चाहते हैं और इस कार्य में उन्हें पूर्ण सफलता मिली है। मानव चरित्र के यथार्थ चित्रण के लिए उन्होंने समाज के सभी वर्गों को बहुत निकट से देखा और उनका सूक्ष्म निरीक्षण किया। ज़मींदार, साहूकार, दरोगा, हाकिम, पटवारी, किसान आदि वर्गों की प्रवृत्ति को वे भली-भाँति जानते थे। चूँकि उनका जीवन ग्रामीण वातावरण से ही आरंभ हुआ इसीलिए स्वाभाविक रूप से वे ग्रामीण जीवन की विशेषताओं से परिचित थे। ग्रामीण जीवन के पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विविध रूपों को वे भली-भाँति जानते थे। परिस्थिति के अनुकूल मानव मन में क्या परिवर्तन होता है, व्यक्ति विशेष के आकार प्रकार, वेशभूषा, आचार-व्यवहार, बोली आदि का उन्होंने निरीक्षण किया था। यही कारण है कि वे पात्रों का यथार्थ चित्रण कर पाए। प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं।
i) अपने औपन्यासिक पात्रों की रचना उन्होंने तत्कालीन परिवेश अर्थात् उस युग के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के अनुकूल की।
ii) मज़दूरों और किसान वर्ग के पात्रों के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति थी। अतः इन वर्गों के पात्रों के प्रति सहानुभूति तथा शोषक वर्ग यानी ज़मींदार, और उनके मातहत काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी, ब्राह्मण वर्ग, सरकारी अफसर और कारिंदे आदि के प्रति आक्रोश व्यक्त किया।
iii) उनके संपूर्ण औपन्यासिक पात्रों को हम मोटे रूप से दो वर्गों में रख सकते हैं- (1) शोषक (2) शोषित। उन्होंने शोषितों की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है और शोषकों की कमजोरियों को उजागर किया है।
iv) उनके सभी पात्र सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुमन, निर्मला, सूरदास, राय साहब, खन्ना, होरी, धनिया, गोबर, सोफिया सभी सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधि हैं।
v) युगों से उपेक्षित नारी को पुरुष की सहयोगी और प्रेरक शक्ति के रूप में उपस्थित किया है। नारी पर हो रहे अत्याचार को दर्शाने के लिए उन्होंने सुमन, निर्मला, सुखदा, मालती, सुधा, जालपा, धनिया आदि की रचना की है। उनके नारी पात्र एक ओर सामान्य रूप से पुरुष की सहधर्मिणी हैं, तो दूसरी ओर परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव भी आता है। वह घर की चारदीवारी से बाहर आकर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में भी सहयोग देती है। प्रेमचंद ने नारी पात्रों में स्वाभाविक गुण-अवगुण का यथार्थ चित्रण किया है।
vi) प्रेमचंद के उपन्यासों में स्त्री-पुरुष दोनों को नायक-नायिका के रूप में रखा गया है। ‘गोदान’ में होरी नायक है, तो ‘सेवासदन’ में सुमन नायिका है।
इस प्रकार प्रेमचंद के सभी औपन्यासिक पात्र प्रायः समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित किए गए हैं। अधिकतर पात्र सजीव और सशक्त बन पड़े हैं। मानवीय चरित्र के सूक्ष्म चित्रण के कारण ही पात्र स्वाभाविक बने हैं।
प्रेमचंद के उपन्यासों में देशकाल
आप यह जान चुके हैं कि उपन्यास में वास्तविकता, स्वाभाविकता और सजीवता लाने के लिए देशकाल और वातावरण का सही चित्रण होना चाहिए। उपन्यासकार जिस देशकाल और वातावरण को अपने उपन्यास में स्थान देता है, उसका सही-सही ज्ञान भी उसे होना चाहिए। प्रेमचंद अपने युग के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी परिवेश को भली-भाँति जानते थे। यही कारण है कि उनके उपन्यासों में परिवेश का यथार्थ चित्रण हो पाया है। परिवेश का निर्माण पात्रों की वेशभूषा, शृंगार, कलाएँ, रहन-सहन, रीति-रिवाज, आचार-विचार, आहार-विहार, पर्व-उत्सव, भाषा आदि के समावेश से होता है। इन सभी बातों का समय और स्थान के अनुकूल चित्रण कर वे परिवेश में वास्तविकता लाते हैं। प्रेमचंद का साहित्य उनके युग के उतार-चढ़ाव तथा विविध राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का ऐतिहासिक दस्तावेज़ है। इनमें वर्ग-संघर्ष है, शोषणयुक्त समाज का चित्रण है, तत्कलीन समाज में व्याप्त पाखंड, धूर्तता, अन्याय, बलात्कार तथा अत्याचार से पीड़ित लोगों का चित्रण है। तत्कालीन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को उन्होंने रंगभूमि, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गबन आदि उपन्यासों में प्रमुख स्थान दिया। भारतीय समाज में व्याप्त एक बड़ी बुराई दलितों के साथ अमानुषिक व्यवहार को भी उन्होंने कथा का आधार बनाया। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन में प्रभाव और उनकी विचारधारा को भी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के द्वारा दर्शाया।
तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियाँ अंधविश्वास, वैमनस्य, बाह्य आडंबर, झूठी मान- मर्यादा आदि सभी का यथार्थ चित्रण किया गया है। गाँवों और शहरों दोनों को प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में स्थान दिया। नगर के वैभव, यातायात, मकान, कल-कारखाने आदि का चित्रण किया। गाँव के पशु-पक्षी, वन, उपवन, नदी-नाले, बाढ़, खेत खलिहान सभी का यथार्थ चित्रण किया।
पात्रों के क्रियाकलापों द्वारा परिवेश को तत्कालीन देशकाल के अनुकूल बनाया गया है। लेखक जिन बातों से भली-भाँति परिचित था उसे ही अपना वर्ण्य विषय बनाया है। पात्रों के झगड़े, चौपाल, टीका-टिप्पणी, सभी परिवेश के अनुकूल हैं। आप ‘निर्मला’ उपन्यास का अध्ययन करने की प्रक्रिया में इन्हीं विशेषताओं को देख सकेंगे।
प्रेमचंद के उपन्यासों की भाषा
भाषा उपन्यास का महत्त्वपूर्ण उपकरण है। यह भावों और विचारों के वहन का माध्यम है। लेखक कथा में स्वाभाविकता लाने के लिए भाषा को भी पात्र, घटनाएँ, देशकाल के अनुरूप रखता है। मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग कर भाषा में स्वाभाविकता लाता है। सरल, बोधगम्य और व्यवहारोपयोगी भाषा द्वारा ही लेखक अपनी बात पाठक तक पहुँचा सकता है।
प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में उपुर्यक्त बातों का ध्यान रखा है। उन्होंने व्यवहारोपयोगी, पात्रानुकूल तथा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। प्रेमचंद आरंभ में उर्दू लिखते थे इसीलिए हिंदी में लेखन कार्य करते हुए उर्दू के शब्दों का प्रयोग स्वभावतः आ गया है। प्रेमचंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए पं. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-
“भाषा में बंगला का अनुकरण केवल शब्दों और मुहावरों में ही नहीं, नामों और विचारों तक में किया जा रहा था। प्रेमचंद ने पहले-पहल इन काल्पनिक चौराहों को ठोकर मारकर तोड़ दिया, उन्होंने हिंदी को हर प्रकार से हिंदी किया। उन्होंने हिंदी उर्दू भेद को कम कर दिया और भाषा में नई प्राण शक्ति फूंँक दी।”
प्रेमचंद का औपन्यासिक शिल्प
आप जानते हैं कि प्रेमचंद से पहले के उपन्यासों में घटना प्रधान उपन्यासों की प्रधानता थी। विचित्र घटनाओं और नायक के अद्भुत कारनामों द्वारा पाठक का मनोरंजन किया जाता था। जीवन के यथार्थ से पहले के उपन्यास दूर थे। उपदेशात्मकता और कृत्रिम संवादों की भरमार होती थी। पात्रों में अस्वाभाविकता भरी होती थी। प्रेमचंद ने उपन्यास शिल्प को इनसे मुक्ति दिलायी। उन्होंने जीवन के यथार्थ को कथा का आधार बनाया, मानव जीवन के दैनिक क्रियाकलापों और घटनाओं की वास्तविकताओं को कथा में स्थान दिया। घटनाओं को कार्य कारण की श्रृंखला से जोड़ा। पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण कर उन्हें सजीव बनाया। पात्रों के कार्य और परिस्थिति में संबंध स्थापित किया। समग्र रूप से उन्होंने औपन्यासिक शिल्प को अवास्तविकता की जगह यथार्थवादी और व्यावहारिक रूप प्रदान किया। संवाद को दैनिक जीवन के वार्तालाप जैसा बनाया और जीवन को एक निश्चित दृष्टि दी। प्रेमचंद की साहित्यिक रचनाओं में शैली की भिन्नता पाई जाती है। उन्होंने वर्णनात्मक, आलंकारिक, चित्रात्मक और व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है।
प्रेमचंद के उपन्यासों की सोद्देश्यता
रचनाकार अपनी रचना किसी न किसी उद्देश्य से रचता है। उपन्यास विधा मानव जीवन के चित्र को विस्तृत रूप में उपस्थित करने का सशक्त माध्यम है। स्वयं प्रेमचंद उपन्यास को मानव जीवन को व्याख्यायित करने का सशक्त माध्यम मानते हैं।
हिंदी के प्रेमचंद-पूर्व उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना था। प्रेमचंद ने सर्वप्रथम उपन्यासों के माध्यम से जीवन दर्शन प्रस्तुत किया। उनके उपन्यासों के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छिपा हुआ है। उपन्यास के माध्यम से यथार्थ परिवेश में जीवन को रखकर सामाजिक पात्रों की सबलता-दुर्बलता का चित्रण किया गया है। उनके उपन्यासों में युग चेतना प्रतिबिंबित हुई है। तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण किया गया है।
प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ने के बाद ऊपरी तौर पर यह बात स्पष्ट होती है कि उन्होंने युग की समस्याओं को ही प्रमुखता दी। लेकिन गहराई से अध्ययन करने पर यह बात भी स्पष्ट होती है कि उन्होंने तत्कालीन प्रासंगिकता के साथ-साथ मानव जीवन की शाश्वत समस्याओं को भी प्रस्तुत किया है। वे शोषण के खिलाफ मानवीय संघर्ष को ही प्रस्तुत करना चाहते हैं। उपन्यास ही नहीं उनके समग्र साहित्यिक रचनाओं के विश्लेषण से यह बात स्पष्ट होती है कि उन्होंने सामाजिक स्तर पर जीवन की विविधताओं का चित्रण किया। घिसी-पिटी परंपराओं की जगह नवीन मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया। मानव के अंदर स्वाभाविक रूप से आदर्श की ओर बढ़ने की भावना को उन्होंने प्रमुख स्थान दिया। उनके उपन्यासों का अध्ययन करने के बाद यह भी पता चलता है कि मध्यवर्ग तथा निम्न वर्ग की सामाजिक विशेषताओं का विश्लेशण करना भी उनका उद्देश्य था। मानव की सबलताओं और दुर्बलताओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना भीउसका उद्देश्य था। प्रेमचंद ने अपने उन उपन्यासों में भी जिनमें उन्होंने तत्कालीन भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रमुख स्थान दिया है, मानव में सवृत्ति के द्वारा संघर्ष पर विजय प्राप्त करने की प्रवृत्ति को ही प्रमुख स्थान दिया है।
इस प्रकार समग्र रूप से प्रेमचंद हिंदी साहित्य की उन विभूतियों में से थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य को विश्व स्तर की ऊँचाई तक पहुँचाया।
प्रेमचंद के समकालीन जयशंकर प्रसाद के उपन्यास में भावात्मकता और अंतःसंघर्ष पर विशेष जोर दिया गया। प्रेमचंद ने शिल्प आदि की दृष्टि से हिंदी उपन्यास में जो आदर्श उपस्थित किया, उसका पालन बाद के उपन्यासकारों ने भी किया। भगवतीचरण वर्मा, यशपाल, उपेन्द्रनाथ अश्क, नागार्जुन के उपन्यासों में प्रेमचंद के शिल्प का ही विकास दृष्टिगत होता है।