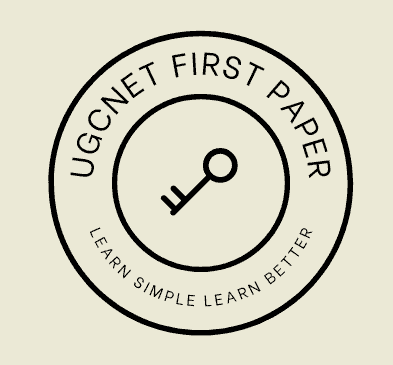Credit : nios
मुद्रा और बंध (MUDRA AUR BANDHA IN YOGA)
मुद्रा और बंध के अभ्यास को आसन और प्राणायाम के अभ्यास से अधिक प्रभावशाली माना गया है। अतः वे लोग जो आसन और प्राणायाम करने में असमर्थ हैं वे अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मुद्रा और बंध से लाभ उठा सकते हैं। योग में, इन्हें प्राण ऊर्जा अर्थात् प्राणाधार ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है
मुद्रा और बंध मन में स्थिरता लाते हैं। वे आसनों की तुलना में बहुत गहरे और सूक्ष्म स्तर पर काम करते हैं। वे तत्वों को संतुलित करते हैं और अंगों के स्तर पर जागरूकता विकसित करते हैं। वे कोशिकाओं को शुद्ध करते हैं और अंगों को साफ करते हैं। मुद्रा एक विशेष आसन है जो ऊर्जा को विशेष चक्रों (प्लेक्सस) में प्रवाहित करता है और बदले में उन अंगों को प्रभावित करता है जिनसे यह जुड़ा होता है। बंध का मतलब है ताला(lock)। इसमें मांसपेशियों और अंगों का संकुचन होता है जिससे ऊर्जा एक विशेष प्लेक्सस(चक्र)में जमा(concentrate )होती है। योग ग्रंथ, घेरंड संहिता में 26 मुद्राएँ दी गई हैं। शिव संहिता में 11 और मुद्राओं की व्याख्या की गई है । सामान्यत: हमारे पास अपने अंगों पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन एक उन्नत हठ योग अभ्यासी इन तकनीकों के माध्यम से अपने अंगों के कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए, खेचरी मुद्रा के लाभों में से एक थायरॉयड ग्रंथि और T3 और T4 हार्मोन के उत्पादन को नियंत्रित और विनियमित करना है जो चयापचय दर को प्रभावित करते हैं।
कुछ मुद्राएँ और बंध आसन और प्राणायाम के साथ किए जाते हैं जबकि अन्य का अभ्यास अलग-अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए, विपरीत करणी मुद्रा, पीठ को फर्श से 45 डिग्री कोण पर रखकर किया जाने वाला एक कंधे का स्टैंड है। इसे सर्वांगासन, सीधे कंधे के स्टैंड से पहले आसनों के क्रम में अभ्यास किया जाना चाहिए। यह थायरॉयड को उत्तेजित करता है और विशुद्धाख्याचक्र (ग्रसनी जाल) को शुद्ध करता है। इसी तरह, उड्डियान बंध, प्राणायाम के क्रम में अभ्यास किया जाता है। इसमें तेजी से श्वास छोड़ना और श्वास को रोकना शामिल है, जबकि पेट को पीछे खींचना और श्वास लेने की आवश्यकता होने तक इसे अंदर रखना शामिल है। खेचरी मुद्रा, जिसमें जिह्वा को पीछे मोड़कर तालु मूल में लगाना शामिल है, आसन और प्राणायाम के बाद किया जाता है।
जैसा कि हठ योग में हमेशा होता है, इन तकनीकों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऊर्जा का प्रवाह रीढ़ के आधार से लेकर सिर के शिखर तक ऊपर की ओर हो।
हठयोग प्रदीपिका में 10 मुद्राओं का उल्लेख कर उनके अभ्यास पर जोर दिया गया है। ये हैं-
महामुद्रा महाबंधो महावेधश्च खेचरी। उड्यानं मूलबंधश्च बंधो जालंधराभिश्चः ।।
करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्तिशालनम। इंद हि मुद्रादशकं जरामरणनाशनम ।।
अर्थात्- महामुद्रा, महाबंध, महावेधश्च, खेचरी, उड्डियान बंध, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्तिचालन- ये दस मुद्राएं जरामरण को नष्ट करने वाली एवं दिव्य ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाली हैं। अर्थात् 4 बंध और 6 मुद्राएंँ हुईं, लेकिन इनके अलावा भी अन्य कई बंध और मुद्राओं का उल्लेख मिलता है।
अलग-अलग ग्रंथों के अनुसार अलग-अलग मुद्राएं और बंध होते हैं। योगमुद्रा को कुछ योगाचार्यों ने ‘मुद्रा’ के और कुछ ने ‘आसनों’ के समूह में रखा है। दो मुद्राओं को विशेष रूप से कुंडलिनी जागरण में उपयोगी माना गया है- शांभवी मुद्रा और खेचरी मुद्रा।
मुख्यतः 5 बंध हैं :
1. मूलबंध,
2. उड्डियान बंध
3. जालंधर बंध,
4. बंधत्रय (जब तीनों एक साथ लगाये जाते हैं)और
5. महाबंध।
मुख्यतः 6 आसन मुद्राएं हैं- 1. वज्रासन या वज्रमुद्रा, 2. अश्विनी मुद्रा, 3. महामुद्रा, 4. योगमुद्रा, 5. विपरीत करणी मुद्रा, 6. शांँभवी मुद्रा। जगतगुरु रामानंद स्वामी पंच मुद्राओं को भी राजयोग का साधन मानते हैं, ये है- 1. चाचरी, 2. खेचरी, 3. भूचरी, 4. अगोचरी, 5. उन्मनी मुद्रा।
मुख्यतः दस हस्त मुद्राएंँ: उक्त के अलावा हस्त मुद्राओं में प्रमुख दस मुद्राओं का महत्व है। जो निम्न हैं: -(1) ज्ञान मुद्रा, (2) पृथ्वि मुद्रा, (3) वरुण मुद्रा, (4) वायु मुद्रा, (5) शून्य मुद्रा, (6) सूर्य मुद्रा, (7) प्राण मुद्रा, (8) अपान मुद्रा, (9) अपान वायु मुद्रा, (10) लिंग मुद्रा।
अन्य मुद्राएं : (1) सुरभी मुद्रा, (2) ब्रह्ममुद्रा, (3) अभयमुद्रा, (4) भूमि मुद्रा, (5) भूमि स्पर्शमुद्रा,
(6) धर्मचक्रमुद्रा, (7) वज्रमुद्रा, (8) वितर्कमुद्रा, (9) जनाना मुद्रा, (10) कर्णमुद्रा, (11) शरणागतमुद्रा, (12) ध्यान मुद्रा, (13) सुची मुद्रा, (14) ओम मुद्रा, (15) जनाना और चीन मुद्रा, (16) अंगुलियां मुद्रा (17) महात्रिक मुद्रा, (18) कुबेर मुद्रा (19) चीन मुद्रा, (20) वरद मुद्रा, (21) मकर मुद्रा, (22) शंख मुद्रा, (23) रुद्र मुद्रा, (24) पुष्पपूत मुद्रा (25) वज्र मुद्रा, (26) हास्य बुद्धा मुद्रा, (27) प्रणाम मुद्रा, (28) गणेश मुद्रा (29) मातंगी मुद्रा, (30) गरुड़ मुद्रा, (31) कुंडलिनी मुद्रा, (32) शिव लिंग मुद्रा, (33) ब्रह्मा मुद्रा, (34) मुकुल मुद्रा (35) महर्षि मुद्रा, (36) योनी मुद्रा, (37) पुशन मुद्रा, (38) कालेश्वर मुद्रा, (39) गूढ़ मुद्रा, (40) बतख मुद्रा, (40) कमल मुद्रा, (41) योग मुद्रा, (42) विषहरण मुद्रा, (43) आकाश मुद्रा, (44) हृदय मुद्रा, (45) जाल मुद्रा, (46) पाचन मुद्रा, (47). शाम्भवी मुद्रा (48) अश्विनी मुद्रा आदि।
मुद्राओं के लाभ :
कुंडलिनी या ऊर्जा स्रोत को जाग्रत करने के लिए मुद्राओं का अभ्यास सहायक सिद्ध होता है। कुछ मुद्रओं के अभ्यास से आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त की जा सकती है। इससे योगानुसार अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों की प्राप्ति संभव है। यह संपूर्ण योग का सार स्वरूप है।
https://www.nios.ac.in/media/documents/373_Hindi/lesson-22.pdf
मुद्रा का अर्थ
योग के अंतर्गत मुद्रा एक प्रतीकात्मक संकेत है। मुद्रा शब्द का संस्कृत अर्थ है- संकेत’, ‘चिह्न’ या मुहर’। योग और ध्यान में मुद्राओं को आमतौर पर हाथों के आसनों के रूप में जाना जाता है, ऐसा माना जाता है कि मानसिक विकारों और ऊर्जा के द्वार को साफ करते हुए ये शरीर और चक्रों में ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करती हैं।
मुद्राओं के विभिन्न प्रकार हैं और प्रत्येक प्रकार का शरीर और मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव पड़ता है। हालाँकि हाथों की मुद्राएँ योग में सबसे सामान्य रूप में जानी जाती हैं वहीं मुख, अन्य हावभाव, बंध और अन्य मुद्राएँ भी महत्वपूर्ण हैं। मुद्राओं के प्रयोग से संबंधित मुख्य ग्रंथ हठयोग प्रदीपिका और घेरंड संहिता हैं। हठ योग प्रदीपिका में 10 मुद्राओं का वर्णन है वहीं घेरंड संहिता में 25 मुद्राओं का वर्णन मिलता है।.
22.1.1 योग मुद्राओं का महत्त्व
सामान्य रूप में योग को आसनों (शरीर खींचने के लिए) और श्वास लेने की तकनीकों (शांति और आराम के लिए) का संयोग माना जाता है। आसन शरीर के सभी तंत्रों को प्रभावित करता है जबकि प्राणायाम शरीर और मस्तिष्क के मध्य संबंध को जागृत करता है।
1. यह शरीर में प्राणों के प्रवाह में मदद करती है यदि इसे यौगिक श्वास अभ्यासों के साथ किया जाए।
2. यह मस्तिष्क के साथ संबंध स्थापित करता है।
3. यह संवेदी अंगों, ग्रंथियों, शिराओं और कंडराओं में परिवर्तन लाता है।
4. मुद्राओं के प्रयोग से ऊर्जा के प्रवाह में सामंजस्य पैदा होता है जो वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि पंचतत्वों के संतुलन को सिद्ध करती हैं।
5. मुद्रा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए किया जाने वाला प्रयास है।
22.2 मुद्रा के प्रकार
हस्त मुद्रा :
हमारा अच्छा स्वास्थ्य हमारे हाथ की उंगलियों से नियंत्रित होता है क्योंकि उंगलियाँ महत्वपूर्ण विद्युत परिपथ (Electric Cerquits)हैं। यह ऊर्जा के प्रवाह में संतुलन स्थापित करता है। हाथ की उंगलियों को विभिन्न स्थानों पर छूना हस्त मुद्रा कहलाता है।
हस्त मुद्रा को शरीर के पाँच मुख्य तत्त्वों में संतुलन स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रत्येक उंगली एक तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ये तत्व इस प्रकार हैं-
चित्र 22.1- तत्वों को दर्शाती उंगलियाँ
1. अंगूठा- अग्नि तत्व
2. तर्जनी उँगली -वायु तत्व
3. मध्यमा- आकाश तत्व
4. अनामिका- पृथ्वी तत्व
5. सबसे छोटी उँगली(कनिष्ठिका)- जल तत्व।
ज्ञान मुद्रा –
यह हस्त मुद्राओं में से सबसे प्रचलित मुद्रा है।
इसमें सभी प्रकार के अभ्यासों जैसे ध्यान, पूजा, चिकित्सा, नृत्य आदि का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत शब्द “ज्ञान” जिसका अर्थ है परम ज्ञान, इसे ज्ञान की मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इस मुद्रा का अभ्यास हमारे मस्तिष्क को मजबूत अधिक सक्षम बनाता है।
विधि
1. ध्यान लगाने के लिए बैठें, अपने शरीर को आराम दें और सीधे (रीढ़ को सीधा रखें)बैठें।
2. अपने दोनों हाथों को जोड़ कर अपने घुटनों के सामने लाएँ और अपने अँगूठे और तर्जनी उँगली के अग्रभाग को मिला दें।
3. अग्रभाग को त्वचा से छुएँ न कि नाखूनों से। अन्य उँगलियों को सीधा और आरामदायक स्थिति में रखें।
लाभ-
1. यह मुद्रा हमारे शरीर के वायु तत्व को उत्तेजित करती है और हमारे मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करती है।
2. यह एकाग्रता बढ़ाने में मदद करती है और मंदता (सुस्ती), निष्क्रियता और उत्साह की कमी, लापरवाही, सर्जनात्मकता की कमी और स्मरण करने में आने वाली समस्याओं से निजात दिलाती है।
3. मानसिक रोगों व अन्य तंत्रिका तंत्र संबंधी रोगों से ग्रस्त लागों को इससे लाभ पहुँचता है।
4. यह अवट्ट अल्पक्रियता (हाइपोथायरायडिज्म), अल्पपरावटुता, अल्प अधिवृक्कता, पीयूषिका अल्पक्रियता के रोगों को कम करने में मदद करता है।
अवधि
ज्ञान मुद्रा का सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए इसका प्रतिदिन 30 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। आप इसे किसी भी स्थान व समय पर कर सकते हैं। शीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए इसे प्रातःकाल ध्यान की मुद्रा में करना चाहिए।
सावधानियाँः
1. योग शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना गर्भवती स्त्रियों को लंबे समय तक इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए।
वायु मुद्रा :
1. अब अपने अँगूठे को अंदर की ओर मोड़ें ताकि यह तर्जनी उँगली को हल्का-सा दबा सके।
2. अन्य उँगलियाँ सीधी होनी चाहिए।
3. इसे बैठ कर किसी भी मुद्रा में किया जा सकता है, आमतौर पर इसे ध्यान की मुद्रा में किया जाता है।
लाभ :
1. इससे शरीर में वायु के संतुलन को स्थापित करने में मदद मिलती है।
Fig.22.3: Vayu Mudra
2. यह पेट फूलने और जोड़ों के दर्द की समस्याओं को हल करने में मदद करता है।
3. यदि किसी को भोजन के पश्चात बैचेनी हो रही हो, तब इसे वज्र आसन में करना चाहिए।
4. पार्किंसन रोग यानी अंग कंपन के रोग को कम करने में सहायता प्रदान करता है।
5. यह चिंता और बेचैनी को कम करने में मदद करता है।
6. यह हार्मोनल असंतुलन को कम करने में मदद करता है।
अवधि
इसका अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए 30-45 तक अभ्यास करना चाहिए। शीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए इसे प्रातःकाल ध्यान मुद्रा में किया जाना चाहिए।
सावधानियाँ
1. दर्द से राहत मिलने के बाद इस मुद्रा से बाहर आ जाना चाहिए। दर्द से राहत मिलने के बाद इसे लंबे समय के लिए करना लाभकारी नहीं होगा।
सूर्य मुद्रा :
यह हस्त मुद्रा की सबसे प्रचलित मुद्राओं में से एक है। इस मुद्रा का अभ्यास शरीर से पृथ्वी तत्व को कम करने में उपयोगी है।
विधि :
1. इसे ध्यान की किसी भी मुद्रा में किया जा सकता है।
2. अनामिका के अग्र भाग को अंगूठे के तल पर रखें।
आकृति 22.4 सूर्य मुद्रा
3. इस उंगली पर अंगूठे से हल्का-सा दबाव बनाएँ।
लाभः
1. इससे शरीर का रूखापन समाप्त होता है।
2. यह थाइराइड ग्रंथि की निष्क्रियता में लाभकारी है।
3. यह अधिक वजन और मोटापे को कम करने में लाभकारी है।
4. यह भूख न लगने की समस्या से निजात पाने के लिए लाभकारी है।
5. यह पाचन की समस्याओं जैसे कब्ज, अपच आदि में लाभकारी है।
6. यह कम या पसीना न आने की समस्या में लाभकारी है।
7. आँखों व नज़र की समस्याओं को ठीक करने में लाभकारी है।
अवधि
इसका अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 30 मिनट तक निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अत्याधिक लाभ अर्जित करने के लिए इसे प्रातःकाल और ध्यान की मुद्रा में करना चाहिए।
सावधानियाँ
1. उच्च रक्तचाप होने की स्थिति में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए।
लिंग मुद्रा :
लिंग मुद्रा शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाने में मदद करती है।
चित्र- 22.5 लिंग मुद्रा
विधि :
1. ध्यान की मुद्रा में बैठें।
2. अब बाएँ अंगूठे को उठाते हुए दोनों हथेलियों को मिला लें।
लाभ :
1. यह शरीर में अत्याधिक वसा को कम करता है जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है।
2. इससे शरीर में गरमी आती है जिससे जुकाम और इससे संबंधित रोग जैसे वायुविवरशोथ की समस्या और बलगम वाली खाँसी एवं चिपचिपे मल की समस्या से निजात मिलती है।
3. दमा और अन्य श्वास संबंधी समस्याओं में लाभकारी है।
अवधि :
इसका अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 30 मिनट का नियमित अभ्यास करना चाहिए। इस मुद्रा का प्रयोग केवल आवश्यकता होने पर ही करना चाहिए।
सावधानियाँ
1. इसका अभ्यास बुखार या पित्त प्रकृति के होने पर नहीं करना चाहिए।
2. इसे अधिक समय तक नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
पृथ्वी मुद्रा :
संस्कृत शब्द पृथ्वी का अर्थ है विशाल।
यह मुद्रा शरीर में पृथ्वी के तत्व को बढ़ाने और अग्नि के तत्व को कम करने में सहायक है।
चित्र- 22.6 पृथ्वी मुद्रा
विधि :
1. किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठें।
2. अनामिका के अग्र भाग तथा अगूंठे को हलका दबाव बनाते हुए छुएँ।
लाभ –
1. यह शरीर में बल और धैर्य को बढ़ाता है।
2. पतले लोगों के लिए यह मुद्रा अत्याधिक लाभकारी है।
3. इसका अभ्यास अल्सर और जलन से निजात दिलाता है।
4. यह पीलिया और बुखार में लाभकारी है।
अवधि :
इसका लाभ प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से 30-45 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। आप इसे प्रातःकाल में किसी भी स्थान पर कहीं भी कर सकते है या जब आप ध्यान की मुद्रा में हो तो इसे करना सर्वश्रेष्ठ रहता है।
सावधानियाँ :
1. कफ दोष प्रकृति के व्यक्तियों को इसे कम समय के लिए करना चाहिए।
प्राण मुद्रा :
प्राण शब्द का अर्थ है- जीवन। प्राण मुद्रा का अभ्यास शरीर की पाँच मुद्राओं को शक्ति प्रदान करता है।
विधि
1. ध्यान की मुद्रा में बैठें।
2. सबसे छोटी उंगली, अनामिका और अँगूठे के अग्रभाग को हल्का-सा दबाते हुए छुएँ।
चित्र- 22.7 प्राण मुद्रा लाभः
1. यह प्राणिक ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोगी है।
2. यह गर्मी के तनाव, सूजन संबंधी विकार, नींद न आना, उच्च रक्तचाप, मुँह, गले और पेट में जलन को सहन करने में भी उपयोगी है।
अवधिः
अच्छा परिणाम पाने के लिए 30-45 मिनट का नियमित अभ्यास किसी भी समय या किसी भी स्थिति में किया जा सकता है लेकिन सुबह का समय सबसे अच्छा समय है और 45 मिनट के अभ्यास के बीच में एक ब्रेक लिया जा सकता है।
सावधानियाँ
1. खांसी और जुकाम की स्थिति में इसे थोडे समय के लिए ही करना चाहिए।
वरुण मुद्रा :
शरीर में जल तत्व को बढ़ाने वाली है वरुण मुद्रा इसलिए इसे जल-वर्धन मुद्रा भी कहा जाता है।
विधि
1. किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठें
2. छोटी उंगली और अंगूठे की युक्तियों को स्पर्श करें हल्का दबाए।
लाभ :
चित्र 22.8: वरुण मुद्रा
1. रूखेपन को हटाता है।
2. त्वचा और रक्त की अशुदधियों से निजात।
3. निर्जलीकरण
अवधि
अच्छे परिणामों की प्राप्ति हेतु नियमित रूप से 30 मिनट तक अभ्यास करें। वैसे तो इसे कभी भी किसी भी मुद्रा में किया जा सकता है परंतु प्रातःकाल का समय सर्वश्रेष्ठ है। 30 मिनट के भीतर इसमें थोड़ा विराम भी दिया सकता है।
सावधानियाँ
शरीर में मोटापे और सूजन की समस्या हो तो इसका अभ्यास नहीं किया जाना चाहिए।
पाठगत प्रश्न 22.2
अ) मिलान कीजिएः
1. अँगूठा क. जल
2. तर्जनी ख. अग्नि
3. मध्यमा ग. आकाश
4. अनामिका घ. पृथ्वी
5. सबसे छोटी उँगली ड. वायु
ब) उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएः
1. हस्त मुद्राओं में से सबसे प्रचलित मुद्रा …. है।
2. ………शरीर में वायु को संतुलित करने में मदद करता है।
3. ज्ञान मुद्रा के अंतर्गत ……….. भागों को मिलाया जाता है। और उँगलियों के अग्र
4. अनामिका के अग्र भाग को अँगूठे के तल पर दबाने का अभ्यास ……….. मुद्रा के अंतर्गत किया जाता है।
5. ……….. और मुद्राएँ मोटापा और वजन कम करने के लिए की जाती हैं।
6. ………..मुद्रा कमज़ोर और पतले व्यक्ति के लिए लाभकारी है।
7. वरुण मुद्रा और ……….. के लिए लाभकारी है।
8. किसी भी मुद्रा का अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए न्यूनतम……….. मिनटों का अभ्यास आवश्यक है।
22.2.1 आसन मुद्रा
वे मुद्राएँ जिन्हें आसनों की तरह किया जाता है, आसन मुद्राएँ कहलाती हैं।
महा मुद्रा
चित्र 22.9 महा मुद्रा
विधि
1. टांगों को सामने की ओर खींचते हुए ज़मीन पर बैठें। बाई टांग को मोड़ें और बाईं एड़ी से सीवन (मूलाधार) को दबाएँ।
2. अभ्यास के दौरान दाईं टांग को खींच कर रखें।
3. आगे की ओर झुकें और दाईं टांग के पंजे को हाथ से पकड़ें। आगे की ओर झुकते हुए श्वास बाहर छोड़ें।
4. अपने सिर को ऊपर की ओर उठाएँ और दोनों आँखों को भौहों के मध्य पर ले जाएँ। धीरे और गहरी श्वास लें।
5. अपनी श्वास को अंदर ही रोकें और मूल बंध करें।
6. अपने गले को सिकोड़ लें ताकि वायु फेफड़ों से बाहर न जा सके।
7. श्वास को अंदर रोकते हुए (अंतर कुम्भक) इस मुद्रा में जितनी देर आराम से रह सकें, रहने का प्रयास करें।
8. यह एक चक्र है। एक व्यक्ति 3 से 12 चक्रों तक अभ्यास कर सकता है।
9. इस मुद्रा को छोड़ते समय, श्वास धीरे से बाहर छोड़ें और सिर को सामान्य स्थिति में ले आएँ। अपने पैरों को खींचे, शरीर को आराम दें और सामान्य ढंग से श्वास लें।
10. समान पद्धति को दूसरी टांग के साथ भी करें।
11. इस अभ्यास के दौरान पूरा ध्यान भौहों के केंद्र पर रहेगा।
लाभः
1. महा मुद्रा अपच, पीड़ा और पेट के विकारों का उपचार करता है।
2. यह त्वचा रोगों को ठीक करने में मदद करता है।
3. यह शरीर में विषैले पदार्थों को निष्प्रभावी करने में मदद करता है।
4. इससे शांति का एहसास होता है और यह एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है।
5. यह अभ्यास रीढ़ को सीधा रखता है और मूलाधार और विशुद्धि चक्र के बीच में जाने के लिए प्राणिक ऊर्जा का प्रसार करता है।
सावधानियाँ
1. इसे गर्भावस्था, उच्च रक्तचाप, नेत्र व हृदय रोग होने पर नहीं करना चाहिए।
2. यदि हाल ही में शल्यचिकित्सा हुई है तो इसे नहीं करना चाहिए।
विपरीत करणी मुद्रा :
चित्र 22.10: विपरीत करणी मुद्रा
विधि :
1. सीधे चित पीठ के बल आराम से लेट जाएँ। अपने हाथों को जमीन पर शरीर के साथ रखें और सामान्य ढंग से श्वास लें।
2. अब अपनी टांगें जमीन से 90 डिग्री तक धीरे-धीरे ऊपर उठाएँ।
3. अब अपने हाथों को नाभि के स्तर पर पीठ के निचले भाग के नीचे रखें। अपने शरीर को ऊपर उठाने के लिए हाथों और कोहनियों का सहारा लें।
4. जब आप अपने शरीर को सीधा कर रहे हों तब श्वास अंदर लें।
5. शरीर को ऊपर उठाने के लिए अपने हाथों का सहारा लें जब तक कि पूरा धड़ जमीन से 45 डिग्री ऊपर न उठ जाए और टांगें सीधी न हो जाएँ। इस अवस्था में शरीर का पूरा भार कंधों पर रहता है। हाथ और कोहनियों से ही शरीर को सहारा मिलता है और संतुलन स्थापित होता है।
6. अंतिम मुद्रा में टांगें जमीन के साथ 90 डिग्री पर और धड़ जमीन के साथ 45 डिग्री पर हो।
7. ऊपर उठी हुई स्थिर अवस्था में सामान्य ढंग से श्वास लेते रहें।
8. इस अवस्था को छोड़ते हुए, श्वास अंदर ही रखें और शरीर को धीरे-धीरे चित अवस्था में वापस ले आएँ।
9. विपरीत करणी मुद्रा को करने के बाद; मत्यासान, उष्ट्रासन या सुप्तासन जैसे प्रतिआसन किए जाते हैं।
लाभः
1. यह थाइराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है।
2. यह अन्य अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के कार्यों को संतुलित करता है।
3. यह मुद्रा बवासीर, अंडकोष वृद्धि और हर्निया की समस्या में फायदेमंद होती है।
4. यह पाचन तंत्र के कार्यों को अच्छा करती है।
सावधानियाँ-
1. इस मुद्रा को माहवारी, गर्भावस्था, उच्च रक्त चाप, हृदय रोगों, नेत्र रोगों और कब्ज होने की स्थिति में नहीं करना चाहिए।
2. यदि आपको पैरों या टांगों में सिहरन महसूस हो, तो तुरंत बैठ जाएँ।
अश्विनी मुद्रा :
गुदाद्वारा को बार-बार सिकोड़ने और फैलाने की क्रिया को ही अश्विनी मुद्रा कहते हैं।
विधि :
1. अश्विनी मुद्रा के लिए पद्मासन , सिद्धासन, वज्रासन या सुखासन में बैठना चाहिए।
2. एक बार मुद्रा में आ जाने के बाद, एक मिनट का आराम करें, मुक्त रूप से गहरी श्वास लें। फिर पूरी तरह से श्वास अंदर लें, अपनी श्वास को रोके रखें और 2 सेकेंड के अंतराल पर गुदाद्वार को सिकोड़ें।
3. अपनी ठोड़ी को गर्दन के नीचे दबाएँ, अपनी जीभ के अग्रभाग से अपने तालु को छुएँ और श्वास बाहर छोड़ना आरंभ करें, फिर मुद्रा को छोड़ें और फिर धीरे से अपना सिर ऊपर करें।
लाभ
1. यह प्रजननीय और पाचन संबंधी अंगों सहित पेट और पेडू को संतुलित रखता है।
2. यह सरल अभ्यास आपको कब्ज से राहत दिलाता है, मलाशय और बवासीर संबंधी रोगों को दूर करता है और यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।
सावधानी :
1. इसे गर्भावस्था के दौरान न करें।
2. इसे मलद्वार संबंधी शल्य चिकित्सा के बाद नहीं करना चाहिए।
पाठगत प्रश्न 22.3
अ. उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:
1. मुद्राएँ जिन्हें आसनों की तरह किया जाता है …….
कहलाती हैं।
2. अभ्यास के दौरान…….. मुद्रा में, ध्यान भौहों के मध्य में होता है।।
3. विपरीत करणी मुद्रा की अंतिम अवस्था में, टांगें हैं और धड़ …….डिग्री पर। डिग्री पर होती
ब. निम्नलिखित कथनों को सत्य या असत्य के रूप में चिह्नित कीजिए।
1. विपरीत करणी मुद्रा को करने के बाद, उसके प्रतिआसन जैसे मत्यासन, उष्ट्रासन या सुप्त वज्रासन को किया जाता है।
2. गुदाद्वारा को बार-बार सिकोड़ने और फैलाने की क्रिया को ही अश्विनी मुद्रा कहते हैं।
3. विपरीत करणी मुद्रा से यौन स्वास्थ्य बेहतर होता है।
मुख मुद्रा
जो मुद्राएँ मुँह से की जाती हैं, उन्हें मुख मुद्रा कहा जाता है। शांभवी, काकी मुद्रा, मुख मुद्रा के अंतर्गत आती है।
शांभवी मुद्रा :
भौहों के मध्य भृकुटि पर, ध्यान और ज्ञान मुद्रा में बैठने को शांभवी मुद्रा कहते हैं। ध्यान के लिए शांभवी मुद्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
चित्र 22:11 शाम्भवी मुद्रा
विधि
1. किसी भी ध्यान की मुद्रा में बैठें जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन या स्वस्तिक आसन।
2. ज्ञान मुद्रा सहित अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखें। 3. अपनी दोनों आँखों को घुमाते हुए ऊपर की ओर ले जाएँ और भौहों के मध्य भृकुटि की ओर देखें। इससे केंद्र में के आकार की रेखा बन जाएगी।
4. v के आकार की रेखा पर आँखों को केंद्रित करने का प्रयास करें।
5. इस स्थिति को जितनी देर तक हो सके बनाए रखें। आपकी आँखों की माँसपेशियाँ में कुछ सेकण्ड पश्चात् या कुछ मिनटों के भीतर दर्द होने लगेगा। अब अपनी आँखों को आराम दें और फिर से सामान्य स्थिति की ओर आएँ। कुछ देर के लिए आराम करें और फिर से प्रयास करें। इसके नियमित प्रयास से आप इस मुद्रा को लंबे समय तक कर पाएँगे।
6. अभ्यास के दौरान सामान्य ढंग से श्वास लें। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी श्वास धीमी हो जाएगी और आप अधिक स्थिर होने लगेंगे।
लाभ :
1. यह चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुँचने में मदद करता है।
2. इससे मस्तिष्क स्थिर होता है और एकाग्रता बढ़ती है।
3. इससे आँखों की माँसपेशियों को मजबूती मिलती है।
4. यह मुद्रा आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है।
सावधानीः
1. ग्लूकोमा या नेत्र संबंधी विकार होने पर इसे न करें।
काकी मुद्रा :
इस मुद्रा के अंतर्गत चेहरा कौए की भाँति दिखता है, इसीलिए इसे काकी मुद्रा कहा जाता है। (काक=कौआ)
चित्रः 22.12 काकी मुद्रा
विधि :
1. पीठ को सीधा रखते हुए किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठें।
2. अपनी आँखों को बंद करें और शरीर को आराम दें।
3. ज्ञान मुद्रा सहित अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें।
4. अब अपनी आँखों को खोलें और नाक के अग्र भाग की ओर देखें।
5. अपनी जिह्वा को घुमाते हुए दोनों होठों से चोंच बनाएँ और इस चोंच से तेज़ी से और सीअअअआआआ कि आवाज आये इस तरह श्वास लें।
6. जब आपके फेफड़ों में पूरी तरह श्वास भर जाए, तब इस श्वास को जितना संभव हो रोक कर रखें। (अंतर कुभंक) और अपनी आँखें बंद रखें।
7. अब नाक से धीरे-धीरे श्वास बाहर निकालें।
8. इसका दो से तीन मिनट तक अभ्यास करें। धीरे-धीरे अवधि को बढ़ाते जाएँ।
लाभ :
1. इससे चेहरा प्रबल होता है।
2. इससे नासिका की नली मजबूत बनती है।
3. इससे ष्वसन प्रणाली मजबूत होती है।
4. इससे त्वचा खिली-खिली रहती है।
5. इससे चक्रों का शुद्धिकरण होता है।
सावधानी
1. इसे प्रदूषित वातावरण में नहीं करना चाहिए।
2. ग्लूकोमा, न्यून रक्तचाप, खाँसी या जुकाम हो तो इसे नहीं करना चाहिए।
3. यदि हाल ही में नेत्र की शल्य चिकित्सा हुई हो तो इस अभ्यास से पहले चिकित्सक से परामर्श लेना आवश्यक है।
पाठगत प्रश्न 22.4
अ. उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:
1. शंभावी एवं काकी मुद्रा मुद्रा के अंतर्गत …….आती हैं।
2. भौहों के मध्य भृकुटि की ओर देखते हुए, ज्ञान मुद्रा सहित किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठने को …… कहा जाता है।
3. …….. मुद्रा में चेहरा कौए की भाँति प्रतीत होता है।
बंध का अर्थ :
बंध आसनों के अभ्यास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संस्कृत शब्द ‘बंध’ का अर्थ है पकड़ना, कसना या बांधना। बंधों का उद्देश्य प्राणों को किसी निश्चित आसनों में बाँधना और आध्यात्मिक जागरण के लिए उनके प्रवाहों को सुषुम्ना नाड़ी की ओर पुनःनिर्देशित करना है। बंध शरीर के बाँध हैं जो कि शरीर की कुछ विशेष माँसपेशियों के कसने और ऊपर उठाने से बनते हैं।
तीन प्रकार के प्रमुख बंध हैं: जलंधर बंध (गला), उड्डियान बंध (उदर) और मूल बंध (सीवन में स्थित) है।
महत्त्व
1. ये चारों तकनीके साधक को विभिन्न तंत्रिकाओं को नियंत्रित करने की अनुमति देती हैं।
2.ये चक्रों को भी प्रभावित करती हैं और सुषुम्ना नाड़ी तक कुंडिलिनी प्रवाह को पहुँचाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का विमोचन करता है।
जलंधर बंध-चिन लॉक
जलंधर बंध हठयोग अभ्यास में प्रयोग होने शक्तिशाली बंधों में से एक है। इसे चिन लॉक भी कहा जाता है। जाला का संस्कृत अर्थ ‘जाल’ और धर का अर्थ धरण रखना है। इसे सिर को नीचे करने से पहले गरदन को फैला और उरोस्थि को ऊपर उठा कर किया जाता है ताकि ठोड़ी को छाती पर आरामदायक ढंग से रखा जा सके।
चित्र 22.13 जलंधर बंध
विधि
1. पद्मासन या सिद्धासन जैसे किसी भी ध्यान आसन में सीधे बैठें।
2. अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखें और ध्यान रखें कि घुटने जमीन को छू रहे हों।
3. अपनी आँखें बंद कर लें और शरीर को आराम दें। सामान्य ढंग से श्वास लें।
4. अब धीरे-धीरे गहरी श्वास अंदर लें और श्वास को रोके रखें।
5. अपने सिर को आगे बढ़ाएँ और ठोड़ी को छाती के साथ दबाएँ।
6. अपनी बाँहों को सीधा करें और बंध की मुद्रा स्थापित करने के लिए अपने घुटनों को हथेलियों से दबाएँ। कंधों को थोड़ा आगे बढ़ाएँ ताकि बाँहें बंधी रहें।
7. आरामदायक ढंग से जितना हो सके इस स्थिति में रहें। याद रहे कि श्वास अंदर रहे। नौसिखिए व्यक्ति को केवल कुछ सेकेंड के लिए ही श्वास रोक कर रखनी चाहिए। इसके बाद इसे अपनी क्षमता के अनुसार एक या अधिक मिनट के लिए बढ़ाया जा सकता है।
8. बंध से बाहर निकलने के लिए, बाँहों को नीचे करें, अपना सिर ऊपर करें और श्वास बाहर छोड़ें। सीधी मुद्रा में वापस आएँ और सामान्य ढंग से श्वास लें।
9. इस प्रक्रिया को आरामदायक स्थिति में जितना हो सके दोहराते रहें।
लाभः
1. यह थाइराइड और पैराथाइराइड ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। यह शरीर के उपापचय को नियमित करता है।
2. जलंधर बंध कंठ (विशुद्धि) चक्र को सक्रिय बनाने में मदद करता है।
3. यह प्राण शक्ति को ऊपर जाने से रोकता है ।
4. यह मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ाता है।
5. जलंधर बंध तीन यौगिक बंधों में से एक है जिसमें महाबंध को करने से पहले विशेषज्ञता प्राप्त करना आवश्यक है।
सावधानियाँ
1. उच्च या निम्न रक्तचाप एवं हृदयरोगी इसे न करें।
2. गर्दन की अकड़न, ग्रीवा संबंधी स्पंडिलाइटिस एवं स्पांडिलोसिस की स्थिति में इस अभ्यास को न करें।
3. उरोस्थि के गड्ढे को छूने के लिए अपनी ठोड़ी पर दबाव न बनाएँ।
उड्डियान बंध :
संस्कृत में उड्डियान शब्द का अर्थ है- उड़ना या ऊपर उठना। उड्डियान बंध का अर्थ है: आंतरिक ऊर्जा अर्थात् प्राण को ऊपर उठाना।
चित्र: 22.14: उड्डियान बंध
विधि
1. किसी भी ध्यान के आसन में बैठें और हथेलियों को घुटनों पर रखें। आँखें बंद करते हुए पूरे शरीर को आराम दें।
2. धीरे-धीरे श्वास अंदर लें और पूरी तरह से श्वास बाहर निकालें ताकि जितना हो सके एक ही श्वास में पेट अंदर की ओर आजाए।
3. फिर जलंधर बंध करें।
4. जब पेट का ऊपरी हिस्सा पसलियों के नीचे और छाती बाहर की ओर आ जाए तो उसे उड्डियान बंध कहा जाता है।
5. आराम से जितना हो सके उतनी देर इस मुद्रा में रहें।
लाभः
1. यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज़ की समस्या में लाभकारी होता है।
2. यह अग्नाष्य को मजबूत बनाता है और मधुमेह के लिए लाभकारी होता है।
3. यह पेट की माँसपेशियों और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है।
4. अवसाद और गुस्से से निजात दिलाता है व मस्तिष्क का संतुलन बैठाने में मदद करता है।
सावधानी
1. उच्च रक्त चाप, हृदय रोग, हरनिया और ग्लूकोमा में इसे नहीं करना चाहिए।
2. महावारी, गर्भावस्था, पेप्टिक और डयूडेनल अल्सर की स्थिति में नहीं करना चाहिए।
मूलबंध
संस्कृत शब्द मूल का अर्थ है ‘आधार, जड़ और तल। बंध का अर्थ है नियंत्रण, धारण, बंधन या बंद’। इसे रूट लॉक भी कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर से संबंधित है। इसका शारीरिक प्रतिरूप सीवन की माँसपेशी है जो कि गुदा और योनिमुख के बीच में स्थित है और ऊपर की ओर बढ़ती है।
विधि
1. बाईं एड़ी से सीवन को दबाते हुए, सिद्धासन में सीधा बैठें।
2. सामने की ओर देखें और गहरी श्वास लें।
3. धीरे-धीरे श्वास लें। जैसे-जैसे पेट सिकुड़े, दृढ़ता से गुदा की माँसपेशियों को सिकोड़ें।
4. माँसपेशियों की सिकुड़न और श्वास को यथासंभव और सुविधाजनक स्थिति तक रोकें।
5. धीरे-धीरे श्वास अंदर लें और गुदा की माँसपेशियों को धीरे-धीरे आराम दें।
लाभ :
1. यह पाचन तंत्र, प्रजनन अंगों और सीवन को मजबूत बनाता है और महिलाओं की कष्टदायक महामारी में मदद करता है।
2. मूल बंध मूल चक्र को सक्रिय करते हुए आध्यात्मिक चेतना के लिए तैयार करता है।
अवधि
शुरूआत में पाँच चक्र करें और अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रत्येक सप्ताह तब तक एक-एक चक्र को बढ़ाते जाएँ जब तक कि इनकी संख्या 10 न हो जाए। सिकुड़न के बीच में पाँच सेकेंड तक आराम करें।
सावधानी :
1. उच्च रक्त चाप, हृदय रोग या अन्य किसी मुख्य रोग के होने पर इसे नहीं करना चाहिए।
2. मलाशय से रक्त आने की स्थिति में इसे नहीं करना चाहिए।
अनुवर्ती प्रश्न 22.5
अ. उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:
1. बंध हैं जिसे शरीर की कुछ विशेष माँसपेशियों के कसने और ऊपर उठाने के लिए किया जाता है।
2. तीन प्रकार के मुख्य बंध और हैं।
3. जलंधर बंध को भी कहा जाता है। 4. थाइराइड और पैराथाइराइड ग्रंथि को जाता है। से संतुलित किया
5. बंध के अंतर्गत पेट का ऊपरी भाग पसलियों के नीचे अंदर छाती आगे की ओर बढ़ती है।
ब. निम्न वाक्यों के आगे सत्य या असत्य का निशान लगाएँ-
1. उड्डियान बंध को डयूडेनल और पेप्टिक अल्सर के दौरान किया जा सकता है।
2. मूल बंध को रूट लॉक भी कहते हैं।
3. महा बंध किन्हीं दो बंधों का संयोजन है।
आपने क्या सीखा
- मुद्रा और बंध का अभ्यास, आसन और प्राणायाम के आसन से अधिक प्रभावशाली होता है।
- मुद्रा योग में प्रयुक्त होने वाला एक प्रतीकात्मक आसन है। मुद्राओं के कई प्रकार हैं और प्रत्येक प्रकार का शरीर और मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव पड़ता है।
- हाथों की उंगलियों को विभिन्न स्थितियों से छूना हस्त मुद्रा कहा जाता है। हस्त मुद्रा के अंतर्गत प्रत्येक उँगली प्रत्येक तत्व को दर्षाती है।
- वह मुद्रा जिसे आसन के रूप में किया जाता है, उन्हें आसन मुद्रा कहते हैं। इसमें महामुद्रा, विपरीत करणी और अष्विनी मुद्रा सम्मिलित है।
- वे मुद्राएँ जिन्हें चेहरे के द्वारा किया जाता है, उन्हें मुख मुद्रा कहा जाता है। शंभावी मुद्रा, काकी मुद्रा, मुख मुद्रा के अंतर्गत आती हैं।
- बंध, आसन के अभ्यास का महत्वपूर्ण भाग है। बंध शारीरिक बंधन हैं जिसे कुछ विषेष माँसपेशियों को कसने और ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। बंध के तीन प्रमुख प्रकार हैं: जलंधर बंध (गला), उड्डियान बंध (पेट) और मूल बंध (सीवन में स्थित है।) महाबंध इन तीनों बंधों का संयोजन है।
पाठांत प्रश्न
1. मुद्रा को पारिभाषित कीजिए।
2. किस मुद्रा को सभी मुद्राओं का सम्राट कहा गया है ?
3. विपरीत करणी मुद्रा के लाभों की व्याख्या कीजिए।
4. महामुद्रा की विधि की व्याख्या कीजिए।
5. शांभवी मुद्रा का अर्थ क्या है ?
6. बंध के अर्थ की व्याख्या कीजिए।
7. उड्डियान बंध के लाभों का वर्णन कीजिए।
8. महाबंध में कितने प्रकार के बंध सम्मिलित हैं ? व्याख्या कीजिए।
9. जलंधर बंध की सावधानियों की व्याख्या कीजिए ?
10. मूल बंध के लाभों की सूची बनाइए ?
पाठगत प्रश्नों के उत्तर
22.1
अ).
1. मुद्रा,
2. हाथ,
3. 10 और 25
22.2
अ).
1. ख,
2. ड.,
3. ग,
4. घ,
5. क
ब).
1. ज्ञान
2. वायु मुद्रा
3. अँगूठा और तर्जनी उंगली
4. सूर्य मुद्रा
5. सूर्य और लिंग
6. पृथ्वी
7. सूखापन, शरीर में होने वाली पानी की कमी।
8. 30-45
22.3
अ).
1. आसन मुद्रा,
2. महामुद्रा, केंद्र,
3. 90, 45
ब).
1. सही,
2. सही,
3. गलत
22.4
अ.
1. मुखा
2. शंभावी
3. काकी
22.5
अ.
1. शारीरिक बंध
2. जलंधर, उड्डियान और मूल बंध
3. चिन लॉक
4. जलंधर बंध
5. उड्डियान
ब.
1. गलत
2. सही
3. गलत