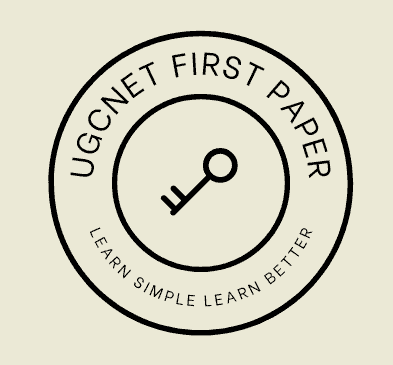अनुमान की व्याप्ति :
अनुमान प्रमाण (अनुमितिकरणम् से इति बाधित्वम् पर्यन्त)
अनुमितिकरणमनुमानम्। परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमितिः । व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः। यथा ‘वह्निव्याप्यधूमवानयं पर्वत इति ज्ञानं परामर्शः। तज्जन्यं पर्वतो वह्निमानिति ज्ञानमनुमितिः। यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति साहचर्यनियमो व्याप्तिः । व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता।
प्रसंग : प्रस्तुत अनुच्छेद में तर्कसंग्रहकार आचार्य अन्नम्भट्ट न्याय-वैशेषिक परम्परा में स्वीकृत अनुमान प्रमाण के स्वरूप का विवेचन करते हैं। इसी प्रसंग में वे अनुमान प्रमाण की सिद्धि में सहायक अनेक शब्दों यथा अनुमिति, व्याप्ति, परामर्श, पक्षधर्मता आदि का लक्षण एवं स्वरूप भी स्पष्ट करते हैं।
व्याख्या : सर्वप्रथम अनुमान का लक्षण करते हुए आचार्य कहते हैं कि अनुमिति ज्ञान का करण ही अनुमान प्रमाण कहलाता है। ‘करण’ का अर्थ असाधारण कारण है अर्थात् जिस कारण का प्रयोग करते ही कार्य की तुरन्त निष्पत्ति हो जाय। जिस प्रकार छिदा रूप कार्य के प्रति परशुकरण है क्योंकि परशु का दारु से संयोग होते ही छिदा की निष्पत्ति हो जाती है, उसी प्रकार अनुमान की प्रक्रिया में ‘परामर्श को अनुमिति का करण कहा जाता है। अनुमिति वस्तुतः परामर्श से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है।
पुनः ग्रन्थकार परामर्श का लक्षण करते हैं “व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः” अर्थात् व्याप्ति से विशिष्ट पक्षधर्मता का ज्ञान परामर्श कहलाता है। उदाहरणरूप में धूम और अग्नि का आपस में जो एक अवश्यप्राप्ति रूप सम्बन्ध है कि जहाँ-जहाँ धूम होगा वहाँ-वहाँ अग्नि अवश्य हुआ करेगी, यह जो विशिष्ट स्थिति है जिसके माध्यम से पक्ष अर्थात् पर्वत में धूम के रहने का ज्ञान ही परामर्श है। व्याप्ति ग्रहण के पश्चात् जब कोई पर्वत रूप पक्ष में धूम को देखता है तो वह व्याप्ति का स्मरण करते हुए यह कहता है कि ‘यह पर्वत अग्नि से व्याप्य धूमवान है’ (क्योंकि जहाँ धूम रहता है वहाँ अग्नि का भी प्राप्त होना निश्चित है), इस प्रकार का ज्ञान ही परामर्श है। इस परामर्श द्वारा उत्पन्न हुआ यह ज्ञान कि ‘यह पर्वत अग्नि वाला है’ अर्थात् इसमें धूम होने के कारण अग्नि अवश्य ही है, यही ज्ञान अनुमिति कहलाती है।
‘व्याप्ति’ का लक्षण स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं कि साहचर्य नियम को व्याप्ति कहा जाता है। उदाहरण रूप में जहाँ-जहाँ धूम होता है वहाँ-वहाँ अग्नि होती है, इसप्रकार अग्नि और धूम की साहचर्यता (साथ-साथ रहने का स्वभाव) का ज्ञान ही व्याप्ति है।
‘पक्षधर्मता’ का अर्थ है व्याप्य का पक्ष में रहना। पर्वत पर धूम को देखकर अग्नि का अनुमान करने की प्रक्रिया में धूम व्याप्य है तथा पर्वत पक्ष है। व्याप्य अर्थात् धूम का पक्ष अर्थात् पर्वत में रहने का जो गुणधर्म है, वही पक्षधर्मता है।
विशेष : अनुमान का शाब्दिक अर्थ है ‘अनु पश्चात् मानम् अनुमानम् जिसके अनुसार अनुमान, प्रत्यक्ष के पश्चात् होने वाला प्रमाण है। न्याय-वैशेषिक परम्परा में अनुमान प्रमाण के दो अंग माने जाते हैं व्याप्ति तथा पक्षधर्मता। इनमें व्याप्ति के द्वारा साध्यसामान्य की सिद्धि होती है तथा पक्षधर्मता के ज्ञान से साध्यविशेष को सिद्ध किया जाता है।
स्वयमेव भूयो गृहीत्वा पर्वतसमीपं ‘यत्र यत्र धूमस्तत्र अनुमानं द्विविधं स्वार्थं परार्थं च। तत्र स्वार्थं स्वानुमितिहेतुः । तथाहि दर्शनेन यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति महानसादौ व्याप्तिं गतस्तद्गते चाग्नौ सन्दिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति तत्राग्निः’ इति। तदनन्तरं वह्निव्याप्यधूमवानयं पर्वत इति ज्ञानमुत्पद्यते। अयमेव लिङ्परामर्श इत्युच्यते। तस्मात्पर्वतो तदेतत्स्वार्थानुमानम् । वह्निमानिति ज्ञानमनुमितिरुत्पद्यते ।
व्याख्या : अनुमान प्रमाण के दो भेद हैं स्वार्थानुमान एवं परार्थानुमान।
‘स्वार्थानुमान’ वह अनुमान है जहाँ अनुमानकर्तता स्वयं ही अनुमिति की प्रक्रिया को संपन्न करता है। यथा स्वयं ही बार-बार के दर्शन या ज्ञान के प्रयास से महानस (रसोईघर) में ‘जहाँ-जहाँ धूम है वहाँ-वहाँ अग्नि अवश्य उपलब्ध होता है’ इस प्रकार की व्याप्ति का निश्चय कर लेता है। इस व्याप्ति ज्ञान को ग्रहण करने के उपरान्त जब कभी वह पर्वत (पक्ष) पर जाता है तथा पर्वत से धूम को निकलते हुए देखता है तो स्वयं को सन्देहयुक्त अनुभव करता है कि यहाँ अग्नि हो सकती है। पुनः वह धूम एवं अग्नि के साहचर्यभूत व्याप्ति का स्मरण करता है कि ‘जहाँ-जहाँ धूम होता है वहाँ-वहाँ अग्नि अवश्य होती है। इसके पश्चात् उसे यह ज्ञान हो जाता है कि यह पर्वत अग्नि से व्याप्त धूम वाला है, इसी ज्ञान को परामर्श ज्ञान कहते हैं। इसी परामर्श ज्ञान के उपरान्त अनुमानकर्ता को यह ज्ञान हो जाता है कि ‘यह पर्वत अग्निमान है’। इसे ही अनुमिति ज्ञान कहते हैं। चूँकि यह अनुमिति अनुमान करने वाला स्वयं ही संपन्न करता है इसलिए इस प्रकार के अनुमान को स्वार्थानुमान कहते हैं।
यथा चायम्, यत्तु स्वयं धूमादग्निमनुमाय परं प्रति बोधयितुं पञ्चावयववाक्यं प्रयुक्ते तत्परार्थानुमानम्। पर्वतो वह्निमान्, धूमत्वात्। यो यो धूमवान् स स वह्निमान्। यथा महानसम्। तथा तस्मात्तथेति। अनेन प्रतिपादिताल्लिङ्ात् परोऽप्यग्निं प्रतिपद्यते। प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनय-निगमनानि पञ्चावयवाः। पर्वतो वह्निमानिति प्रतिज्ञा। धूमवत्त्वादिति हेतुः। यो यो धूमवान् स स वह्निमान् इत्युदाहरणम्। तथा चायमित्युपनयः । तस्मात्तथेति निगमनम्। तस्माल्लिंगपरामर्शोऽनुमानम् । स्वार्थानुमितिपरार्थानुमित्योर्लिंगपरामर्श एव करणम् ।
व्याख्या : ग्रन्थकार अनुमान प्रमाण के द्वितीय भेद ‘परार्थानुमान’ का लक्षण, उदाहरण तथा उसके अवयवों का निरूपण करते हैं। परार्थानुमान का शाब्दिक अर्थ है दूसरों को कराया गया अनुमान का ज्ञान। जब कोई व्यक्ति स्वयं धूम से अग्नि का अनुमितिज्ञान करने के उपरान्त किसी अन्य व्यक्ति को उस अनुमान का ज्ञान कराना चाहता है तो वह मात्र स्वार्थानुमान की प्रक्रिया से उस दूसरे व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं करा सकता है। इसके लिए वह एक भिन्न पद्धति का प्रयोग करता है जिसमें अनुमान के पञ्चावयव वाक्यों की सहायता से दूसरे व्यक्ति को अनुमान की प्रक्रिया का निदर्शन कराता है। इस माध्यम से दूसरे व्यक्ति को भी अनुमान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसे ही परार्थानुमान कहते हैं। परार्थानुमान के पञ्चावयव वाक्यों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तथा परार्थानुमान की सिद्धि प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए अन्नम्भट्टाचार्य कहते हैं कि पर्वत अग्निवाला है, धूमवाला होने से, क्योंकि जो जो धूमवाला होता है वह अग्निवाला अवश्य होता है, जैसे महानस; उसी प्रकार का यह पर्वत भी धूमवाला है अतः वह अग्निवाला भी है। इन पंच अवयवों से युक्त वाक्य की सहायता से प्रतिपादित लिंग (चिन्ह) से दूसरे को भी पर्वत में अग्नि का ज्ञान हो जाता है। इन पंच वाक्यों का क्रम तथा स्वरूप इस प्रकार है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन। ये परार्थानुमान के पञ्च अवयव वाक्य हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार है –
प्रतिज्ञा : पर्वत अग्निमान् है
हेतु : धूमवान होने से
उदाहरण : क्योंकि जो-जो धूमवान होता है वह-वह अग्निमान अवश्य होता है यथा-महानस
उपनय : यह (पर्वत) भी उसी तरह (अग्निव्याप्यधूमवान) का है
निगमन : अतः पर्वत अग्निमान है
विशेष : आचार्य स्पष्ट करते हैं कि स्वार्थानुमान से उत्पन्न ज्ञान स्वार्थानुमिति तथा परार्थानुमान से उत्पन्न ज्ञान परार्थानुमितिः इन दोनों में लिंगपरामर्श (अग्निव्याप्यधूमवान पर्वत) ही प्रकृष्ट कारण होने से करण है। इसलिए लिंगपरामर्श ही अनुमान प्रमाण है।
लिङ त्रिविधम् अन्वयव्यतिरेकि, केवलान्वयि, केवलव्यतिरेकि चेति। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमदन्वयव्यतिरेकि। यथा वह्नौ साध्ये धूमवत्त्वम्। ‘यत्र धूमस्तत्राग्निः, यथा महानसः’ इत्यन्वयव्याप्तिः। ‘यत्र वहिर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, यथा महाहृदः’ इति व्यतिरेकव्याप्तिः । अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयि। यथा घटोऽभिधेयः, प्रमेयत्वात्, पटवत्। अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोव्यतिरेकव्यप्तिर्नास्ति, सर्वस्यापि प्रमेयत्वादभिधेयत्वाच्च । व्यतिरेकमात्रव्याप्तिकं केवलव्यतिरेकिय यथा पृथिवीतरेभ्यो भिद्यते; गन्धवत्त्वात् । यदितरेभ्यो न भिद्यते न तद् गन्धवत्, यथा जलम्, न चेयं तथा, तस्मान्न तथेति। अत्र यद्गन्धवत्तदितरभिन्नमित्यन्वयदृष्टान्तो नास्ति, पृथिवीमात्रस्य पक्षत्वात् ।
व्याख्या : अनुमान की प्रक्रिया में लिंग (हेतु / साधन) का ज्ञान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है। इसकी सहायता से ही अनुमान प्रमाण पूर्णता को प्राप्त होता है। लिंग के तीन भेद हैं- केवलान्वयि, केवलव्यतिरेकि तथा अन्वयव्यतिरेकि। यह तीन प्रकार का लिंग भेद व्याप्ति का प्रकार विशेष है क्योंकि जिस अनुमानवाक्य की व्याप्ति अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही प्रकारों से बन जाती है, उस वाक्य में प्रयुक्त लिंग को अन्वयव्यतिरेकि लिंग कहा जाता है। उदाहरण अग्नि की सिद्धि में धूमत्व हेतु अन्वयव्यतिरेकि है क्योंकि अग्नि और धूम की साथ-साथ रहने की स्वभावसिद्धि अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों माध्यमों से हो जाती है। ‘जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होता है जैसे महानस’, यह अन्वय व्याप्ति का स्वरूप है। ‘जहाँ अग्नि नहीं होता है वहाँ धूम भी नहीं होता है जैसे जलाशय’, यह व्यतिरेकि व्याप्ति का स्वरुप है। चूँकि यहाँ अग्नि और धूम का साहचर्य सम्बन्ध अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही तरीकों से सिद्ध हो जाता है, अतः धूमत्व हेतु अन्वयव्यतिरेकि हेतु है।
जिस अनुमानवाक्य की व्याप्ति केवल अन्वय प्रकार से ही बनती है, वहाँ हेतु को केवलान्वयि हेतु कहा जाता है। यथा घट अभिधेय है, प्रमेय होने से, पट की तरह। यहाँ पर हेतु मात्र केवलान्वयि है क्योंकि प्रमेयत्व एवं अभिधेयत्व में व्याप्ति सम्बन्ध केवल अन्वय प्रकार (जहाँ जहाँ प्रमेयत्व है वहाँ-वहाँ अभिधेयत्व है) से ही सम्भव है। यहाँ यदि व्यतिरेक व्याप्ति बनाई जाय तो उसका स्वरूप इस प्रकार से होगा ‘जहाँ-जहाँ अभिधेयत्व नहीं है वहाँ-वहाँ प्रमेयत्व नहीं है’ किन्तु न्याय-वैशेषिक मतानुसार संसार का कोई भी पदार्थ अभिधेयत्व तथा प्रमेयत्व से रहित नहीं है। अतः उपरोक्त अनुमान वाक्य की व्यतिरेक व्याप्ति सम्भव नहीं है इसलिए यहाँ प्रयुक्त हेतु केवलान्वयि हेतु है।
जिस अनुमानवाक्य की व्याप्ति केवल व्यतिरेक प्रकार से ही बनती है, वहाँ हेतु को केवलव्यतिरेकि हेतु कहा जाता है। यथा पृथिवी अन्य पदार्थों से भिन्न है, गन्धवती होने से, जो अन्य पदार्थों से भिन्न नहीं है, वह गन्धवाला भी नहीं है यथा जल, यह पृथिवी वैसी अर्थात् गन्धहीन नहीं है, अतः इतर पदार्थों के समान नहीं है। इस अनुमान वाक्य में ‘जो गन्धवान नहीं है वह इतर पदार्थों से भिन्न भी नहीं है’ इस प्रकार की व्यतिरेक व्याप्ति तो बन जाती है किन्तु यदि हम अन्वय व्याप्ति बनाना चाहें तो उसका स्वरूप इस प्रकार होगा जो गन्धवान है वह इतर पदार्थों से भिन्न है यथा पृथिवी’ किन्तु पृथिवी का उदाहरण देना सम्भव नहीं है क्योंकि वह पक्ष में समाविष्ट है। अतः उपरोक्त अनुमान वाक्य की अन्वय व्याप्ति सम्भव नहीं है। इसलिए यहाँ प्रयुक्त हेतु केवलव्यतिरेकि हेतु है।
विशेष अन्वय व्याप्ति में साधन का कथन पहले किया जाता है तथा साध्य का कथन बाद में किया जाता है। व्यतिरेक व्याप्ति में साध्याभाव का कथन पूर्व में होता है तथा साधनाभाव का कथन उसके पश्चात् होता है।
संदिग्धसाध्यवान् पक्षः। यथा धूमवत्त्वे हेतौ पर्वतः। निश्चितसाध्यवान् सपक्षः। यथा तत्रैव महानसः । निश्चितसाध्याभाववान् विपक्षः। यथा तत्रैव महाहृदः ।
व्याख्या : आचार्य अन्नम्भट्ट अनुमान की सिद्धि में सहायक अवयवों (पक्ष, सपक्ष एवं विपक्ष) के स्वरूप का विमर्श प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम वे पक्ष का लक्षण करते हैं- ‘संदिग्धसाध्यवान् पक्षः’ अर्थात् जहाँ पर संदिग्ध वस्तु साध्य होता है वह पक्ष कहलाता है। दूसरे शब्दों में जिस स्थल पर साध्य की सत्ता का सन्देह होता है उसे ही पक्ष कहते हैं। जैसे पर्वत पर धूमत्व हेतु से अग्नि का अनुमान करने की प्रक्रिया में जब कोई व्यक्ति धूम और अग्नि की व्याप्ति का ग्रहण करके पर्वत पर पहुँचता है तो वहाँ धूम को देखकर उसे अग्नि की सत्ता के विषय में यह सन्देह उत्पन्न होता है कि यहाँ धूम तो दिखाई दे रहा है किन्तु अग्नि नहीं अतः यहाँ अग्नि विद्यमान है अथवा नहीं। यहाँ अग्निविषयक सन्देह का अधिकरण पर्वत है अतः पर्वत ही पक्ष है।
‘निश्चितसाध्यवान् सपक्षः’ अर्थात् जहाँ साध्य का होना निश्चित हो वह स्थल सपक्ष कहलाता है। सपक्ष का अर्थ है समान पक्ष। यथा पर्वत पर धूमत्व हेतु से अग्नि का अनुमान करने की प्रक्रिया में जब कोई व्यक्ति धूम और अग्नि की व्याप्ति का ग्रहण करके पर्वत पर पहुँचता है तो वहाँ धूम को देखकर उसे अग्नि की सत्ता के विषय में यह सन्देह उत्पन्न होता है कि यहाँ धूम तो दिखाई दे रहा है किन्तु अग्नि नहीं अतः यहाँ अग्नि विद्यमान है अथवा नहीं। इस सन्देह के उपरान्त वह पूर्व में गृहीत व्याप्ति का स्मरण करता है कि महानस में जब-जब मैंने धूम को देखा था तब-तब वहाँ अग्नि की भी उपलब्धि हुई थी, अतः यहाँ भी ऐसा ही होगा। इस प्रकार महानस वह स्थल है जहाँ साध्य की सत्ता निश्चित है, अतः उपरोक्त अनुमान में महानस सपक्ष है।
‘निश्चितसाध्याभाववान् विपक्षः’ अर्थात् जहाँ पर साध्य का अभाव निश्चित होता है वह विपक्ष कहलाता है। विपक्ष का अर्थ है विरुद्ध (विपरीत) पक्ष। जिस अधिकरण में साध्य निश्चित रूप से नहीं रहता है वह विपक्ष कहलाता है। यथा धूमत्व हेतु से अग्नि के अनुमान में जलाशय विपक्ष है क्योंकि वहाँ साध्यभूत अग्नि का नितान्त अभाव है।
विशेष : अनुमान की प्रक्रिया में सद् हेतु का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। सद् हेतु के 5 लक्षण होते हैं पक्षधर्मत्व (हेतु का पक्ष में रहना), सपक्षसत्त्व (हेतु का सपक्ष में रहना), विपक्षव्यावृत्ति (हेतु का विपक्ष में न रहना), अबाधितविषयत्व (हेतु का किसी अन्य प्रबल प्रमाण से बाधित न होना) तथा असत्प्रतिपक्षत्व (हेतु का कोई प्रतिपक्षी अन्य हेतु न होना)। जब कोई हेतु उपरोक्त 5 लक्षणों में से किसी भी एक लक्षण से हीन हो जाता है तो वह असद् हेतु बन जाता है। असद् हेतु को ही हेत्वाभास कहा जाता है।