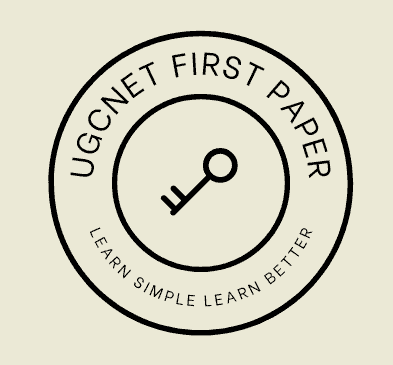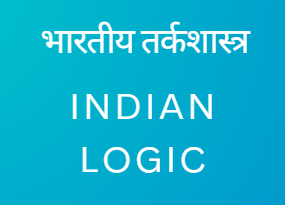02. अनुमान (Anumana ,Inference ) :
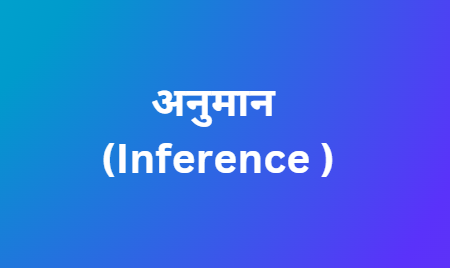
अनुमान शब्द का अर्थ
संस्कृत शब्द अनुमान दो शब्दों, अनु अर्थात उत्तरवर्ती और मान अर्थात मापन से मिलकर बना है। इस प्रकार सम्पूर्ण शब्द से तात्पर्य है किसी घटना का उत्तरवर्ती आकलन। यह वह ज्ञान है जो प्रमाण के पश्चात् आता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार का ज्ञान इसलिए अपरोक्ष/प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता; “क्योंकि यह भूतकाल में ज्ञान के अन्य साधनों जैसे कि प्रत्यक्ष, शब्द आदि से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करता है” और व्यक्ति को “अग्रिम ज्ञान ज्ञाप्त करने में सक्षम बनाता है”। सभी भारतीय दार्शनिक अनुमान को ज्ञान का वैध साधन नहीं मानते हैं। उदाहरणार्थ, भौतिकवादी चार्वाक केवल भौतिक पदार्थ को ही अन्तिम सत्य मानते हैं। फलतः वह अनुमान को ज्ञान के वैध साधन के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं।
अनुमान की संरचना(Structure of Anuman)
यद्यपि सभी प्रधान भारतीय दार्शनिक अनुमान को ज्ञान का वैध साधन स्वीकार करते हैं किन्तु ज्ञान की अपनी विशिष्ट समझ के कारण वे अनुमान को भिन्न ढंग से समझते हैं और उसी के अनुरूप अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। भारतीय दर्शन में अनुमान स्वयं के लिये (स्वार्थानुमान) तथा दूसरों के लिये (परार्थानुमान) हो सकता है। स्वार्थानुमान में चूँकि हम अपने स्वयं के लिये अव्यभिचारी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं इसलिए कथन भलिभाति संरिचत नहीं होते हैं। जबकि चूँकि परार्थानुमान में दूसरे को सत्य से अवगत कराना होता है इसलिए इस प्रकार के अनुमान को भलिभांति संरचित होना आवश्यक होता है। इस इकाई में हम न्याय दर्शन के अनुमान पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। वास्तव में, सभी भारतीय दर्शनों में न्याय दर्शन ही अपने तर्कशास्त्र के लिये प्रसिद्ध है।
न्याय दर्शन के अनुसार, अनुमान में व्यक्ति दो वस्तुओं अथवा तथ्यों के मध्य उपस्थित स्थाई सहचर्य सम्बन्ध (व्याप्ति) के आधार पर किसी चिह्न (लिंग) को समझ कर एक तथ्य से S दूसरे तथ्य पर पहुँचता है। वैध अनुमान मूलतः व्याप्ति पर ही निर्भर होता है। व्याप्ति सम्बंध के लिये विभिन्न भारतीय दर्शन भिन्न-भिन्न नामों का प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ, वैशेषिक इसे प्रसिद्धि और सांख्य प्रतिबन्ध कहते हैं। न्याय दर्शन के न्याय वाक्य में पाँच कथन होते हैं। इस प्रकार, अनुमानिक युक्ति के पाँच भाग होते हैं। यथा; पक्ष या प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय और निगमन। उदाहरण के लिए;
1. पक्ष-वाद/प्रतिज्ञा कथन = पर्वत में आग है।
2. हेतु-कारण या आधार = क्योंकि पर्वत में धुआँ है।
3. दृष्टान्त-सिद्धि = जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहीं वहीं आग होती है। जैसे कि रसोईघर।
4. उपनय-अनुप्रयोग = पर्वत में धुआँ है।
5. निगमन-निष्कर्ष = अर्थात् पर्वत में आग है।
इस प्रक्रिया में हम परिकल्पनात्मक कथन से प्रारम्भ करते हैं, फिर हम उसके लिए कारण/आधार प्रस्तुत करते हैं और सर्वव्यापी कथन पर पहुँचते हैं। यह सर्वव्यापी कथन दो वस्तुओं के मध्य उपस्थित स्थाई सहचर्य सम्बंध को उदाहरण के साथ प्रस्तुत करता है। फिर सर्वव्यापी कथन को वर्तमान प्रकरण पर लागू किया जाता है और उत्तरवर्ती कथन के द्वारा निष्कर्ष निगमित किया जाता है। सकारात्मक स्थाई सम्बंध जैसेकि यदि धुआँ है तो आग भी होगी को निर्देशित करने के कारण इस प्रकार के न्याय वाक्य में अन्वय व्याप्ति होती है।
हम पाश्चात्य उदाहरण के माध्यम से इसे अग्रलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं; (1) राम मरणशील है, (2) क्योंकि वह मानव है, (3) सभी मानव मरणशील होते हैं जैसे कि हमारे दादा जी, (4) राम एक मानव है, (5) अतः, राम मरणशील है। पाश्चात्य ढंग का उदाहरण देने का मुख्य उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि भारतीय दर्शन अनुमान में आगमन एवं निगमन दोनों को एक ही न्यायवाक्य में एक साथ प्रस्तुत करता है। प्रथम तीन कथन (1-3) आगमनात्मक न्याय वाक्य को जबकि अन्तिम तीन (3-5) निगमनात्मक न्यायवाक्य को प्रदर्शित करते हैं। तृतीय कथन आगमनात्मक निष्कर्ष है और यह पुनः निगमनात्मक न्याय वाक्य के मुख्य आधार वाक्य को निर्देशित करता है।
नकारात्मक स्थाई सम्बंध में व्यतिरेक व्याप्ति होती है। इसके उदाहरण के रूप में उपरोक्त उदाहरण की विपरीत स्थिति को प्रस्तुत किया जा सकता है। पर्वत में धुआँ नहीं है; क्योंकि पर्वत में आग नहीं है; जहाँ आग नहीं होती वहाँ धुआँ नहीं होता जैसे कि झील में (क्योंकि जल और आग विरोधी द्रव्य है); पर्वत में आग नहीं है; अतः पर्वत में धुआँ नहीं है।
अनुमान का वर्गीकरण (Classification of Anuman)
हेतु (धुआँ) और साध्य (आग) के मध्य व्याप्ति की प्रकृति के आधार पर अनुमान का वर्गीकरण किया जाता है। व्याप्ति दो तथ्यों जिनमें से एक व्यापित करता है और दूसरा व्यापित होता है। उदाहरणार्थ, धुआँ आग के द्वारा व्यापित होता है और आग धुएं को व्यापित करती है। व्याप्ति सन्दर्भगत सभी दृष्टान्तों में उपस्थित (जहाँ-जहाँ धुआँ है वहीं-वहीं आग है) रहने के आधार पर और विपरीत सभी दृष्टान्तों में अनुपस्थित (जहां आग नहीं है वहां धुआं नहीं है) रहने के आधार पर स्थापित होती है। अनुमान का वर्गीकरण कारण और अनुमित के मध्य के सम्बंध (कारणगत एकरूपता अथवा अकारणगत एकरूपता) पर आधारित होता है। मूलतः, तीन प्रकार के अनुमान होते हैं।
1. पूर्ववत अनुमान
इसमें व्यक्ति दृष्टिगत कारण के आधार पर अदृष्टिगत प्रभाव कार्य का अनुमान करता है। उदाहरण स्वरूप, व्यक्ति घने काले बादलों के आधार पर भविष्य में होने वाली वर्षा का अनुमान कर लेता है।
2. शेषवत अनुमान
इसमें व्यक्ति दृष्टिगत प्रभाव के आधार पर अदृष्टिगत कारण का अनुमान करता है; जैसे कि नदी में मटमैले पानी के तीव्र बहाव के आधार पर भूतकाल में हुई वर्षा का अनुमान करना।
3. सामान्यतोदृष्ट अनुमान
इस प्रकार के अनुमान में व्यक्ति कारणात्मक सम्बंध के आधार पर अनुमान न करके एकरूपता के नियत अनुभव के आधार पर अनुमान करता है। उदाहरणार्थ, चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों को प्रत्यक्षित करने के लम्बे अनुभव के आधार पर व्यक्ति चन्द्रमा की गतिशीलता का अनुमान कर सकता है। यद्यपि, व्यक्ति के द्वारा चन्द्रमा की गतिशीलता का प्रत्यक्ष वास्तव में नहीं किया जाता।