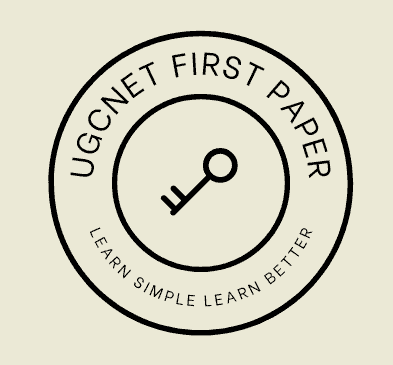भारतीय तर्कशास्त्र: ज्ञान के साधन।(Indian Logic: Means of knowledge.)
प्रस्तावना
भारतीय दार्शनिक चिन्तन परम्परा स्वाभिमत सैद्धान्तिक चिन्तन को जिज्ञासुओं के समक्ष
प्रस्तुत करने के लिए तीन पद्धतियों का प्रयोग करती है तत्त्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा तथा आचारमीमांसा। तत्त्वचिन्तन की इस प्रक्रिया में प्रमाणमीमांसा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि प्रमाणों की सहायता से ही प्रमेयों (तत्त्वों) का ज्ञान सम्भव होता है। दर्शनसरणियों में यह प्रसिद्ध उक्ति भी है ‘मानाधीना मेयसिद्धिः अर्थात् मेय (प्रमेय) की सिद्धि मान (प्रमाण) के अधीन होती है। प्रमा या यथार्थज्ञान की उपलब्धि किसी साधन की सहायता से ही होती है इसलिए सामान्य रूप से प्रमा की उपलब्धि के साधन ही प्रमाण कहलाते हैं। ‘प्रमाण’ शब्द की व्युत्पत्ति भी इसी तथ्य को उद्घाटित करती है- ‘प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम्’ अर्थात् जिससे प्रमा की प्राप्ति हो उसे प्रमाण कहते हैं। न्यायभाष्यकार आचार्य वात्स्यायन का कथन है
‘उपलब्धिसाधनानि प्रमाणानि’ अर्थात् उपलब्धि ज्ञान के साधन ही प्रमाण हैं।
भारतीय दर्शन के विविध सम्प्रदायों में प्रमाणों की संख्या तथा उसके लक्षण एवं स्वरूप में अत्यन्त मतभेद है। चार्वाक दर्शन जहाँ केवल प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है वहीं वैशेषिक एवं बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष तथा अनुमान; सांख्य-योग एवं जैन दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द, न्यायदर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द, प्रभाकर मीमांसा में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द तथा अर्थापत्ति, भाट्ट मीमांसा एवं अद्वैतवेदान्त में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति तथा अभाव को प्रमाण स्वीकार किया जाता है।
आचार्य अन्नम्भट्टकृत ‘तर्कसंग्रह’ यद्यपि वैशेषिक दर्शन का प्रकरण ग्रन्थ है तथापि इसमें न्यायदर्शनसम्मत चतुर्विध प्रमाणव्यवस्था का विवेचन किया गया है। इन्द्रिय तथा अर्थ (विषय) के संनिकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अनुमान प्रमाण लिंगपरामर्श से जन्य होता है। संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध का ज्ञान कराने वाला प्रमाण उपमान कहलाता है। आप्तवाक्य से जन्य प्रमाण को शब्द प्रमाण कहते हैं।
निगमन तथा आगमन तर्कशास्त्र (Inductive And Deductive Logic)
परम्परागत दृष्टि से तर्क को दो भागों में विभाजित किया जाता है; यथा निगमनात्मक तर्क तथा आगमनात्मक तर्क। इसी प्रकार तर्कशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया है – निगमनात्मक तर्कशास्त्र तथा आगमनात्मक तर्कशास्त्र। कहा जाता है कि निगमनात्मक तर्कशास्त्र निष्कर्ष से सम्बन्धित होता है तथा आगमन तर्कशास्त्र अधिष्ठापन के साथ सम्बंधित होता है। निगमनात्मक तर्कशास्त्र में युक्ति होती है जिनमें आधार वाक्य तथा एक निष्कर्ष होता है। निगमनात्मक युक्ति में निष्कर्ष अनिवार्य रूप से आधार वाक्यों का अनुसरण करता है। इसके अतिरिक्त, यह निगमनात्मक तर्क की विशेषता यह है कि यदि कोई आधार वाक्यों को स्वीकार करता है तो उसे निष्कर्ष को भी स्वीकार करना होता है।
इस प्रकार के तर्क गणित तथा बीज गणित में उपलब्ध रहते हैं। निगमनात्मक तर्कशास्त्र सत्यता या असत्यता से संबंधित नहीं है बल्कि यह वैधता तथ अवैधता से संबंधित है। वैधता तथा अवैधता तर्क की विशेषताएं हैं, जबकि सत्यता तथा असत्यता तर्कवाक्यों की विशेषताएं हैं। इस दृष्टिकोण से निगमनात्मक तर्कशास्त्र तर्कवाक्यों की सत्यता तथा असत्यता से संबंधित नहीं है बल्कि वह तर्क की वैधता और अवैधता, संगतता तथा असंगतता से संबंधित है।
तर्कशास्त्र की प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र (Nature and scope of logic)
एक अन्य प्रकार का तर्क आगमनात्मक तर्क होता हैं। कुछ दार्शनिकों के अनुसार आगमनात्मक तर्क प्राकृतिक अनुभविक विज्ञानों जैसे भौतिकी, रासायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामाज शास्त्र, मनोविज्ञान आदि में पाया जाता है। तथापि यह विचार बहुत विवादास्पद है। कारण कार्य सम्बन्ध का नियम आगमनात्मक तर्कशास्त्र के आधार का निर्माण करता है। सामान्यीकरण तथा पूर्वानुमान आगमन तर्क के उद्देश्य हैं।
सामान्यीकरण आगमनात्मक तर्क का महत्वपूर्ण मानक है। आइये इसे स्पष्ट करे। माना हम दस काले कौओं को देखते हैं और हम अन्य कौओं को देखे बिना यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि सभी कौए काले हैं। इस प्रकार निष्कर्ष अवलोकन से परे चला जाता है। ऐसे निष्कर्ष ही सामान्यीकरण कहलाते हैं। अतः केवल आधार वाक्यों की सत्यता निष्कर्ष के सत्य होने को न्याय संगत नहीं ठहराती है। वास्तव में, यहाँ निष्कर्ष संभावयता प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी। यही पर संभावयता आगमनात्मक तर्कशास्त्र के क्षेत्र में प्रवेश करती है।
मनुष्य को प्रकृति द्वारा तर्क करने की शक्तियां प्राप्त हैं। तर्कशास्त्र इन्हीं शक्तियों के प्रयोग का अध्ययन है। तर्कशास्त्र के अध्ययन में हम अपनी स्वयं की क्षमताओं को पहचानते हैं तथा अभ्यास द्वारा उन्हें सुदृढ़ बनाते हैं। तर्कशास्त्र का अध्ययन व्यक्ति को सही तर्कना के सिद्धांतों के वर्णन द्वारा सही तर्क में सहायता प्रदान करता है। जहाँ कहीं
तर्कशास्त्र की प्रकृति (Nature of the logic)
ज्ञान की आवश्यकता होती है, वहां सही तर्कना उपयोगी होती है। चाहे विज्ञान हो, राजनीति हो या हमारे निजी जीवनों में आचरण हो, हम सही निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए तर्कशास्त्र का प्रयोग करते हैं। औपचारिक अध्ययन में हमारा उद्देश्य यह सीखना होता है कि विश्वसनीय सूचना कैसे प्राप्त करें तथा सत्य के लिए प्रतिस्पर्धी दावों का मूल्यांकन कैसे करें।
प्रमुख शब्द
लोगोस (Logos)
दर्शनशास्त्र, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, व्याख्यानशास्त्र तथा धर्म दर्शन में एक महत्वपूर्ण शब्द है। हेराक्लिट्स (535- 475 ई.पू.) ने इस शब्द की स्थापना पश्चिमी दर्शनशास्त्र में ब्रह्माण्ड में व्याप्त नियमबद्धता तथा ब्रह्माण्ड के स्रोत दोनों के रूप में की है। सोफिस्टों ने इस शब्द का प्रयोग वाद-विवाद करने के अर्थ में किया, जबकि अरस्तु ने इसे विवेकपूर्ण विवेचन के रूप में प्रतिस्थापित किया। हेलेनिस्टिक दार्शनिकों ने इस शब्द को ब्रहमाण्ड में विद्यमान सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए किया।
सकारात्मक विज्ञान (Positive Science)
मानवशास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान में ‘सकारात्मक’ शब्द का प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है। एक ओर इसे उस विश्लेषण या सिद्धांतों के रूप में प्रयोग किया जाता है जो वास्तव में वस्तु क्या है तथा इसके विपरीत, उसे आदर्श रूप में क्या होना चाहिए, का वर्णन करने का प्रयास करता है। इस दृष्टि के अनुसार सकारात्मक का विपरीत है-नियामक। नियामक के विपरीत, सकारात्मक विज्ञान का एक उदाहरण आर्थिक विश्लेषण हो सकता है। सकारात्मक कथनों को भी कई बार विवरणात्मक कथन भी कहा जाता है।
प्रमाण (Pramana) :
01. प्रत्यक्ष प्रमाण (Pramanas) :
तर्कसंग्रहकार आचार्य अन्नम्भट्ट के अनुसार इन्द्रिय और अर्थ (विषय) का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु है। ज्ञानेन्द्रियों की संख्या 5 है चक्षु, श्रोत, त्वक्, रसना एवं घ्राण। प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय नियत विषय का ही ग्रहण करती है जैसे चक्षु रूप का, श्रोत शब्द का, त्वक् स्पर्श का, रसना रस का तथा घ्राण गन्ध का। जब कोई इन्द्रिय अपनेनियत विषय के साथ संयुक्त होती है तो उस सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहते हैं। इन्द्रिय और अर्थ (पदार्थ) के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रदत्त लक्षण में सन्निकर्ष पद का अर्थ-संयोग आदि सम्बन्ध विशेष है एवं अर्थ पद का अर्थ विषय है। इन्द्रियों का उनके विषयों के साथ सन्निकर्ष होना प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करता है। यथा
| इन्द्रिय | अर्थ (विषय) | प्रत्यक्ष |
| घ्राण | गन्ध | घ्राणज |
| रसना | रस | रासन |
| चक्षु | रूप | चाक्षुष |
| त्वक् | स्पर्श | स्पार्शन (त्वाक) |
| श्रोत्र | शब्द | श्रोतज |
| मन | सुखदुःख आदि | मानस |
प्रत्यक्ष ज्ञान के भेदों का निरूपण करते हुए आचार्य कहते हैं कि प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है- (1) निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, (2) सविकल्पक प्रत्यक्ष ।
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का स्वरूप है ‘निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम्’ अर्थात् निष्प्रकारक ज्ञान को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। न्याय-वैशेषिक मत में प्रकार का अर्थ विशेषण होता है, अतः प्रकारता का अर्थ ‘विशेषणता’ है। जो ज्ञान विशेषणता से रहित होता है वह निर्विकल्पक कहलाता है। निर्विकल्पक शब्द की व्युत्पत्ति है ‘निर्गतः विकल्पो यस्मात् स निर्विकल्पकः’ अर्थात् जिससे समस्त विकल्प निकल गए हों वह निर्विकल्पक कहलाता है। निर्विकल्पक पद में प्रयुक्त ‘विकल्प’ का अर्थ है ‘नामजात्याद्ययोजना’ । किसी ज्ञान में प्रतीत होने वाले नाम, जाति, गुण आदि को ही विकल्प कहा जाता है। जिस ज्ञान में नाम, जाति इत्यादि की प्रतीति नहीं हुआ करती है वही निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। आशय यह है कि जिस ज्ञान में वस्तु के केवल स्वरूप मात्र की अनुभूति होती है, उसकी किसी विशेषणता का अनुभव नहीं होता है उसे ही निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। उदाहरणरूप में अबोध बालक तथा किसी मूक व्यक्ति का ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान के तुल्य होता है ‘बालमूकादिविज्ञानसदृशं निर्विकल्पकम्’ । तर्कसंग्रहकार ने निर्विकल्पक ज्ञान का स्वरूप ‘इदं किंचित्’ (यह कुछ है) रूप से निरुपित किया है। किसी पदार्थ का प्रथम दर्शन होने पर जब हमें ‘यह कुछ है’ इस प्रकार से वस्तु के केवल अस्तित्व मात्र का अनुभव होता है तो वही ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान माना जाता है।
सविकल्पक प्रत्यक्ष का स्वरूप है ‘सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकम्’ अर्थात् सप्रकारक ज्ञान को सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। सविकल्पक शब्द की व्युत्पत्ति है ‘विकल्पेन सहितः सविकल्पः’ अर्थात् जिसमें विकल्प विद्यमान हो वह सविकल्पक कहलाता है। सविकल्पक का अर्थ है ‘नामजात्याद्ययोजनासहितं सविकल्पकम्’ । जो ज्ञान नाम, जाति आदि प्रकार से युक्त होता है उसे सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। आशय यह है कि जिस ज्ञान में विशेषण, विशेष्य तथा उनके मध्य के सम्बन्ध की प्रतीति होती है उसे ही सविकल्पक ज्ञान कहा जाता है। सविकल्पक ज्ञान का उदाहरण है ‘यह डित्थ है’ यहाँ डित्थ एक व्यक्तिविशेष का नाम है जो कि इस ज्ञान में भासित हो रहा है, इसलिए यह सविकल्पक ज्ञान है। इसी प्रकार ‘यह श्याम है’ इस ज्ञान में श्याम एकवर्ण है जो किसी पदार्थ का विशेषण है, इसलिए यह भी सविकल्पक ज्ञान है। मानव जीवन का समस्त व्यवहार सविकल्पक ज्ञान के आधार पर ही होता है।