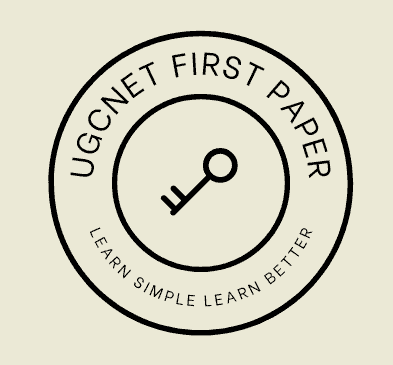अयोध्या : एक ऐतिहासिक विहंगम दृष्टिकोण
।। मनोज कुमार धुर्वे ।।
हृदय का गहरा घाव घट गया,
दुख का कुछ तो भार हट गया।
कुछ बड़े मीडिया घराने के कट्टरपंथी वामपंथी लोग जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं कि यह मंदिर चूंकि एक मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है अतः यह अन्याय है। यह असहनशीलता है। यह बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार है। और ऐसी ही अनेक अनर्गल बातें हो रही हैं किंतु क्या यही बात सत्य है।
जी नहीं! बिल्कुल भी नहीं।
इतिहास में अपने दृष्टिकोण से हम झाँकें :
यदि आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको आपका यह कर्तव्य है ।है यह दायित्व है और मीडिया घराने में होने के नाते आपका यह परम उत्तरदायित्व है कि आप सत्य का अनुसरण करें। और सत्य किसी समय सीमा में बंधा हुआ कैसे हो सकता है ? आप आज से केवल 500 वर्ष पूर्व तक ही क्यों जाते हैं? 500 वर्ष के पूर्व क्या कोई इतिहास नहीं था? आप हमेशा अपना ही दृष्टिकोण समग्र संसार पर क्यों थोपते हैं ?जब भारतीय परंपरा में जिसे भारतीय इतिहासकार इतिहास कहते हैं और अपने इतिहास को अपनी रीति से लिखते हैं और उन्हें वह पुराण कहते हैं।उन्हें महाभारत कहते हैं। उन्हें वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण कहते हैं तो आप अस्वीकार करने वाले कौन होते हैं? क्या हमें हमारा इतिहास भी आपकी दृष्टि से देखना होगा? हमने संसार में क्या किया है कब किया है कैसे किया है और हम अपने दृष्टिकोण को ऐसा क्यों रखते हैं यह क्या आप निश्चित करेंगे ? क्या यह हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपने दृष्टिकोण का निश्चय स्वयं करें। और वह दृष्टिकोण जो लाखों वर्षों से स्थापित है उसे हम आपके दृष्टिकोण की अधीनता में क्यों रखें?
अयोध्या नगरी की विशालता:
तो बात मंदिर की है, वहां पर अनेक प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। जो कोर्ट में भी पेश किए गए हैं कि वहां पर दर्शन करने और पूजा करने के लिए गुरु नानक देव जी भी गए थे। और यह घटना सिख अनुयायियों के ग्रंथों में आज भी उपलब्ध है। इसके अलावा वहां निरंतर पूजा होती रही है।इसके अलावा भारत के सभी ऐतिहासिक ग्रंथ इस बात से भरे पड़े हैं कि वहां पर अयोध्या पुरी नाम का एक बहुत ही विशाल शहर था, विशाल नगर था। जिसकी तुलना आज के मेट्रोपोलिटन सिटी में केवल मुंबई से की जा सकती है। इस बात के लिखित प्रमाणों को सभी को जांचना चाहिए।
पाँच सौ वर्ष पूर्व क्या हुआ:
आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि जब आज से 500 वर्ष पूर्व भारत की प्रजा में 90% से भी अधिक लोग या जनसमूह था। 100% के आसपास ही सभी गैर इस्लामिक लोग थे। और वह सभी भारतीय परंपरा का सम्मिलित रूप से निर्वाह करते हैं और ऐसे लोगों की श्रृद्धास्थली को एक अत्यंत बर्बर दृष्टिकोण रखने वाले बाबर ने जब लाखों लोगों की लाखों साधू सन्यासियों गृहस्थों भक्तों की निर्ममता से हत्या कर दी। हत्या करके उसने पर वह ध्वस्त हो चुकी बाबरी मस्जिद को बना दिया था।
भारतीय जनसमूह कि सामूहिक स्मृति का सतत प्रवाह:
(Social Trauma of Hindus)
तो क्या इस बात से समग्र भारतीय जनमानस में कोई पीड़ा नहीं हुई होगी ? क्योंकि वह मंदिर समग्र समाज की श्रद्धा का, भावना का प्रतीक था। सभी के लिए सम्मान का प्रतीक था। केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि संसार के अनेक देशों में रहने वाले भारतीय मूल के धर्म के लोगों के लिए वह श्रद्धा का पर्याय था। तब उनके मन में यह कैसी पीड़ा हुई होगी कि वह 500 साल से अपने बच्चों को उस घटना का वृतांत सुना सुना कर उन्हें यह समझाते रहे हैं कि हमारे साथ कितनी दुखद घटना घटित हुई थी। और बार-बार अपनी श्रद्धा से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि क्षमा करना रामलला हम मंदिर अब तक नहीं बना पाए, पर हम मंदिर बनाएंगे। रामलला हम आएँगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और वे जानते थे कि उस समय की सरकार इस तरह की विचारधारा की घोर विरोधी है और इसके उपरांत भी वे वहां गए और उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाईं। अपने प्राणों को निछावर करके भी उन्होंने यह कार्य किया। क्योंकि वे जानते थे कि यह हमारे दो पांच लोगों के हमारे कुछ लोगों के प्राणों से अधिक दुखदाई है। जो लोगों के अंतःकरण में सदियों से वह दुख की धारा सतत प्रवाहमान है। और वह दुख की धारा सुख की धारा में परिवर्तित करने के लिए किसी न किसी को तो बलिदान करना ही होगा और उन्होंने किया। और इस बात से उनका समाज उनके माता-पिता सभी को गर्व की अनुभूति होती है। भारतीय समाज इस मस्जिद के हटने से उसी प्रकार अपने को सुखी मान रहा है जैसे कि किसी के हृदय में कोई गहरा घाव हो गया हो और कोई डॉक्टर उस गहरे घाव का ऑपरेशन करके उसे ठीक कर दे। और हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के हृदय में इस मंदिर विध्वंस का गहरा घाव उनमें से एक यह अयोध्या थी। जिसको लेकर उन्होंने एक दो को नहीं बल्कि आने वाले हजारों वर्षों की परंपरा को सुख की अनुभूति करने के लिए एक कारण दिया एक सुखद आधार दिया है। इसलिए जो लोग भी यह समझते हैं कि यह मंदिर किसी का विरोध करके बना है तो वे यह इतिहास नहीं जानते कि यह इतिहास केवल 500 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ नहीं हुआ है। जिसे आप वहां तक जाकर रुक जाते हैं। बल्कि यह इतिहास भारतीय परंपरा के युगों का इतिहास है। जिसे भारतीयों ने न केवल अपने धर्म ग्रंथो में अपने इतिहास में बल्कि अपने जन समूह की संचित मनोवृति में, स्मृति में, लोकगीतों लोक कथाओं लोक आख्यानों आदि के रूप में पूरी तरह जीवंत बना कर रखा हुआ है। यदि इस प्रकार की कोई कल्पना मिथ या माइथॉलजी होती तब भी आपको क्या अधिकार है कि आप दूसरों से उनकी कल्पना का अधिकार छीन लो और उन पर अपनी संकुचित संकीर्ण दूषित और झूठी मान्यता को थोप दो।
सत्यप्रियता भारतीय स्वभाव:
यह कभी भी सत्यप्रिय मानव समुदाय सत्यप्रिय भारतीय जनमानस में स्वीकार्य नहीं हो सकता। चाहे इसके लिए हजारों वर्षों का समय ही क्यों न लगा देना पड़े। विश्व के उन लोगों को यह भ्रम है कि भारतीय संस्कृति को कुछ भौतिक प्रतीकों के मिटा देने से नष्ट किया जा सकता है।
इस बात पर यही कहना उचित रहेगा कि यह आपका दिन में देखा गया स्वप्न है जो कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता वास्तविकता में परिवर्तित नहीं हो सकता।
प्रजातंत्र पर रुदाली रुदन ढकोसला है :
जो लोग कह रहे हैं कि भारतवर्ष से प्रजातंत्र ही मिट गया है। क्या वे नहीं जानते कि जिनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की गई है उन्होंने अपनी प्रजा के केवल कुछ लोगों के सुख और आनंद के लिए अपने सबसे महान सुखों का भी बलिदान कर दिया था। क्या इससे बढ़कर भी कोई लोकतंत्र हो सकता है? क्या इससे बढ़कर भी कोई लोकतांत्रिक सरकार हो सकती है? क्या इससे बढ़कर भी कोई लोकतंत्र का नेता हो सकता है?
सामाजिक समरसता के पुरोधा श्रीराम:
जब सामाजिक समरसता की बात आती है, तो हम यह देख सकते हैं कि उनके जीवन में उन्होंने किसी को को भी अकारण दुत्कार नहीं दिया। उन्होंने सभी के भावों को उसी सहजता से ग्रहण किया जैसा उन्होंने भारत के प्रेम को ग्रहण किया था। जैसा उन्होंने वानर राज सुग्रीव और हनुमान जी के सद्भाव को ग्रहण किया था। जैसे उन्होंने राक्षसराज रावण के भाई विभीषण के भावों को ग्रहण किया था। जैसे उन्होंने पक्षीराज गरुड़ के भावों का ग्रहण करके उन्हें अपने पिता के तुल्य सम्मान दिया था। उन्होंने जंगल में जाकर वनवासियों के लिए योग क्षेम की व्यवस्था की थी। शबरी जो भील जनजाति से आई थी उस समय तो जनजातियों की कोई संकल्पना भी नहीं थी। वहां उस समय इस तरह के कभी प्रमाण नहीं आते कि व्यक्ति व्यक्ति में किसी तरह का भेदभाव किया करते थे। तब भी उन्होंने शबरी के भावों को ग्रहण किया यह नहीं देखा कि वह बेर जूठे करके उन्हें दे रही हैं।
संसार में ऐसे उदाहरणों का अन्यत्र अभाव :
क्या हृदय के निर्मल भावों को ग्रहण करने वाला ऐसा कोई स्वीकार्य चरित्र विरोध करने वालों के समग्र ग्रंथों में समग्र देश और काल में एक भी दिखाई देता है?
यदि आप धर्म के विरोधी हैं धर्म को नहीं मानते हैं संस्कृति को नहीं मानते हैं इतिहास को नहीं मानते हैं किंतु आप मानवीय संबंधों को मानवीय संवेदनाओं को तो मानते होंगे? ऐसा कौन सा प्राणी है जो भावनात्मक संवेदनाओं को ग्रहण नहीं करता और उनका सम्मान नहीं करता। सभी प्राणी करते हैं। तब एक मानव होने के नाते आप इन संवेदनाओं की दृष्टि से भी यदि चरित्र को देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इससे अधिक उत्तम लोकतंत्र की स्थापना होती है। इससे अधिक मानवीय दृष्टिकोण लागू होता है। इससे संवेदनाएं केवल मानवीय नहीं रह जाती बल्कि समग्र प्राणियों तक वह विस्तृत हो जाती है। और यह केवल प्राणी जगत तक न होकर यह समग्र जड़ चेतन तक व्याप्त हो जाती है।
इसलिए लोकतंत्र के नष्ट होने या धर्म की सिद्धि होने या राजनीति और धर्म के एक हो जाने का रुदाली रुदन निरंतर जो लोग कर रहे हैं उन्हें यह समझ में आना चाहिए कि आप जो कुछ सोच रहे हैं वह न सत्य है न वास्तविकता है। न वैसा होने वाला है। भारतीय जन समुदाय ही वह समुदाय है जो अपनी परंपराओं से लोकतंत्र को स्वीकारता है। और जहां पर उसके प्रति दुराग्रह रखने वाले उसकी संस्कृति और सभ्यता के प्रतीकों को बर्बरता से नष्ट करने वाले लोगों के प्रति भी वह सहनशील होकर उन्हें चैन से जीने खाने देता है अपने वंश की वृद्धि करने देता है।
स्वरक्षा का सबको नैतिक अधिकार है:
वह तभी उनके प्रति प्रतिकार करता है जब वह उसे उसकी जीवन यात्रा से ही अलग कर देना चाहते हैं। जब वह उसे उसके जीवन की प्राण वायु तुल्य अपनी संस्कृति से अलग करके उसे अपने सीमित संकीर्ण और दुराग्रह भारी विचारधारा में उसकी अपनी इच्छा के विरुद्ध शामिल कर लेना चाहते हैं। अब आप यह देखिए कि यह तो संवैधानिक कानून भी है कि अपने प्राणों की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति यदि हिंसा करता है तो वह हिंसा हिंसा नहीं मानी जाती, बल्कि अपनी प्राण रक्षा मानी जाती है। और इस प्रकार उस व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है। भले ही उसने अपनी रक्षा में लोगों के प्राण हर लिए हों। क्योंकि यह उसका मूलभूत कर्तव्य है कि वह अपने अस्तित्व की रक्षा करे। अपने प्राणों की रक्षा करे। और अपने प्राणों की रक्षा करने के आड़े जो भी आता है उसे नष्ट कर दे क्योंकि वह विघ्नों के पास नहीं गया था वे विघ्न उसे नष्ट करने के लिए उसके पास आए थे। और यही नियति है यही आदि नीति है।
आततायी हन्तव्यम् :
और इसीलिए भारतीय संस्कृति कहती है कि आततायी हन्तव्यम्। जो भी ऐसे लोग हैं जो अकारण सज्जनों को सताते हैं उनके प्राण हरने में कोई पाप नहीं है कोई दोष नहीं है। भारतीय परंपरा में सामान्यतः यह कहा जाता है की स्त्री ब्राह्मण बालक निहत्थे और अपने समूह से जो अलग हो गया है उस पर कभी भी आक्रमण नहीं करना चाहिए। आक्रमण करके उसे कभी नष्ट नहीं करना चाहिए।
किंतु जब राजकुमार राम को उनके गुरुदेवता विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए और उन्होंने कहा कि हे राम! इस ताड़का का वध कर दो। तब राम के हाथों में संकोच आ गया कि वह एक स्त्री का वध कैसे करें? यह तो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। तब विश्वामित्र ने उन्हें शिक्षा दी कि हे राम! यह स्त्री स्त्री धर्म का पालन नहीं कर रही है। बल्कि यह शत्रु के रूप में तुम्हारे हमारे समक्ष प्रकट हुई है। और यह हमारे सहज कर्तव्यों में अकारण ही विघ्न डाल रही है अतः इसका वध करने में कोई पाप नहीं है। और उन्होंने उसका वध कर दिया।
भारतवर्ष में वर्ण के आधार :
दूसरा दृष्टांत आता है कि जब भगवान परशुराम जी ने पितामह भीष्म से कहा कि तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। तब भीष्म पितामह ने अपने आयुध धारण करते हुए उनसे कहा कि इस समय आप क्षत्रिय धर्म का निर्वाह कर रहे हैं इसलिए आपके साथ युद्ध करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय को क्षत्रिय के साथ युद्ध करना चाहिए और उन्होंने युद्ध किया। इस पर कभी किसी ने प्रश्न खड़ा नहीं किया। रावण हुआ तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न था किंतु उसके कर्तव्यों को देखकर सभी उसे राक्षस राज रावण कहा करते थे यह इस बात की भी पुष्टि करता है कि गीता में कहा गया गुण कर्म विभागश: के अनुसार ही वर्णों का निश्चय होता है जाति की कल्पना तो भारतीय शास्त्रों में कहीं है ही नहीं व्यर्थ का हौवा बना दिया गया है। गीता में जो कहा गया है कि ‘गुण कर्म विभागश:’। जिसका अर्थ है कि यह वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी। जाति शब्द का इन अर्थों में किसी भी मूलभूत संस्कृत ग्रंथों में वर्णन नहीं है। हां यह दोष भारतीय समाज में आ गया था और अब उसी प्रकार जा भी रहा है किंतु यह यहां के शास्त्रों में सांस्कृतिक सिद्धांँतों के रूप में उपस्थित नहीं है।
- 11 – भाद्रपद मासकी ‘अजा’ और ‘पद्मा’ एकादशीका माहात्य
- 14 – पुरुषोत्तम मासकी ‘कमला’ और ‘कामदा’
- 13 – कार्तिक मासकी ‘रमा’ और ‘प्रबोधिनी’एकादशीका माहात्म्य
- 12 – आश्विन मासकी ‘इन्दिरा’ और ‘पापाङ्कुशा’ एकादशीका माहात्य
- 10 – श्रावण मासकी ‘कामिका’ और ‘पुत्रदा’ एकादशीका माहात्म्य