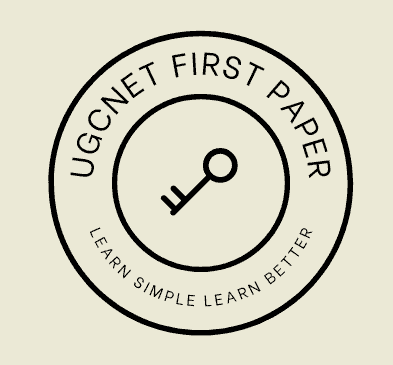10.6-Policies Governance and Administration part-01
“नीतियाँ-शासन एवं प्रशासन” विषय उच्च शिक्षा प्रणाली का कोई नया विषय नहीं है। पेपर 1 के संशोधित यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में शब्द “राजनीति” से “नीति” में एकमात्र परिवर्तन है। भारत की नीतियां, शासन और प्रशासन भारत के संविधान द्वारा चलाए जाते हैं।

भारतीय संविधान की मूल बातें
भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने वाली रूपरेखा तैयार करता है, सरकारी संस्थानों की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों को स्थापित करता है, और मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है।
भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 25 भागों में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 104 संशोधन शामिल हैं।
लेकिन प्रारंभ के समय भारतीय संविधान में 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। अंग्रेजी संस्करण के अलावा, एक आधिकारिक हिंदी अनुवाद भी है ।
मौलिक अधिकार समिति और संघ संविधान समिति जैसी विभिन्न विषय समितियों ने अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे और सभी प्रस्तावों पर सामान्य चर्चा के बाद, डॉ. बीआर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति नियुक्त की गई थी। मसौदा समिति को समितियों द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव को जोड़ने, संशोधित करने या हटाने का पूर्ण अधिकार था। भारतीय संविधान के अंतिम मसौदे पर 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर हुए, जिसे पारित होने की तिथि के रूप में जाना जाता है । चूंकि संविधान सभा, जिसने संविधान को अंतिम रूप दिया था, भारत के लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से विधिवत चुनी गई थी, भारत का संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है। इस प्रकार संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 1930 की स्वतंत्रता की पूर्ण स्वराज घोषणा को मनाने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। इसके अपनाने के साथ, भारत संघ आधिकारिक तौर पर बन गया। आधुनिक और समकालीन भारत गणराज्य और इसने देश के मौलिक शासकीय दस्तावेज़ के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान ले लिया।
भारतीय संविधान ने दुनिया के अन्य संविधानों से काफी हद तक उधार लिया है और इसे “सुंदर पैचवर्क” कहा जा सकता है।
उधार ली गई कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
| विशेषता | स्रोत/प्रेरणा | |
| 1. | मौलिक अधिकार | यूएसए |
| 2. | सरकार की संसदीय प्रणाली | यूके |
| 3. | राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत | आयरलैंड (आयर) |
| 4. | आपातकालीन प्रावधान | जर्मनी (तीसरा रैह) |
| 5. | संशोधन प्रक्रिया | दक्षिण अफ्रीका |
| 6. | भारत के संविधान की प्रस्तावना | फ्रांस |
| 7. | शासन का संघीय मॉडल | कनाडा |
संरचना: संविधान, अपने वर्तमान स्वरूप में, एक प्रस्तावना, 25 भागों से युक्त है जिसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 2 परिशिष्ट और 104 संशोधन शामिल हैं।
प्रस्तावना: प्रस्तावना का मसौदा जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और यह अमेरिकी मॉडल पर आधारित है। 42 वें संशोधन में “धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी” शब्द जोड़े गए और अब प्रस्तावना इस प्रकार है:
“हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का गंभीरता से संकल्प लेते हैं:
न्याय; सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;
स्वतंत्रता; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा का;
समानता; स्थिति और अवसर का; और उन सब के बीच प्रचार करना;
बिरादरी; व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना;
26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाएं, अधिनियमित करें और स्वयं को सौंपें।”
प्रस्तावना, तकनीकी रूप से, संविधान का हिस्सा नहीं है (और इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने भी की है), लेकिन इसमें पूरे संविधान का मूल दर्शन और संविधान निर्माताओं के आदर्श शामिल हैं। इसका उपयोग न्यायालयों द्वारा कुछ मामलों में संविधान की व्याख्या में मदद करने के लिए किया जा सकता है जहां संविधान स्वयं मौन है।
संविधान के भाग
संविधान के अलग-अलग अनुच्छेदों को निम्नलिखित भागों में एक साथ बांटा गया है:
प्रस्तावना
भाग I – संघ और उसका क्षेत्र
भाग II – नागरिकता।
भाग III – मौलिक अधिकार।
भाग IV – राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
भाग IVA – मौलिक कर्तव्य।
भाग V – संघ।
भाग VI – राज्य।
भाग VII – प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्य (निरस्त) ।
भाग VIII – केंद्र शासित प्रदेश
भाग IX – पंचायतें।
भाग IXA – नगर पालिकाएँ।
भाग IXB – सहकारी समितियाँ
भाग X – अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र
भाग XI – संघ और राज्यों के बीच संबंध।
भाग XII – वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे
भाग XIII – भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य
भाग XIV – संघ, राज्यों के अधीन सेवाएँ।
भाग XIVA – न्यायाधिकरण।
भाग XV – चुनाव
भाग XVI – कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान।
भाग XVII – भाषाएँ
भाग XVIII – आपातकालीन प्रावधान
भाग XIX – विविध
भाग XX – संविधान का संशोधन
भाग XXI – अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान
भाग XXII – संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ की तारीख, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन
| भाग | लेख | संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित है |
| भाग I | अनुच्छेद 1-4 | भारत का क्षेत्र, नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना या गठन |
| भाग द्वितीय | अनुच्छेद 5-11 | सिटिज़नशिप |
| भाग III | अनुच्छेद 12-35 | मौलिक अधिकार |
| भाग IV | अनुच्छेद 36-51 | राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत |
| भाग IV ए | अनुच्छेद 51-ए | भारत के नागरिक के कर्तव्य. इसे 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था |
| भाग वी | अनुच्छेद 52-151 | संघ स्तर पर सरकार |
| भाग VI | अनुच्छेद 152-237 | राज्य स्तर पर सरकार |
| भाग सातवीं | अनुच्छेद 238 | पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों से संबंधित है। इसे 1956 में 7वें संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया |
| भाग आठवीं | अनुच्छेद 239-241 | केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन |
| भाग IX | अनुच्छेद 242-243 | पहली अनुसूची के भाग डी के क्षेत्र और अन्य क्षेत्र। इसे 1956 में 7वें संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया |
| भाग एक्स | अनुच्छेद 244-244 ए | अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र |
| भाग XI | अनुच्छेद 245-263 | संघ और राज्यों के बीच संबंध |
| भाग XII | अनुच्छेद 264-300 | वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे |
| भाग XIII | अनुच्छेद 301-307 | भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और यात्रा |
| भाग XIV | अनुच्छेद 308-323 | संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएँ |
| भाग XIV-ए | अनुच्छेद 323ए-323बी | 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया और विवादों और अन्य शिकायतों की सुनवाई के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है |
| भाग XV | अनुच्छेद 324-329 | चुनाव और चुनाव आयोग |
| भाग XVI | अनुच्छेद 330-342 | कुछ वर्गों एसटी/एससी और एंग्लो इंडियंस के लिए विशेष प्रावधान |
| भाग XVII | अनुच्छेद 343-351 | आधिकारिक भाषायें |
| भाग XVIII | अनुच्छेद 352-360 | आपातकालीन प्रावधान |
| भाग XIX | अनुच्छेद 361-367 | राष्ट्रपति और राज्यपालों को आपराधिक कार्यवाही से छूट के संबंध में विविध प्रावधान |
| भाग XX | अनुच्छेद 368 | संविधान में संशोधन |
| भाग XXI | अनुच्छेद 369-392 | अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान |
| भाग XXII | अनुच्छेद 393-395 | संक्षिप्त शीर्षक, संविधान का प्रारंभ और निरसन |
संघीय व्यवस्था
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को “राज्यों का संघ” के रूप में वर्णित करता है। “संघ” शब्द का तात्पर्य यह है कि:
- भारतीय संघ स्वयं राज्यों द्वारा स्वैच्छिक समझौते का परिणाम नहीं है। जैसा कि सर्वविदित है, भारत की स्वतंत्रता के बाद, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 550 से अधिक राज्यों को भारत संघ में एकीकृत किया गया था, जिसके कारण उन्हें “भारत का लौह पुरुष” कहा जाने लगा। इसलिए, भारत में उनका समावेश पूरी तरह से अनैच्छिक है।
- भारतीय संघ के घटकों को इससे अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। (तत्कालीन यूएसएसआर या वर्तमान यूएसए के विपरीत जहां ऐसी स्वतंत्रता राज्यों में निहित थी/है)।
भारतीय संघीय व्यवस्था इस अर्थ में अद्वितीय है कि एक संघीय व्यवस्था होने के बावजूद, इसमें अभी भी एक विशिष्ट संघीय व्यवस्था (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका) की कई विशेषताएं नहीं हैं। सामान्य तौर पर, भारतीय व्यवस्था को ज्यादातर अर्ध – संघीय या अर्ध – संघीय के रूप में वर्णित किया गया है , इस तथ्य के कारण कि शक्ति का संतुलन केंद्र के पक्ष में भारी झुकता है यानी राज्यों को अधिकांश क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कम शक्तियों का आनंद मिलता है। केंद्र।
संघ का क्षेत्र
भारत के क्षेत्र में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र शामिल है जिस पर कुछ समय के लिए भारत की संप्रभुता कायम है। दूसरी ओर, भारत संघ में केवल वे घटक इकाइयाँ, यानी राज्य शामिल हैं, जो केंद्र के साथ शक्ति साझा करते हैं। केंद्रशासित प्रदेश केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। आज की तारीख में, भारत के क्षेत्र में 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी- दिल्ली न तो पूर्ण राज्य है और न ही केंद्र शासित प्रदेश) शामिल है। भारत एक संघीय संवैधानिक गणराज्य है जो संसदीय प्रणाली के तहत शासित होता है जिसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। सभी राज्यों, साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निर्वाचित विधानसभाएं और सरकारें हैं, दोनों वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित हैं । नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में विधानसभाएं और सरकारें भी होंगी। शेष पांच केंद्र शासित प्रदेशों पर नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से सीधे केंद्र द्वारा शासन किया जाता है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया।
इस प्रावधान का उपयोग करते हुए, भारतीय क्षेत्र की राजनीतिक संरचना में कई ऐतिहासिक परिवर्तन लाए गए हैं, जिनमें से कुछ नीचे दी गई तालिका में पाए गए हैं:
| अधिनियम/विधान | परिवर्तन | |
| 1 | राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 | आंध्र, केरल का गठन (भाषाई आधार पर आंध्र पहला राज्य) |
| 2 | बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960 | नये राज्य के रूप में गुजरात, महाराष्ट्र का जन्म हुआ |
| 3 | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 | पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ बनाया गया |
| 4 | मैसूर राज्य अधिनियम, 1973 | मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक हो गया |
| 5 | मिज़ोरम राज्य अधिनियम, 1986 | मिज़ोरम, जो पहले एक केंद्रशासित प्रदेश था, एक राज्य बन गया |
| 6 | अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 | अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया |
| 7 | गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 | गोवा को राज्य बनाया |
मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य
10.6-Policies, Governance, and Administration part-01
मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानवाधिकार हैं जिनकी गारंटी सभी नागरिकों को दी गई है। वे नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना लागू होते हैं। गौरतलब है कि मौलिक अधिकार कुछ शर्तों के अधीन अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं।
इन अधिकारों को दो कारणों से मौलिक अधिकार कहा जाता है:
- वे संविधान में निहित हैं जो उन्हें गारंटी देता है।
- वे न्याययोग्य (अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय) हैं। उल्लंघन के मामले में, कोई व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब मौलिक अधिकार सात थे, लेकिन बाद में एक अधिकार हटा दिया गया।
- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
- सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
- संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) (इसे बाद में हटा दिया गया)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)।
छह मौलिक अधिकार
भारतीय संविधान में छह मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। वे नीचे सूचीबद्ध हैं:
1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण
अनुच्छेद 15: केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता
अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत
अनुच्छेद 18: उन्मूलन
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
अनुच्छेद 19: यह भारत के नागरिकों को निम्नलिखित छह मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है:
- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- सदन की स्वतंत्रता
- संघ बनाने की स्वतंत्रता
- आंदोलन की स्वतंत्रता
- निवास और निपटान की स्वतंत्रता
- पेशे, व्यवसाय, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण
अनुच्छेद 21 ए: शिक्षा का अधिकार
अनुच्छेद 22: कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध
अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध।
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने, अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 26: धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 27: धार्मिक आधार पर करों पर रोक लगाता है
अनुच्छेद 28: कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक समारोहों में भाग लेने की स्वतंत्रता
5. सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा
अनुच्छेद 30: शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार
अनुच्छेद 31: 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा छोड़ा गया
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32-35)
अनुच्छेद 32: अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय (और उच्च न्यायालयों में भी) जाने का अधिकार
अनुच्छेद 33: अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद 34: किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर अधिकारों पर प्रतिबंध।
अनुच्छेद 35: प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान।
रिट क्या है?
रिट नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन से बचाने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी लिखित आदेश हैं।
रिट का प्रकार
संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देता है। रिट के प्रकार निम्नलिखित हैं:
- बन्दी प्रत्यक्षीकरण
- सर्टिओरारी
- निषेध
- परमादेश
- क्वो वारंटो
मौलिक कर्तव्य
1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए मौलिक कर्तव्य, संस्कृति को बनाने और बढ़ावा देने के अलावा, मौलिक अधिकारों के साथ-साथ इन कर्तव्यों को लागू करने में विधायिका के हाथों को भी मजबूत करते हैं।
अनुच्छेद 51-ए के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक द्वारा पालन किए जाने वाले 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची नीचे दी गई है:
- संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें।
- स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोएं और उनका पालन करें।
- भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें।
- देश की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करें।
- धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना।
- देश की मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दें और उसका संरक्षण करें।
- जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करें और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखें।
- वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करें।
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें।
- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करें ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके।
- छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के उसके बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
- LIFE SCIENCES – 703 Exam Date : 01-Mar-2025 Batch : 15:00-18:00
- EARTH ATMOSPHERIC OCEAN AND PLANETARY SCIENCES – 702-Solved Paper-02-Mar-2025 Batch : 09:00-12:00
- SOLVED FIRST PAPER -CSIR UGC NET EXAM-20Q-28-FEB-25
- CSIR NET-CHEMICAL SCIENCES- FIRST PAPER-27-JUL-24-SOLVED PAPER
- CSIR NET SOLVED FIRST PAPER 28 JULY 2025