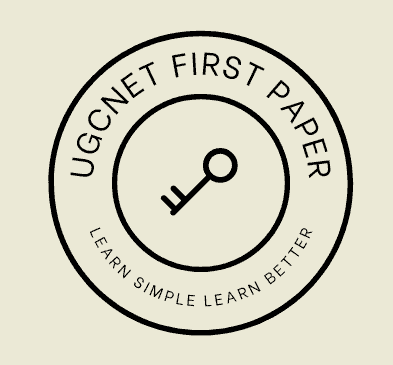10.2 Evolution of Higher Learning and Research in hindi
यदि आप यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उच्च शिक्षा प्रणाली क्षेत्र में हाल में हो रही घटनाओं पर नजर रखनी होगी। ऐसा देखा गया है कि अधिकांश समय प्रश्न कुछ तथ्यात्मक डेटा और नए अनुकूलन या नीति में बदलाव के आधार पर पूछे जाते थे। अगर हम (यूजीसी) नेट पेपर 1 के पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं तो पेपर 1 के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली अनुभाग निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में निहित था।
इसलिए निम्नलिखित विषयों पर बुनियादी विचार रखना महत्वपूर्ण है:-
उच्च शिक्षा में संगठन और शासन की समझ। (विभिन्न प्रकार के कॉलेज और विश्वविद्यालय)
उच्च शिक्षा के विभिन्न संस्थान।
उच्च शिक्षा शासन, प्रशासन और शैक्षिक राजनीति। (नई शिक्षा नीति)
विशिष्ट संगठनात्मक नीति लक्ष्य और कार्यान्वयन (यूजीसी, एनएएसी, एआईसीटीई)
बदलते संगठन और प्रणालियाँ। (हाल के बदलाव)
सचेत! इस इकाई पर आपके ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि विषय विशाल हैं और आपको इस इकाई पर आधारित हमेशा आश्चर्यजनक प्रश्न मिलेंगे।
इस लेख के पूरा होने के बाद आप –
स्वतंत्रता के बाद के भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान की अवधारणा को समझना
- उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका को समझना
- यूजीसी और उच्च शिक्षा नियामक ढांचे के महत्व को समझना
- भारत में नियामक और वैधानिक निकायों की सूची (कुल-15)
- उच्च शिक्षा प्रणाली पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे ।
- नई शिक्षा नीति एवं उच्च शिक्षा की चुनौतियों को जानना।
तो आइए उच्च शिक्षा प्रणाली पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण विषयों और मुख्य तथ्यों पर नजर डालें।
स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास।
मानव सभ्यता की शुरुआत से ही भारत की पहचान हमेशा ज्ञान केंद्र के रूप में की गई है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में वर्षों से कायापलट के बदलाव और चुनौतियाँ देखी जा रही हैं, यानी प्राचीन गुरुकुल प्रणाली से लेकर आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण प्रणाली ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है।
यह इस बात से स्पष्ट है कि ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में शिक्षा के केंद्र बौद्ध मठ थे और तीसरी शताब्दी ईस्वी में नालंदा थे। इनमें से कुछ केंद्र बहुत बड़े थे जिनमें कई संकाय थे। देश में आक्रमणों और अव्यवस्थाओं ने प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को ख़त्म कर दिया है।
भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने वाला पहला कॉलेज 1918 में बंगाल के सेरामपुर में स्थापित किया गया था। 1857 में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के तीन केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, 27 कॉलेज संबद्ध किए गए। 1947 में भारत में 19 विश्वविद्यालय थे। (सीएबीई, 2005)।
स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली उल्लेखनीय रूप से विकसित हुई है और दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली बन गई है।
भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली ने अपनी स्वयं की प्रणाली और संरचना विकसित की। चूँकि भारतीय संविधान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संघ और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी का प्रावधान करता है।
उच्च शिक्षा के भीतर सीखने, अनुसंधान और नवाचार के बीच संबंध टिकाऊ ज्ञान समाज के निर्माण की कुंजी है।
शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय लचीलेपन के प्रावधानों के आधार पर, देश में उच्च शिक्षा प्रणाली में विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय और संस्थान हैं
भारत में अलग-अलग उच्च शिक्षा संस्थान हैं, जैसे केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय, एकात्मक और संबद्ध विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, डीम्ड विश्वविद्यालय और मुक्त विश्वविद्यालय।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या एआईसीटीई के माध्यम से केंद्र सरकार विभिन्न राज्य संचालित विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करती है। भारत में विश्वविद्यालय कार्यात्मक रूप से बहु-संकाय विश्वविद्यालय, एकल संकाय विश्वविद्यालय (कृषि, तकनीकी और चिकित्सा विश्वविद्यालय) हैं, इसके अलावा विश्वविद्यालयों के अलावा आईआईटी, आईआईएम जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी हैं जो विश्वविद्यालय माने जाते हैं (बीआईटीएस, आईआईएससी)।
देश में उच्च शिक्षा प्रणाली कई एजेंसियों द्वारा शासित होती है, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) सर्वोच्च निकाय है।
इन एजेंसियों के नियम और कानून उच्च शिक्षा प्रणाली को और अधिक जटिल बनाते हैं। देश में नियामक ढांचे में विभिन्न हितधारक राज्य सरकारें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) आदि जैसी पेशेवर परिषदें हैं।
स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा का विकास अभूतपूर्व है। आधी सदी से भी अधिक समय हो गया है जब से सरकार ने विशेष रूप से 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के साथ देश में उच्च शिक्षा के नियोजित विकास की शुरुआत की है। 1950 और 2012 के दौरान विश्वविद्यालयों की संख्या 20 से बढ़कर लगभग 659 हो गई है, और कॉलेज 500 से 33023 तक, और शिक्षक 15,000 से 9.46 लाख.
परिणामस्वरूप, छात्रों का नामांकन 1950 में मात्र 0.1 मिलियन से बढ़कर 25.9 मिलियन हो गया है। (यूजीसी रिपोर्ट 2012 के आधार पर)।
आइए अब तक हुई प्रगति पर नजर डालें…
राधाकृष्णन आयोग (1948-49)
आज़ादी के बाद भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करने वाला पहला प्रमुख आयोग 1948-49 में राधाकृष्णन आयोग (जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है) था।
आयोग को ‘भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट करने और देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप वांछनीय सुधार और विस्तार का सुझाव देने’ के विशिष्ट उद्देश्य से नियुक्त किया गया था।
राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट का एक प्रमुख अध्याय विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम (भाषा) की समस्या के लिए समर्पित था।
आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफ़ारिश यह थी कि ग्रेट ब्रिटेन में विश्वविद्यालय अनुदान समिति की तर्ज़ पर एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए, जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के बीच संपर्क स्थापित करे।
सरकार और विश्वविद्यालय.
यह अंतिम सिफ़ारिश 1956 में वास्तविकता बन गई जब संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना की गई जिसमें कहा गया था कि “संविधान का
भारत उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के संबंध में विशेष अधिकार संसद को देता है।
माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदलियार आयोग)-
देश में माध्यमिक शिक्षा की प्रचलित प्रणाली की जांच करने के लिए 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में भारत सरकार के संकल्प द्वारा माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी।
इसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों, संगठन और सामग्री, प्राथमिक और उच्च शिक्षा के साथ इसके संबंध और विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्संबंध के संदर्भ में इसके पुनर्गठन और सुधार के लिए उपाय सुझाना था।
कोठारी आयोग 1964
आयोग की नियुक्ति भारत सरकार के 14 जुलाई, 1964 के एक संकल्प के प्रावधान के तहत की गई थी और इसने 2 अक्टूबर,1964 को अपना कार्य शुरू किया।
आयोग में भारत और विदेश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात शिक्षाविद् शामिल थे। इसमें कुल 17 सदस्य शामिल थे, जिसमें 14 सदस्य, 1 सदस्य – सचिव, 1 सहयोगी – सचिव और यूजीसी के अध्यक्ष डॉ. डीएस कोठारी को आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसलिए इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है।
आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसे 29 अगस्त, 1966 को सदन के पटल पर रखा गया था। आयोग की रिपोर्ट, लगभग 700 पृष्ठों का एक विशाल दस्तावेज़ है। इसे शिक्षा में सभी बदलावों और सुधारों के लिए संदर्भित माना गया है।
हालांकि यह 20 साल पुराना है, फिर भी इसकी खुशबू और ताजगी बरकरार है। यहां तक कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) भी मुख्य रूप से इसकी सिफारिशों पर आधारित है। इसे शिक्षकों के लिए बाइबिल कहा जाता है और इसे उत्साह के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
राममूर्ति समीक्षा समिति-
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए समिति का गठन 7 नवंबर 1990 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष आचार्य राममूर्ति और सोलह अन्य सदस्य थे। इस समिति की रिपोर्ट का शीर्षक है “एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर ” ।
समिति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने और समय-सीमा के भीतर संशोधित नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नीति और कार्रवाई के संशोधन के संबंध में सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था।
उच्च शिक्षा विभाग, एमएचआरडी, नीति और योजना दोनों के संदर्भ में, उच्च शिक्षा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार है। एक नियोजित विकास प्रक्रिया के तहत, विभाग विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों के माध्यम से उच्च शिक्षा तक पहुंच के विस्तार और गुणात्मक सुधार पर ध्यान देता है।
उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका
सभी तरीकों से पहुंच का विस्तार करके सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि।
समाज के उन वर्गों की भागीदारी को बढ़ावा देना जिनका जीईआर राष्ट्रीय औसत से कम है।
गुणवत्ता में सुधार करना और शैक्षणिक सुधारों को बढ़ावा देना
नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और मौजूदा संस्थानों की क्षमता विस्तार और सुधार भी।
उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग।
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास का विकास।
भारतीय भाषाओं का विकास.
शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
[स्रोत – http://mhrd.gov.in/overview ]
यूजीसी और उच्च शिक्षा नियामक ढांचा
आजादी के तुरंत बाद, 1948 में डॉ. एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य “भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट करना और देश की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप सुधार और विस्तार का सुझाव देना” था। .
इसने सिफारिश की कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति को यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल पर पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से नियुक्त किया जाए।
1952 में, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के संस्थानों को सार्वजनिक निधि से सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा जा सकता है । नतीजतन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का औपचारिक उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री स्वर्गीय श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था।
हालाँकि, यूजीसी को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
पूरे देश में प्रभावी क्षेत्र-वार कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बैंगलोर में छह क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करके अपने संचालन को विकेंद्रीकृत किया है। यूजीसी का मुख्य कार्यालय स्थित है
नई दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, 35, फ़िरोज़ शाह रोड और दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर से भी दो अतिरिक्त ब्यूरो संचालित होते हैं।
इसके बारे में और पढ़ें – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम और अधिनियम, 1956 के तहत नियम और विनियम – यूजीसी अधिनियम
उच्च शिक्षा नियामक ढांचा
भारत में उच्च शिक्षा की नियामक संरचना
भारत में इस क्षेत्र का नियामक ढांचा बहुस्तरीय है। वितरण की अंतिम श्रृंखला – कक्षा में, नियमों के तीन सेट संचालित होते हैं – विश्वविद्यालय, कॉलेज और परिषद
अपनी स्वयं की डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों को उनके प्रबंधन के आधार पर पांच प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है – केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय-मानित संस्थान और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। कॉलेज उस विश्वविद्यालय के नाम पर डिग्री प्रदान करते हैं जिससे वे संबद्ध हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक संगठन है।
पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अलावा, आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उन उपायों पर सलाह भी देता है जो उच्च शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक हैं। यह नई दिल्ली के साथ-साथ बैंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थित अपने छह क्षेत्रीय कार्यालयों से कार्य करता है।
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) और बार काउंसिल इंडिया (बीसीआई) जैसे विभिन्न नियामक निकाय विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रबंधन करते हैं। दो मान्यता प्राप्त संस्थान हैं- अर्थात् एआईसीटीई द्वारा स्थापित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) और यूजीसी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी)।
तृतीयक क्षेत्र में मुख्य शासी निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) है। इसमें अनुदान प्रदान करने के साथ-साथ उच्च शिक्षा संस्थानों के मानकों का समन्वय और रखरखाव करने का दोहरा कार्य है।
सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा शासित होते हैं, साथ ही इसके द्वारा वित्त पोषित भी होते हैं। 1956 का यूजीसी अधिनियम उस विश्वविद्यालय के संपूर्ण चरण-दर-चरण प्रशासन को निर्दिष्ट करता है जिसे वह नियंत्रित करता है, जिसमें कार्य दिवसों की संख्या से लेकर प्रति विषय व्याख्यान घंटों की संख्या, साथ ही छात्रों के नामांकन और शिक्षकों के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता शामिल है। एक पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए.
यूजीसी विनियम, 2012 कहता है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को एक मान्यता एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
यूजीसी की शक्तियों और कार्यों में विकास, रखरखाव के साथ-साथ अनुसंधान उद्देश्यों, विश्वविद्यालयों के निरीक्षण, डिग्री प्रदान करने आदि के लिए केंद्र/राज्य सरकार से धन का आवंटन और संवितरण शामिल है।
केंद्र सरकार देश में उच्च शिक्षा से संबंधित प्रमुख नीति के लिए जिम्मेदार है। यह यूजीसी को अनुदान प्रदान करता है और देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करता है। केंद्र सरकार यूजीसी की सिफारिश पर शिक्षा संस्थानों को ‘मानित विश्वविद्यालय’ घोषित करने के लिए भी जिम्मेदार है।
केंद्र सरकार की विशेष संवैधानिक जिम्मेदारी: शिक्षा संविधान की संघ सूची में प्रविष्टि 66 के अधीन ‘समवर्ती सूची’ पर है। यह केंद्र सरकार को विशेष विधायी शक्ति प्रदान करता है। उच्च शिक्षा या अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए।
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में संघ और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग लाया जाता है।
यूजीसी का समर्थन करते हुए, विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए मान्यता की देखरेख निम्नलिखित पंद्रह स्वायत्त नियामक और वैधानिक संस्थानों द्वारा की जाती है:
भारत में नियामक और वैधानिक निकायों की सूची (कुल-15)
भारत में उच्च शिक्षा के लिए नियामक और वैधानिक निकायों की सूची
• अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)
• भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)*
• केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच)
• दूरस्थ शिक्षा परिषद (दिसंबर)
• भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई)
• केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (सीसीआईएम)
• भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)
• ग्रामीण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय परिषद
• भारतीय फार्मेसी परिषद (पीसीआई)
• भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी)
• वास्तुकला परिषद
• राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई)
• भारतीय बार काउंसिल (बीसीआई)
• राज्य उच्च शिक्षा परिषदें
• भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई)
संक्षेप में, ये उपरोक्त परिषदें पाठ्यक्रमों की मान्यता, व्यावसायिक संस्थानों को बढ़ावा देने, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम को विनियमित करने, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुदान और अन्य पुरस्कार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये निकाय उच्च शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
स्रोत – (भारत में विनियामक और वैधानिक निकायों की सूची का विवरण यूजीसी की वेबसाइट से लिया गया है। समय-समय पर इसमें बदलाव होता रहता है। हम इस पृष्ठ को अद्यतन रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, भले ही कभी-कभी आपको यह पुराना लगे। – आप यूजीसी वेबसाइट का संदर्भ ले सकते हैं)
- 11 – भाद्रपद मासकी ‘अजा’ और ‘पद्मा’ एकादशीका माहात्य
- 14 – पुरुषोत्तम मासकी ‘कमला’ और ‘कामदा’
- 13 – कार्तिक मासकी ‘रमा’ और ‘प्रबोधिनी’एकादशीका माहात्म्य
- 12 – आश्विन मासकी ‘इन्दिरा’ और ‘पापाङ्कुशा’ एकादशीका माहात्य
- 10 – श्रावण मासकी ‘कामिका’ और ‘पुत्रदा’ एकादशीका माहात्म्य