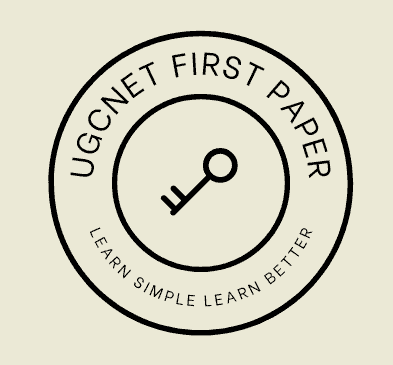सम्प्रेषण की प्रक्रिया में ऐसा कोई भी कारण जो सम्प्रेषण के रूप को बिगाड़ दे अथवा उसको पंहुचने से रोक दे, अवरोध कहलाता है। इसके कारण विचारों, सूचना और सुझावों के प्रभावी आदान-प्रदान में बाधा उत्पन्न होती है। अवरोधों को ठीक प्रकार से समझने के लिए उनकों मुख्य रूप से तीन वर्गों में वैयक्तिक अवरोध, पर्यावरणीय अवरोध और यांत्रिक अवरोध में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक को उपवर्गो में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है।
वैयक्तिक अवरोध
वैयक्तिक अवरोध दो प्रकार के हैं : अन्तः वैयक्तिक अवरोध और अन्तर वैयक्तिक अवरोध । आइये इनका विस्तृत अध्ययन करें ।
अन्तः – वैयक्तिक सम्प्रेषण अवरोध
किसी व्यकित की अपनी कमियों के कारण उत्पन्न अवरोध अन्तः- वैयक्तिक अवरोध कहलाते हैं । अन्तः वैयक्तिक अवरोध निम्नलिखित पांच प्रकार के होते हैं।
शारीरिक अवरोध : यह व्यक्ति को किसी शारीरिक कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। कुछ शारीरिक अवरोध के उदाहरण है : हकलाना, कम सुनना, अनाकर्षक व्यक्तित्व, आदि ।
सांस्कृतिक अवरोधः संस्कृति और भाषा एक दूसरे से जुड़े हैं। विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न कहावतें होती हैं जो भिन्न मूल्य, रिवाज और परम्पराएं दर्शाते हैं। किसी भाषा में मुहावरों और कहावतों का एक विशिष्ट सन्दर्भ में विशिष्ट अर्थ होता है जो दूसरी भाषा में अटपटा लग सकता है। उदाहरणस्परूप उत्तरी अमेरिका में प्रचलित कहावत है, “अर्ली बर्ड गेट्स दें वर्म – The early bird gets the worm”, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति तैयार और स्फूर्त है, उसी को प्रतिफल मिलता है। अब आप अन्दाजा लगाइये यदि हम इसका अनुवाद हिन्दी में करें तो वह कितना बेतुका लगेगा। अतः विचारों का आदान-प्रदान करते समय व्यक्ति को दूसरी संस्कृति की संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए। कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में बहुसांस्कृतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं ताकि सम्प्रेषण सुचारू रूप से हो सकें।
वैयक्तिक सोच के कारण अवरोध इस प्रकार के अवरोध व्यक्ति की स्वयं की सोच के कारण उत्पन्न होते हैं। कुछ व्यक्ति अपनी सामाजिक, आर्थिक और सास्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण एक विशेष प्रकार की सोच बना लेते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ व्यक्ति अन्तर्मुखी (अपने आप में ही सिमटे रहना) हो जाते हैं। जबकि कुछ अत्यधिक मिलनसार इस प्रकार की दो श्रेणियों के व्यक्तियों के सम्प्रेषण करने के तरीकें पूर्णतः भिन्न होते हैं। कुछ व्यक्तियों में अत्यधिक अहंकार होता है और वे कई व्यक्तियों की उपस्थिति में बात करते समय सहजता अनुभव नहीं करते हैं।
भावात्मक अवरोध : इस प्रकार के अवरोध विशिष्ट परिस्थितियों में व्यक्ति के अपने भावावेश के कारण उत्पन्न होते हैं। उदाहरणस्वरूप कुछ व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में घबरा जाते है और अनुभव करते हैं।
उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का उपाय सोचने के स्थान पर रोने लगते हैं। अनुभूति-जनक अवरोध इस प्रकार के अवरोध व्यक्ति द्वारा परिस्थितियों को एक विशिष्ट प्रकार के दृष्टिकोण से अनुभव करने के कारण उत्पन्न होते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि जैसे शैक्षणिक, सामाजिक, सास्कृतिक और पारिवारिक से आने वाले व्यक्ति एक स्थिति को विभिन्न प्रकार
अन्तर- वैयक्तिक अवरोध
अन्तर- वैयक्तिक अवरोध व्यक्ति के बाहरी कारणों से उत्पन्न होते हैं। यह अवरोध संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य विभिन्न कारणों से होते हैं। कभी तो इन अवरोधें को दूर किया जा सकता है और कभी यह व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होते हैं। पूर्वाग्रह, भ्रान्ति, अभिरूचि की कमी, गलत तथ्य, क्रोध, एक निश्चित परिणाम के लिए धुन आदि। कुछ प्रमुख अन्तर- वैयक्तिक अवरोधों का वर्णन नीचे किया गया है।
सांस्कृतिक अवरोध : संस्कृति और भाषा एक दूसरे से जुड़े हैं। विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न कहावते होती हैं जो भिन्न मूल्य, रिवाज और परम्पराएं दर्शाते हैं। किसी भाषा में मुहावरों और कहावतों का एक विशिष्ट सन्दर्भ में विशिष्ट अर्थ होता है जो दूसरी भाषा में अटपटा लग सकता है। उदाहरणस्परूप उत्तरी अमेरिका में प्रचलित कहावत है, “अर्ली बर्ड गेट्स दें वर्म – The early bird gets the worm”, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति तैयार और स्फूर्त है, उसी को प्रतिफल मिलता है। अब आप अन्दाजा लगाइये यदि हम इसका अनुवाद हिन्दी में करें तो वह कितना बेतुका लगेगा। अतः विचारों का आदान-प्रदान करते समय व्यक्ति को दूसरी संस्कृति की संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए। कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में बहुसांस्कृतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं ताकि सम्प्रेषण सुचारू रूप से हो सकें।
भाषीय अवरोध: यह सम्प्रेषण में सर्वाधिक सामान्य अवरोध है। प्रत्येक भाषा के तीन नियम होते हैं : वाक्य-रचना (वाक्य में शब्दों का क्रम), अर्थ-सम्बंधी (शब्दों का अर्थ ) और प्रासंगिक (प्रसंग और सामाजिक प्रथा के अनुसार शब्दों का अर्थ)। यह नियम विभिन्न भाषाओं के लिए भिन्न हैं। जब व्यक्ति अपनी मातृभाषा का उपयोग नही करता है तब भ्रम की काफी सम्भावना होती है। कभी-कभी श्रोता पर अपना प्रभाव जमानें के लिए वक्ता / प्रेषक कुछ कठिन अथवा सामान्य रूप से प्रयुक्त न होने वाले शब्दों अथवा किसी खास बोली के शब्दों का इस्तेमाल करता है। ऐसी स्थिति में प्राप्तकर्ता संदेश का ठीक अर्थ नहीं लगा पाता है। किसी स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करने से सम्प्रेषण बेकार हो जाता है। एक ही संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी विभिन्न पृष्ठभूमियों और क्षेत्रों से हो सकते हैं जिनका भाषा ज्ञान का स्तर भिन्न हो सकता है। जिसके कारण प्रभावी सम्प्रेषण पर प्रभाव पड़ता है।
नैतिक अवरोध नैतिक अवरोधों का सम्बंध उन परिस्थितियों से है जब व्यक्ति की नैतिकता और उसके प्रोफेशनल कर्तव्य के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के रूप में किसी खुदरा शोरूम का बिक्रीकर्ता पर यह दबाव है कि वह दोषपूर्ण उत्पादों को भी बेचनें का प्रयत्न करें क्योंकि उसको तनख्वाह बिक्री से होने वाले लाभ से मिलती है। इस प्रकार की परिस्थिति में बिक्रीकर्ता ग्राहकों को सामान बेचने का प्रयत्न करता है। आवश्यक होने पर वह उत्पाद के गुणों की झूठी प्रशंसा करता है। इस प्रकार उसकी नैतिकता और उसके व्यवसायिक कर्तव्य के मध्य सीधे विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
पदक्रम अथवा ओहदा जनित अवरोध जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कुछ व्यक्तियों में अंहकार होता है और अपने से कनिष्ठ पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति से बात करते समय वह सहजता अनुभव नहीं करते हैं। दूसरी ओर, निचले स्तर पर कार्य करने वाला व्यक्ति अपने बॉस से बात करने में झिझकता है। इस प्रकार का अवरोध सामंतवादी समाज में सामान्य है ।
पर्यावरणीय अवरोध
संगठन के बाहरी कारणों से उत्पन्न अवरोध पर्यावरणीय आधारित सम्प्रेषण अवरोध कहलाते हैं। इनमें से कुछ कारकों पर संगठन का नियंत्रण होता है। परन्तु कुछ ऐसे कारण होते है जिन पर संगठन का नियंत्रण नही होता है। इन अवरोधो को कई उप-समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
भौतिक अवरोध: सम्प्रेषण में भौतिक अवरोध पर्यावरणीय और प्राकृतिक स्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं। इसके कई कारण हैं जैसे शोर, तकनीकी समस्याएं, त्रुटिपूर्ण डिजाइन के कारण आवाज का गूंजना आदि । उदाहरणस्वरूप यदि कोई नेता रैली में बोलता है तो आसपास के ट्रैफिक और भीड़ के शोर के कारण उसकी आवाज सुनने में बाधा आती है टेलीफोन लाइन और मोबाइल कनेक्शन में शोर हो सकता है जिसके कारण प्राप्तकर्ता संदेश ठीक प्रकार प्राप्त नहीं कर पाता है। कभी-कभी इण्टरनेट कनेक्शन में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है अथवा वह तकनीकी समस्या अथवा प्राकृतिक व्यवधान के
कारण बहुत धीमा होता है जिसके कारण उपभोक्ता ई-मेल सुविधा और वीडियों चैट का उपयोग नहीं कर पाते हैं। भौतिक अवरोध के अन्य कारण कम्प्यूटर वायरस, प्रेषक के चिन्हित न होने के कारण ई-मेल का स्पैम-बॉक्स में पहुँचना, आदि हैं।
इनको निम्नलिखित उप-समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
शोरः
आसपास का अनुपयुक्त वातावरण सम्प्रेषण में बाधा उत्पन्न करता है। उदाहरणस्वरूप यदि कोई नेता रैली में बोल रहा है तो आसपास के ट्रैफिक के कारण यहां तक की भीड़ के शोरगुल के कारण उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। कमरों के गलत डिजाइन अथवा बैठने के गलत प्रबन्ध अथवा पुराने फर्नीचर की कड़कड़ की आवाज के कारण भी व्यवधान हो सकता है। इन कारणों से प्रेषक का भेजा गया संदेश अस्पष्ट होगा और यही अस्पष्ट संदेश प्राप्तकर्ता के पास पहुंचेगा
तकनीकी समस्याएं तकनीकी समस्याएं सम्प्रेषण भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाले खराब उपकरणों के कारण उत्पन्न होती है। टेलीफोन लाइन और मोबाइल कनेक्शन में शोर हो सकता है जिसके कारण प्राप्तकर्ता संदेश ठीक प्रकार प्राप्त नहीं कर पाता है। कभी-कभी इण्टरनेट कनेक्शन में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है अथवा वह तकनीकी समस्या अथवा प्राकृतिक व्यवधान के कारण बहुत धीमा होता है जिसके कारण उपभोक्ता ई-मेल सुविधा और वीडियों चैट का उपयोग नहीं कर पाते हैं। भौतिक अवरोध के अन्य कारण कम्प्यूटर वायरस, प्रेषक के चिन्हित न होने के कारण ई-मेल का स्पैम बॉक्स में पहुँचना, आदि हैं।
क्रोमैटिक अवरोध
समय से सम्बंधित अवरोध जैसे संदेश का देर से पहुंचना क्रोमैटिक अवरोध कहलाता है। इन अवरोधों का कारण प्रेषक और प्राप्तकर्ता में लम्बी दूरी, उनके भिन्न समय- जोन आदि हैं। उदाहरण के रूप में किसी बहुदेशीय कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत में है और उसको किसी महत्वपूर्ण सूचना कम्पनी के संयुक्त राज्य अमेरीका स्थित कार्यालय से लेनी है तो विभिन्न समय-जोन के कारण हो सकता है उसे वह सूचना तुरंत न मिले। इन सब बातो को ध्यान रखते हुए मीटिंग की तिथि काफी पहले तय करनी पड़ती है।
संगठनीय अवरोध:
किसी संगठन में कर्मचारियों के मध्य सम्प्रेषण के प्रवाह में आने वाली कठिनाईयां संगठनीय अवरोध कहलाते हैं। इसके कारण उनकी कार्यकुशलता पर असर पड़ता है और संगठन को वित्तीय हानि होती है। संगठनीय अवरोध के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
(i) निम्न स्तर की सम्प्रेषण सुविधाएं इसमें टेलीफोन, इण्टरनेट, वाई फाई, फैक्स, कम्प्यूटर, स्टेशनरी आदि सम्मिलित हैं। इन सुविधाओं का समय-समय पर आधुनिकीकरण न करनें पर कर्मचारी प्रभावी सम्प्रेषण करने में अपने आपको असहाय पाते हैं।
(ii) जटिल प्रशासनिक संरचना कभी-कभी कर्मचारियों को बाहय एंजेसियों से सीधे सम्पर्क करने की अनुमति नहीं होती है। इसके स्थान पर तैयार किया मसौदा एक जटिल प्रशासनिक श्रृंखला के माध्यम से पहले उच्च अधिकारियों को भेजना पड़ता है और फिर यह वापिस उसी श्रृंखला से नीचे की ओर उसी कर्मचारी के पास पंहुचता है जो उसके
पश्चात् उसे भेजता है। यह जटिल प्रक्रिया संगठनीय अवरोध है जिसके कारण कम्पनी का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पाता। भारत के अनेक सरकारी संगठनो में अभी भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है जिसके कारण उनकी कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है।
(iii) जटिल नियम : यह भी इसके पहले के बिन्दू से सम्बंधित है। कुछ संगठनों में कर्मचारियों को कहा जाता है कि वें पूर्व- निश्चित सम्प्रेषण प्रणाली का ही उपयोग सम्प्रेषण के लिए करें आपस में वे सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए उनसे निश्चित मीडिया का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संगठन में सूचना के मुक्त प्रवाह पर पाबन्दी होती है जिसके कारण सम्प्रेषण में विलम्ब होता है।
(iv) अकुशल डिलीवरी नेटवर्क बड़े संगठनों में बाहरी डाक और अन्य सामग्री पावती विभाग द्वारा प्राप्त की जाती है जो बाद में सम्बंधित विभागों को वितरित की जाती है। यह डिलीवरी नेटवर्क चुस्त-दुरूस्त न होने की स्थिति में दस्तावेज सम्बंधित विभागों को देने में गलती हो सकती है जिसके कारण उसका उत्तर देने में विलम्ब हो सकता है।
यांत्रिक अवरोध
सम्प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी और उपकरणों में तकनीकी खराबी के कारण यांत्रिक अवरोध उत्पन्न होते हैं। यांत्रिक उपकरणों जैसे कम्प्यूटर, टेलीफोन, फैक्स मशीन, पेजर इत्यादि में लगातार रख-रखाव की आवश्यकता होती है जिसके न होने पर उनमें शोर होता है और सम्प्रेषण में रूकावट पड़ती है।
व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले उपकरण, जैसे श्रवण-यंत्र, ध्वनि विस्तारक, सिंगनलिंग उपकरण, बैली और विशेष प्रकार की आवश्यकता के लिए टेलीफोन आवर्धक (मैगनीफायर), टेक्स्ट, टेलीफान और टी डी डी (बहरों के लिए टेलीफोन यंत्र) आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं और इनमें से किसी में भी खराबी आना यांत्रिक अवरोध उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त विद्युत सप्लाई में बाधा और इण्टरनेट में व्यवधान भी सम्प्रेषण में यांत्रिक अवरोध हैं।
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अवरोधो को भी यांत्रिक अवरोधो की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है ।
संचरण व्यवधान :
सम्प्रेषण जैसे ई-मेल, फैक्स संदेश, मोबाइल, सिटिजन बैण्ड रेडियों, वी एच एफ रेडियों और सैटेलाइट सम्प्रेषणों का संचरण डिजिटल रूप में होता है। कुछ कारणों से संचारण में व्यवधान होने पर सम्प्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी।
पुराने उपकरण जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सम्प्रेषण में उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों का निरंतर रख-रखाव जरूरी है और आवश्यक होने पर पुराने उपकरणों का बदला जाना आवश्यक होता है। कभी-कभी धन की कमी के कारण इनको बदलना सम्भव नहीं हो पाता जिसके कारण सम्प्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है।
बिजली सप्लाई में बाधा सभी आधुनिक सम्प्रेषण प्रणाली बिजली पर आधारित हैं। अतः बिजली की लगातार सप्लाई और स्थिर वोल्टेज सम्प्रेषण के लिये आवश्यक हैं। विकसित देशो में बिजली की सप्लाई में बाधा साधारणतः नही होती है। परन्तु अविकसित देशों में, विशेष रूप से दूर दराज के स्थानों में बिजली की सप्लाई में बाधा पड़ती है जिसके कारण सम्प्रेषण में व्यवधान होता है।
सफल संप्रेषण के अवरोध
हम यह पहले ही बता चुके हैं कि वक्ता से श्रोता तक या लेखक से पाठक तक जब संदेश सही रूप में नहीं पहुँच पाता तो संप्रेषण असफल रहता है। इस असफलता के कई कारण हो सकते हैं उनमें कुछ का उल्लेख हम कर रहे हैं:
गलत संदेश
संदेश को सही ढंग से संप्रेषित न करना और उसे ठीक ढंग से समझ न पाना सफल संप्रेषण में सबसे बड़ा अवरोध है। आप अपने जीवन में कई बार ऐसे अनुभवों से गुजर चुके होंगे जब या तो आप अपनी बात ठीक से संप्रेषित नहीं कर पाए या संदेश को ठीक से समझ नहीं पाए। ऊपर मोमबत्ती वाली जिस घटना जिक्र किया गया उसका सबसे बड़ा कारण था कि संदेश अस्पष्ट था। अगर यह कहा जाता है कि ‘पीछे जल रही मोमबत्ती को बुझा दें तो श्रोता संदेश को ठीक-ठीक समझता, पीछे मुड़ता और मोमबत्ती बुझा देता। क्या आप बता सकते हैं कि यह संप्रेषण क्यों अधूरा रहा गया?
संदर्भ नहीं बताया गया ( क्या बुझाना है ? )
गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया (फेंकना)
अगर संदर्भ स्पष्ट न हो और उपयुक्त शब्द का प्रयोग न किया जाए तो संप्रेषण कभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। अतः सफल संप्रेषण के लिए संदर्भ और भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और प्रयुक्त शब्द उपयुक्त होना चाहिए ।
गलत शब्दों का चुनाव
कुछ भी बोलिए सोच समझकर बोलिए। एक भी गलत शब्द आपके संप्रेषण को तो बाधित कर ही सकता है, आपको इससे नुकसान भी हो सकता है, आपके संबंधों में दरार आ सकती है, आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है, आपकी स्थिति हास्यास्पद भी हो सकती है।
सुनना और समझना
यदि श्रोता वक्ता की बात ध्यान से नहीं सुनता है या पुस्तक पढ़ते वक्त मन कहीं और लगा होता है तो वक्ता की बात श्रोता सुनकर भी सुन नहीं रहा होता और पाठक पुस्तक की पंक्तियों से गुजरता तो जरूर है पर वह उस तक संप्रेषित नहीं हो पाती। आपने भी कई बार अनुभव किया होगा कि आपसे कोई बात कर रहा है और आप थोड़ी देर बाद पूछ बैठते हैं क्या कहा, मैंने सुना नहीं।’ क्या कभी आपने इस पर विचार किया है कि सामने वाले की बात आप क्यों नहीं समझ पाए। इसी प्रकार कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा होता है और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और रहता है और वह अध्यापक के मुख से निकला एक भी शब्द पकड़ नहीं पाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आप किसी दफ्तर में जाते हैं। उस अधिकारी के पास जाते हैं जिससे आपको काम है। आप पूछते हैं अंदर आ सकता हूँ । अधिकारी किसी काम में व्यस्त है। आपकी बात सुन नहीं पाता। आप खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी निगाह आपकी ओर उठती है। वह पूछता है ‘हाँ! क्या काम है? आपके इस संदेश को मैं अंदर आ सकता हूँ उसने सुना ही नहीं। अतः यदि श्रोता संदेश को ठीक से सुनता नहीं है तो भी संप्रेषण बाधित होता है। फोन पर बातचीत करते हुए आपने कई बार महसूस किया होगा कि उधर से बोलने वाले की आवाज सुनाई नहीं दे रही। टेलीफोन पर जब बात करने वाले बार बार हेलो हेलो बोलते हैं तो समझ लीजिए संप्रेषण पूरा नहीं हो पा रहा। टेलीफोन से आवाज धीमी आना, टेलीफोन लाइन में शोर या खड़खड़ाहट, कुछ भी कारण हो सकता है। परंतु मूल बात यह है कि वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुँच नहीं पा रहा है।
भाव भंगिमा
भाव-भंगिमा संप्रेषण का एक माध्यम भी है और बाधा भी मुस्कराते हुए किसी का स्वागत करना, क्रोध से किसी की ओर देखना, किसी को देखकर मुँह बिचकाना, व्यंग्य से हँसना, कंधे उचकाना, आदि कई ऐसी भाव-भंगिमाएँ हैं जिनसे व्यक्ति विशेष अपनी भावना दूसरे व्यक्ति या समूह तक संप्रेषित करता है। परंतु इस प्रकार के संप्रेषण से सबसे बड़ा खतरा यह है कि आपके द्वारा संप्रेषित भाव का गलत अर्थ न लगा लिया जाए। इस कारण संप्रेषण
में हाव-भाव की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा यहाँ मौन होती है। इस प्रकार के संप्रेषण में स्थानीय विभिन्नता भी होती है। यदि उत्तर भारत का कोई व्यक्ति दक्षिण भारत जाए और अगर वह वहाँ की परंपरा से परिचित न हो तो उसे हमेशा ‘हाँ ‘नहीं’ प्रतीत होगा। क्योंकि उत्तर भारत में ‘नहीं’ के लिए जिस प्रकार सिर हिलाते हैं उसी प्रकार दक्षिण भारत में ‘हाँ’ के लिए सिर हिलाते हैं। उत्तर भारत में ‘हाँ’ के लिए आगे-पीछे और ‘नहीं’ के लिए दायें-बायें सिर हिलाते हैं जबकि दक्षिण भारत में ‘हाँ’ के लिए भी दायें-बायें सिर हिलाते हैं। अतः सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण भी भाव-भंगिमा सफल संप्रेषण में बाधक बन सकती है।
बोलने का ढंग
आपके बोलने के ढंग से भी संप्रेषण प्रभावित होता है। यदि आप सही बात भी ऊँची आवाज़ में या चिल्लाकर बोलते हैं तो आपके संदेश के गलत संप्रेषण की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी की आवाज़ भारी या कर्कश हो तो भी संप्रेषण बाधित हो सकता है।
भाषा ज्ञान
सफल संप्रेषण के लिए यह जरूरी है कि वक्ता और श्रोता की भाषा एक हो या वे एक दूसरे की भाषा जानते हों। यदि कोई हिंदीभाषी इंग्लैंड चला जाए और उसे अंग्रेजी न आती हो तो उसके लिए संप्रेषण एक दुःसाध्य कार्य हो जाएगा।
(Part Two : Another view to the topic)
सम्प्रेषण के अवरोध
यद्यपि कि किसी संगठन में सम्प्रेषण की प्रक्रिया और प्रतिमान सुपरिभाषित और सुसंगठित है फिर भी कुछ दूरियों, बाधाओं और अवरोधों के कारण सम्प्रेषण में गलतफहमी और असफलता की संभावनाएं होती हैं। ये बाधायें कई प्रकार की हो सकती हैं जिसमें भौतिक और मनोवैज्ञानिक अवरोध भी शामिल हैं। चलिए सम्प्रेषण की विभिन्न प्रकार के अवरोधों के बारे में चर्चा करें:
भौतिक बाधायें
भौतिक बाधायें पर्यावरण से जुड़ी वही बाधायें होती हैं जो प्रभावशाली सम्प्रेषण में अवरोध उत्पन्न करती हैं। इनमें से कुछ बाधायें इस प्रकार हैं:
दूरी
कोई भी सम्प्रेषण जो किसी हॉल अथवा विशिष्ट स्थान में घटित हो रही होती है, जहाँ व्यक्ति भौतिक रूपसे उपस्थित रहते हैं, तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकती जब तक कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य लम्बी दूरी न हो। यद्यपि आजकल डिजिटल तकनीकी में प्रगति होने के कारण, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच कितनी भी दूरी होने बावजूद, कई ऑनलाइन बैठकें हो रही हैं।
कोलाहल
जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है कि यदि आधारिक कोलाहल, जो हॉर्न, गाड़ी और माइक्रोफोन की ध्वनि हो सकती है. प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच अंतःक्रिया को अस्त-व्यस्त कर सकती है।
तकनीकी
लाउडस्पीकर की अनुपस्थिति में माइक्रोफोन अथवा जान उद्बोधन तंत्र एक भौतिक अवरोश हो सकता है जब किसी को आमने-सामने की बैठक में बड़ी संख्या में सदस्यों को सम्प्रेषित करना हो। जबकि इंटरनेट सुविधा का अभाव अथवा अन्य तकनीकें स्वाभाविक सम्प्रेषण के प्रवाह को बाधित कर देता है।
संगठनात्मक जलवायु आयाम
समूह के सदस्यों के अंतर्वैयक्तिक सम्बन्ध एक महत्त्वपूर्ण संगठनात्मक जलवायु आयाम जो प्रभावशाली सम्प्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है प्रतिकूल सम्बन्ध संगठनों में गलतफहमी और गलत निर्णयों को जन्म दे सकती हैं।
विभिन्न समय क्षेत्र
प्रेषक और प्राप्तकर्ता के समय क्षेत्र में भिन्नता भी प्रभावशाली सम्प्रेषण के समक्ष अवरोध उत्पन्न कर सकता है। समय विभाजन सम्प्रेषण की प्रक्रिया में समन्वय के अभाव का कारण हो सकती है।
मनोवैज्ञानिक बाधायें
कई बार व्यक्ति के संवेग और मानसिक क्षमताएं सम्प्रेषण के लिए अवरोध का काम करती है मनोवैज्ञानिक बाधायें भय की अभिव्यक्ति, दुश्चिंता, अन्यमनस्कता, अभिरुचि का अभाव, उत्तेजना अथवा कई अन्य सम्बंधित तरह की विषेशताओं के रूप में घटित होती है।
पूर्वकल्पित विचार की संकल्पनाएं
प्रभावी सम्प्रेषण तब घटित नहीं होगा यदि प्रेषक पहले से संकल्पना कर ले कि प्राप्तकर्ता सूचना को समझता है और उनसे कोई भी पुनर्निवेशन नहीं प्राप्त करना चाहता। इसी प्रकार, व्यक्तिगत अनुभव अथवा पूर्वकल्पित विचार प्रेषक अथवा प्राप्तकर्ता को आलोचनात्मक बना देते हैं और प्रभावी सम्प्रेषण में असफलता का कारण बनते हैं।
सांवेगिक अवस्था
व्यक्तियों की सांवेगिक अवस्था सम्प्रेषण में एक अवरोध के रूप में कार्य कर सकती है। यदि प्रेषक सन्देश भेजते समय क्रोध अथवा आक्रामक अवस्था में है तब यह प्राप्तकर्ता के संदश की व्याख्या के तरीके को प्रभावित करेगा।
अभिवृत्तियाँ और मूल्य
अभिवृत्ति का अभिप्राय एक पूर्व-अधिगमित प्रवृत्ति से है और समय के साथ यह स्व-अनुभवों, विश्वासों और मूल्यों के परिणामस्वरुप व्यक्ति के अंदर विकसित होता रहता है। किसी विषय से जुड़ा एक प्रबल विश्वास के कारण सकारात्मक अभिवृत्ति जन्म ले सकती है और प्रेषक अथवा प्राप्तकर्ता सूचनाओं के प्रति संवेदनशील तरीके से प्रतिक्रिया कर सकता है। इसके अलावा, व्यक्ति इसके विरुद्ध या पक्ष में कोई बात सुनने या बोलने ले लिए तैयार नहीं हो सकता है।
नकारत्मक आत्म- छवि का भय
कई बार व्यक्तियों में नकारात्मक छवि के भय से वे स्पष्टता या पारदर्शिता से सूचना को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। यह गलत या अधूरी सूचना के प्रसारण को जन्म दे सकता है।
कमजोर सुनने की क्षमता
यदि प्राप्तकर्ता अधीर है और चयनात्मक रूप से सुनने के लिए प्रवृत्त है तब भी पूरी सूचना उनके द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकेगी।
अन्य बाधायें
भौतिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं के आलावा कई अन्य बाधायें भी हैं जो प्रभावशाली सम्प्रेषण की प्रक्रिया में बाधा पंहुचा सकती हैं। वे हैं:
भाषाशास्त्रीय बाधायें
उचित भाषा के द्वारा सम्प्रेषण न कर पाने की क्षमता अनुभवों और मौखिक या लिखित रूप से विचारों की अभिव्यक्ति की अयोग्यता का जन्म देती है। इसके अलावा, यदि सूचना के प्रसारण की भाषा की प्रेषक को जानकारी नहीं है तब भी सूचना प्राप्तकर्ताओं को स्पष्ट नहीं होगी।
बाधायें
कंपनियों का सार्वभौमिकीकरण और अधिग्रहण ने विभिन्न देश के कर्मचारियों को साथ-साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक देश की अपनी अद्वितीय संस्कृति और संस्कृति की भिन्नता भी प्रभावी सम्प्रेषण में अवरोध को जन्म देती हैं।
सामाजिक कारक
लोगों की सामाजिक प्रस्थितियों में भिन्नता भी प्रभावी सम्प्रेषण में अवरोध उत्पन्न करती है । कर्मचारियों का पदानुक्रम, प्रस्थिति और पद भी सहज सूचना के प्रवाह में बाधा पैदा करते हैं।
ऊपर कुछ अवरोधों की चर्चा की गयी है जो सहज सम्प्रेषण के प्रवाह में उत्पन्न करते हैं। यद्यपि कई रणनीतियाँ हैं जो इन अवरोधों को को दूर करने में सहायता कर सकती हैं। उदाहरण के लिए भाषा प्रशिक्षण की सहायता से भाषाशास्त्रीय बाधाओं को काम किया जा सकता है। जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रभावी सम्प्रेषण की बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकती हैं।
सम्प्रेषण अवरोध किस प्रकार दूर किये जायें ?
इससे पहले के खंड में विविध प्रकार के सम्प्रेषण अवरोधों का विवरण दिया गया था। इन अवरोधों का वर्णन करते समय प्रत्येक अवरोध कारण भी बताया गया था। अतः यदि हम सावधानीपूर्वक इन कारणों से बचें तो इन अवरोधों पर नियंत्रण किया जा सकता है।
इस खंड में हम संक्षेप में यह बतायेंगे कि इन सम्प्रेषण अवरोधों पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है।
शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अवरोधो पर नियंत्रण व्यग्रता और डर (फोबिया) पर नियंत्रण के लिए आवश्यक होने पर मनोवैज्ञानिक डाक्टर से सलाह लें। लगातार अभ्यास उपयुक्त मार्गदर्शन और उपयुक्त उपकरणों के इस्तेमाल से शारीरिक कमियों जैसे हकलाना, कम सुनना आदि पर विजय पायी जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों से जिनसे आपको परेशानी होती है कुछ समय दूर रह कर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। सामान्य मानसिक स्थिति होने पर आप पुनः सम्प्रेषण प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। कभी-भी कमी को सहना पड़ता है क्योंकि दूसरे व्यक्ति पर जिससे आप सम्प्रेषण कर रहें हैं, आपका नियंत्रण नहीं है।
अन्तर- वैयक्तिक अवरोधो पर नियंत्रण जैसा कि पहले बताया गया था, अन्तर- वैयक्तिक अवरोधो में : सांस्कृतिक अवरोध, भाषीय अवरोध, नैतिक अवरोध और ओहदा जनित अवरोध सम्मिलित हैं। इन अवरोधो पर विजय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:
क) सहज भाषा का प्रयोग सहज भाषा और स्पष्ट शब्दों का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही संदेश के शब्द विनम्र होने चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता की भावनाओं को ठेस न पहुॅचे। संदेश संक्षिप्त और केवल उद्देश्य से सम्बंधित होना चाहिए।
ख) संदेश की सुसंगता संदेश संगठन के उद्देश्यों, रणनीतियों कार्यक्रमों और तकनीक के सुसंगत होना चाहिए।
ग) एक धैर्यवान श्रोता होना का प्रयत्न कीजिए मौखिक रूप से सम्प्रेषण करते समय प्रेषक और प्राप्तकर्ता से यह अपेक्षित हैं कि वें धैर्यवान श्रोता की तरह व्यवहार करें। उनको एक दूसरे के प्रति धैर्य और सकारात्मक सोच प्रदर्शित करनी चाहिए।
घ) अन्तर-सांस्कृतिक कार्यशाला करनाः बड़े सगठनों में जहां विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति कार्य करते हैं, अन्तर-संस्कृतिक कार्यशाला का आयोजन करना अच्छा रहता है जहां पर व्यक्तियों को एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का अवसर मिलता है।
च) सम्प्रेषण के पहले विचार विमर्श: अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्प्रेषण से पहले ऐसे व्यक्तियों से विचार विमर्श करना अच्छा रहता है जिनको प्राप्तकर्ता की पृष्ठभूमि के विषय में ज्ञात हो ।
छ) सरल पदक्रम की स्थापनाः पश्चिमी देशो में ओहदा जनित अवरोध देखने में नही आते। अतः भारत में कार्य कर रहे संगठन में यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह इस प्रकार की संस्कृति अपनाये जिसमें विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहें व्यक्तियों में आपस में सम्प्रेषण करते समय इस प्रकार का अवरोध न हो।
पर्यावरणीय संगठनात्मक और भौतिक अवरोधो पर विजय
क) आधुनिक उपकरणों का उपयोग संगठन में आधुनिक उपकरणों के उपयोग से पर्यावरणीय और भौतिक अवरोध कम किये जा सकते हैं। इसके साथ इन उपकरणों का सतत रूप से रख-रखाव और आधुनिकीकरण होना चाहिए। कमरों का डिजाइन इस प्रकार का होना चाहिए कि वे गूंजन (इको) मुक्त हो और जहां तक सम्भव हो अन्य ढांचागत सुविधाएं जैसे फर्नीचर, आडियो-वीडियों उपकरण आदि भी आधुनिक होने चाहिए।
ख) प्रभावी आन्तरिक डिलीवरी तंत्र किसी भी संगठन में प्रभावी आन्तरिक डिलवरी तंत्र होना आवश्यक है ताकि प्राप्ति-सेक्शन में प्राप्त लिखित संदेशो को सम्बंधित व्यक्तियों तक तीव्र और और सही तरीके से पहुँचाया जा सकें।
तकनीकी समस्याओं पर विजय : सरकारी और म्युनिस्पिल प्रशासन से अच्छा तालमेल बैठा कर तकनीकी समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है।
- 11 – भाद्रपद मासकी ‘अजा’ और ‘पद्मा’ एकादशीका माहात्य
- 14 – पुरुषोत्तम मासकी ‘कमला’ और ‘कामदा’
- 13 – कार्तिक मासकी ‘रमा’ और ‘प्रबोधिनी’एकादशीका माहात्म्य
- 12 – आश्विन मासकी ‘इन्दिरा’ और ‘पापाङ्कुशा’ एकादशीका माहात्य
- 10 – श्रावण मासकी ‘कामिका’ और ‘पुत्रदा’ एकादशीका माहात्म्य
- About Culture-संस्कृति के विषय में
- About Institution-संस्था के विषय में
- ACT.-अधिनियम
- Awareness About Geography-भूगोल के विषय में जागरूकता
- Awareness About Indian History-भारतीय इतिहास के विषय में जागरुकता
- Awareness About Maths-गणित के बारे में जागरूकता
- Awareness about Medicines
- Awareness About Politics-राजनीति के बारे में जागरूकता
- Awareness-जागरूकता
- Basic Information
- Bharat Ratna-भारत रत्न
- Biography
- Chanakya Quotes
- CLASS 9 NCERT
- CMs OF MP-मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
- CSIR UGC NET
- e-Test-ई-टेस्ट
- Education
- Education-शिक्षा
- Ekadashi Mahatmya
- FULL TEST SERIES
- GK
- Granthawali-ग्रन्थावली
- Hindi Biography – जीवन परिचय
- Hindi Literature
- Hindi Literature-हिंदी साहित्य
- HINDI NATAK-हिंदी नाटक
- Hindi Upanyas-हिंदी उपान्यास
- ICT-Information And Communication TEchnology
- Jokes-चुटकुले
- Kabir ji Ki Ramaini-कबीर जी की रमैणी
- KAHANIYAN
- Katha-Satsang-कथा-सत्संग
- Kavyashastra-काव्यशास्त्र
- Meaning In Hindi-मीनिंग इन हिंदी
- Meaning-अर्थ
- MOCK TEST
- Motivational Quotes in Hindi-प्रेरक उद्धरण हिंदी में
- MPESB(VYAPAM)-Solved Papers
- MPPSC
- MPPSC AP HINDI
- MPPSC GENERAL STUDIES
- MPPSC GS PAPER
- MPPSC-AP-HINDI-EXAM-2022
- MPPSC-Exams
- MPPSC-मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
- Nibandha
- Padma Awardees-पद्म पुरस्कार विजेता
- PDFHUB
- PILLAR CONTENT
- QUOTES
- RSSU CHHINDWARA-राजा शंकर शाह वि.वि. छिंदवाड़ा
- RSSU QUESTION PAPERS
- SANSKRIT
- SANSKRIT VYAKARAN
- SANSKRIT-HINDI
- Sarkari Job Advertisement-सरकारी नौकरी विज्ञापन
- Sarkari Yojna-सरकारी योजना
- Sarkari-सरकारी
- Sarthak News-सार्थक न्यूज़
- SCHOOL
- SOLVED FIRST PAPER CSIR NET
- Theoretical Awareness-सैद्धांतिक जागरूकता
- UGC
- UGC NET
- UGC NET COMPUTER SCIENCE
- UGC NET HINDI MOCK TEST
- UGC NET NEWS
- UGC_NET_HINDI
- UGCNET HINDI
- UGCNET HINDI PRE. YEAR QUE. PAPERS
- UGCNET HINDI Solved Previous Year Questions
- UGCNET-FIRST-PAPER
- UGCNET-FIRSTPAPER-PRE.YEAR.Q&A
- UPSC-संघ लोक सेवा आयोग
- Various Exams
- VEDIC MATHS
- Yoga
- इकाई – 02 शोध अभिवृत्ति (Research Aptitude)
- इकाई – 03 बोध (Comprehension)
- इकाई – 04 संप्रेषण (Communication)
- इकाई – 07 आंकड़ों की व्याख्या (Data Interpretation)
- इकाई – 10 उच्च शिक्षा प्रणाली (Higher Education System)
- इकाई -01 शिक्षण अभिवृत्ति (Teaching Aptitude
- इकाई -06 युक्तियुक्त तर्क (Logical Reasoning)
- इकाई -09 लोग विकास और पर्यावरण (People, Development and Environment)
- इकाई 08 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT-Information and Communication Technology)
- इकाई-05 गणितीय तर्क और अभिवृत्ति (Mathematical Reasoning And Aptitude)
- कबीर ग्रंथावली (संपादक- हजारी प्रसाद द्विवेदी)
- कविताएँ-Poetries
- कहानियाँ – इकाई -07
- कहानियाँ-KAHANIYAN
- कहानियाँ-Stories
- खिलाड़ी-Players
- प्राचीन ग्रन्थ-Ancient Books
- मुंशी प्रेमचंद
- व्यक्तियों के विषय में-About Persons
- सार्थक न्यूज़
- साहित्यकार
- हिंदी व्याकरण-Hindi Grammar