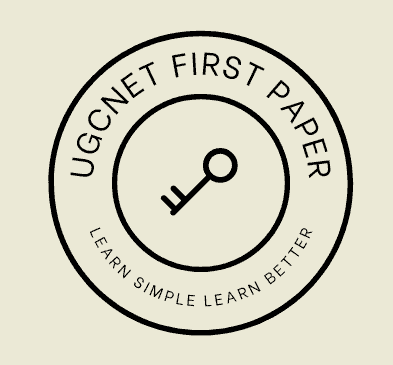(Acknowledgement : Based On ignou university study material on the topic)
Steps Of Communication / संप्रेषण प्रक्रिया
संप्रेषण एक प्रक्रिया है। वस्तुतः प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुँचने की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। इस प्रकार संप्रेषण के तीन हिस्से होते हैं- प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता । पत्र इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। आप अपने भाई को पत्र लिखते हैं। आप प्रेषक हुए आप पत्र में कुछ लिखते हैं। यह संदेश हुआ। यह पत्र आपके भाई तक पहुँचता है। भाई उस पत्र को पढ़ता है। आपका भाई प्राप्तकर्ता है। इस प्रकार संप्रेषण पूरा होता है।
आइए, देखें संप्रेषण कैसे पूरा होता है?
- स्रोत
- सोचने की प्रक्रिया अनुभूति निर्णय क्षमता
- माध्यम
- संदेश
- सोचने की प्रक्रिया अनुभूति निर्णय क्षमता
- प्राप्तकर्ता
संप्रेषण प्रक्रिया में नौ तत्व प्रमुख रूप से शामिल होते हैं।
- स्रोत
- वक्तृत्व क्षमता
- संदेश
- माध्यम
- प्राप्तकर्ता
- संदेश प्राप्ति
- प्रतिक्रिया
- संदर्भ
- जीवन मूल्य और दृष्टकोण
स्रोत
किसी भी संदेश का जन्म स्रोत से होता है। यह स्रोत कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वह स्रोत अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है। इसके लिए वह अपने अनुभव और भाषा ज्ञान का उपयोग करता है। वह स्रोत या व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों में ढालता है। मौखिक संप्रेषण के संदर्भ में इस स्रोत को वक्ता कहते हैं।
वक्तृत्व क्षमता
विचारों को भाषागत अभिव्यक्ति देने की कला को वक्तृत्व क्षमता कहते हैं। वक्ता की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसके जरिए वह अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त कर सके और श्रोता उसके संदेश को समझ सके ।
संदेश
वक्ता के विचारों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति को संदेश कहते हैं। यह संदेश लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और गैर मौखिक या आंगिक भी हो सकता है। भाषा में शब्दों, वाक्यों, प्रतीकों, बिंबों आदि के माध्यम से संदेश प्रसारित किए जाते हैं। भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। ‘राम ने श्याम को मारा’ और ‘श्याम ने राम को मारा का अर्थ बिल्कुल विपरीत है। व्याकरण के कारण संदेश का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक भाषा का अपना मुहावरा होता है। भाषा किसी संस्कृति का हिस्सा होती है। किसी भाषा को बोलने और समझने के लिए भाषा के व्याकरण, मुहावरे और संस्कृति को समझना आवश्यक है। भाषा संदेश का आधार है। वस्तुतः भाषा के जरिए ही संदेश बनाए और समझे जाते हैं।
परंतु संदेश केवल लिखित, मौखिक या शाब्दिक ही नहीं गैर-मौखिक, गैर-शाब्दिक या आंगिक भी होते हैं। मनुष्य अपने हाव-भाव, शारीरिक मुद्राओं और चेष्टाओं, आवाज के उतार-चढ़ाव, गति, सुरपरिवर्तन से भी काफी कुछ कह जाता है। अपनी भावनाओं को संप्रेषित कर देता है। कहने का तात्पर्य कि हमारे संदेश कई बार आंगिक या गैर-शाब्दिक भी होते हैं। इसमें भाषा नहीं होती परंतु अर्थ पूरा होता है।
सुविधा की दृष्टि से मौखिक और अमौखिक संप्रेषण को अलग तो कर दिया जाता है, परंतु यह विभाजन कृत्रिम है। वस्तुतः मौखिक और आंगिक अभिव्यक्ति एक दूसरे में गुथे होते हैं। ‘जाओ’ एक शब्द है परंतु कहने के अंदाज़ से इसका अर्थ बदल जाता है। यह आदेश भी हो सकता है, अनुमति भी, क्रोध की अभिव्यक्ति भी हो सकती है स्नेह का भी, हड़बड़ी का बोधक भी हो सकता है और गड़बड़ी का भी संप्रेषक को भाषा और वाणी में तालमेल रखना चाहिए ताकि उसका संदेश सही ढंग से संप्रेषित हो सके।
माध्यम
संदेश किसी माध्यम से प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुँचता है। मौखिक संप्रेषण में हवा माध्यम होता है। वक्ता से श्रोता तक संप्रेषण हवा के माध्यम से होता है। वक्ता द्वारा बोला हुआ संदेश हवा में तैरता हुआ श्रोता तक पहुँचता है। अब तो रेडियो तरंगों, सैटेलाइट आदि के माध्यम से संदेश को दूर-दूर तक फैलाया जा सकता है। जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लिखित संप्रेषण की स्थिति में लिपि माध्यम होती है जिसे हम आँखों से ग्रहण करते हैं।
प्राप्तकर्ता
वक्ता या स्रोत जिस तक अपना संदेश भेजना चाहता है उसे श्रोता या प्राप्तकर्ता कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में श्रोता ही प्राप्तकर्ता होता है जो संदेश ग्रहण करता है। यह भी हो सकता है कि संदेश जिसके लिए तैयार किया गया हो उसके अतिरिक्त दूसरे श्रोता भी उस संदेश को सुन लें और उन पर उस संदेश का प्रभाव पड़ सकता है। मान लीजिए हम किसी दोस्त का हँसी में मज़ाक उड़ा रहे हों और वह हमारी बात सुन ले। जिस तक हम अपना संदेश नहीं पहुँचाना चाहते उस तक संदेश पहुँच गया और इससे दोस्ती खतरे में पड़ सकती है।
संदेश प्राप्ति
प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को विचारों में ढालने की प्रक्रिया को संदेश प्राप्ति कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसे decoding कहा जाता है। सर्वोत्तम स्थिति वह होती है जिसमें श्रोता वक्ता द्वारा भेजे गए संदेश को उसी तरह समझता है जिस तरह वक्ता कहना चाहता है। श्रोता एवं वक्ता की भूमिका बदलती रहती है। अर्थात् श्रोता वक्ता की भूमिका निभाने लगता है और वक्ता श्रोता बन जाता है। टेलीफोन पर बातचीत करते समय ध्यान दीजिए। जब आप वक्ता होते हैं तो दूसरे छोर पर टेलीफोन सुन रहा व्यक्ति श्रोता की भूमिका निभा रहा होता है। फिर जब वह आपकी बात का जवाब देने लगता है तो आप श्रोता बन जाते हैं।
प्रतिक्रिया
वक्ता और श्रोता के बीच संवाद या आपसी बातचीत से ही संप्रेषण अपनी प्रक्रिया पूरी करता है। बड़ी मशहूर कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती संप्रेषण या पूर्ण संप्रेषण पर भी यही बात लागू होती है। श्रोता द्वारा वक्ता को भेजे गए संदेश को ‘प्रतिक्रिया’ या ‘फीडबैक’ कहते हैं। आमने-सामने के संप्रेषण में, जैसे कक्षा में पढ़ाते शिक्षक और व्याख्यान सुनते विद्यार्थियों के बीच यह प्रतिक्रिया तुरंत हो जाती है। दूर शिक्षा पद्धति के अध्ययन में यह प्रतिक्रिया तत्काल नहीं हो पाती। परंतु आज दूरस्थ शिक्षा में टेलीकांफ्रेंसिंग, ई-मेल, इंटरनेट आदि जैसी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग हो रहा है जिसके जरिए दूर बैठे विद्यार्थी भी अपने शिक्षकों को अपनी प्रतिक्रिया तुरंत भेज सकते हैं।
प्रतिक्रिया शाब्दिक भी हो सकती और गैर-शाब्दिक भी कभी प्रतिक्रिया मौखिक हो सकती है कभी श्रोता की आँखों या शारीरिक प्रतिक्रिया से भी यह पता चल सकता है कि वक्ता की बात का असर श्रोता पर क्या पड़ा? इसी प्रकार प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी।
संदर्भ
कोई भी संप्रेषण किसी न किसी संदर्भ से जुड़ा होता है। यह संदर्भ शारीरिक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी और सांस्कृतिक भी उदाहरण के लिए यदि आप दीवार में कील ठोक रहे हों और हथौड़ा आपकी उंगली पर लग जाए और वहाँ कोई न हो तो आपके मुँह से • अपशब्द भी निकल सकता है। परंतु यदि वहाँ आपकी माँ या पिता मौजूद हों तो शायद अपशब्द आपके मुँह से न निकलें और आप कह बैठे….ओ माँ, या बाबू जी …. । इस समय आप केवल अपने आपसे ही बात नहीं कर रहे होते हैं। बल्कि आप अपने माता-पिता को भी संदेश पहुँचा रहे होते हैं। इसी प्रकार मित्र से बात करते समय सहकर्मी से बात करते समय, शहर में अपने पड़ोसी से बात करते हुए, गाँव में अपने किसी संबंधी से बात करते हुए, आपके संदेश का स्वरूप एक सा नहीं रहता। हर परिवेश में संदेश को अलग-अलग ढंग से संप्रेषित किया जाता है।
जीवन मूल्य और दृष्टिकोण
संप्रेषण की प्रक्रिया में सहायक जिन तत्वों की चर्चा की गई वे आधारभूत तत्व हैं। इनके अलावा वक्ता के जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का भी उसके विषय के चुनाव, शब्दों के चुनाव आदि पर असर पड़ता है। इसी प्रकार श्रोता के जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का असर भी उसके संदेश को समझने और व्याख्यायित करने पर पड़ता है।
सफल संप्रेषण
कई बार ऐसा होता है कि जो आप कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते। उसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिल पाते। कई बार हम कहते कुछ हैं और सुनने वाला समझ कुछ और लेता है। कई बार इसका मज़ाक भी बन जाता है। मैं एक घटना सुनाता हूँ जो मेरे साथ घटी थी। बिजली गुल थी। मोमबत्ती जल रही थी। परिवार के सारे सदस्य गप-शप कर रहे थे। तभी बिजली आ गई। मेरी बहन ने मुझसे कहा- ‘फूँक दो।’ मैंने समझा मेरे चेहरे के सामने कोई मकड़ा का जाला है। मैंने मुँह उठाकर फूँक दिया। सारे लोग हँस पड़े क्योंकि मेरी
बहन मोमबत्ती फूँकने के लिए कह रही थी। मोमबत्ती मेरे पीछे खिड़की पर जल रही थी। अतः मैं अपनी बहन की बात समझ न पाया। संप्रेषण पूरा नहीं हो पाया। इसी प्रकार आपके जीवन में भी ऐसी ही कई घटनाएँ घटती होंगी जिसमें संप्रेषण पूरा नहीं हो पाता है। वक्ता कुछ और कहता है एवं श्रोता कुछ और समझ बैठता है। ‘गलत शब्द’ का प्रयोग करने से दोस्तों के बीच झगड़ा हो जाता है, परिवार के सदस्यों के बीच मन-मुटाव पैदा हो जाता है।
संप्रेषण संपर्क का काम करता है। जब यह संपर्क टूटता है तो संप्रेषण अधूरा रह जाता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बोलकर, सुनकर लिखकर और पढ़कर संप्रेषण पूरा होता है।
यहाँ हम सफल संप्रेषण की बात कर रहे हैं। वक्ता द्वारा प्रेषित संवाद श्रोताओं तक पहुँचता है और वक्ता जो कुछ कहना चाहता है श्रोता उसे उसी रूप में ग्रहण करता है तो संप्रेषण सफल माना जाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया पर बातचीत करते हुए हमने विस्तार से इसकी चर्चा की है। आइए अब यह पता लगाने की कोशिश करें कि सफल संप्रेषण में बाधा कैसे है?
सम्प्रेषण का अर्थ और प्रासंगिकता
सम्प्रेषण का अर्थ
अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ के अनुसार, सम्प्रेषण का अभिप्राय सूचनओं के प्रसार से है जो वाचिक (मौखिक या लिखित) अथवा अवाचिक (आंगिक अभिनय, संकेतों या प्रतीकों) के माध्यम से होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो विचारों, ज्ञान, अनुभूतियों और अनुभवों के विनिमय में सहायक होती है और अंतर्वैयक्तिक तथा सामाजिक लक्ष्यों के लिए आवश्यक होती है। प्रमुख रूप से इसके लिए भाषा एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है जो लोगों के विचारों और अभिमतों के विनिमय में सहायक होता है। यह सूचनाओं के साझा करने, निर्णय लेने, समस्या समाधान और संगठनों के निष्पादन को उन्नत बनाने में सहायक होता है। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रसारित होती है और एक अर्थपूर्ण अंतःक्रिया होती है जो एक माध्यम (उदाहरण के लिए माइक्रोफोन, ईमेल, डिजिटल माध्यमों इत्यादि) की सहायता से घटित होती है
सम्प्रेषण की प्रासंगिकता
चलिए सम्प्रेषण की कुछ प्रासंगिकता के बारे में विवेचना करें:
- यह प्रसार के साथ-साथ बातचीत, लेखन अथवा आंगिक अभिनयों के द्वारा सूचनाओं की प्राप्ति में सहायक होता है।
- यह एक स्रोत होता है जो संगठनों में समस्याओं के समाधान और निर्णयन की प्रक्रियाओं में सहायक होता है।
- यह कर्मचारियों के कार्य जिम्मेदारियों को नियोक्ताओं को सम्प्रेषित करने के साथ-साथ उनसे पुनर्निवेशन प्राप्ति में सहायक होता है।
- यह एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से कर्मचारियों के संदेहों और शिकायतों को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार, अप्रत्यक्ष रूप से यह कर्मचारियों की अभिप्रेरणा और प्रतिबद्धता को उन्नत बनाता है।
सम्प्रेषण एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से कर्मचारियों की अभिवृत्ति और व्यव्हार परिवर्धित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो पूर्ण सूचित है वह निश्चित रूप से असूचित व्यक्ति की तुलना में बेहतर निष्पादन करेगा।
- यह एक तंत्र है जो संगठन के कर्मचारियों के समाजीकरण, नेटवर्किंग और बेहतर टीम प्रबंधन को उन्नत बनाता है।
- यह कर्मचारियों के नियंत्रण तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह संगठन के कर्मचारियों के व्यवहार के नियंत्रण में भी सहायक होता है।
- यह संगठनों के समूहों और मंडलियों के मध्य के संघर्षों के समाधान में भी सहायक होता है।
- यह कर्मचारियों कार्य-निष्पादन और कार्य जिम्मेदारियों को निष्पादित करने में भी सहायक होता है।
- यह संगठन के मंडलियों के सदस्यों के मध्य सहयोग को सुगम बनाता है।
सम्प्रेषण के प्रकार्य
अब तक आप सम्प्रेषण की प्रासंगिकता से परिचित हो गए होंगे। आईये हम सम्प्रेषण की प्रक्रिया के प्रकार्यों की विवेचना करें:
अभिव्यक्ति
सम्प्रेषण संगठन के लिए एक प्रासंगिक प्रक्रिया है। यह उन साधनों में से एक है जो जिसके द्वारा कर्मचारीरी अपने आपको अभिव्यक्त करते हैं, समाजिक रूप से अंतः क्रिया करते हैं और अपने शिकायतों को साझा करते हैं। कई व्यवसायों में (जैसे अधिवक्ता, टेलीफोन संचालक इत्यादि) उनका रोजगार सामाजिक अंतःक्रिया का प्राथमिक स्रोत होता है। यह संगठन की संस्कृति के निर्माण को भी दिशा देता है।
नियंत्रण
सम्प्रेषण की सहायता से संगठन अपने नियमों, अधिनियमों, मानकों और संस्कृति को व्यक्त करते हैं। यह संगठनों को अपने कर्मचारियों को अनुशासन में रखने और नियमों का पालन करवाने में भी मददगार हो सकते हैं। इसके अलावा यह कर्मचारियों को अपने अनुभूतियों और अभिमतों को साझा करने में सहायक होते हैं।
अभिप्रेरणा
अभिप्रेरणा का अभिप्राय चलन प्रभाव से होता है जो व्यक्तियों को कार्य करने अथवा अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। संगठन या नियोक्ता अपने कर्मचारियों को निपुणता से निष्पादन करने के तरीकों को जानने के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं। इन परिस्थितियों में संगठन को अपने लक्ष्यों और पुनर्निवेशन को सम्प्रेषित करने की आवश्यकता होती है और इसके साथ कर्मचारियों को उनके निष्पादन को उन्नत बनाने के लिए पुनर्बलित करने की भी आवश्यकता होती हैं।
समन्वय
संगठन को लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने कार्यकलापों, लक्ष्यों, प्रक्रियाओं, नवीन विकासों और तकनीकी इत्यादि को समन्वित करने की जरूरत होती है। इस प्रकार की सूचनाओं को सतत बैठकों के द्वारा कर्मचारियों को बताने की जरूरत होती है। वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बैठकों में नियोक्ता और कर्मचारी उत्पादन चक्रों, वितरण के तरीकों और अन्य क्षेत्रों जैसे मुद्दों पर परिचर्चा करते हैं। इस प्रकार सम्प्रेषण संगठनों में समन्वय बनाने में सहायक होते हैं।
समस्या समाधान
सम्प्रेषण कर्मचारियों संगठन की कार्य- सम्बंधित समस्याओं पर चर्चा करने में सहायक होता है। यह बुद्धि-उत्तेजक क्षमता अनुक्रियाओं और समाधानों को अंतिम रूप देने में सहायक होता है। इस प्रकार यह अंतिम रूपसे संगठन को लाभान्वित करता है।
द्वंद्व प्रबंधन
कर्मचारियों में किसी प्रकार का संघर्ष प्रतिभावान कर्मचारियों को खोने अथवा मुकदमेबाजी का कारण हो सकता है। सम्प्रेषण प्रक्रिया की मदद से कर्मचारी अपने मतभेदों की चर्चा कर सकते हैं और इस प्रकार संघर्षों का प्रबंधन कर सकते हैं।
सम्प्रेषण प्रक्रिया के तत्व
उपर्युक्त खण्डों में आपको सम्प्रेषण के अर्थ, प्रासंगिकता और प्रकार्यों के बारे में बताया गया था। आईये अब हम सम्प्रेषण की प्रक्रिया की चर्चा करें। क्या अपने कभी सोचा है। कि सम्प्रेषण किस प्रकार घटित होता है? सम्प्रेषण की प्रक्रिया में क्या मूल अवयव अथवा तत्व सम्मिलित होते हैं? इस खंड में उन मूल तत्वों की चर्च की जाएगी जो सम्प्रेषण की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं।
मूलतः एक आदर्श सम्प्रेषण तंत्र में पांच अवयव / तत्व सम्मिलित होते हैं:
स्रोत / प्रेषक
स्रोत का अभिप्राय एक माध्यम से होता है जहाँ से सम्प्रेषण का आरम्भ अथवा शुरुआत होती है। सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में बोलने में वह व्यक्ति एक स्रोत होता है जो बोलता है। जबकि लिखित सन्देश में लेखक एक स्रोत होता है।
प्रसारक
इसका उपयोग सूचनाओं को यंत्रावली जैसे रेडियो अथवा दूरदर्शन के संकेतों द्वारा प्रसारित करने में किया जाता है।
माध्यम
स्रोत और गंतव्य के बीच सम्प्रेषण को प्रसारित करने अथवा भेजने के लिए एक माध्यम होता है जिसके द्वारा सम्प्रेषण को प्रसारित किया जाता है। उदाहरण के लिए जब एक व्यक्ति बोल रहा होता है तब हवा सम्प्रेषण का एक माध्यम होती हैं जबकि लेखन में कागज सम्प्रेषण का एक माध्यम होता है।
प्राप्तकर्ता / गंतव्य
प्राप्तकर्ता का अभिप्राय उस लक्षित व्यक्ति से होता है जो प्रेषक द्वारा भेजी गयी सूचनाओं को प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो बात सुनकर अथवा सन्देश पढ़कर जो उसके लिए बनाया गया हो, एक प्राप्तकर्ता अथवा सम्प्रेषण का गंतव्य होता है।
पुनर्निवेशन
इस बात पर नियंत्रण रखने के लिए कि क्या प्राप्तकर्ता को सूचनाएं उचित रूपसे सम्प्रेषित की गयी हैं, प्रेषक को एक निरंतर पुनर्निवेशन की आवश्यकता पड़ती है। पुनर्निवेशन एक वाचिक अथवा अवाचिक अनुक्रिया के रूप में हो सकता है। यह प्रेषक अथवा स्रोत के लिए इस बात की पुष्टि में सहायक होता है कि क्या उसने सन्देश को सही अथवा गलत रूप से प्रेषित किया है। यह ऐसे भी अवसर उपलब्ध कराता है जिसमें प्राप्तकर्ता स्पष्टीकरण कर सके। पुनर्निवेशन सम्प्रेषण की शुद्धता को उन्नत करने में सहायक होता है।
कोलाहल
कोई भी आवाज / संकेत अथवा ध्वनि जो किसी सन्देश को उचित रूपसे प्रेषित करने अथवा प्राप्त करने में अवरोध करता है, कोलाहल कहलाता है। उदाहरण के लिए एक माइक्रोफोन की शुरुआत एक तेज ध्वनि से होती है जबकि आप अथवा आपका बॉस बोल रहा होता है। इस प्रकार का कोलाहल एक भौतिक कोलाहल होता है लेकिन कई बार हमारे विचार एक मनोवैज्ञानिक कोलाहल के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि ये किसी सूचना को सुनने अथवा पढ़ने में केंद्रित होने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
कूटसंकेतन और विकूटसंकेतन
कूटसंकेतन का अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें प्रेषक सूचनाओं को कूटसंकेतित / बदलता है जो उसे अपने शब्दों / तरीकों में भेजना चाहता है जबकि विकूटसंकेतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से प्राप्तकर्ता सूचनाओं को विसंकेतित करता है और समझता है।
सम्प्रेषण की प्रक्रिया
सम्प्रेषण की प्रक्रिया में सूचनाओं का विनिमय (प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच ) सम्मिलित होता है और यह एक चक्रीय प्रक्रिया होती है (चित्र ) जैसा की पहले कहा जा चुका है जो सूचना को भेजता है प्रेषक अथवा स्रोत होता है और जो इसे प्राप्त करता है वह गंतव्य अथवा प्राप्तकर्ता होता है। प्रेषक और प्राप्तकर्ता की प्रस्थिति परस्पर बदलाव योग्य होती है। चलिए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। यदि एक अध्यापक कक्षा में किसी गोचर की व्याख्या करा रहा हो तब अध्यापक एक प्रेषक होता है और विद्यार्थी प्राप्तकर्ता होते हैं। इसी बीच यदि एक विद्यार्थी अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है तब वह विद्यार्थी प्रेषक और अध्यापक एक प्राप्तकर्ता हो जाता है। इस प्रकार सूचना प्रेषक द्वारा किसी माध्यम द्वारा प्राप्तकर्ता को भेजी जाती है। सम्प्रेषण पुनर्निवेशन के द्वारा प्रभावी हो जाती है जबकि किसी कोलाहल की उपस्थिति में यह अप्रभावी हो जाती है।

- 11 – भाद्रपद मासकी ‘अजा’ और ‘पद्मा’ एकादशीका माहात्य
- 14 – पुरुषोत्तम मासकी ‘कमला’ और ‘कामदा’
- 13 – कार्तिक मासकी ‘रमा’ और ‘प्रबोधिनी’एकादशीका माहात्म्य
- 12 – आश्विन मासकी ‘इन्दिरा’ और ‘पापाङ्कुशा’ एकादशीका माहात्य
- 10 – श्रावण मासकी ‘कामिका’ और ‘पुत्रदा’ एकादशीका माहात्म्य
- About Culture-संस्कृति के विषय में
- About Institution-संस्था के विषय में
- ACT.-अधिनियम
- Awareness About Geography-भूगोल के विषय में जागरूकता
- Awareness About Indian History-भारतीय इतिहास के विषय में जागरुकता
- Awareness About Maths-गणित के बारे में जागरूकता
- Awareness about Medicines
- Awareness About Politics-राजनीति के बारे में जागरूकता
- Awareness-जागरूकता
- Basic Information
- Bharat Ratna-भारत रत्न
- Biography
- Chanakya Quotes
- CLASS 9 NCERT
- CMs OF MP-मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
- CSIR UGC NET
- e-Test-ई-टेस्ट
- Education
- Education-शिक्षा
- Ekadashi Mahatmya
- FULL TEST SERIES
- GK
- Granthawali-ग्रन्थावली
- Hindi Biography – जीवन परिचय
- Hindi Literature
- Hindi Literature-हिंदी साहित्य
- HINDI NATAK-हिंदी नाटक
- Hindi Upanyas-हिंदी उपान्यास
- ICT-Information And Communication TEchnology
- Jokes-चुटकुले
- Kabir ji Ki Ramaini-कबीर जी की रमैणी
- KAHANIYAN
- Katha-Satsang-कथा-सत्संग
- Kavyashastra-काव्यशास्त्र
- Meaning In Hindi-मीनिंग इन हिंदी
- Meaning-अर्थ
- MOCK TEST
- Motivational Quotes in Hindi-प्रेरक उद्धरण हिंदी में
- MPESB(VYAPAM)-Solved Papers
- MPPSC
- MPPSC AP HINDI
- MPPSC GENERAL STUDIES
- MPPSC GS PAPER
- MPPSC-AP-HINDI-EXAM-2022
- MPPSC-Exams
- MPPSC-मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
- Nibandha
- Padma Awardees-पद्म पुरस्कार विजेता
- PDFHUB
- PILLAR CONTENT
- QUOTES
- RSSU CHHINDWARA-राजा शंकर शाह वि.वि. छिंदवाड़ा
- RSSU QUESTION PAPERS
- SANSKRIT
- SANSKRIT VYAKARAN
- SANSKRIT-HINDI
- Sarkari Job Advertisement-सरकारी नौकरी विज्ञापन
- Sarkari Yojna-सरकारी योजना
- Sarkari-सरकारी
- Sarthak News-सार्थक न्यूज़
- SCHOOL
- SOLVED FIRST PAPER CSIR NET
- Theoretical Awareness-सैद्धांतिक जागरूकता
- UGC
- UGC NET
- UGC NET COMPUTER SCIENCE
- UGC NET HINDI MOCK TEST
- UGC NET NEWS
- UGC_NET_HINDI
- UGCNET HINDI
- UGCNET HINDI PRE. YEAR QUE. PAPERS
- UGCNET HINDI Solved Previous Year Questions
- UGCNET-FIRST-PAPER
- UGCNET-FIRSTPAPER-PRE.YEAR.Q&A
- UPSC-संघ लोक सेवा आयोग
- Various Exams
- VEDIC MATHS
- Yoga
- इकाई – 02 शोध अभिवृत्ति (Research Aptitude)
- इकाई – 03 बोध (Comprehension)
- इकाई – 04 संप्रेषण (Communication)
- इकाई – 07 आंकड़ों की व्याख्या (Data Interpretation)
- इकाई – 10 उच्च शिक्षा प्रणाली (Higher Education System)
- इकाई -01 शिक्षण अभिवृत्ति (Teaching Aptitude
- इकाई -06 युक्तियुक्त तर्क (Logical Reasoning)
- इकाई -09 लोग विकास और पर्यावरण (People, Development and Environment)
- इकाई 08 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT-Information and Communication Technology)
- इकाई-05 गणितीय तर्क और अभिवृत्ति (Mathematical Reasoning And Aptitude)
- कबीर ग्रंथावली (संपादक- हजारी प्रसाद द्विवेदी)
- कविताएँ-Poetries
- कहानियाँ – इकाई -07
- कहानियाँ-KAHANIYAN
- कहानियाँ-Stories
- खिलाड़ी-Players
- प्राचीन ग्रन्थ-Ancient Books
- मुंशी प्रेमचंद
- व्यक्तियों के विषय में-About Persons
- सार्थक न्यूज़
- साहित्यकार
- हिंदी व्याकरण-Hindi Grammar