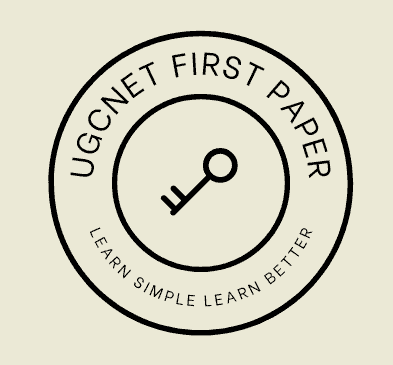10.4-(Professional Technical and Skill Based Education)
भारतीय शिक्षा प्रणाली मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के तहत (10+2+3) पैटर्न पर आधारित है। एमएचआरडी 26 सितंबर, 1985 को भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 में 174वें संशोधन के माध्यम से बनाया गया था।
मंत्रालय के मुख्य उद्देश्य होंगे:
शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि इसे अक्षरश: लागू किया जाए
नियोजित विकास, जिसमें पहुंच का विस्तार करना और पूरे देश में शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है, उन क्षेत्रों में भी जहां लोगों की शिक्षा तक आसान पहुंच नहीं है।
गरीबों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों पर विशेष ध्यान देना
समाज के वंचित वर्गों के योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति, ऋण सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
देश में शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए यूनेस्को और विदेशी सरकारों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम करने सहित शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना।
एमएचआरडी दो विभागों के माध्यम से काम करता है:
- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
- उच्च शिक्षा विभाग
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसमें स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव है।
भारतीय शिक्षा प्रणाली की संरचना
भारतीय शिक्षा प्रणाली प्राथमिक शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षा पर शोध करने के लिए काम करती है। इसे निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:
- स्कूली शिक्षा और साक्षरता
- व्यावसायिक शिक्षा (कुशल आधारित)
यूजीसी नेट के नए संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार हमें केवल उच्च और कौशल आधारित शिक्षा से संबंधित अध्ययन करना होगा।
उच्च शिक्षा प्रणाली
उच्च शिक्षा को तृतीयक शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है, जिसमें अकादमिक, पेशेवर और तकनीकी डिग्री शामिल हैं।
यह खंड व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा पर चर्चा करेगा
शैक्षणिक डिग्री (गैर-व्यावसायिक शिक्षा)
गैर-पेशेवर शिक्षा सैद्धांतिक अध्ययन पर जोर देती है और इसे मुख्य रूप से पेशेवर करियर की तैयारी के रूप में नहीं बनाया गया है। ये डिग्री प्रोग्राम अनुसंधान की ओर ले जा सकते हैं, जिससे ‘डॉक्टर’ की उपाधि दी जा सकती है। ये पाठ्यक्रम छात्रों को पेशेवर प्रथाओं के ज्ञान के विशिष्ट अनुप्रयोगों के बजाय अकादमिक अनुशासन में छात्रवृत्ति के जीवन के लिए तैयार करते हैं। इसके अलावा, अकादमिक योग्यता अर्जित करने वाले छात्र अक्सर अपने पेशे में डिग्री का उपयोग नहीं करते हैं।
ऐसे डिग्री पाठ्यक्रमों के उदाहरण हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स (बीए), बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी), मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए), मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी), मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एम.फिल), डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी), आदि।
शैक्षणिक डिग्री, जैसे बीए, बी.एससी. और बी.कॉम को उच्च शिक्षा का अधिक ‘पारंपरिक’ और सुस्थापित रूप माना गया है और ये विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञताओं में उपलब्ध हैं, जैसे कि बी.ए. अर्थशास्त्र, बी.ए. अंग्रेजी, बी.ए. हिंदी, बी.एससी. भौतिकी, बी.एससी. कंप्यूटर साइंस, बीएससी एप्लाइड साइंस, और सूची जारी होती है। एक अकादमिक डिग्री आमतौर पर विशिष्ट विषय पर पूरी तरह से शिक्षा और ज्ञान प्रदान करती है, जिसके बाद छात्र मास्टर डिग्री या पेशेवर पाठ्यक्रम का पीछा कर सकता है।
परंपरागत रूप से, अकादमिक डिग्री पाठ्यक्रमों का अधिक महत्व था, लेकिन हाल के दिनों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की लोकप्रियता ने नौकरी के बाजार में मजबूती से अपनी जगह बना ली है।
गैर-व्यावसायिक शिक्षा: (Non-Professional Education)
अधिक करियर विकल्प खुला रखता है
विशेषज्ञता हासिल करने में आपकी मदद करता है
पेशेवर डिग्री की तरह आपको नौकरी के लिए तैयार नहीं करता है
व्यावसायिक शिक्षा (Professional Education)
एक पेशेवर डिग्री छात्रों को कानून, फार्मेसी, चिकित्सा और शिक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में करियर के लिए तैयार करने में मदद करती है। व्यावसायिक शिक्षा एक पेशेवर स्कूल में विशेष प्रशिक्षण के लिए एक औपचारिक दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से प्रतिभागी सामग्री ज्ञान प्राप्त करते हैं और तकनीकों को लागू करना सीखते हैं।
व्यावसायिक शिक्षा के कुछ सामान्य लक्ष्यों में शामिल हैं:
- एक पेशेवर अनुशासन के लिए बुनियादी ज्ञान और मूल्यों को शामिल करना;
- अभ्यास में लागू केंद्रीय अवधारणाओं, सिद्धांतों और तकनीकों को समझना;
- पेशेवर अभ्यास में जिम्मेदार प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यता का स्तर प्राप्त करना; और
- क्षमता के निरंतर विकास के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना।
- व्यावसायिक शिक्षा के उदाहरण (डिग्री) सर्जरी और दवाएं (एमबीबीएस, एमएस, एमडी)
- दंत चिकित्सा (बीडीएस)
- प्रबंधन अध्ययन (एमबीए)
- कानून (एलएलबी, एलएलएम)
- शिक्षा (बी.एड., एम.एड.)
- सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस आदि।
- तकनीकी शिक्षा (तकनीकी डिग्री)
- ब्रिटानिका के अनुसार, “तकनीकी शिक्षा विज्ञान और आधुनिक तकनीक से जुड़े नौकरियों के लिए छात्रों की शैक्षणिक और तकनीकी तैयारी है। यह विज्ञान और गणित के बुनियादी सिद्धांतों की समझ और व्यावहारिक अनुप्रयोग पर जोर देता है।
- भारतीय संदर्भ में, तकनीकी शिक्षा में इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, नगर नियोजन, फार्मेसी, अनुप्रयुक्त कला और शिल्प, होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी के कार्यक्रम शामिल हैं।
AICTE :
तकनीकी शिक्षा का शीर्ष निकाय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ( (AICTE) ) है। नवंबर 1945 में तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर एक सर्वेक्षण करने और समन्वित और एकीकृत तरीके से देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में, (AICTE) की स्थापना (AICTE) अधिनियम, 1987 द्वारा की गई थी।
तकनीकी शिक्षा के उदाहरण:
- इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (डिप्लोमा, बी.टेक, एम.टेक)
- आर्किटेक्चर (B.Arch, M.Arch)
- फार्मेसी (बी.फार्मा, एम.फार्मा), आदि।
कौशल आधारित शिक्षा (व्यावसायिक शिक्षा)
व्यावसायिक शिक्षा जिसे करियर और तकनीकी शिक्षा (सीटीई) भी कहा जाता है, शिक्षार्थियों को उन नौकरियों के लिए तैयार करती है जो मैन्युअल या व्यावहारिक गतिविधियों पर आधारित होती हैं, पारंपरिक रूप से गैर-शैक्षणिक और पूरी तरह से एक विशिष्ट व्यापार, व्यवसाय या व्यवसाय से संबंधित होती हैं, इसलिए यह शब्द, जिसमें शिक्षार्थी भाग लेता है . इसे कभी-कभी तकनीकी शिक्षा के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि शिक्षार्थी सीधे तकनीकों या प्रौद्योगिकी के एक विशेष समूह में विशेषज्ञता विकसित करता है।
व्यावसायिक शिक्षा एक कौशल आधारित शिक्षा है, जहाँ शिक्षार्थी व्यावहारिक और शैक्षणिक ज्ञान के माध्यम से कौशल प्राप्त करते हैं। कौशल आधारित शिक्षा एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए पूरी तरह से रोजगारोन्मुखी है।
कौशल आधारित शिक्षा के उदाहरण (व्यावसायिक शिक्षा) यह है
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
- संकल्प (आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता)
- उड़ान
- पॉलिटेक्निक योजनाएं
- स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना
- व्यावसायिक परिषदें
- व्यावसायिक परिषदें पाठ्यक्रमों की मान्यता, व्यावसायिक संस्थानों के प्रचार और स्नातक कार्यक्रमों और विभिन्न पुरस्कारों के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।
वैधानिक पेशेवर परिषदें हैं:
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ( (AICTE) )
- मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI)
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ( (ICAR) )
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE)
- भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (DCI)
- फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) भारतीय
- नर्सिंग काउंसिल (INC)
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI)
- सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी (CCH) सेंट्रल
- भारतीय चिकित्सा परिषद (CCIM)
- वास्तुकला परिषद
- दूरस्थ शिक्षा परिषद ( (DEC) )
- पुनर्वास परिषद
- ग्रामीण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय परिषद ( (NCRI) )
- राज्य उच्च शिक्षा परिषद (एससीएचई)
1. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), फरीदाबाद
aicte-india.org
As per official website :
अवलोकन (Overview)
भारत में तकनीकी शिक्षा समग्र शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा योगदान देती है और हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
संगठन (The Organisation)
एआईसीटीई अधिनियम (1987) के प्रावधानों के अनुसार, 1988 में इसकी स्थापना के बाद पहले पांच वर्षों के लिए, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री, परिषद के अध्यक्ष थे। पहला पूर्णकालिक अध्यक्ष 2 जुलाई, 1993 को नियुक्त किया गया था और मार्च 1994 में तीन साल की अवधि के साथ परिषद का पुनर्गठन किया गया था। 7 जुलाई, 1994 को कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया गया और 1994-95 में अखिल भारतीय अध्ययन बोर्ड और सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कोलकाता, चेन्नई, कानपुर और मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को एआईसीटीई में स्थानांतरित कर दिया गया और इन कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी विदेशी सेवा शर्तों पर परिषद में प्रतिनियुक्त किया गया। 1 अक्टूबर 1995.
ये कार्यालय चार क्षेत्रों (उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण) में क्षेत्रीय समितियों के सचिवालय के रूप में कार्य करते थे। 27 जुलाई, 1994 को दक्षिण-पश्चिम, मध्य और उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों में तीन नई क्षेत्रीय समितियाँ भी स्थापित की गईं, जिनके सचिवालय क्रमशः बैंगलोर, भोपाल और चंडीगढ़ में स्थित हैं। दक्षिण-मध्य क्षेत्र में एक और क्षेत्रीय समिति, जिसका सचिवालय हैदराबाद में है। 8 मार्च 2007 को अधिसूचित किया गया।
हमारे उद्देश्य (Our Objectives)
- में गुणवत्ता को बढ़ावा देना
- तकनीकी शिक्षा।
- योजना एवं समन्वित विकास
- तकनीकी शिक्षा प्रणाली के.
- के विनियम एवं रखरखाव
- मानदंड और मानक.
हमारा नज़रिया (Our Vision)
“तकनीकी जनशक्ति की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर और समाज के सभी वर्गों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा सुनिश्चित करके देश के तकनीकी और सामाजिक-आर्थिक विकास का नेतृत्व करने वाला एक विश्व स्तरीय संगठन बनना।”
हमारा विशेष कार्य (Our Mission)
- एक सच्चा सुविधाप्रदाता और एक वस्तुनिष्ठ नियामक;
- पारदर्शी शासन और समाज के प्रति जवाबदेह दृष्टिकोण;
- मान्यता के माध्यम से संस्थानों के विश्व स्तरीय मानकों को सुनिश्चित करके देश में तकनीकी शिक्षा का नियोजित और समन्वित विकास;
- उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान, शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवीन अनुसंधान और विकास कार्यक्रम विकसित करने पर जोर;
- इष्टतम संसाधन उपयोग के लिए/या संस्थानों के नेटवर्क के साथ नेटवर्किंग;
- ज्ञान का प्रसार;
- प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान और वैश्विक जनशक्ति योजना;
- नए उत्पादों, सेवाओं और पेटेंट के विकास के लिए उद्योग-संस्थान संपर्क को बढ़ावा देना;
- उद्यमशीलता को बढ़ावा देना;
- स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना;
- अनौपचारिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना;
- सभी को सस्ती शिक्षा प्रदान करना;
- भारत में तकनीकी शिक्षा को विश्व स्तर पर स्वीकार्य बनाना;
2. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI), नई दिल्ली
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) की स्थापना भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 द्वारा 1993 में संशोधित की गई थी। परिषद को भारत में विश्वविद्यालयों या चिकित्सा संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक चिकित्सा शिक्षा के लिए न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने का अधिकार है।
3. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), नई दिल्ली
As per official website : https://www.icar.org.in
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE) के तहत एक स्वायत्त संगठन है। पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के रूप में जाना जाता था, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को कृषि पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसरण में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। आईसीएआर का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
परिषद पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। देश भर में फैले 113 आईसीएआर संस्थानों और 74 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है। आईसीएआर ने अपने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से भारत में हरित क्रांति और उसके बाद कृषि में विकास लाने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसने देश को खाद्यान्न उत्पादन में 6.21 गुना, बागवानी फसलों में 11.53 गुना, मछली में 21.61 गुना वृद्धि करने में सक्षम बनाया है। 1950-51 से 2021-22 तक दूध में 13.01 गुना और अंडे में 70.74 गुना वृद्धि हुई है, जिससे राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। इसने कृषि में उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई है।
यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के अत्याधुनिक क्षेत्रों में लगा हुआ है और इसके वैज्ञानिकों को अपने क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), नई दिल्ली
https://ncte.gov.in/website/about.aspx

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय)
परिचय
एनसीटीई, भारत सरकार के एक वैधानिक निकाय के रूप में, 17 अगस्त, 1995 को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के अनुसरण में पूरे देश में शिक्षक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करने और शासन करने के लिए अस्तित्व में आया। शिक्षक शिक्षा के लिए मानदंडों और मानकों का विनियमन और उचित रखरखाव। यह संगठन एक अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार है और इसमें 4 क्षेत्रीय समितियों अर्थात् उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के साथ विभिन्न प्रभाग शामिल हैं, जो सभी नई दिल्ली में तैनात हैं। एनसीटीई द्वारा किए जाने वाले कार्यों का दायरा बहुत व्यापक है, जिसमें सभी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शामिल हैं। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed), बैचलर ऑफ एजुकेशन (B.Ed), मास्टर ऑफ एजुकेशन (M.Ed) आदि। इसमें छात्रों-शिक्षकों को बुनियादी, प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाने के लिए सक्षम बनाने के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण शामिल है। एनईपी 2020 के अनुरूप नई स्कूल प्रणाली का मध्य और माध्यमिक स्तर।
एनसीटीई को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है और उसने एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी), शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) और नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग (एनएमएम) जैसे विभिन्न राष्ट्रीय जनादेश लिए हैं। एनईपी 2020 के अनुरूप एनसीटीई द्वारा अन्य शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों यानी विनियमन, पाठ्यक्रम और डिजिटल वास्तुकला में संशोधन किया जा रहा है। इस तरह की पहल के साथ एनसीटीई न केवल शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए प्रयास करती है, बल्कि हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखती है। देश। एनईपी 2020 में सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा और सेवाकालीन शिक्षक क्षमता निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ शिक्षकों की भूमिका में एक आदर्श बदलाव की परिकल्पना की गई है।
उद्देश्य (Objectives)
एनसीटीई का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास, शिक्षक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन और उचित रखरखाव और उससे जुड़े मामलों को प्राप्त करना है। एनसीटीई को दिया गया अधिदेश बहुत व्यापक है और इसमें शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के पूरे दायरे को शामिल किया गया है, जिसमें स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक चरणों में पढ़ाने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने और गैर-औपचारिक शिक्षा शामिल है। अंशकालिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और दूरस्थ (पत्राचार) शिक्षा पाठ्यक्रम।
परिषद के कार्य
यह परिषद का कर्तव्य होगा कि वह शिक्षक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने और शिक्षक शिक्षा के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए और इसके तहत अपने कार्यों को करने के उद्देश्यों के लिए ऐसे सभी कदम उठाए जो वह उचित समझे। अधिनियम, परिषद यह कर सकती है:
- शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करना और उसके परिणाम प्रकाशित करना;
- शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाएँ और कार्यक्रम तैयार करने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मान्यता प्राप्त संस्थानों को सिफारिशें करना;
- देश में शिक्षक शिक्षा और उसके विकास का समन्वय और निगरानी करना;
- स्कूलों या मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक के रूप में नियोजित होने वाले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित करना;
- शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षणों की किसी निर्दिष्ट श्रेणी के लिए मानदंड निर्धारित करना, जिसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड, और उम्मीदवारों के चयन की विधि, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम सामग्री और पाठ्यक्रम का तरीका शामिल है;
- मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अनुपालन के लिए, नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए, और भौतिक और शैक्षणिक सुविधाएं, स्टाफिंग पैटर्न और स्टाफ योग्यता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना;
- शिक्षक शिक्षा योग्यता, ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश के मानदंड और पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण की योजनाओं के लिए परीक्षाओं के संबंध में मानक निर्धारित करना;
- मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन फीस और अन्य शुल्कों के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित करना;
- शिक्षक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना और संचालित करना और उसके परिणामों का प्रसार करना;
- परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों, दिशानिर्देशों और मानकों के कार्यान्वयन की समय-समय पर जांच और समीक्षा करना और मान्यता प्राप्त संस्थान को उचित सलाह देना;
- मान्यता प्राप्त संस्थानों पर जवाबदेही लागू करने के लिए उपयुक्त प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली, मानदंड और तंत्र विकसित करना;
- शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए योजनाएं बनाना और मान्यता प्राप्त संस्थानों की पहचान करना और शिक्षक विकास कार्यक्रमों के लिए नए संस्थान स्थापित करना;
- शिक्षक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएँ; और
- ऐसे अन्य कार्य करना जो केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं।
एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम
एनसीटीई ने निम्नलिखित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए 28 नवंबर 2014 को संशोधित विनियम और मानदंड और मानक अधिसूचित किए:
- प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा प्रीस्कूल शिक्षा में डिप्लोमा (डीपीएसई) की ओर ले जाता है।
- प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, जो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.ई.एल.एड.) की ओर ले जाता है।
- बैचलर ऑफ एलीमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (बी.एल.एड.) की डिग्री प्राप्त होती है।
- बैचलर ऑफ एजुकेशन कार्यक्रम बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.) की डिग्री की ओर ले जाता है।
- मास्टर ऑफ एजुकेशन कार्यक्रम से मास्टर ऑफ एजुकेशन (एम.एड.) की डिग्री प्राप्त होती है।
- शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) प्राप्त होता है।
- बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम जिसके परिणामस्वरूप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी.पी.एड.) की डिग्री प्राप्त होती है।
- मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम से मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (एम.पी.एड.) की डिग्री प्राप्त होती है।
- मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा, जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.ई.एल.एड.) होता है।
- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बैचलर ऑफ एजुकेशन कार्यक्रम, जिसके फलस्वरूप बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.) की डिग्री प्राप्त होती है।
- कला शिक्षा (दृश्य कला) में डिप्लोमा कार्यक्रम कला शिक्षा (दृश्य कला) में डिप्लोमा की ओर ले जाता है।
- कला शिक्षा में डिप्लोमा (प्रदर्शन कला) कार्यक्रम कला शिक्षा में डिप्लोमा (प्रदर्शन कला) की ओर ले जाता है।
- B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed की ओर ले जाने वाला 4-वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम। डिग्री।
- बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम 3-वर्षीय (अंशकालिक) जिससे बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड) की डिग्री प्राप्त होती है।
- बी.एड., एम.एड (एकीकृत) डिग्री के लिए 3-वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम।
एनसीटीई विनियम 2014: मुख्य बातें
- एनसीटीई ने सिफारिशों का पालन करते हुए भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना संख्या 346 (एफ.सं. 51-1/2014/एनसीटीई/एन एंड एस) के तहत 28 नवंबर 2014 को 15 कार्यक्रमों के लिए मानदंडों और मानकों के साथ संशोधित विनियम 2014 को पूरा और अधिसूचित किया। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर सरकार द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति वर्मा आयोग (जेवीसी)।
- मैं एक। जेवीसी ने शिक्षक शिक्षा में व्यापक सुधारों का सुझाव दिया था जिसे नए विनियम 2014 में संबोधित किया गया है। नए विनियम एनसीटीई द्वारा हितधारकों के साथ किए गए व्यापक परामर्श का परिणाम हैं।
- विनियम 2014 की महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं:
- 15 कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश की गई है, जिसमें पहली बार तीन नए कार्यक्रमों को मान्यता दी गई है – 4-वर्षीय B.A/B.Sc.B.Ed., 3-वर्षीय B.Ed. (अंशकालिक), और 3-वर्षीय बी.एड.-एम.एड. कार्यक्रम.
- तीन कार्यक्रमों की अवधि – बी.एड., बी.पी.एड., एम.एड. – अधिक पेशेवर कठोरता प्रदान करते हुए और सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इसे बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है।
- अब से, स्टैंड-अलोन संस्थानों के स्थान पर, समग्र संस्थानों (बहु-विषयक या बहु-शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम) में शिक्षक शिक्षा स्थापित की जाएगी।
- प्रत्येक कार्यक्रम पाठ्यक्रम में तीन घटक शामिल होते हैं – सिद्धांत, व्यावहारिक, इंटर्नशिप; और कार्यक्रम का कम से कम 25% स्कूल-आधारित गतिविधियों और इंटर्नशिप के लिए विकसित किया गया है।
- आईसीटी, योग शिक्षा, लिंग और विकलांगता/समावेशी शिक्षा प्रत्येक कार्यक्रम पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग हैं।
- अधिक एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाता है।
- शिक्षक प्रशिक्षक एम.एड. डिग्री या तो प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा में विशेषज्ञता के साथ आती है।
- अंतर्निहित गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के साथ मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) अधिक कठोर हो गई है।
- सेवारत शिक्षकों के पास उच्च टीई योग्यता-डीएलएड (ओडीएल), बी.एड. प्राप्त करने के लिए अधिक विकल्प हैं। (ओडीएल), बी.एड. (पार्ट टाईम)।
- आवेदन करते समय संबद्ध विश्वविद्यालय/निकाय से एनओसी अनिवार्य है।
- आवेदन, शुल्क का भुगतान, विजिटिंग टीम की रिपोर्ट आदि का प्रावधान ऑनलाइन। निरीक्षण/निगरानी के लिए मुख्यालय और क्षेत्रीय समितियों दोनों द्वारा पारदर्शी उपयोग के लिए केंद्रीकृत कम्प्यूटरीकृत विजिटिंग टीम। (इसके लिए ई-गवर्नेंस अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है)।
- प्रत्येक शिक्षक शिक्षा संस्थान को एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त एजेंसी से प्रत्येक 5 वर्ष में अनिवार्य मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। (इस संबंध में NAAC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं)।
5. डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (DCI), नई दिल्ली
डेंटिस्ट अधिनियम, 1948 के तहत गठित डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे भारत में दंत चिकित्सा शिक्षा और दंत चिकित्सा के पेशे को विनियमित करने के लिए संसद के एक अधिनियम के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। टी
वह परिषद विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डेंटल डिग्री को मान्यता देने और भारत में दंत चिकित्सा शिक्षा के समान मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे के संबंध में न्यूनतम आवश्यकताएं निर्धारित करती है और पाठ्यक्रम और परीक्षाओं की योजना निर्धारित करती है।
6. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI), नई दिल्ली
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), जिसे केंद्रीय परिषद के रूप में भी जाना जाता है, का गठन फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत किया गया था। पीसीआई भारत में स्नातक स्तर तक फार्मेसी शिक्षा और पेशे को नियंत्रित करता है। परिषद फार्मासिस्ट के रूप में योग्यता के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करती है।
7. इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC), नई दिल्ली
इंडियन नर्सिंग काउंसिल, भारतीय नर्सिंग काउंसिल अधिनियम, 1947 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। काउंसिल नर्सों, दाइयों, सहायक नर्स मिडवाइव्स और स्वास्थ्य आगंतुकों के लिए प्रशिक्षण के एक समान मानक के विनियमन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।
भारतीय नर्सिंग परिषद भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जिसका गठन एक समान मानक स्थापित करने के लिए संसद के भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 3(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। नर्सों, दाइयों और स्वास्थ्य आगंतुकों के लिए प्रशिक्षण।
नर्स पंजीकरण और ट्रैकिंग सिस्टम (एनआरटीएस) – नर्सों का एक लाइव रजिस्टर है।
8. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI), नई दिल्ली
https://www.barcouncilofindia.org/info/about-bci

बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। एक महत्वपूर्ण नियम बनाने की शक्ति अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने के संदर्भ में है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के हकदार व्यक्ति के वर्ग या श्रेणी के लिए निर्धारित कर सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया उन शर्तों को भी निर्दिष्ट कर सकती है जिनके अधीन एक वकील को प्रैक्टिस करने का अधिकार होना चाहिए और किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को अदालत में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए समझा जाना चाहिए।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय बार को विनियमित करने और प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद द्वारा बनाई गई एक वैधानिक संस्था है। हम पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करके और बार पर अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके नियामक कार्य करते हैं। हम कानूनी शिक्षा के लिए मानक भी निर्धारित करते हैं और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करते हैं जिनकी कानून की डिग्री एक वकील के रूप में नामांकन के लिए योग्यता के रूप में काम करेगी।
इसके अलावा, हम अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करके और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए धन के निर्माण के माध्यम से कुछ प्रतिनिधि कार्य करते हैं।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना संसद द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत की गई थी। धारा 7 के तहत निम्नलिखित वैधानिक कार्य भारत में कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा के लिए बार काउंसिल के नियामक और प्रतिनिधि जनादेश को कवर करते हैं:
- अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करना।
- अपनी अनुशासनात्मक समिति और प्रत्येक राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समितियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करना।
- अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना।
- कानून सुधार को बढ़ावा देना और समर्थन करना।
- किसी भी मामले से निपटना और निपटान करना जो राज्य बार काउंसिल द्वारा उसे भेजा जा सकता है।
- कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देना और कानूनी शिक्षा के मानक निर्धारित करना। यह भारत में कानूनी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों और राज्य बार काउंसिल के परामर्श से किया जाता है।
- ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता देना जिनकी कानून की डिग्री एक वकील के रूप में नामांकन के लिए योग्यता होगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों का दौरा और निरीक्षण करती है या राज्य बार काउंसिल को विश्वविद्यालयों का दौरा और निरीक्षण करने का निर्देश देती है।
- प्रतिष्ठित न्यायविदों द्वारा कानूनी विषयों पर सेमिनार और वार्ता आयोजित करना और कानूनी रुचि की पत्रिकाओं और पत्रों को प्रकाशित करना।
- गरीबों के लिए कानूनी सहायता की व्यवस्था करना।
- पारस्परिक आधार पर पहचान करना; भारत में एक वकील के रूप में प्रवेश के उद्देश्य से भारत के बाहर प्राप्त कानून में विदेशी योग्यताएँ।
- बार काउंसिल के धन का प्रबंधन और निवेश करना।
- इसके सदस्यों के चुनाव का प्रावधान करना जो बार काउंसिल को चलाएंगे।
9. सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी (CCH), नई दिल्ली
http://nrh.nch.org.in/cch/aboutus
सैमुअल हैनीमैन स्मारक, वाशिंगटन डी.सी. “सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेन्टूर” के साथ – जैसा इलाज वैसा।
होम्योपैथी – कानूनी स्वीकृति की दिशा में एक दृष्टिकोण
“प्रकृति के खजाने में, कई रत्न हैं; केवल वे ही ले जाने लायक हैं, जिन्हें हम स्थापित करना जानते हैं” – होनिगबर्गर
भारत में होम्योपैथी का इतिहास एक फ्रांसीसी व्यक्ति डॉ. होनिगबर्गर के नाम से जुड़ा है, जो भारत में होम्योपैथी लाए थे। वह महाराजा रणजीत सिंह के दरबार से जुड़े थे। वह 1829-1830 में लाहौर पहुंचे और बाद में उन्हें पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का इलाज करने के लिए आमंत्रित किया गया, जो पैरों की सूजन के साथ स्वर रज्जु के पक्षाघात से गंभीर रूप से बीमार थे और 1839 में देशी चिकित्सक उनके स्वास्थ्य में सुधार करने में असमर्थ थे। डॉ. होनिगबर्गर बाद में कलकत्ता चले गए और वहां प्रैक्टिस शुरू की, जहां उन्हें मुख्य रूप से ‘हैजा डॉक्टर’ के नाम से जाना जाता था।
यह चिकित्सीय प्रणाली भारत में होम्योपैथी के जनक डॉ. हैनीमैन के जीवनकाल के दौरान प्रचलित हुई, जब एक जर्मन चिकित्सक और भूविज्ञानी भूवैज्ञानिक जांच के लिए 1810 के आसपास भारत आए और कुछ समय के लिए बंगाल में रहे जहां उन्होंने होम्योपैथिक दवा का वितरण किया। लोगों को
डॉ. महेंद्र लाल सरकार, भारत के पहले योग्य चिकित्सक थे, जो ले-होम्योपैथ बाबू राजेन दत्ता के पक्ष से प्रेरित थे, जिन्होंने स्वयं होम्योपैथी का अभ्यास किया और कई रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया, जिनमें से कुछ उस समय के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जैसे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राधाकांत देब बहादुर। बाद में डॉ. महेंद्र लाल सरकार ने होम्योपैथी की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि को भारत में दूर-दूर तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः अधिक से अधिक लोगों ने विभिन्न रोगों के लिए होम्योपैथिक उपचार लेना शुरू कर दिया।
सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की स्थापना होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 के तहत की गई थी। काउंसिल सभी होम्योपैथिक चिकित्सा योग्यताओं को निर्धारित और मान्यता देती है। होम्योपैथी में चिकित्सा योग्यता प्रदान करने की इच्छा रखने वाले किसी भी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान को परिषद में आवेदन करना आवश्यक है। परिषद होम्योपैथी के एक केंद्रीय रजिस्टर के गठन और रखरखाव और उससे जुड़े मामलों के लिए जिम्मेदार है। भारत में सभी विश्वविद्यालयों और चिकित्सा संस्थानों के बोर्ड को अध्ययन और परीक्षा के पाठ्यक्रमों के बारे में सभी जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। परिषद को परीक्षाओं में निरीक्षकों और सुविधाओं की जांच के लिए आगंतुकों को नियुक्त करने का अधिकार है।
10. सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन (CCIM), नई दिल्ली
भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के गजट अधिसूचना असाधारण भाग (ii) खंड 3(ii) दिनांक 10.8.71 के तहत किया गया है।
1971 में अपनी स्थापना के बाद से, केंद्रीय परिषद भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सहित विभिन्न नियमों को तैयार और कार्यान्वित कर रही है। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्बत। राजपत्र अधिसूचना संख्या 2345 दिनांक 16.12.2011 के अनुसार सोवा रिग्पा चिकित्सा प्रणाली को वर्ष 2012 से केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद में शामिल किया गया है। अब, भारतीय चिकित्सा पद्धति के सभी कॉलेज देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं। ये कॉलेज केंद्रीय परिषद द्वारा निर्धारित शिक्षा के न्यूनतम मानकों और पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का पालन कर रहे हैं।
11. वास्तुकला परिषद, नई दिल्ली
वास्तुकला परिषद (सीओए) का गठन भारत की संसद द्वारा अधिनियमित आर्किटेक्ट अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था। अधिनियम वास्तुकारों के पंजीकरण, शिक्षा के मानकों, मान्यता प्राप्त योग्यताओं और अभ्यास के मानकों का अभ्यास करने वाले वास्तुकारों द्वारा अनुपालन करने का प्रावधान करता है। आर्किटेक्चर काउंसिल आर्किटेक्ट्स के रजिस्टर को बनाए रखने के अलावा पूरे भारत में शिक्षा और पेशे के अभ्यास को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। “आर्किटेक्ट” के पेशे को जारी रखने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को खुद को आर्किटेक्चर परिषद के साथ पंजीकृत कराना होगा।
12. दूरस्थ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
दूरस्थ शिक्षा परिषद का गठन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 25 से उत्पन्न क़ानून 28 के तहत किया गया था। दूरस्थ शिक्षा परिषद (DEC) मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के प्रचार और समन्वय के लिए और इसके निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। मानकों। परिषद उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, नवीन तकनीकों और दृष्टिकोणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने, सभी प्रणालियों के अभिसरण को सक्षम करने और सभी के लिए सतत शिक्षा, कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण तक पहुंच के लिए सहयोगी नेटवर्किंग के माध्यम से संसाधनों को साझा करने के लिए अकादमिक दिशानिर्देश प्रदान करती है।
13. भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली
भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। हालांकि, जल्द ही यह पाया गया कि एक सोसायटी उचित मानकीकरण और अन्य संगठनों द्वारा मानकों की स्वीकृति सुनिश्चित नहीं कर सकती है। संसद ने 1992 में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम बनाया। भारतीय पुनर्वास परिषद 22 जून 1993 को वैधानिक निकाय बन गई। आरसीआई अधिनियम को 2000 में संसद द्वारा संशोधित किया गया ताकि इसे और अधिक व्यापक आधार पर काम किया जा सके। अधिनियम परिषद पर भारी जिम्मेदारी डालता है। यह यह भी निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहा है
चौथी विकलांगता, जिसके पास आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं है, पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इस प्रकार परिषद के पास पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कर्मियों और पेशेवरों के प्रशिक्षण के मानकीकरण और विनियमन की दोहरी जिम्मेदारी है।
14. राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद
ग्रामीण संस्थानों की राष्ट्रीय परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक स्वायत्त समाज है। भारत की। 19 अक्टूबर 1995 को हैदराबाद में अपने मुख्यालय के साथ पंजीकृत, यह महात्मा गांधीजी की नई तालीम की क्रांतिकारी अवधारणा के आधार पर शिक्षा के साधन के साथ ग्रामीण आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था। गांधीजी द्वारा प्रस्तावित मूल्य परिषद के अन्य उद्देश्यों में अन्य शैक्षिक संस्थानों और स्वैच्छिक एजेंसियों को गांधीवादी के अनुसार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा यूजीसी, (AICTE) और (CSIR) , (AICTE) जैसे अनुसंधान संगठनों जैसे नीति-निर्माण निकायों के साथ नेटवर्किंग द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण, विस्तार और अनुसंधान शामिल हैं। शिक्षा का दर्शन।
संदर्भ:
https://www.encyclopedia.com/finance/finance-and-accounting-magazines/professional-education
https://www.msde.gov.in/index.html
https://www.aicte-india.org/about-us/overview
https://www.barcouncilofindia.org/info/about-bci
https://ncte.gov.in/website/index.aspx
- 11 – भाद्रपद मासकी ‘अजा’ और ‘पद्मा’ एकादशीका माहात्य
- 14 – पुरुषोत्तम मासकी ‘कमला’ और ‘कामदा’
- 13 – कार्तिक मासकी ‘रमा’ और ‘प्रबोधिनी’एकादशीका माहात्म्य
- 12 – आश्विन मासकी ‘इन्दिरा’ और ‘पापाङ्कुशा’ एकादशीका माहात्य
- 10 – श्रावण मासकी ‘कामिका’ और ‘पुत्रदा’ एकादशीका माहात्म्य