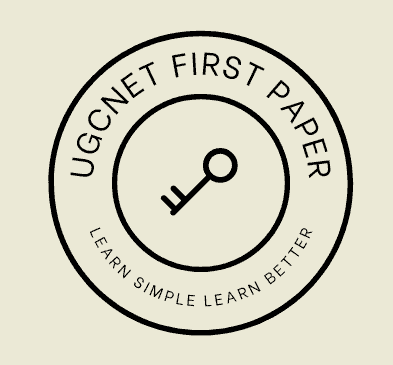रस की अवधारणा
रस शब्द की व्युत्पत्ति :
भारतीय संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी गई है – “ रस्यते आस्वाद्यते इति रसः ” अर्थात् जिसका आस्वादन किया जाए, वही रस है – अथवा “ सते इति रसः ” अर्थात् जो बहे, वह रस है। इस प्रकार रस की दो विशेषताएँ लक्षित होती हैं – आस्वाद्यत्व और द्रवत्व। हमारे आदि ग्रंथ वेद , उपनिषद और पुराणों में “ स ” शब्द का प्रयोग व्यवहारिक जीवन के लिए मिलता है काव्यानन्द के अर्थ में नहीं। तैतिरी योपनिषद की मान्यता है कि वह अर्थात् ‘ ब्रह्म ’ निश्चय ही रस है और जो उस रस को प्राप्त करे उसे आनन्द की अनुभूति होती है उपर्युक्त सभी प्रयोगों से स्पष्ट है कि रस का मूल अर्थ कदाचित् द्रवरूप वनस्पति – सार ही था। यह द्रव निश्चय ही आस्वाद – विशिष्ट होता था – अतः एव। “ आस्वाद ” रूप में भी इसका अर्थ – विकास स्वतः ही हो गया , यह निष्कर्ष सहज निकाला जा सकता है। सोम नामक औषधि का रस अपने आस्वाद और गुण के कारण आर्यों को विशेष प्रिय था , अतः सोमरस के अर्थ में रस का प्रयोग और भी विशिष्ट हो गया। अत : सोमरस के संसर्ग से रस की अर्थ – परिधि में क्रमशः शक्ति , मद और अंत में आह्लाद का समावेश हो गया। आह्लाद का अर्थ भी सूक्ष्मतर होता गया – वह जीवन के आहलंद से आत्मा के आल में परिणत हो गया और वैदिक युग में ही आत्मानंद का वाचक बन गया , अथर्ववेद में उपर्युक्त अर्थ – विकास के स्पष्ट प्रभाव मिल जाते हैं।
परिचय
भारतीय सौन्दर्य – दर्शन का मूल आधार है काव्यशास्त्र। यद्यपि दर्शन में भीय विशेषकर आनंदवादी आगमन – ग्रन्थों में , आत्म – तत्व के व्याख्यान के अन्तर्गत सौन्दर्य की अनुभूति के विषय में प्रचुर उल्लेख मिलते हैं , फिर भी सौन्दर्य के आस्वाद और स्वरूप का व्यवस्थित विवेचन काव्यशास्त्र में ही मिलता है। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से सौन्दर्य – चेतना एक मिश्रवृत्ति है।
इसके योजक तत्व हैं। ( १ ) प्रीति अर्थात् आनंद और ( २ ) विस्मय।
भारतीय काव्यशास्त्र इस रहस्य से आरंभ से ही अवगत था : उसके दो प्रतिनिधि सिद्धांत रस और अलंकार क्रमशः प्रीति और विस्मय के ही शास्त्रीय विकास हैं । सौन्दर्य के आस्वाद में निहित प्रीतितत्व का प्राधान्य रस – सिद्धांत में प्रस्फुटित और विकसित हुआ , और उधर विस्मय – तत्व की प्रमुखता ने वक्रता , अतिशय आदि के माध्यम से अलंकारवाद का रूप धारण किया । इन दोनों में रस – सिद्धांत केवल कालक्रम की दृष्टि से ही नहीं वरन् प्रभाव और प्रसार की दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण है – वास्तव में भारतीय काव्यशास्त्र की आधारशीला यही है।
1. रस शब्द का अर्थ – विकास :
रस भारतीय वाङ्मय के प्राचीनतम शब्दों में से है। सामान्य व्यवहार में इसका चार अर्थों में प्रयोग होता हैं :
1. पदार्थों का रस – अम्ल , तिक्त , कषाय आदिय
2. आयुर्वेद का रस ,
3. साहित्य का और इससे मिलता – झुलता रस ,
4. मोक्ष या भक्ति का रस ।
प्राकृतिक ( पार्थिव ) रस में रस का अर्थ है पदार्थ ( वनस्पति ) आदि को निचोड़कर निकाला हुआ द्रव जिसमें किसी न किसी प्रकार का स्वाद होता है। इस प्रसंग में रस का प्रयोग पदार्थ – सार और आस्वाद दोनों अर्थों में होता है : पदार्थ का सार ( या सार – भूत द्रव ) भी रस है और उसका आस्वाद भी रस है। आगे चलकर ये दोनों अर्थ स्वतंत्र रूप में विकसित हो गये। आयुर्वेद में रस का अर्थ है पारद – यह प्राकृतिक रस का ही अर्थ – विकास है। यहाँ पदार्थ – सार तो अभिप्रेत है ही , किन्तु उसके साथ उसके आस्वाद का नहीं वरन् गुण ( शक्ति ) को ग्रहण किया जाता है। पदार्थ – रस जहाँ आस्वाद – प्रधान है , वहाँ आयुर्वेद का रस शक्ति प्रधान है। आयुर्वेद में रस का एक और अर्थ है देह – धातु – अर्थात् शरीर में अन्तर्भूत ग्रंथियों का रस जिस पर शरीर का विकास निर्भर रहता है यहाँ भी शक्ति का ही प्राधान्य है। तीसरा प्रयोग है साहित्य का रस , जहाँ रस का अर्थ है -( १ ) काव्य – सौन्दर्य , और ( २ ) काव्यास्वाद तथा काव्यानंद भी। मोक्ष – रस या आत्म – रस ब्रह्मानंद अथवा आत्मानंद का वाचक हैय भक्ति – रस का अर्थ भी , सिद्धांत – भेद होने पर , भी मूलतः यही है ।
साहित्य की समीक्षा
शतला महाकाव्य के काव्य शाजीथ अध्ययन के आधार सामान्य रूप से प्रत्येक कवि का काव्य उसके जन्मजात संस्कार , अनुभव एवं ज्ञान – ध्यान का प्रतिफलन होता है। काव्य एवं उसके स्वरूप के विषय में चेतन एवं अवचेतन दोनों में कुछ – न – कुछ आदर्श अवश्य विद्यमान रहते हैं। उन काव्यादर्शों के प्रति कवि की धारणा ही काव्य – सिद्धान्त कहे जाते हैं। प्रो 0 आदेश जी ने “ शकुन्तला ” की रचना महाकाव्य के रूप में की है। उन्होंने किसी सिद्धान्त को लेकर काव्य की रचना नहीं की , किन्तु उनके काव्य के सूक्ष्म अध्ययन एवं अनुशीलन से भारतीय काव्य शास्त्रीय सिद्धान्तों का उद्घाटन सहज ही किया जा सकता है।
प्रस्तुत शोध विषय के अन्तर्गत ‘ शकुन्तला ’ महाकाव्य के काव्यगत मूल्यों को निम्नलिखित परम्परागत शीर्षकों के अन्तर्गत ही विवेचन किया जाएगाः
1. रस सिद्धान्त 2. ध्वनि सिद्धान्त 3. अलंकार सिद्धान्त 4. वक्रोकित सिद्धान्त 5. रीति , वृत्ति और गुण ।
1. रस सिद्धान्त :
भारतीय काव्य शास्त्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विवेच्य है – रस। रस काव्य की आत्मा हैं। समीक्षको ने मूल रूप से इसके निकष पर ही कवियों का मूल्यांकन कर उनकी विभिन्न कोटियाँ निर्धारित की हैं।
रस शब्द आनन्द के अर्थ में प्रचलित है। आनन्द से रस का संबंध भारतीय मनीषियों ने जोड़ा है। भारतीय संस्कृति और साहित्य के चरम विकास से रस संबंधित है।
रस शब्द का अर्थ और स्वरूप
भारतीय जीवन में रस शब्द का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ तत्त्व के लिए होता है , जैसे – पदार्थों का रस – फलों का रस , गन्ने का रस , विभिन्न भोज्य वस्तुओं के स्वाद । मीठा , खट्टा , कड़वा , नमकीन , तीखा , कसैला। इन सब का मिला – जुला चटपटा रस तैयार होता है। इन भोज्य रसों को षड्रस भी कहते हैं। इन रसों का आस्वादन जीभ से होता है। इसलिए जीभ को रसना कहते हैं।
आयुर्वेद में भी रस शब्द का प्रयोग होता है। विभिन्न द्रव्यों के सार तत्त्वों को रस कहते हैं। जैसे – सुवर्णरस , मौवतक रस आदि। साहित्य में भी रस शब्द का प्रयोग होता है। साहित्य के श्रवण , पठन से उत्पन्न होने वाला मानसिक आनन्द रस कहलाता है। भरत मुनि ने इसका विवेचनदृप्रवर्तन किया है। यहाँ इसी “ स ” का विवेचन अपेक्षित है।
भरतमुनि ने नाटक के संदर्भ में , नाटक से प्राप्त होने वाले आनन्द को लेकर अपने ग्रंथ “ नाट्यशास्त्र में सांगोपांग विवेचन किया है। रस सम्बन्धी मान्यताएँ भरतमुनि का रससूत्र ” कहलाई। भरतमुनि रस के संबंध में वैज्ञानिक विवेचना करने वाले पहले आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। भरतमुनि का रस संबंधी प्रसिद्ध सूत्र इस प्रकार है – ‘ विभावानुभावव्य भिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः। अर्थात् विभाव , अनुभाव और व्यभिचार ( संचारी ) भावों के संयोग से रस की निष्पति होती है।
रस आस्वाद्य पदार्थ है। रस का आस्वादन इस प्रकार किया जाता है जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों , औषधियों तथा द्रव्यों के संयोग से भोज्य रस की निष्पति होती है। जिस प्रकार गुड़ादि द्रव्यों , व्यंजनों और औषधियों से षड्वादि रसों का निवर्तन होता है , उसी प्रकार नाना भावों के उपगत होने पर स्थायी भाव रस रूप को प्राप्त होते हैं।
रस का आस्वादन इस प्रकार होता है – जिस प्रकार प्रसन्नचित व्यक्ति नाना प्रकार के व्यंजनों से सुस्वाद भोजन का उपभोग करते हुए रसों का आस्वादन करते हुए हर्षादि का अनुभव करते हैं , उसी प्रकार सहृदय सामाजिक अभिनय द्वारा व्यंजित नाना भावों तथा वाचिक , आंगिक और सात्विक अभिनयों से सम्पृक्त स्थायी भावों का आस्वादन करता हुआ हर्षादिका अनुभव करता है। नाटक के माध्यम से आस्वादित होने के कारण इन्हें नाट्य रस कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इस बात को इन शब्दों में कहा है ‘ विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणी तथा।
रसतामेति इत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम्।। अर्थात् सहृदय पुरुषों के हृदय में स्थित , वासनारूप रति आदि स्थायी भाव ही अनुभाव और संचारी भावों के द्वारा अभिव्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त करते हैं।
रस के प्रमुख चार अव्यय
रस के प्रमुख चार अव्यय हैं – स्थायी भाव , विभाव , अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव ।
• स्थायी भाव
जो भाव वासनात्मक होकर चित में चिरकाल तक अचंचल रहता है , उसे स्थायी भाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में आश्रय के हृदय में सुप्तावस्था में अवस्थित जन्मजात प्राप्त हुए भावों को स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त होते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने स्थायी भावों को रस रूप अंकुर का मूल या कंद कहा है।
स्थायी भाव जन्मजात होते हैं और सभी प्राणियों में वासनारूप में होते हैं जैसे मिट्टी में गंध। स्थायी भाव की पाँच विशेषताएँ हैं – 1) आस्वाद्यता 2) उत्कटता 3) सर्वजन सुलभता 4) पुरुषार्थ उपयोगिता 5) औचित्यता। इन्हीं विशेषताओं के कारण स्थायी भाव संवेद्य होते हैं।
स्थायी भावों की संख्या के बारे में विद्वानों में एकमत नहीं है। प्रचलित मान्यता के अनुसार स्थायी भाव नौ हैं। जिनमें नवरस सम्पन्न होते हैं। स्थायी भाव हैं – रति , हास्य , शोक , क्रोध , उत्साह , भय , जुगुप्सा , आश्चर्य और निर्वेद । ये ही स्थायी भाव परिपुष्ट होकर क्रमशः शृंगार , हास्य , करुण , रौद्र , वीर , भयानक , वीभत्स , अद्भुत और शान्त रसों में परिणत हो जाते हैं।
• विभाव
स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। सहृदय के हृदय में संस्कार रूप से स्थित स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारणरूप व्यक्ति , वस्तु अथवा बाहरी विकार को विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के काम करते हैं। एक भावों को जगाते हैं , दो भावों को उद्दीप्त करते हैं। इस कारण विभाव के दो प्रकार बनते हैं। क ) आलम्बन विभाव ख ) उद्दीपन विभाव
• अनुभाव
मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएँ अनु़भाव कहलाती हैं। अनुभाव शब्द अनुभव से बना है। “ अनु ” का अर्थ है पीछे आने वाला या पीछे होने वाला।
सुन्दरी शकुन्तला ( आलम्बन ) द्वारा दुष्यन्त ( आश्रय ) के मन में रति ( स्थायी भाव ) का जगना और उद्दीपन खिला उद्यान , एकांत के द्वारा दुष्यन्त के हाथ पकड़ना , रोमांचित होना आदि शरीर के लक्षण ( अनुभाव ) रति का कार्यरूप फल है।
इस प्रकार आलम्बन उद्दीपनादि अपने – अपने कारणों से उत्पन्न भावों को व्यक्त करने वाली लोक में जो – जो कार्यरूप चेष्टाएँ होती हैं , वे काव्य – नाटकादि में निबद्ध होकर अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं 1) कायिक 2) वाचिक 3) आहार्य 4) सात्त्विक ।
• व्यभिचारी
भाव हृदय में नित्य विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। कुछ भाव ऐसे भी होते हैं , जो अस्थिर, अस्थायी अर्थात् संचरणशील होते हैं। उन्हें व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए निमित्त अथवा सहायक कारण रूप में अल्पकालिक भाव संचारी भाव कहलाते हैं। रसों के स्थायी भाव निश्चित होते हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
जैसे – श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु संचारी के संबंध में ऐसा कोई नियम नहीं है। एक ही संचारी भाव अनेक रसों में हो सकता है। जैसे – चिंता संचारी भाव , शृंगार , वीर , करुण और भयानक आदि अनेक रसों में पाया जाता है। संचारी भावों की संख्या तैतीस मानी गई है। अतः रस नौ हैं और सहृदय के हृदय में स्थायी भाव आलम्बन या उद्दीपन रूप से उद्भुत होते हैं। “ शकुन्तला ” महाकाव्य में नवरसों में से कितने रस विद्यमान हैं। इसका अध्ययन आवश्यक है। नवरसों का विस्तार से अध्ययन प्रस्तुत महाकाव्य के संदर्भ में आगे के अध्याय में किया जाएगा।
- 11 – भाद्रपद मासकी ‘अजा’ और ‘पद्मा’ एकादशीका माहात्य
- 14 – पुरुषोत्तम मासकी ‘कमला’ और ‘कामदा’
- 13 – कार्तिक मासकी ‘रमा’ और ‘प्रबोधिनी’एकादशीका माहात्म्य
- 12 – आश्विन मासकी ‘इन्दिरा’ और ‘पापाङ्कुशा’ एकादशीका माहात्य
- 10 – श्रावण मासकी ‘कामिका’ और ‘पुत्रदा’ एकादशीका माहात्म्य