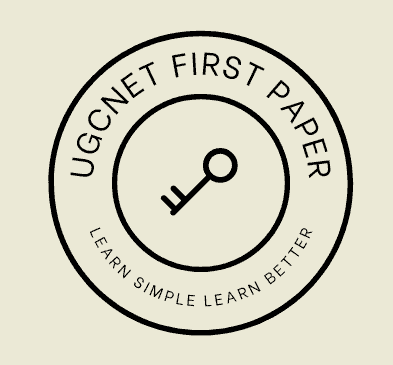पद:170
वै क्यू कासी तजै मुरारी। तेरी सेवा-चोर भये बनवारी।।
जोगी-जती-तपी संन्यासी। मठ-देवल बसि परसै कासी।।
तीन बार जे नित् प्रति न्हावे। काया भीतरि खबरि न पावे।।
देवल-देवल फेरी देही। नांव निरंजन कबहुँ न लेही।।
चरन-विरद-कासी को न दैहूं। कहै कबीर भल नरकहि जैहूं।।
शब्दार्थ : – देवल=देवालय । अरसं = स्पशॆ, उपयोग । विरद=यश ।
संदर्भ :- –कबीरदास जी केवल बाह्याचारी दंभियो की निंदा करते हैं।
भावार्थ :-
हे मुरारी, जिन लोगो ने भगवान की सेवा मे चोरी की है वे काशी को क्यो छोड़ने लगे ? तात्पयॆ यह है कि जिन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया है, वे काशीवास द्वारा ही अपने उद्वार की आशा कर सकते है । योगी, यती, तपस्वी, सन्यासी ये सव मठो और देवालयो मे रहते हुए काशी-वास का उपभोग करते है | वे नित्य प्रति तीन बार स्नान (गगा स्नान) करते है, परन्तु अन्त:करण मे विराजमान परम तत्व की ओर ध्यान नहीं देते है । वे मंदिर-मंदिर घूमते फिरते है,परन्तु निराकार निर्गुण ब्रह्म का नाम कभी नही लेते है। कबीर केहते है कि {मोक्ष की प्राप्ति तो भगवान के चरणो की कृपा से सम्भव है) भगवान के चरणो का यह यश मै काशी को कभी नही दूंगा ,चाहे मुझे नरक मै ही क्यो न जान पडे ।
अलंकार-(१) पुनरूक्ति प्रकाश – देवल देवल ।
विशेष- (१) मुक्ति का श्रेय भगवान को ही है ,काशी को नही । अनन्य भक्त की भाँति कबिरदास अपने इश्टदेव की महिमा को अक्षुप्ण मानते है। वह तो अन्यन्न भी कह चुके है कि ‘ जो कासी तन तजै कबीरा ,रामहि कहा निहोरा?”
(२) काशी मे मृत्यु होने पर मुक्ति हो जाती है । यह रूढिबद्ध धारणा है।
✓
- MPSET EXAM 01 MARCH 2026 BY MPPSC (SOLVED)
- 11 – भाद्रपद मासकी ‘अजा’ और ‘पद्मा’ एकादशीका माहात्य
- 14 – पुरुषोत्तम मासकी ‘कमला’ और ‘कामदा’
- 13 – कार्तिक मासकी ‘रमा’ और ‘प्रबोधिनी’एकादशीका माहात्म्य
- 12 – आश्विन मासकी ‘इन्दिरा’ और ‘पापाङ्कुशा’ एकादशीका माहात्य